Malavgadh Ki Malvika: Novel in Hindi: मालवगढ़ की मालविका, एक महत्वपूर्ण उपन्यास
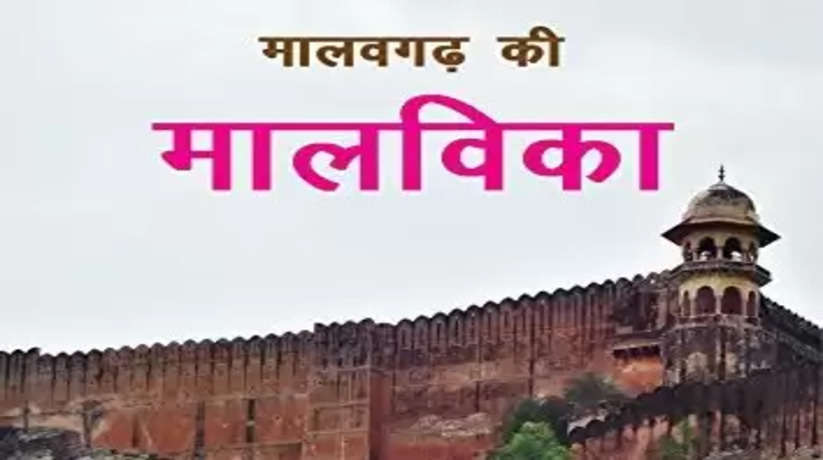
सामने नीम, पीपल के वृक्षों पर शाम उतर आई है। आर्ट गैलरी के आगे बढ़ती भीड़ मुंबई को हसीन जवान बना रही है। मैंने शकुंतला का तैलचित्र खरीदा है और समित को उसके घर की तरफ़ जाती हुई पतली कच्ची पगडंडी पर छोड़ती हुई घर लौट आई हूँ। कार पोर्टिको में पार्क की तो लछमन ने दरवाज़ा खोलकर देखा और नज़दीक आ गया।
“लछमन, कार में पेंटिंग रखी है। उसे मेरे बेडरूम की दीवार पर टाँग दो।”
लछमन ने कमरे में आकर पहले मुझे पानी दिया फिर एक लंबा लिफाफा। मैंने संकेत से पूछा- काम हो गया?
“जी।”
और वह पेंटिंग लाने पोर्टिको की ओर चला गया। मैंने लिफाफा खोलकर टिकट निकाली मालवगढ़ की।
मालवगढ़! हाँ....मालवगढ़ जाना है मुझे! अतीत के तहख़ाने टटोलने.... या अतीत के नहीं बल्कि अपने अंदर दबे दर्द के तहख़ाने पहचानने कि उनमें कितना दम है अभी। उन बिखर गए पलों को बटोरने की ज़िद बार-बार मुझे मालवगढ़ की ओर ढकेल रही थी।
जीप वाले रास्ते को याद कर मन सिहर जाता है। ऊबड़-खाबड़, रेत के ढूहों से भरा....बबूल, कीकर के कँटीले पेड़, झाड़ियाँ....शाम होने से पहले पहुँचने की हड़बड़ी क्योंकि रात होते ही डाकुओं का भय घेरे रहता। जाने कितनी अथाह स्मृतियाँ समाई हैं मुझमें....मैं भूल ही नहीं पाती कुछ....उन स्मृतियों की ही ज़िद है ये जो आज मेरे एकाकी जीवन की ज़िम्मेवार है।
शादी नहीं करने के मेरे संकल्प की ज़िम्मेवार है। मुझमें भरोसा भी खूब जगाया है उन स्मृतियों ने। एम. ए. .... इटली जाकर पी-एच.डी., फिर कलकत्ता के कॉलेज में लैक्चरर, हैड ऑफ़ दि डिपार्टमेंट और फिर यहाँ प्रोफेसर....ये बुलंदियाँ उन्हीं स्मृतियों की देन हैं। नाते रिश्तों में खुसर-पुसर मच गई थी। पायल नौकरी करेगी, शादी नहीं करेगी? बड़ी दादी बिस्तर पर पड़े-पड़े माथा ठोककर चीखी थीं- “बावरी हो गई है, मत मारी गई है? मैं न कहती थी कि अभी माहवारी शुरू नहीं हुई है, सयानापन से पहले कर दो शादी। पर सुना किसी ने? अब लो भुगतो, कुँवारपन नहीं उतरेगा, अधर्मी हम कहलाएँगे।”
ज्यों पटाखे की लड़ी में किसी ने जलती अगरबत्ती छुआ दी हो....यहाँ से वहाँ तक ख़बर फ़ैल गई....सबने नाक-भौं सिकोड़ी- “हुआ है ऐसा इतने बड़े ख़ानदान में कभी। बाप-दादों का मान-सम्मान, रुतबा डुबोने पर तुली है।”
मगर मैं दृढ़ थी। क्यों नहीं खड़ी हो सकती मैं अपने पैरों पर, क्यों नहीं रूपया कमा सकती, क्यों नहीं स्वावलंबी बन सकती? मानती हूँ रुपयों की कमी नहीं है इस ख़ानदान को, लेकिन क्या वह मेरा कमाया हुआ है? मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहती हूँ, कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। यही चुनौती आज भी मेरी रगों में समाई है। अपने फैसले खुद करना। तभी तो बाबूजी मेरे बनारस नहीं आने पर चौंके नहीं। हालाँकि यूनिवर्सिटी की तमाम लंबी छुट्टियों में वे आतुरता से मेरी प्रतीक्षा करते हैं।
ज़रूरी कपड़ों से सूटकेस भर जब मैं ट्रेन में बैठती हूँ तो समित समझाता है- इत्मीनान से छुट्टियाँ गुज़ारना, उतने दिनों के लिए भूल जाना मुंबई को।
मैं मुस्कुराती हूँ, कहना चाहती हूँ....तुम्हें भी समित। अनजान-सा रिश्ता है समित से मेरा। मेरी हर बेचैनी, हर तकलीफ़, हर उदासी का एकमात्र साथी। बीसियों बार जब अकेलेपन से घबराकर मैंने अपने आपको जुहू या चौपाटी के किनारे पाया है....या मरीन ड्राइव की समुद्री फुहारों में खुद को भिगोया है तो इसी समित ने मेरे ऊबे हुए समय को बाँटा है।
खुद की लिखी कविताओं को तरन्नुम में गाकर उन पलों के भारीपन को हलका किया है। कभी-कभी हम बहस में डूब जाते हैं। अमेरिकन साहित्य, अफ्रीकी साहित्य या फिर जापान की हाहूक कविताएँ....समित कहता- “ये जापानियों की दृष्टि इतनी सूक्ष्ण क्यों होती है? तीन या चार पंक्ति की कविता, एक फुट के बरगद, पीपल के बोन्साई, चावल खाने की लंबी चम्मच ऐसी कि एक बार में चार कण चावल मुँह में जाएँ।”
मैं हँसकर कहती- “देखन में छोटे लगें, घाव करैं गंभीर” ट्रेन चली तो समित ने मेरे हाथों को हलके से छुआ- “ऑल दि बेस्ट।”
देर तक वह मेरी आँखों में बना रहा, ओझल होने के बावजूद भी।
ताँगा कोठी के ऐन फाटक पर आकर रुका जहाँ कोठी के ऊँचे रोशनदान के ऊपर देवनागरी लिपि में धुँधले पड़ गए काले हर्फ़ झिलमिला रहे हैं ‘प्रताप भवन’। रामू काका कनेर, तगड़ और गुलबकावली के पेड़ों में पाइप से पानी डाल रहे थे। रामू काका मेरे बाबा के ज़माने के नौकर कोदू के बेटे....कोठी की देखभाल करने के लिए तैनात, ताँगा रुकने की आवाज़ सुनते ही वे पाइप छोड़ दौड़े-
“अरे पायल बेटी, यो म्हें कै देखूँ हूँ, यो कठ सपणो तो कोणी?”
और ताँगे से उतरते ही मैं बाबूजी सादृश रामू काका से लिपट गई। वे कंधे पर पड़े गमछे से अपने झर-झर बहते आँसू पोंछते हैं। गला भर आया है रामू काका का। कहते कुछ नहीं, ताँगे से सामान उतारकर कोठी के मेन हॉल में रखते हैं- “बैठ बेटी, थारे खातिर सरबत बणा ल्याऊँ।”
मुझसे मना नहीं किया जाता। बरसों से इस अपनत्व की भूखी थी मैं। मैंने धीरे-धीरे सैंडिलें उतारीं....स्लीपर पैरों में डाली और घूम-घूमकर कोठी का कोना-कोना पहचानने की कोशिश करने लगी। पहचान अम्मा ने दी थी....जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को रणभूमि का आँखों देखा हाल सुनाया था....वैसी ही जीवंत पहचान....कि मुझे लगा जैसे मैं ताउम्र इसी कोठी में रहती आई हूँ और देख रही हूँ हॉल की दीवारें जहाँ बड़े बाबा, बड़ी दादी और मेरे बाबा की आदमकद पेंटिंग्स हैं जिन पर चंदन की मालिकाएँ पड़ी हैं और जिन्हें आज भी रामू काका बदस्तूर झाड़ते-पोंछते रहते हैं लेकिन दादी की पेंटिंग नहीं है....क्यों?
क्यों दादी को उच्छिष्ट-सा इस कोठी से बुहार दिया गया। बाबा के ऐन बाजू की जगह खाली है।....एक शून्य का फैलाव, लेकिन यह भी सच है कि तमाम आकाशगंगाएँ इसी शून्य की ओर खिंचती हैं, समाती हैं, विलीन हो जाती हैं। शून्य बना का बना रहता है। दादी की पेंटिंग अम्मा ले गई थीं! अम्मा ने बनारस में अपने बंगले, जिसका नाम उन्होंने मालविका कुंज रखा था, की बैठक की दीवार पर उसे टाँग दिया था। उसी पेंटिंग से अतीत ने मुँह-बाया था....
मालवगढ़ का अतीत। अतीत की दराजें खुली हैं और यादों के पतंगे उड़-उड़कर मेरी स्मरण शक्ति पर मँडरा रहे हैं। सामने दादी का कमरा है, बड़ा-सा शीशम का पलंग जिस पर रेशमी गद्दा बिछा था। शकरपारों की शक्ल के टाँकों वाला। दादी के ज़माने में इस पर नर्म रेशम की कत्थई चादर बिछा करती थी जिसके कोनों पर क्रोशिये से बुनी तितलियाँ टँकी थीं।
तख़्त के पाये नक्काशीदार थे जिनकी जाली में हाथीदाँत जड़ा था। पलँग के ऊपर रेशमी, झालरदार हथपँखा था। दादी घर की दिनचर्या से फारिग हो जब अपने लंबे बालों का जूड़ा खोल इस पर आराम करतीं तो दरवाज़े पर बैठा दरबान पंखे की डोर खेंचने लगता। एक रोज़ बाबा ने उसे काम के दौरान तंबाखू मलते देख लिया था तो ज़ोर से दहाड़े थे- “काम के वक़्त नशा करता है, ऐंऽऽऽ?”
दरबान के हाथ की तंबाकू समूची नीचे और हाथ सैल्यूट की मुद्रा में माथे पर- “हुज़ूरऽऽ“
इसी दरबान की लड़की की शादी में दादी ने दस हज़ार की मदद की थी। बारातियों के लिए आलू, प्याज़ के बोरे भिजवाए थे सो अलग। तभी तो प्रताप भवन की डाँट-फटकार भी यहाँ के नौकरों को वरदान-सी लगती थी।
अंग्रेज़ों का वक़्त! अभयसिंह यानी बाबा थे ज़मीदार। लेकिन स्वतंत्र भारत देखने का सपना लहू बनकर बह रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता महात्मा गाँधी के सक्रिय सहयोगियों में उनका नाम अवश्य था किंतु चाणक्य नीति के वे हामी भी थे। उनकी जड़ें काटने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों की ही कुल्हाड़ी इस्तेमाल की। इलाक़े के सभी अंग्रेज़ बाबा की मुट्ठी में।
अंग्रेज़ी राज्य के गुणों का बखान करते वे थकते नहीं थे। लिहाज़ा विदेशी गाड़ी हमेशा प्रताप भवन के गेट पर खड़ी रहती, विदेशी शराब, विदेशी सिगरेट....दादी चिढ़ती- “यह सब क्या है? आखिर काहे को आने देते हो उन्हें घर?”
“मित्र हैं हमारे! उनके राज में जी रहे हैं तो घर न आवेंगे?”
बाबा ठहाका लगाकर बात उड़ा देते। लेकिन उनकी गतिविधियों की जानकारी उन्हें कुछ-कुछ भासने लगी थी। रात को चुपके से स्टडी के कमरे में जाकर टेबिल लैंप की रोशनी में न जाने क्या लिखते थे वे। एक दिन दादी ने चुपचाप काग़ज़ देखे तो दंग रह गईं। न भाषा समझ में आई, न कुछ कूत में घुसा। आड़ी टेढ़ी रेखाओं का जाल और सांकेतिक शब्द....कोठी में एक तलघर भी था जहाँ कभी कोई नहीं जाता था। लेकिन बूढ़ी महाराजिन, जो थी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की लेकिन बरसों से अपने पति के साथ कोठी का चूल्हा-चौका सम्हाले थी, बड़े राज़दाराना अंदाज़ में अम्मा को बताती थी- “हुँआ पुरखों के कपड़ा, लत्ता, माल असबाब धरा है लोहे के संदूकों में।”
“तुझे कैसे मालूम?”
“लो सुनो दुलहिन की बात। अरे, तुमसे पहले से हम जो हियाँ जमे बैइठे हैं। सब कुछ हमार आँखिन के सामने ही हुआ है। थोड़ा आटा और दो दुलहिन.... आज बहुत रोटियाँ सिकेंगी।”
“क्यों?” अम्मा को महाराजिन की जानकारी पर आश्चर्य होता। उन्हें तो किसी ने नहीं बताया कि ज़्यादा रोटी सिंकवा लो।
“अरे, छोटे मालिक का हुकुम है। अब हम कइसे पूछें कि क्यों?”
छोटे मालिक यानी बाबा....बड़े बाबा को सब बड़े मालिक कहते थे। बड़ी दादी बड़ी मालकिन लेकिन दादी सिर्फ़ मालकिन के नाम से मशहूर थीं।
काग़ज़ों में रोटियों के पैकेट बने। आलू की सूखी भुजिया कटोरदान में भरी गई। दादी समझ गईं अब सारा पसारा देवबाबा की मड़िया भेजा जाएगा। हर आड़े दूसरे वहीँ भेजा जाता है। पूछने पर संक्षिप्त-सा उत्तर बाबा का- “कुछ गरीब हैं वहाँ....बेआसरा, और सुनो महारानी मालविका, कल सिविल लाइन के अंग्रेज़ अफसर रात का खाना खाएँगे।”
उनका खाना यानी मुर्ग मुसल्लम।
चार-पाँच मुर्गे दरबान से कटवाए गए। पिछवाड़े पक्के चबूतरे पर....तमाम पंखों को गड्ढा खोदकर गाड़ा गया और खून भरा चबूतरा पानी से धोया गया। दादी की देखरेख और निर्देशन में मुर्ग मुसल्लम, मुर्ग कोरमा, मुर्ग तंदूरी पकता....लेकिन चौके में नहीं, बाहर आँगन में अँगीठी पर....बर्तन भी अलग होते। दादी यह सब बाबा की ख़ातिर करतीं। हालाँकि वे कभी अंग्रेज़ों के सामने नहीं जातीं।
उनके खाने के कमरे और हॉल के बीच जो दरवाज़ा था उस पर रंग-बिरंगी काँच की सलाखों का परदा पड़ा था। दादी इसी परदे के पीछे खड़े हो बंसीलाल के ज़रिए भोजन परोसवातीं। उनके खाने के बाद नुची-चुसी हड्डियाँ फिर गड्ढा खोदकर गाढ़ी जातीं। पूरे घर में धूप लोबान का धुआँ किया जाता। एक दिन जिद्दिया गईं- “नहीं बनेगा मुर्गा-शुर्गा....शुद्ध भारतीय भोजन कराएँगे हम।”
बाबा कुछ नहीं बोले लेकिन टेबिल पर सुगंधित मसालेयुक्त गट्टे की सब्ज़ी, हींग लहसुन से छौंकी गई अरहर की दाल, बासमती चावल, आम का अचार और गोभी दम जब परोसा गया तो अंग्रेज़ अफसर वाह-वाह कर उठे। खाने के बाद चूरमा के लड्डू। देर रात तक अंग्रेज़ों ने उठने का नाम नहीं लिया।
दादी ने सोने में सुहागा यह भी कर दिया कि चाँदी के वर्क लगे कलकतिया पान के बीड़े भिजवा दिए। सलाखों के परदे के पीछे से जब उन्होंने सामने बैठे अंग्रेज़ के मुँह में भरी पान की पीक ठोड़ी तक बहते देखी तो हलके से हँस दीं। पर बाबा को उनकी हँसी की खनक सुनाई दे गई। वे परदे की ओर देखने लगे।
इसके ठीक हफ्ते भर बाद दादी के आगे सारे रहस्य खुल गए। बाबा ने शायद सब कुछ छुपाया इसलिए होगा कि कहीं बात प्रताप भवन से बाहर न चली जाए। उस दिन फिर मुर्गे कटे थे, फिर विदेशी शराब की बोतलें खुली थीं और जब कोहरा गहराने लगा था, ठंड बढ़ने लगी थी तो नशे में लड़खड़ाते, गिरते-पड़ते अंग्रेज़ अफसर गाड़ियों में ठुँस गए थे और जब उनकी गाड़ियों की पिछली बत्तियाँ कोहरे के सागर में टिमटिमाते दीये-सी दिखाई देने लगीं तो बाबा ने दरबान को फाटक बंद करने का हुक्म दिया और दादी के पास पलंग पर बैठते हुए दहाड़े- “मरेंगे साले, कुत्तों की मौत मरेंगे। समझा क्या है कि हम हिन्दुस्तानियों ने चूड़ियाँ पहन राखी हैं?”
“क्यों, तुम्हारे तो दोस्त हैं सब?”
“हुँह।” बाबा ने हिक़ारत से गर्दन को लोच दी। फ़दादी ताज्जुब से उन्हें देखने लगीं- “तो बुलाते क्यों हो? मुझे तो इनका आना ही बर्दाश्त नहीं। बाम्हन को खिलाओ तो पुन्न मिले, मरे म्लेच्छों को खिलाकर क्या पा लोगे? न स्वर्ग, न नरक, लटके रहोगे त्रिशंकु बने।”
“अरे....यही बात समझ लो तो तुम झांसी की रानी न बन जाओ। ये कूटनीति है महारानी, कूटनीति....जिस दिन हमारी पार्टी को मैंने इनके सारे भेद पकड़ा दिए उस दिन विस्फोट होगा विस्फोट....”
और वे दादी की बाँह पकड़कर उन्हें चुपचाप तलघर में लिवा ले गए- “देखो....देखो आज़ादी का इंतज़ाम....सब कुछ तैयार है यहाँ।”
दादी की आँखें फटी की फटी रह गईं। बम, बारूद, हथगोलों, हथियारों से भरा तलघर....वे डरकर बाबा से सट गईं।
“जानती हो मालविका? देव बाबा की मड़िया के पीछे जंगल में स्वतंत्रता सेनानी इन्हें चलाने की ट्रेनिंग पा रहे हैं। महीनों से छुपे हैं उस जंगल में वेश बदलकर। उन्हीं के लिए मैं थोड़ा-बहुत खाना भिजवा देता हूँ। जंगल से लगे गाँव के सरपंच के यहाँ से नियमित कलेवा भेजा जाता है। तुम तो सोती रहती हो और मैं सारी-सारी रात काग़ज़ों पर नक्शे, योजनाएँ बनाता हूँ।”
दादी और सट गईं बाबा से....बल्कि लिपट ही गईं। बदन थरथरा रहा था कमल के पत्ते पर बूँद-सा....आँखों में जल प्लावन....
“कल से नियमित खाना भेजिए देव बाबा की मड़िया।”
बाबा ने हुलसकर दादी को चूम लिया था और सब कुछ गुप्त रखने का आदेश दिया था। दादी सारे रहस्य गोली के समान निगल गई थीं और दूसरे दिन से बदस्तूर स्वादिष्ट भोजन उन रण बाँकुरे देशभक्तों के लिए भेजा जाने लगा।
खुद के लिए बाबा सादा भोजन पसंद करते। प्रताप भवन का बाबा के पड़बाबा के समय से नियम चला आ रहा था, सुबह नौ बजे बड़े हॉल के बड़े गोल टेबिल के किनारे रखी कुर्सियों पर पूरे परिवार का आ जुटना। पड़बाबा के समय टेबिल की जगह संगमरमर की चौकियों पर बैठकर खाना, नाश्ता खाया जाता था। नाश्ते के समय घर की बहुओं का भी उपस्थित रहना आवश्यक था। दोपहर का भोजन नियमित नहीं था। जो जब आता परोस दिया जाता। अलबत्ता बहुएँ मिलकर खाती थीं।
बाबा शुद्ध भारतीय थे। उनके जैसा अनुशासित योगी व्यक्ति मैंने कभी सुना नहीं आज तक। बाबा सुबह चार बजे उठ जाते। नित्यकर्म से फुरसत हो सफेद बुर्राक़ धोती-कुरता पहन चाँदी के मूठ वाली छड़ी हाथ में ले घूमने निकल जाते। घूमना उनका बनास नदी के तट तक नहीं होता। लौटकर आते तो बाहर लॉन में बैठकर अखबार पढ़ते। तब तक दादी नहा चुकतीं। कोदू गोल छोटी तिपाई लॉन में रखता जिस पर कश्मीरी काढ़ की सुंदर टीकोज़ी से ढकी ख़ास दार्जिलिंग की खुश्बूदार चाय होती। दूध, शक्कर चाँदी के अलग-अलग बर्तनों में।
सुबह की चाय में बाबा शक्कर नहीं लेते थे। यह चाय दादी खुद अपने हाथ से बनाती थीं। चाय पीते हुए बाबा कुछ ख़ास ख़बरें दादी को पढ़कर सुनाते। दादी साक्षर थीं। फिर भी सुबह की ख़बरें बाबा के मुँह से ही सुनती थीं। ख़बरों पर चर्चा भी होती। दादी के तर्क बाबा को दंग कर जाते, वे लाड़ से उन्हें देखते।
फिर शुरू होती बागवानी, पीले पत्तों को काटना, पौधों की काट-छाँट करना, उन्हें सुंदर आकार देना, लताओं को गेट या मण्डप पर चढ़ाना, पौधों में खाद, पानी, मिट्टी अपनी देखरेख में माली से डलवाना बाबा का ख़ास शगल था। माली देर से आता, तब तक दादी बाबा के साथ रहतीं, उनके शौक में हाथ बँटाती। उनके रुई से मुलायम हाथ खुरपी की मूठ पकड़े लाल हो जाते। इतने बड़े ज़मींदार होने का घमंड न कभी बाबा को हुआ, न दादी को। अपनी सरलता, सादगी और निश्छलता ने उन्हें तमाम छोटे-बड़े पदों के व्यक्तियों का चहेता बना दिया था।
बाबा ने लॉन के बीच गोलाई में सफेद गुच्छेदार गुलाबों के पौधे लगवाए थे। इन पौधों पर इतने अधिक फूल खिलते कि इनकी पत्तियाँ छुप-सी जातीं। दिसंबर की शुरुआत में न जाने कहाँ से आकर हर साल इन फूलों पर तितलियों का दल नर्तन करता था। ये तितलियाँ काले-पीले पंखों वाली मोनार्क तितलियों जैसी थीं। बाबा अमेरिका रिटर्न थे। किसी कार्यवश उन्हें अमेरिका जाना पड़ा था।
बाद में वे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, जर्मनी और नॉर्वे भी घूम आये थे जहाँ मध्यरात्रि में सूर्य निकलता है लकिन जब वे अमेरिका गए थे तो प्रताप भवन में सन्नाटा छा गया था। सबके ख़ामोश होंठों पर बस यही तर्क था कि बाबा दिसावर क्यों जा रहे हैं? मालवगढ़ के निवासियों के लिए राजस्थान उनका अपना देश था बाकी परदेस। आदमी कलकत्ता, बंबई, दिल्ली कमाने जाए तो कहते दिसावर गया है....न जाने कितने दिन लगे थे उन्हें समझाने में कि वे विदेश जा रहे हैं....और कमाने नहीं।
तो जब भी बाबा फूलों पर काले-पीले पंखों वाली तितलियाँ देखते एकदम उत्साह से भर जाते, बताते- “जब मैं मैक्सिको गया था....ओहो हो क्या बताऊँ। इतने खूबसूरत और घने जंगल हैं वहाँ....चीड़, देवदार के दरख़्तों से भरे, झरने, पहाड़ी चश्मों से भरे....झर-झर पानी बहता रहता है उनमें कितना पानी....अथाह....और बिल्कुल इन्हीं तितलियों जैसी मोनार्क तितलियाँ सैकड़ों की तादाद में मँडराती रहती हैं पेड़ों पर....झुंड-की-झुंड....सैलाब जैसी....कुछ तितलियाँ तो मेरे ऊपर बरस रही थीं। मेरे बादामी कुर्ते पर उनके पंखों के दाग उभर आए थे।”
दादी मुस्कुराती हुई न जाने कितनी बार तितलियों के बरसने का किस्सा सुन चुकी थीं और हर बार उनकी उन दिनों की स्मृति में वह घटना बिजली-सी कौंध जाती जब बाबा के अमेरिका चले जाने पर बड़ी दादी ने उन्हें तब तक सिर नहीं धोने दिया था जब तक उनके पहुँचने की ख़बर नहीं आ गई थी। दादी बाबा को बहुत चाहती थीं लेकिन ऐसी ऊटपटाँग मान्यताओं में उनका विश्वास न था, फिर भी करना पड़ता। वरना दादी बाबा के इश्क से तो पूरे खानदान को रश़्क था। दादी जानती थीं, यह चंदन वन उन्होंने ऐसे ही नहीं पा लिया है। क़दम-क़दम पर फुफकारते नागों का सामना किया है।
दादी खुद भी नियम-धर्म वाली थीं। व्रत-उपवास, तीज-त्यौहार और भारतीय परंपराओं का निर्वाह उनके रक़्त में पगा था। रसोईघर में महाराज और महाराजिन प्रवेश कर सकते थे। वो भी नहा-धोकर, चुटिया में गाँठ मारकर, जनेऊ पहनकर और सिल्क की कोसई धोती पहनकर। महाराजिन कोसई साड़ी ब्लाउज़ में। चोली, घाघरा न दादी ने कभी पहना न अम्मा को पहनने दिया। महाराजिन के लिए भी मनाही थी।
घर में कुल दस सदस्य, बाबा, दादी, अम्मा, बाबूजी, बड़े बाबा, बड़ी दादी और उनकी तीन बेटियाँ....उषा बुआ, संध्या बुआ, रजनी बुआ और मैं....नौकर-चाकरों को मिलाकर बीस लोगों की रसोई महाराज के ज़िम्मे। नौकरों को दाल, सब्ज़ी कटोरों में दे दी जाती। जसोदा और कंचन मिलकर नौकरों की रोटी सेक लेतीं। जसोदा अम्मा की सेविका थी और कंचन दादी की। पन्ना तीनों बुआओं की और मेरी सेविका। खाना परोसने और ऊपरी कामों के लिए बंसीमल था। सुबह सारा राशन घी, तेल, मसाले, मेवा मिश्री, पापड़, कुरैरी, अचार भंडार घर से निकालकर महाराज को सौंपने का काम दादी करतीं।
अम्मा रसोईघर में मुढ़िया डाल बैठ जातीं। महाराज पकाता, महाराजिन रोटी सेंकती। हर सब्ज़ी में काजू, पिस्ता, बादाम पड़ना ज़रूरी था वरना बड़े बाबा, बड़ी दादी निवाला नहीं तोड़ते थे। वैसे भी बड़ी दादी बरसों से खटिया पर थीं। न जाने कौन-कौन से रोग तोते की तरह पले थे उनके शरीर में। एक नर्स चौबीसों घंटे तीमारदारी के लिए तैनात थी। नर्स मिशिनरी अस्पताल से बुलाई गई थी, ईसाई....देखते ही बड़ी दादी ने नाक-भौं सिकोड़ी थी लेकिन कुछ ही दिनों में नर्स मारिया ने अपने सुंदर स्वभाव से उनका मन जीत लिया था- “हम हिंदू ईसाई हैं बड़ी आंटी, साउथ में बैंगलोर शहर के।”
बड़ी दादी सुनकर आश्वस्त तो हुई फिर भी ‘दुलहिनऽऽऽ’ की पुकार हर दसवें मिनट में लगा ही देतीं और उनकी हर पुकार पर दादी हाज़िर- “हाँ जीजी, बुलाया आपने?”
“हाँ, मैं कह रही थी तीजें आ रही हैं। समधियानों में भेंट भिजवाने की तैयारी कर ली?”
भेंट यानी केवल सत्तू के लड्डू नहीं बल्कि अचार, पापड़, मुरब्बे, मुंगोड़ियाँ...तीजों पे ननदों, बेटियों के घर सिंजारा के लिए मेहँदी, साड़ियाँ, इक्कीस-इक्कीस चाँदी के सिक्के, केशर रचे बासमती चावल सब भेजा जाता। दादी अपनी देखरेख में बड़े-बड़े मर्तबानों में ल्हिसौड़े टैंटी के अचार डलवातीं। अम्मा के हाथ का आम और काबुली चनों का हैदराबादी अचार मेरी फुफेरी बुआओं को ख़ास पसंद था।
राजापुरी आमों का कसा हुआ मीठा लच्छा चचेरी बुआओं के ससुराल भेजा जाता। पापड़ के पाँच-पाँच किलो के पैकेट, कनस्तरों में घी, गुड़ की भेलियाँ, कुटी सौंठ, गरम मसाला, गोंद बादाम की बर्फी, सत्तू के लड्डू सब प्रताप भवन के लिए तो तैयार होता ही लेकिन पूरे ख़ानदान की बेटियों, ननदों के ससुराल भी उसी मिक़दार में भेजा जाता और यह सब केवल दादी करतीं। दादी से ख़ानदान चल रहा था। दादी धरती की तरह सबको समेटें थीं, ऐसे बीजों को, जो कल आबाद होकर जंगल बनेंगी। तो दादी ही जंगल कहलाई न।
जहाँ दादी संस्कार, परंपरा और मान्यताओं से ओत-प्रोत थीं, अम्मा में भीतर विद्रोह सुलगता रहता था। अम्मा का यही विद्रोही स्वभाव मेरे अंदर रचा-बसा था। इस स्वभाव के कारण मुझे ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़ा तो वह नगण्य है क्योंकि मैं जो बनना चाहती थी बनी, जो कर दिखाना चाहती थी.... किया....अम्मा मेरा आदर्श रहीं....मैं तो इस्लाम, कैथोलिक, यहूदी धर्म की पुस्तकें पढ़कर धीरे-धीरे ख़ानदान से अलग-थलग मार्ग का चुनाव करती रही लेकिन अम्मा कीचड़ में खिला वो कमल पुष्प थीं जो सूर्य उगते ही अपने जागरण का, खिलने का संकेत देता है। मैंने हमेशा अम्मा को अपनी सोच, अपने विचारों पर चलते देखा तभी तो बाल वय की मेरी ज़िद, मेरे तर्क को उन्होंने दुत्कारा नहीं था।
होलि काष्टक लगते ही दादी माली से गोबर मँगवाकर बड़कुले बनवाने लगतीं। गोबर के चाँद, सूरज, नारियल बड़कुलों को सुतली में पिरोकर बड़ी-सी जेळ माला की होली तैयार होती। आँगन के ऐन बीचों-बीच। पूरा मालवगढ़ फागुन से महक उठा था इस बार कुछ अधिक। महुए की गमक हवा को नशीला बना रही थी। मालवगढ़ है भी राजस्थान का दक्षिण-पूर्वी भाग जहाँ अभ्रक के पर्वत, हरी भरी पहाड़ियाँ, उपजाऊ धरती, घने जंगल और बनास नदी का छलछल बहता जल है। मालवगढ़ में होली का रंग महीने भर पहले से ही लोगों के दिलों पर छा जाता है। क़दम थिरक उठते हैं ‘गींदड़’ नृत्य के लिए। चंग की थाप, नगाड़े की धुन और मंजीरे के कर्णप्रिय तरन्नुम में पूरा नगर श्रृंगार रस में आकंठ डूब जाता है।
बड़कुलों से जलाई होली जब सुबह राख में परिवर्तित हुई तो दादी ने बुआ लोगों को और मुझे बुलाकर कहा- “चलो गणगौर की पिंडियाँ बना लो। टोकनियाँ मँगवा ली हैं, उनमें दूब बिछाकर पिंडियाँ रख दो। रोली, काजल, मेहँदी की बिंदी लगेंगी....जो भूलो कुछ तो पूछ लेना।”
संध्या बुआ, रजनी बुआ, उषा बुआ अपनी-अपनी पिंडियाँ बनाने लगीं। मैं अड़ गई- “मैं भी बनाऊँगी पिंडियाँ।”
“क्यों....तुझे बींद (वर) की कामना नहीं....शिव-सा गुणवान, रूपवान....”
“अगर मैं बनाऊँगी तो भैया भी बनाएगा। वह क्यों नहीं बनाता पिंडियाँ? वह क्यों नहीं गणगौर पूजता? क्या उसे नहीं चाहिए गौरी-सी बिणनी?”
बड़ी दादी पलंग पर लेटे –लेटे दाँत किटकिटाने लगीं- “अरी अपशगुनी.... भक्-भक् बोले जा रही है। लुगाई का जनम और तेवर ऐसे?”
अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और तमककर बड़ी दादी को देखा। कहा कुछ नहीं लेकिन एक विद्रोह उनकी आँखों में सुलग उठा था। उन्होंने आहिस्ता से दादी से कहा- “अम्माजी, इसे जाने दें। नहीं बनाती पिंडियाँ तो न बनाए....मैं तो बना रही हूँ न।”
वे मुझे लेकर अपने कमरे में आ गईं। बाल सँवारकर मेरी चुटिया बाँधी, घाघरा चोली पहनाई फिर मेरे गालों को चूमकर कहा- “पायल, अपनी बात को हमेशा उन्हीं लोगों के सामने रखा करो जो उसे सुनें। अपने मोती-से अनमोल शब्दों को व्यर्थ मत करना।”
मैं अम्मा से लिपट गई। बूटे से कद की, दुर्बल देह की अम्मा भैया होने के टाइम पर सूज फूल कर डबलरोटी हो गई थीं। दर्द आने तो दो दिन पहले से ही शुरू हो गए थे। घर में डॉक्टरों का हुजूम खड़ा कर दिया था बाबा ने। सारे नौकर-चाकर हाथ बाँधे कोठी के दरवाज़े पर दादी के हुक्म की प्रतीक्षा में थे कि कब किस चीज़ की ज़रुरत पड़ जाए। दादी रात भर मंदिर में दीया जलाए, हाथ जोड़े प्रार्थना करती रही थीं।
दादी का मंदिर उनके कमरे की बगल में था। सुंदर-सा, छोटा-सा कृष्णजी का मंदिर। वे उनको भोग लगाए बिना और भागवत पाठ किए बिना जल की बूँद तक गले के नीचे नहीं उतारती थीं। आज उन्हें अपनी भक्ति का फल देखना था। घर का कोई प्राणी नहीं सोया था। रजनी बुआ और मैं तो अम्मा से ज़्यादा दादी की चिंता में थे।
वे सीधी बैठी प्रार्थना करती रही थीं, घंटों। बाबा दो-तीन बार मंदिर में आकर झाँक गए थे, फिर हॉल में चहलक़दमी करने लगे थे। अम्मा में ज़ब्त का माद्दा बहुत था। और कोई होता तो चीखों से कोठी भर देता पर अम्मा की दँतकड़ी बंध गई, लेकिन चीख नहीं निकली। मुँहअँधेरे प्रताप भवन भैया के रुदन की गूँज से भर उठा। दादी की प्रार्थना समाप्त हुई। अकड़ी कमर, सुन्न हुए घुटनों को आहिस्ता-आहिस्ता सहलाते हुए वे उठीं। चल नहीं पाईं ज़्यादा, वहीँ चौकी पर बैठ गईं। मुझे और रजनी बुआ को बुलाया- “थाली बजाओ दोनों जनीं।”
रजनी बुआ ने काँसे की थाली बजाई और मैं ठुमक-ठुमककर नाचने लगी। उषा बुआ ने थाल में मीठा परोसा और प्रताप भवन खुशी और मिठास से भर उठा। शाम तक कोठी के सहन में शहनाइयाँ बज उठीं। भैया होने का जश्न कोई मामूली न था। छोटी-मोटी शादी-सा जलसा हो रहा था। भैया है भी बहुत सुंदर.... उजला रंग, भोला-भाला मुखड़ा। “अम्मा, मुझे भैया से कोई दुश्मनी थोड़ी है लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि गणगौर की पिंडियाँ लड़कियों के ही ज़िम्मे क्यों आती हैं?”
अम्मा मुस्कुराई थीं- “तू खुद इसका उत्तर ढूँढ पायल।” खुद ही ढूँढना पड़ेगा। इन एहसासों को पहेली नहीं बनने देना है वरन उन चाबियों को ढूँढ निकालना है जो औरत की नियति की तमाम दराज़ें खोल डाले, उन तहखानों को टटोलना है जो दादी जैसी शख़्सियत में ताउम्र पैबिस्त रहे हैं। मैं जब अतीत की परतें हटाती हूँ तो ताज़ा रक़्त रिसता है....एक ख़ामोश दहशत....निरंतर डूबते जाने, जलते जाने, रिसते जाने का आंदोलित भय! हाँ....उन नंगी सच्चाइयों ने मेरे शरीर के पोर-पोर में जड़ें जमा ली हैं।
इस प्रताप भवन में बिताया कोई भी पल ऐसा नहीं जो घायल न हो....जो टीसता न हो। बड़ी दादी लगातार औरत होने का एहसास कराती रहीं....दादी प्रेम और बलिदान की मूरत बनकर उस एहसास को सौम्यता प्रदान करती रहीं....और अम्मा....ख़ामोश अंतर्द्वंद्व, आंदोलन और चुनौती को अपने अंदर अंकुरित कर मुझे सौंपती रहीं। मैंने उनकी इस उपज को स्वीकारा लेकिन दादी बड़ी गहराई से अपील करती रहीं....मैं उनके प्रेम में पगी सब कुछ तो भूले थी। उस विरोध के बावजूद भी मैं दादी की इच्छा के कारण पिंडियाँ बनाने में लग गई थी। एक सुकून था कि दादी संतुष्ट होंगी, सुकून इस बात का भी था कि इसका उत्तर मुझे ही खोजना है और यह अम्मा का सौंपा हुआ काम है।
मालवगढ़ आकंठ गणगौर उत्सव में डूबा था। लोकगीत हवाओं में घुल गए थे। तालाब, पनघट, गीतों के माधुर्य से चहक उठे थे। लड़कियों, बहुओं की हथेलियाँ हिना से रंगीन हो उन पर चित्रित फूल, कलश, चाँद, सूरज, चौपड़, स्वस्तिक का परिचय दे रही थीं और चैत्र लगते ही चैती तीज के दिन शोभायात्रा निकली। मैंने और रजनी बुआ ने ऊपरी मंज़िल के झरोखे से आदम़कद मूर्तियों में ईसर गणगौर की भव्य शोभायात्रा देखी। थिरकते, मचलते लोग, मंजीरे, खड़ताल की धुन....पूरी धरती मस्ती में भर उठी थी। प्रकृति भी अपने सूखे पत्तों के खड़ताल बजा हवा को बौराए दे रही थी। वसंत आगमन हो चुका था और वृक्षों, दरख़्तों में फूलों से श्रृंगार की होड़-सी मच गई थी।
बड़ी दादी की नर्स मारिया भी कुछ पल झरोखे के निकट आ खड़ी हुई। बहुत हँसमुख और नम्र स्वभाव की थी वो। बताने लगी- “हमारे गाँव में भी ऐसा ही होता है। होली के आसपास लोकगीतों पर हम खूब नाचते थे। कुल सत्ताइस झोपड़ियों का छोटा-सा गाँव, बिजली, पानी, सड़क से परिचय तक न था। सबके पास खेत तो थे पर जब खेतों में फसल तैयार हो जाती तो जंगली हाथी सब कुछ ख़त्म कर देते। फसल रौंद डालते, कई बार तो हमारी झोपड़ियाँ तक नेस्तनाबूद की हैं हाथियों ने।”
“फिर तुम कैसे नर्स बनीं मारिया?” मेरी जिज्ञासा पर मारिया हँसी- “पढ़कर, ट्रेनिंग लेकर। जर्मनों ने ऐसे बीहड़ गाँव में भी अपनी मिशनरी खोली है। शुरू में कुल दस विद्यार्थी थे, फिर आसपास के गाँवों से भी लड़के-लड़कियाँ आने लगे।”
“बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी?”
“बहुत ज़्यादा। बापू को तैयार करना ही मेहनत का काम था। उन्होंने मेरी शादी पड़ोस के गाँव में तय कर दी थी। मेरी इच्छा पढ़ने की थी तो बापू की डाँट भी खाई, मार भी। पर तैयार हो गए वे। शादी तो मुझे करना ही नहीं थी। नर्स बनना था, सेवा करनी थी असहायों की....जैसे जर्मन मिशनरी करती है।”
मैं अभिभूत थी मारिया की लगन से। अपना जीवन उत्सर्ग करने वाली ये देवमानवियाँ नमन करने योग्य लगीं।
“देखो....आंटी रो रही हैं।”
मेरे कान नीचे से आती आवाज़ों की ओर गए। बड़ी दादी रो-रोकर बड़े बाबा से कह रही थीं- “कब से माँग रही हूँ नींबू का शरबत....लेकिन उधर पहुँच गई रजनी, पायल के बीच झरोखे से दीदे मटकाने।”
मारिया तेज़ी से उनके पास पहुँच गई- “आंटी, नीबू मना है आपको....जोड़ दुखेंगे बदन के....ग्लूकोज़ का पानी रखकर तो आई थी मैं।”
“हाँ....हाँ....ग्लूकोज़ पिला-पिलाकर मार डाल मुझे।” और वे हिचक-हिचककर रोने लगीं। मारिया उनकी पीठ सहलाती रही। जब उनका रोना थमा तो चम्मच से उन्हें ग्लूकोज़ पिलाने लगी।
दादी ने मारिया के लिए गणगौर का मिष्ठान्न परोसा लेकिन मारिया ने इंकार कर दिया- “नहीं छोटी आंटी....मुझसे नहीं खाया जाएगा। आंटी भी तो यही सब खाना चाहती हैं लेकिन उनकी बीमारी....”
दादी ने हुलसकर मारिया को गले से लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। बड़े आग्रहपूर्वक उसके मुँह में मिठाई का टुकड़ा जब दादी ने रखा तो देखा उसकी आँखें अश्रुपूर्ण थीं। फिर दादी ने भी कुछ नहीं खाया। मुँह जुठार कर उठ गईं।
रात को मारिया हमारे कमरे में आई। माहौल से उत्सव की रौनक धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। सड़कें निपट सुनसान थीं। बगीचे में रातरानी महक रही थी। रजनी बुआ की आँखें झपकने लगीं लेकिन मारिया व्याकुल थी।
“आंटी का दुःख देखा नहीं जाता पायल बाई।”
वह मुझे ‘बाई’ कहती। राजस्थानी परंपरा में बाई सम्मान सूचक शब्द है। पर मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका तर्क था- “आप मना क्यों करती हैं? मीरा बाई भी तो थी आपके जात की....इतनी बड़ी पोयेट।”
उसके हाथों में बाइबिल थी।
“क्या लिखा है इसमें? पढ़कर सुनाओ।”
“लिखा है कोढ़ियों और नारियों पर समान दया की भावना रखो।”
“इसीलिए तुम बड़ी दादी पर दया करती हो।”
वह फिस्स से हँस दी- “मैं क्या दया करूँगी, प्रभु यीशु दया करेगा....ईश्वर सबकी रक्षा करता है। उसने मेरी भी रक्षा की।”
“तुम्हारी रक्षा!!” रजनी बुआ ने आश्चर्य से पूछा।
“हाँ, जब मैं पढ़ने जाने लगी तो वह राक्षस....हाँ, राक्षस ही था वह जिसके संग बापू ने मेरी शादी करने का सोचा था लेकिन मेरी ज़िद्द के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे लेकिन थॉमस ने नहीं टेके थे। मुझसे शादी न होना उसने अपना अपमान समझा था। एक दिन मिशनरी अस्पताल जाते हुए जंगल के बीचोंबीच सर्पिल पगडंडी पर वह मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया- “मुझसे शादी के लिए इंकार क्यों किया?” उसने कड़ककर पूछा।
“क्योंकि मैं नर्स बनना चाहती हूँ....सेवा में जीवन लगाना चाहती हूँ।”
“और मैं ख़ामोश बैठा रहूँ....तेरे बापू ने मुझसे शादी का वादा किया था, अब साला मुकर गया।”
“गाली मत दो थॉमस, चले जाओ यहाँ से। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है।” मैंने उससे छुटकारा पाना चाहा तो वह अट्टहास कर उठा। सहसा मैंने देखा उसके चेहरे पर विकृत भाव पसरता जा रहा है। उसकी हथेलियाँ आक्रामक हो उठीं, आँखें रक्तवर्ण....
“छोड़ दूँ तुझे और अपने अपमान से झुलसता रहूँ? नहीं, तुझे भी अपमान में झुलसना होगा। तुझे भी मुँह दिखाने में शर्म आएगी।” कहता हुआ वह मेरी ओर झपटा और मुझ पर दाँतों, नाखूनों की खरौंचे डालता हुआ मेरा ब्लाउज़ फाड़ने लगा। तभी जर्मन डॉक्टर वहाँ से गुज़रे....वे ऑक्सीज़न सिलेंडर लेने कार से शहर जा रहे थे....उन्होंने थॉमस की इस वहशियाना हरक़त पर उसे दो तमाचे जड़े और मुझसे कार में बैठने को कहा। बदले में उन्हें भी थॉमस के हाथों अपने बाल नुचवाने पड़े। थॉमस ने उनका कॉलर इतनी ज़ोर से खींचा कि आगे के बटन टूट गए।
मैं रास्ते भर रोती रही। किसे दोष दूँ पायल बाई! थॉमस की ज़लील हरक़त से क्या पूरे पुरुष समाज को दोष दूँ? फिर डॉक्टर की इंसानियत कहाँ जाएगी जिसने मुझे बचाया। ईसाई धर्म कहता है कि ईश्वर ने स्त्री बनाने में उस मिट्टी को नहीं लगाया जो पुरुष बनाने में लगाई थी बल्कि उसने आदम के शरीर के मांसल हिस्से से ईव को रचा था। इसीलिए तो ईव आदम की पूरक बनी। उसका एकाकीपन दूर करने का साधन....फिर भी मुझे अपने औरत होने पर अफ़सोस नहीं।”
मैं मारिया के इस तर्क पर चकित थी। यह साधारण-सी, साँवली-सी, अनाकर्षक चेहरे वाली आदिवासी महिला इस कद़र असाधारण। यह महिला बड़ी दादी की पीड़ाओं से पीड़ित है जबकि उनकी तीनों लड़कियाँ- मेरी बुआएँ उनके पास फटकती तक नहीं। तीनों बुआओं ने अपनी माँ को पलंग के दायरे में कैद मान लिया है। रजनी बुआ को गहरी नींद सता रही है, जबकि मारिया की आँखें झपक भी नहीं रही हैं।
“सो जाओ पायल बाई....अब मैं थोड़ी देर प्रेयर करूँगी....प्रेयर में बड़ी शक्ति होती है। वह हममें आत्मविश्वास भी जगाती है। मेरे बापू ने मुझे पढ़ाया, नर्स बनाया और माँ ने प्रेयर करना सिखाया। प्रेयर करते-करते मेरी माँ बड़ी शांति से मरी। सारा गाँव उनकी मौत पर नतमस्तक था....सोते-सोते रात के किसी प्रहर में ही अंतिम साँस ली उसने। न वह बीमार थी, न उसे साँप-बिच्छू ने ही काटा था। उसे तो देवदूत उठाकर ले गए।”
“और तुम्हारे बापू?”
“बापू उसी झोपड़ी में रहते हैं। मैं उन्हें पैसे भेजती हूँ....अब तो वे मिशनरी अस्पताल के रोगियों के सिरहाने बैठकर उन्हें थपकियाँ देकर सुलाते हैं। बापू की उँगलियों में जादू है, मिनटों में नींद आ जाती है।”
मारिया के बापू की उँगलियाँ मानो तानपुरा हों....हलका-हलका नशीला संगीत गुँजाती जिनकी तरन्नुम में अपने रोगों से जूझता असहाय प्राणी सपनों की बाँहों में खो-सा जाता होगा।
सुबह जब मैं बाथरूम की ओर जा रही थी और बाबा के टहलने जाने से दादी का कमरा भी अँगड़ाई ले रहा था तो मैंने देखा मारिया बड़ी दादी के पायताने करवट लिए सो रही है और बड़े बाबा कमरे के सामने गलियारे में तख़त पर लेटे खिड़की की ओर टकटकी बाँधे हैं। पन्ना ने मेरे नहाने के पानी में गुलाबजल डालकर गुलाब की पंखुड़ियाँ भी तैरा दी थीं। मुझे वे पंखुड़ियाँ नहाते हुए खूब चुभीं, मारिया के आगे अपना ऐश्वर्य उपहासजनक प्रतीत हुआ।
होश सम्हालते ही अगर किसी व्यक्ति को मैंने ख़ामोश, विरक्त और गुमसुम देखा है तो वे बड़े बाबा थे। वैसे भी वे अपना बड़प्पन नहीं निभा पाए.... सब कुछ बाबा ने ही सम्हाला....ज़मीन, जायदाद....खेत-खलिहान....ख़ानदान.... सब कुछ बाबा और दादी के ज़िम्मे था। बड़े बाबा के स्वभाव का सीधापन और बड़ी दादी की बीमारी दोनों ने उन्हें दीमक-सा चाट लिया था।
वे गलियारे में तख़त पर अक्सर रात बिताते या फिर अपने स्टडी रूम में मोटी किताबों में उलझे रहते और लगातार कुछ लिखते रहते। वे लिखते....बड़ी दादी छीजतीं....वे ज़िंदगी को थामने की कोशिश में लगे रहते और बड़ी दादी के हाथ से ज़िंदगी फिसलती जाती। ज्यों मुट्ठी में दबी रेत आहिस्ता-आहिस्ता फिसलती रहती है, फिर मुट्ठी ख़ाली हो जाती है। बड़ी दादी ख़ाली मुट्ठी से घबराती थीं इसीलिए मारिया पर झल्लाती रहतीं। लेकिन उनकी झल्लाहट मारिया की तड़प को कई गुना बढ़ा देती है यह बड़ी दादी क्यों नहीं समझ पातीं।
एक दिन बड़े बाबा से मिलने कोई साधू आया। लंबी दाढ़ी, सिर पर जटाएँ, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर त्रिपुंड....उनके आते ही बड़े बाबा ने कमरा बंद कर लिया और घंटों नहीं खोला लेकिन उनके कमरे की खिड़की से निकलता चिलम का धुआँ दादी को बेचैन करता रहा।
“इस घर में साधू फ़क़ीरों का क्या काम?”
“मालकिन....आप तो खाने का परोसा सोचो। पूड़ी आलू की सब्ज़ी और हलवा मँगवाया है सूजी का बड़े मालिक ने।”
महाराजिन ने दादी को बताया और पल्लू में मुँह छुपाकर हँसी। अब साधू फ़क़ीर का मन हलवा-पूड़ी खाने को हो तो हम गिरस्ती वालों का क्या हाल हो?
लेकिन दादी सोच में पड़ गई....कहीं जेठजी संन्यास तो नहीं ले रहे....भले ही घर के चार कामों में हाथ नहीं बँटाते लेकिन उनकी मौजूदगी का साया ही काफ़ी है घर के लिए। कम-से-कम बड़ों की मौजूदगी तो बनी है। और जब दादी ने बाबा से यह कहा तो बाबा ठहाका लगाने लगे- “तुम भी महारानी कबूतरी-सी सहम जाती हो बात-बात पर....अरे भाभी सा के बीमार रहने पर भाई सा विरक्त नहीं होंगे क्या? वो तो उस साधू की लँगोटी तक धोते हैं अपने हाथ से....हाँ, मैंने खुद देखा है।”
“कब? ये तो पहली बार आया है घर।”
“तो क्या हुआ? भाई सा जाते हैं उसके घर बिलानागा, कुएँ के पास ही तो कुटिया है इसकी। बनास नदी जाते हुए जो दाहिने हाथ पर कुआँ पड़ता है।”
दादी ने भी देखी है यह कुटिया कई बार नदी की ओर जाते हुए। कुटिया की गोबर लिपी दीवारों पर कचरी, फूट की बेलें छाई हैं और कुएँ के नज़दीक ही एक धूनी भी जलती रहती है। कुएँ से पानी भरने के लिए आई हुई पनिहारिनें कभी सत्तू, कभी बाजरे की रोटी और गुड़ साधू के लिए लाती रहती हैं। बदले में वह उनके माथे पर भभूत लगाकर आशीर्वाद देता है।
इलाक़े भर में प्रसिद्ध है कि उसके भभूत का आशीर्वाद फलित होता है। वैसे साधू है औघड़दानी....शंकरजी के लिंग के ऊपर रोटी रखकर खाता है, शराब पीता है और साथ-ही-साथ पास बैठे कुत्ते को भी खिलाता जाता है। ऐसे अघोरी का घर में आना दादी को नागवार लगता पर करें भी क्या। बड़े बाबा से कहने की हिम्मत ही नहीं, वैसे भी गृहस्थी में उनका दख़ल न के बराबर है।
दादी ही एकमात्र वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी गृहस्थी ओढ़ रखी है। किसी का ब्याह हो, मुंडन हो, कनछेदन हो, नए घर में प्रवेश, भूमि पूजा हर नेग दस्तूर दादी को बिना भूल-चूक याद रहता। दादी मानो वो समंदर थीं जिसकी लहरें भाप बनकर बादल के रूप में आकाश में छा जातीं और फिर बरसकर सबको तृप्त करतीं। बुआओं की हर फ़रमाइश दादी से और दादी का सदाव्रत हमेशा खुला रहता।
तभी तो ज़िद्द कर बैठी थी मैं। अम्मा ने मुझे शमीज़ पर नींबू रंग की सुंदर फ्रॉक पहनाई थी जिसके गले और बाँहों में शटल की लेस और मोती जड़े थे। हफ्ते भर बाद दादी, अम्मा, उषा बुआ, संध्या बुआ समेत ख़ानदान के क़रीब पचास लोग सवा महीने की वृंदावन यात्रा पर जा रहे हैं। दादी के गुरूजी मथुरा से इस तीर्थ यात्रा का नेतृत्व करेंगे। कुल मिलाकर पाँच सौ यात्री तो होंगे। खूब मज़ा आएगा। “मैं भी चलूँगी दादी।”
“ऊब जाओगी पायल बिट्टो....सवा महीने कुछ कम नहीं होते। तपस्या है पूरी....उधर बच्चों का न सधेगा।”
“पर मैं जाऊँगी....तंग नहीं करूँगी दादी आपको।”
दादी नहीं मानीं। उनका तर्क सही था। तीर्थ यात्रा कष्टों से भरी होती है....मेरी वयस के बच्चे बाधक ही तो होंगे उनके....लेकिन कोई भी तर्क मानने को मैं तैयार न थी। बस, जाना है मुझे....रजनी बुआ न जाएँ, उषा बुआ और संध्या बुआ तो जा रही हैं। घर में बचेगा कौन....बड़ी दादी....मुझे नहीं रहना बड़ी दादी के साथ।
एकादशी के दिन यात्रा शुरू होने वाली थी। मेहमानों से प्रताप भवन खचाखच भरा था। पूरी तैयारी हो चुकी थी और मैं आसन पाटी लिए ऊपर की मंज़िल में पड़ी थी। रात दादी आई....हाथ में मखानों की खीर से भरा चाँदी का कटोरा था- “ले, जीम ले ज़िद्दन और चल, सूटकेस में कपड़े रखवा ले अपनी अम्मा से।”
“क्याऽऽऽ”....मैं खुशी से लगभग चीखती हुई सी दादी के गले से झूल गई और उनके गालों को चूम डाला- “अरी, मार थूक लिभड़ाये दे रही है। चल, चल, बहुत हो गया लाड़।”
और प्यार से मेरे मुँह में खीर की चम्मच रख दी- “ईश्वर परम कल्याणकारी है, तेरी यात्रा में उनकी मर्ज़ी है तभी मुझे संकेत मिला।” कहकर उन्होंने श्रृद्धा से अपने मुरली मनोहर को याद किया। मैं परम तृप्ति से खीर खाने लगी।
पता चला रजनी बुआ भी जा रही है। बाबा नहीं जाएँगे। पार्टी के बहुत ज़रूरी कार्यक्रम हैं। फिर उनका उद्देश्य भारत की आज़ादी है और वे तन-मन-धन से उसी में लगे हैं। रात्रि जागरण से उनकी आँखें सूजी थीं। दादी उनके सिर में तेल ठोंक रही थीं- “मैंने महाराजिन को सब समझा दिया है। देव बाबा की मड़िया बिलानागा खाना जाएगा। तुम चिंता नहीं करना और अपना ख़याल रखना।” बाबा ने तरलाई युक्त आँखों से अपनी मालविका को देखा। तीर्थ यात्रा के तेज से उनका चेहरा दमक रहा था। बालों का जुड़ाबाँधा था फिर भी कुछ लटें माथे पर बिखर आई थीं।
“सवा महीने बाद लौटोगी, इस बार अमावस सवा महीने की पड़ रही है न।”
पहले तो दादी कुछ समझी नहीं और जब बात समझ में आई तो शरमा गईं। बाबा ने उनका चाँद-सा चेहरा हथेलियों में भर लिया था। प्रताप भवन के बुर्ज पर बैठे मयूर कूकने लगे थे।
दादीका घर से बाहर जाना कोई मामूली बात न थी। माली, दरबान, महाराज, महाराजिन, नौकर-चाकर, दास-दासियाँ सब बार-बार बुलाए गए। मारिया को अलग ताक़ीद की गई कि वह एक मिनट को भी बड़ी दादी को अकेला न छोड़े। मारिया खुद अपने गाँव जाना चाहती थी पर दादी के लौटने के बाद ही उसे छुट्टी मिल सकती थी।
तारों की छाँव में ही जीपों का काफ़िला चल पड़ा स्टेशन की ओर। मैं और रजनी बुआ तो खुशी, उत्तेजना और जोश के सागर में गोते लगा रहे थे। तीसरे दिन हम सब मथुरा पहुँचे जहाँ गुरूजी के निर्देशन में यात्रा आरंभ होनी थी। मैं आँखें फाड़-फाड़कर देख रही थी उस भव्य इंतज़ाम को। ट्रकों में बड़े-बड़े बर्तन, चूल्हा, अँगीठी....कनस्तरों में खाने का सामान, बोरों में भरी सब्ज़ियाँ रसोइयों के सुपुर्द कर दी गई थीं।
बड़े-बड़े तंबू, गद्दे, चादर, तकिए, फोल्डिंग पलंग, जेनरेटर....सवा महीनों तक पाँच सौ यात्रियों के लिए रोज़मर्रा का सारा सामान गुरूजी की देखरेख में जुटाया गया था। मेरे लिए तो मानो एक दूसरी ही दुनिया का हवाला था ये। गुरूजी चौकी पर बैठे थे। पैरों में खड़ाऊँ। दादी ने उनके पैरों में शीश नवाया- “कल्याणी भव। देवियों की नेता तुम हो। सभी देवियों का सारा भार तुम्हारे ज़िम्मे।”
दादी गद्गद- “इतना बड़ा भार उठा पाऊँगी मैं?”
“तुम कल्याणी हो देवी मालविका, उठो, ठीक नौ बजे प्रस्थान मुहूर्त है।”
काफ़िला चल पड़ा। राजपथ के दोनों ओर घने जंगल। आम, आँवला, नीम, कटहल। कटहल के झाड़ पर बंदर बैठे थे। मैंने उनकी तस्वीर खींच ली। मैंने राजस्थानी हथकरघे का काँच जड़ा कपड़े का बैग कंधे सेलटकाया हुआ था जिसमें दूरबीन, कैमरा, नोटबुक, पेन रखे थे। ऐसा ही बैग रजनी बुआ के कंधे पर भी था लेकिन उसमें कैमरा न था। हम दोनों के बीच साझा कैमरा था....हर रील आधी उनकी, आधी मेरी। वे तरह-तरह के पोज़ में फोटो खिंचवातीं। मैं प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीरें लेती- तो वे कहतीं- “रील बरबाद कर रही हो तुम।” उनके बैग में चिकनी सुपारियों की थैली भी थी।
हर वक़्त उनके मुँह में चिकनी सुपारी का टुकड़ा दबा रहता। शाम ढलने को थी। जंगल में ही तंबू गाड़े गए। गद्दे, चादरें बिछे....जेनरेटर से सभी तंबुओं में बिजली जल उठी। दूर अलग-थलग रसोइए ने चूल्हा जलाया और देखते ही देखते भोजन तैयार होने लगा। गुरूजी के तंबू में उन्होंने कुछ ख़ास लोगों को बुलाया था। दादी और अम्मा भी थीं। मैं अम्मा के साथ ही बैठी लेकिन गुरूजी ज़राभी नाराज़ नहीं हुए। प्रवचन शुरू हुआ जिसकी गूँज माइक के द्वारा अन्य तंबुओं तक भी पहुँची।
मेरे जीवन की यह ऐसी रात थी जिसे भूल पाना कठिन था। चतुर्दशी का चाँद निरभ्र आकाश में इतना शुभ्र और निर्मल तो कभी दिखा नहीं। ओर-छोर जंगल ही जंगल। पेड़ों पर कभी-कभार पंख फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ जाती।
प्रवचन, भोजन और प्रार्थना के बाद सब गहरी नींद में सोए थे। लेकिन मैं जंगली सौंदर्य में पलकें भी नहीं झपका रही थी। कभी इस डाल से उस डाल तक मोर अपनी लंबी पूँछ लेकर उड़ता। कभी नीली चिड़ियाँ अदृश्य-सी अपने नन्हे-नन्हे पर फड़फड़ातीं। अचानक सियारोंका रुदन सुन मैं अम्मा से लिपटकर सोने का प्रयास करने लगी। चाँदनी भी फीकी हो चली थी।
तड़के सुबह चुस्त-दुरुस्त हम पुनः यात्रा पर चल पड़े। मथुरा से एक पंडितजी भी आए थे जो उधर कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते थे। बड़े फख्र से वे रास्ते भर अंग्रेज़ अफ़सर के किस्से सुनाते रहे जिनकी बेटियों को वे संस्कृत पढ़ाते थे। वृंदावन के बारे में उन्होंने बताया कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसके विषय में बहुत विस्तार से लिखा है। प्राचीन काल में महाराजा केदार की पुत्री थी वृंदा।
उसने श्रीकृष्ण के प्रेम में वशीभूत हो उन्हें पति रूप में पाने की तपस्या इन्हीं जंगलों में की थी। तभी से इसका नाम वृंदावन पड़ा। वृंदा देवी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी इन्हीं तमाल वृक्षों के नीचे ही तो प्रेम की अद्भुत क्रीड़ाएँ करती थी। रास्ते में चलते हुए जितने मंदिर मिलते थे सभी के दर्शनों के लिए हमें रुकना पड़ता था। मैं मंदिरों में भक्तिभाव से कभी नहीं गई बल्कि उसके स्थापत्य की बारीकियों को देखने-परखने ही जाती थी। जितना बन सका तस्वीरें लीं। अम्मा जब चढ़ाने को पैसे देतीं तो मैं चुपचाप रजनी बुआ की हथेली में सरका देती....न जाने कहाँ की विद्रोही अक्खड़ आत्मा थी मेरी।
कुंड स्नान के लिए सारा काफ़िला रुका। दादी ने दान-दक्षिणा देने के लिए ख़ासी रेजगारी, चाँदी के रुपए वगैरह बाँधकर अलग-अलग बटुओं में रखे थे। मछ कुंड से बिछिया दान करते हैं।लौह कुंड में लोहे से बनी वस्तुएँ....लव कुंड में भी दान-दक्षिणा का महत्व है। महाराजजी ने प्रथम रात्रि प्रवचन में ही संकेत दे दिया था, कि कोई भी तीर्थयात्री, बाल गोपाल जंगल की फूल-पत्तियाँ नहीं तोड़ेंगे, लड़ाई-झगड़ा नहीं करेंगे, साबुन तेल नहीं लगाएँगे। सो मैं तो खुश थी।
इन सब चीज़ों से मुझे भी परहेज़ था। हाँ, साबुन का न लगाना अखर गया। दादी मुल्तानी मिट्टी लाई थीं। उसी को साबुन मान लिया था। कुंडों में स्नान तरोताज़ा कर देता था। फिर सूर्य को जल अंजलि चढ़ाई जाती और कीर्तन होता।
तमाम मंदिरों के दर्शन, परिक्रमा, कुंड स्नान आदि करते हुए, रात में जंगलों में विश्राम करते हुए हम डीग पहुँचे जो किसी समय भगवान कृष्ण की लीलाभूमि था। चौरासी कोस की ब्रजयात्रा के समापन का यह पूर्व पड़ाव था। गुरूजी ने सबको एकत्रित करके प्रवचन दिया और यात्रा समाप्ति की घोषणा की। दादी गुरूजी के चरणों पर गिर पड़ीं- “स्वामीजी, आपके आशीर्वाद से ब्रजयात्रा, गोबर्धन परिक्रमा निर्विघ्न निपट गई। दया बनाए रखें।”
“तुम तो कल्याणी हो देवी मालविका। मैं तुम्हारे हृदय में संपूर्ण मानवता का सागर लहराता देख रहा हूँ। स्वाति नक्षत्र की बूँद सीपी का मर्म बड़ी कठोरता से भेदकर मोती बननेको उसमें समा जाती है। यह संसार का नियम है साध्वी। किंतु तुम बड़ी कोमलता से मुक्ता बनी चली जाती हो....मुक्ता बनना कोई सहज कार्य नहीं है।” दादी की आँखों में मानो मुक्ता लड़ियाँ पिघल-पिघलकर टपकने लगीं। उन्होंने गुरूजी के चरण मानो आँसुओं से पखार डाले।
उस अंतिम रात्रि में गुरूजी ने अपने निजी कोष सेहम सबको भोजन कराया। महाप्रसाद में मिले बेसन के लड्डुओं का वैसा स्वाद फिर दुबारा नहीं मिला।
मैं अपने आपको अक्खड़ और विद्रोही मानती हूँ। फिर क्या बात है किसब कुछ करने का मन करता है। सारे तीज-त्यौहार, तीर्थयात्रा, दान यज्ञ....क्यों मोहते हैं इतना जबकि इनके समापन पर मैं हमेशा सोचती रही....नहीं, मैं आस्तिक नहीं हूँ....ईश्वर पर मेरा विश्वास नहीं। फिर कौन सी शक्ति कराती है यह सब? मन की जिज्ञासा क्यों कुरेद-कुरेदकर अपना शमन चाहती हैं। शायद इसी कुरेद से मजबूर हो मैंने दादी से पूछा था-
“दादी, आपको गुरूजी ने पहले सागर कहा, फिर सीप और मोती। ये विरोधी उपमाएँ समझ में नहीं आईं।”
दादी मुस्कुराती रहीं। शायद इसका जवाब उनके पास न था। मेरी जिज्ञासा शांत की अम्मा ने- जानती हो पायल सागर में सीपियाँ होती हैं जो मोती पैदा करती हैं। अगर सागर न होतो सीपियों का जीवन भी असंभव है। तुम्हारी दादी का हृदय वह सीप है जो सारे सागर को अपने में समेटे है....है न अनहोनी बात....लेकिन गुरूजी का यही तात्पर्य था। अब साधू-संतों की बातें होती तो गूढ़ हैं। समझना मुश्किल।
मैं अम्मा के तर्क पर चकित थी। अगर अम्मा को मौका मिला होता तो वे एक काबिल प्रोफ़ेसर, लैक्चरर तो ज़रूर हुई होतीं।
वृंदावन से विदाई लेते हुए जाने क्यों मन उदास था। क्या यह उदासी बरसाने की राधा की थी जो कृष्ण के द्वारिका जाने पर उदास, बेचैनथी? या कृष्ण की जो राधा से बिछुड़ते हुए स्वयं राधामय हो उठे थे।
मालवगढ़ लौटकर मारिया को बेचैन पाया। उसके बापू का ख़त था कि वे सख़्त बीमार हैं। इधर बाबा अलग खौल रहे थे। उनके एक साथी को पुजारी के वेश में नदी किनारे अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और जब उससे भेद नहीं उगलवा पाए थे तो चौराहे के बरगद पर उसे फाँसी दे दी थी। बाबा फूट-फूटकर रोए थे- “महीनों उस व्यक्ति ने जंगलों की ख़ाक़ छानी थी। रातों की नींद हराम की थी। कई-कई बार बारूद से उसकी उँगलियाँ जली थी पर उसने उफ़ भी नहीं की। वह शहीद हो गया....देश को आज़ाद कराने का कण भर का प्रयास।”
दादी ख़ामोश बैठी रही थीं। जब बाबा चुप हुए तो उन्हें ठंडे पानी का गिलास थमाया और चुपचाप अपने कमरे के बाजू में कृष्णजी के मंदिर में दिया जलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की....मन-ही-मन शिकायत भी की होगी कि मैंतो तुम्हारे दर्शनों के लिए द्वारका, ब्रज की गलियाँ मापती रही, गोवर्धन परिक्रमा करती रही और तुमने हमारे ही एक साथी के साथ ऐसा अन्याय किया।
शायद जवाब भी पाया हो कि आज़ादी के दीवानों के साथ कौन अन्याय कर सकता है? उस रात बाबा के साथ-साथ दादी भी निराहार सोईं। मारिया की हिम्मत नहीं पड़ी छुट्टियाँ माँगने की। लेकिन अगले दिन भोर होते ही दादी ने रेलवे टिकट के लिए नौकर को भेज दिया और मारिया से तैयारी करने को कहा। बड़ी दादी की तबियत में कुछ सुधार नज़र आ रहा था। मारिया ने उनके बाल धो दिए थे और वे पलंग से टिकी वृंदावन के मंदिरों का प्रसाद खा रही थीं। दादी उन्हें मुख़्तसर में यात्रा के किस्से सुना रही थीं।
मारिया के जाते ही बड़ी दादी का सारा काम दादी के ज़िम्मे आ गया। कंचन उनका काम करने में नाक-भौं सिकोड़ती थी। जसोदा तो कनबहरी लादे रहती। बुलाने पर ‘आती हूँ’ ज़रूर कहती पर घंटों गायब रहती और पन्ना पंद्रह-सोलह साल की खिलंदड़ी किसी काम को गंभीरता से नहीं लेती थी। उषा बुआ बड़ी दादी को सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना खिला देतीं और संध्या बुआ रात का लेकिन दवाई के लिए, दर्द और तकलीफ़ में दादी के नाम की गुहार लगाती।
अलबत्ता एक नौकरानी मारिया के एवज़ बुला ली गई थी पर दादी को उसका पहनावा भाता नहीं था। भड़कीले रंग का चोली घाघरा, ओढ़नी सिर परतो रहती पर पूरी की पूरी पीठ के ऊपर पड़ी रहती। दोनों छातियाँ आधी-आधी चोली के अंदर बाकी बाहर। वैसे यहराजस्थान का ख़ास पहनावा था। घूंघट के बाबजूद ओढ़नी छाती पर नहीं रहती। दादी ने समझाया- “देखो, मर्दों का आना-जाना होता है। तुम ओढ़नी ज़रा ढंग से लिया करो।”
नौकरानी फिस्स से हँस दी थी- “माई, मर्द देखें तब न।”
दादी ने उसे फौरन रुख़सत किया। ऐसी निर्लज्ज का सेवा चाकरी में ध्यान रमेगा?
कई बार ऐसी औरतों को दादी ने साधू के कुएँ पर अपना घाघरा-चोली उतारकर धोते देखा है। तब ये नंगे बदन पर ओढ़नी लपेट लेती हैं और घाघरा-चोली धोकर रेत पर सूखने के लिए फैला देती हैं। मर्द आते-जाते इनकी ओर पलटकर भी नहीं देखते। साधू तो खर्राटे भरता चटाई पर लंबा चित्त पड़ा रहता है। जब तक कपड़े सूखते ये औरतें आपस में सिर जोड़कर सुरीले गाने गातीं।
जिनमें रेगिस्तान के ऊँटों का काफ़िला, रेत के ढूह, सपाट चट्टानें, बबूल, कीकर और भटकटैया की झाड़ियाँ, उनमें खिले बैंगनी फूल और खुश्क, रेतीले मैदानों का ज़िक्र होता। उन गानों में सजनी का साजन उनकी आँखों के सामने कुदाल चला रहा है, चट्टानें तोड़ रहा है और वे बेचैन हैं- “साजन आओ....मिलकर सत्तू खाएँ। लेकिन सत्तू माँडे किससे? यहाँ तो रेत ही रेत है, पानी का निशाँ तक नहीं।
रात भर पपीहा टेरता है- पी कहाँ, पी कहाँ? टिटहरी भी उसी की खोज में अपने शुष्क गले से पुकारती है- टिटीहट, टिटीहट।” अम्मा कहती हैं प्यासे को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए नहीं तो पपीहा या टिटहरी का जनम मिलता है।
सावन लग चुका है। कभी बादल छा जाते हैं, कभी हलके बरसकर रुख़सत हो जाते हैं। चिलचिलाती धूप में सपेरे साँपों की पिटारी लेकर निकले हैं। कल नागपंचमी जो है। सपेरों के चीकट झोलों में बीन है। ये झोले इतने गहरे होते हैं कि जो कुछ दो, सब उस सुरंग में समाता जाता है। प्रताप भवन की ड्योढ़ी पर जब बीन बजी तो दादी ने नारियल की नरैटी में दूध भरा और पुराने कपड़े दरबान के हाथ सपेरे के लिए भेजे।
सपेरा बीन बजा-बजाकर नाग का फन काढ़ रहा था, उसके पैरों में घुँघरू बँधे थे। सपेरन ढोल बजा रही थी। ऐसा लगता मानो बरसात अब होने ही वाली है, ढोल बिल्कुल बादल की गर्ज़न-तर्जन करता बजता। घंटे भर के इस सुरीले समाँ के बाद सपेरों के जाते ही सन्नाटा-सा छा गया। अंदर से उषा बुआ की चीख सन्नाटे को तोड़ रही थी। सभी को पता था क्या होने वाला है।
पुश्तान पुश्तों से प्रताप भवन में एक साँप भी रहता था। जो ऐन नागपंचमी के दिन कोठी के अहाते की दीवार पर रेंगता था। लंबा...चितकबरा...बूढ़ा साँप...सब अपनी-अपनी खिड़कियों, झरोखों से उसके दर्शन करते। बिल से बाहर निकलते ही वह पाखाना करना शुरू कर देता। अजीब तरह की चिर्-चिर् की आवाज़ होती और उसकी जीभ लपलपाती रहती। यह साँप कोठी की स्त्रियों का शाप था ऐसा अम्मा कहती थीं। उनका कहना था कि पुश्तान पुश्तों से इस कोठी की बहुएँ, बेटिएँ न कभी सुखी रहेंगी, न रही हैं।
क्या मारिया पर भी साँप का शाप फलीभूत हो रहा है? लेकिन खुश लौटी है मारिया। उसके साँवले सलोने चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव व्याप्त है। पूरे मुखड़े पर उसके दाँत ही हैं जो आकर्षक हैं, मोती-से सफ़ेद...बेहद आकर्षक हँसी...जैसे ग्रेनाइट की चट्टान पर दुग्ध धार का सोता फूट पड़ा हो।
बड़ी दादी का बदन टोहकर, दवा-दारु से निपटकर मारिया हमारे कमरे में आई। तब तक सड़क पर लैंप पोस्ट के उज्ज्वल दायरे फैल चुके थे। हवा रुक-रूककर चल रही थी लेकिन ठंडक थी। दूर सन्नाटे को तोड़ता किसी अंग्रेज़ का घोड़ा अपनी टाप छोड़ता निकल गया...पीछे-पीछे ऊँटों का बलबलाना.....नीम की ताज़ी टूटी डालियों की तुर्श कड़वी गंध...
\"कैसे हैं तुम्हारे बापू मारिया।\"
\"बापू कमज़ोर हो गए हैं पायल बाई। अब कोई उधर टोकने वाला तो है नहीं। जब मनचाहा खा लिया, नहीं तो लेट गए भूखे ही। लेकिन अब थॉमस खाना बना देता है।\"
\"थॉमस।\" मैं चौंक पड़ी- \"वही, तुम्हारा मंगेतर?\"
\"हाँ, वह मिशनरी अस्पताल में कंपाउंडर हो गया है। शादी भी नहीं की उसने। इस बार मेरे से बोला कि जब तू नर्स हो गई मारिया तो मुझे तो कंपाउंडर बनना ही चाहिए। पायल बाई...उस दिन का उसका वो ख़ौफ़नाक अटैक एक जुनून ही था सच्चे प्यार का। मुझे पाने की एक दहशतनाक़ कोशिश.....\"
मारिया की आँखें झुकीं और उनमें से दो बूँदें चादर पर चू पड़ीं।
\"एक बेटे की तरह थॉमस बापू का ख़याल रख रहा है। कहता है- \'बापू, तुम मेरी मारिया के बापू यानी मेरे बापू। तुम्हारी सारी ज़िम्मेवारी मेरी।\' \"
\"तुम शादी क्यों नहीं कर लेतीं उससे? वह तुम्हें कितना अधिक चाहता है।\" रजनी बुआ बोलीं तो मारिया के हाथ कानों तक पहुँच गए- \"नहीं.....नहीं.....मैंने प्रभु यीशु को वचन दिया है लाचार, असहाय व्यक्तियों की सेवा करने का। शादी बहुत बड़ी बाधा बन जाएगी मेरे इस मिशन में।\"
बड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। जहाँ ऊँटों के काफ़िले ने डेरा जमाया था, उधर तंबू के आगे आग जल रही थी। एक चहल-पहल-सी थी जो लौ की लपलपाहट में चलती-फिरती नज़र आ रही थी। पाजेब की छुनछुन, हँसी की खिलखिलाहट फिर बिरहा की थाप.....एक मनुहार.....
म्हारी लाड़ली नी कीमत कीजो, घण मान सू रखियो जी,
कुँवर सा अर्जी सुणियों जी, कुँवर सा काँची भोली जी।
मानो मारिया का बापू ही थॉमस से मनुहार कर रहा है, शायद वात्सल्य की ऐसी ही पुकार होती है लेकिन मारिया तो इस भाव से कोसों दूर चली गई है..... दूर.....एकाकी.....तपस्विनी-सी.....कल्याण को आतुर।
मारिया कोठी में पुत्री की हैसियत से रहने लगी। उसके समर्पण भाव और ग़ज़ब के बर्दाश्त ने सबका मन मोह लिया। जब दादी रात के पहर बिस्तर पर जाती तो मारिया ज़िद्द करके पैर दबाती, बालों में तेल डालती। उषा बुआ बड़ी दादी की मर्ज़ी के खिलाफ़ इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। भादों के लगते ही कोठी चहल-पहल से भर उठी थी। उषा बुआ की फुफेरी बहन राधो बुआ और फूफाजी आ रहे थे। फूफाजी अपनी साली को अंग्रेज़ी पढ़ाने आ रहे थे।
\"इस बार तीजों पर रौनक रहेगी, राधो और कुँवरसा के आने से।\" दादी ने अम्मा से कहा और झटपट तैयार होने की ताक़ीद की। तीजों का बाज़ार भर गया है। तमाम बेटियों के लिए ख़रीदी करनी है। सिंजारा होगा। बेटी दामाद जीमेंगे। मेहँदी, चूड़ी, टिकली, बिंदी, पायल, बिछिये, साड़ी, कपड़ों के थान.....दादी ने मारिया की पसंद के भी कपड़े ख़रीदे, नई चप्पलें ख़रीद कर दीं और सोने की चौकोर घड़ी। मारिया गद्गद हो दादी से लिपट ही तो गई। मेरी ननिहाल से अम्मा, बाबूजी, दादी, बाबा के लिए तीज की भेंट मामा लेकर आए। भैया के जन्म पर छोटे मामा आए छूछक लेकर.....अब बड़े मामा अम्मा का सिंजारा करने आए हैं। कोठी के गेट पर उनकी फिटन खड़ी है। अम्मा को और कुछ चाहिए तो बता दें, आज ही लौटना होगा।
अम्मा क्या कहतीं, मन भर आया था उनका, बस पूजा तक रुकने की ज़िद्द की जो मामा को माननी पड़ी। दादी ने गोबर से आँगन लिपवाकर बीचोंबीच मिट्टी का ढेर लगाकर उसमें नीम की डगाल रोपी। पूजा की तैयारी सभी बुआओं ने मिलकर की। सत्तू के लड्डूओं का थाल आया। बुआएँ लकदक कपड़ों में थीं। राधो बुआ ने दुल्हन जैसा सिंगार किया था। फूफा सा ने शेरवानी पर कटार लटकाई थी। सिर पर हलकी गुलाबी पगड़ी। पगड़ी में हीरे की कनी।
ऊपर छत से बाबा ने नौकर दौड़ाया, चाँद निकल आया है। सभी सुहागिनों ने चाँद को अर्घ दिया और आपस में कहानी कही। लड्डू के छोटे-छोटे टुकड़े काटे गए और नीम के पत्तों के साथ श्रद्धापूर्वक खाए गए। मैंने मुँह बनाया तो अम्मा ने घुड़क दिया। मैं घुटनों में मुँह छुपाए मन-ही-मन हँसती रही। बड़े होकर मैं तो कभी तीज का व्रत नहीं रखूँगी, कभी नीम के कड़ू पत्ते नहीं खाऊँगी।
अम्मा ने बड़े मामा के लिए पापड़ भूनकर उसका चूरा बनाकर उसमें घी-नमक डाला और घी का धुआँ दिखाकर उनकी थाली में परोसा। यह उनका प्रिय व्यंजन था। उन्होंने थाली के नीचे नए करारे नोट रखकर खाना खाया और सबसे विदा ले फिटन में जा बैठे। मैं अम्मा बाबूजी के साथ उन्हें छोड़ने गेट तक आई थी। तभी देखा फिटन के बाजू में अंग्रेज़ अफ़सर का घोड़ा खड़ा है।
बाबा छत पर थे, बातें करने की आवाज़ वहीँ से आ रही थी। दादी ने बड़े बेमन से छत पर परोसा भिजवाया लेकिन मन उनका बेचैन हो गया था। बार-बार बाबा के स्टडी रूम में जातीं। टेबिल पर फैले तमाम काग़ज़ों पर टेबिल क्लॉथ बिछा दिया उन्होंने। फिर आहट लेती रहीं। तलघर की सीढ़ियाँ गहरे अँधेरे में थीं। बाबा कोहरे जैसे धूमिल आलोक में बहुत रात तक छत पर बैठे रहे। जब घोड़े की टाप दादी ने सुन ली तब जाकर मुँह जुठारा। दादी के खाने के बाद अम्मा ने खाया।
जब दादी सोने के कमरे में आईं तो बाबा पलंग पर लेट चुके थे।
\"पूरे चार घंटे चाट गया वो फिरंगी।\"
\"मैं तो डर रही थी.....ढंग से पारायण भी नहीं किया, कान वहीँ लगे रहे।\"
\"अरे, तुम नाहक डरती हो.....हम महात्मा गाँधी के सहयोगी ज़रूर हैं पर अहिंसक नहीं.....बिना हिंसा के आज़ादी कैसे मिल सकती है? हिंसा होगी तो लहू भी बहेगा, एक-न-एक दिन हमारा भी बहेगा।\" आज़ादी की चमक उनकी आँखों में मशाल-सी जल उठी। उन्होंने अपनी मालविका को बाहों में दबोच लिया था। रेशमी गद्दे पर वे मोम-सी पिघल गईं। बाबा के क़द्दावर जिस्म में बीर बहूटी-सी गुम हो गईं। यही क़द्दावर जिस्म बाबा के इकलौते बेटे मेरे बाबूजी ने पाया था। बाबा अक़्सर कहते- \"शेरनी एक ही नर शेर जन्मती है।\"
उन्होंने अपने शेर-से पुत्र का नाम समरसिंह रखा था। बाबूजी जितने ऊँचे, तगड़े, अम्मा उतनी ही नाज़ुक, बूटे से क़द की....उजला रंग और भोला-भाला चेहरा। बाह-विवाह था उनका। बाबूजी तब बारह के थे, अम्मा दस साल की। प्रताप भवन में तब भी बाबा का ही हुक्म चलता था। अंग्रेज़ों से चिढ़ के कारण ही उन्होंने अंग्रेज़ी स्कूल में बाबूजी को नहीं पढ़ाया। बनारस में अपने दोस्त को पत्र लिखा- \"समर को भेज रहा हूँ अध्ययन के लिए। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला करवाने और हॉस्टल के लोकल गार्जियन बनने का ज़िम्मा तुम्हारा।\" लौटती डाक से जवाब आया-
\"समर मेरा भी पुत्र है, आप निश्चिंत रहिए।\"
पड़बाबा के नाम से प्रसिद्ध प्रताप भवन अपनी आन, बान, शान के लिए तो प्रसिद्ध था ही, पढ़ाई के लिए भी उसका ख़ासा नाम था। लड़कों की तो छोड़ो, लड़कियों तक की पढ़ाई विधिवत हुई जबकि उस ज़माने में ज़्यादातर छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी.....बहुत हुआ तो साक्षर हो गई जैसे अम्मा। लड़कों को व्यापार में लगा दिया जाता। लेकिन बाबा इन सबसे परे थे। हालाँकि पड़बाबा का सूरत में सूती कपड़ों का कारखाना था पर बाबा ने कभी रूचि नहीं दिखाई। ख़ानदान के तीनों चाचा और उनके लड़कों ने व्यापार सम्हाला और बाबा और बड़े बाबा के हिस्से का रूपया बदस्तूर आता रहा। बाबा तो पूरी तरह आज़ादी के दीवाने हो चुके थे और बड़े बाबा विरक्त।
बाबूजी कई सालों तक बनारस में पढ़ते रहे। लॉ पास किया, संस्कृत के वेदों, उपनिषदों और गीता का अध्ययन किया। गीता के श्लोक उन्हें ज़बानी याद थे। योग सीखा, संगीत, सितारवादन, चित्रकारी यहाँ तक कि मूर्तिकला भी। दादी अम्मा को बाबूजी की ग़ैरमौजूदगी में गृहस्थी के लिए पारंगत करती रहीं। चादरें, तकिए के ग़िलाफ़, परदे, कुशन कव्हर पर एम्ब्रॉइडरी करना सिखाया।
अम्मा ने दादी के पेटीकोट के लिए इतनी बारीक क्रोशिये की लेस बुनी और बाबा के लिए चिकन वर्क का कुरता बनाया कि सब देखते ही रह गए। काँच की रंगीन सलाख़ों और मोतियों से बनाए परदे बेमिसाल थे।
अध्ययन के वे वर्ष आज दिन भी बाबूजी को ज़बानी याद हैं। अक़्सर रात के भोजन के समय बनारस का क़िस्सा छिड़ जाता था। सब धीरे-धीरे उठ जाते थे पर मैं बड़े चाव से सुनती रहती थी। अम्मा भी बैठी रहतीं।
तपोभूमि है बनारस। बाबूजी प्रतिदिन संध्या होते ही दशाश्वमेध घाट चले जाते और चबूतरे पर बैठकर योगासन लगाते। उनके एक साथी ने योगासन में इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि ज़मीन से एक फुट ऊपर पद्मासन की मुद्रा में उठ जाते थे। इलाक़े के अंग्रेज़ यह करिश्मा देखने आए थे। अंग्रेज़ कलेक्टर ने तो स्केल पद्मासन के नीचे घुमाकर देखी थी और ताज्जुब से उसकी आँखें फटी की फटी रह गई थीं। उस ज़माने में पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। छात्रावास के विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह मानते थे।
उनके खाने-पीने, दूध, मेवे का पूरा इंतज़ाम उनकी देखरेख में होता था। बाबूजी ने सभी वेदों का अध्ययन वहीँ रहकर किया। केवल अथर्ववेद के कुछ मंडल के श्लोक वे नहीं समझ पाए थे। लिहाज़ा गुरु तलाशा गया। किसी ने बताया बंगाली टोले में एक पंडित यह सिखा सकते हैं। बाबूजी गए। पीपल के दरख़्तों से घिरा एक खंडहरनुमा घर। मुख्य दरवाज़ों पर टूटे-फूटे-से लकड़ी के किवाड़ लोहे की ज़ंग लगी साँकल.....अंदर भुतहा कमरा.....दीवार में आला और आले में जलता हुआ मिट्टी का दीपक।
पंडितजी की शर्त थी कि अँधेरा होने पर ही वे पढ़ाएँगे। इसके लिए छात्रावास से विशेष अनुमति लेनी पड़ी थी। पंडितजी आसन पर विराजमान हो लगातार तीन महीनों तक बाबूजी को पढ़ाते रहे। जब सभी श्लोक स्पष्ट हो गए तो दूसरे दिन बाबूजी ने गुरुदक्षिणा के नाम पर एक कीमती शॉल ख़रीदा और जब वे उसे देने पंडितजी के घर गए तो वहाँ दूर-दूर तक भुतहा सन्नाटा पसरा था।
जहाँ बैठकर वे पढ़ाते थे वहाँ तमाम कबूतरों की बीट बिखरी थी। आले का दिया तेल के बिना सूखा और जल-जल कर काला हो चुका था। बाहर पीपल के दरख़्तों से होकर जब हवाएँ चलतीं तो पत्तों से भरी डालियाँ साँय-साँय का ख़ौफ़नाक मंजर पेश करतीं। तभी साइकिल पर दूध के डब्बे लटकाए एक दूध वाला वहाँ से गुज़रा। बाबूजी ने उसे रोककर पूछा- भैया, बाबा मिश्रीनाथ दत्त कहीं चले गए क्या? मुझे आज ही उनसे मिलना था, सुबह की गाड़ी से घर लौटना है।
दूध वाले का मुँह खुला का खुला रह गया- \"बाबा मिश्रीनाथ!! अरे भैया.....उनको गुज़रे तो सालों हो गए। अब यहाँ कोई नहीं रहता। कोई इस खंडहर को ख़रीदता भी नहीं.....सुना है इधर भूतों का साया है।\"
\"भूतों का? तो क्या वे बाबा मिश्रीनाथ के भूत से पढ़ते रहे? तीन मास तक?\"
और बाबूजी बेहोश हो गए थे।
होश आया तो वे अस्पताल में थे। सामने छात्रावास के विद्यार्थी, गुरु और बाबा..... बाबा ख़बर मिलते ही बनारस आ गए थे। बाबूजी को डिस्चार्ज कराके बाबा तुलसी घाट ले गए जहाँ
संवत् सोलह सौ असी, असी गंग के तीर
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर।
जहाँ चरण पादुका और स्मारक चिह्न बने हैं वहाँ बैठकर बड़ी देर तक बाबा बाबूजी से बातें करते रहे। बाबूजी के दिमाग़ में बस एक बात थी.....बाबा मिश्रीनाथ क्या भूत बन गए, ब्रह्मराक्षस बन गए। हाँ, जिस विद्वान की विद्या की पिपासा अधूरी रह जाती है वह मरकर ब्रह्मराक्षस ही होता है ऐसा दादी बताती हैं.....वे सिहर गए थे, उन्हें बंगाली टोले का वह पीपल का हरहराता दरख़्त याद आया जिसके साए में वह खंडहरनुमा मकान था।
सामने गंगा की लहरों पर एक बजरा तैर रहा था। डूबते सूरज की सुनहली किरणें गंगा को पारदर्शी बना रही थीं.....तट के उस पार रेतीला विस्तार और उस पर चलते इक्का-दुक्का लोगों के काले साए.....अचानक बजरा किनारे पर आकर रुका। बाबा तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर बजरे पर चढ़ गए। बाबूजी को भी चढ़ने का इशारा किया। तब तक अँधेरा हो चला था। दूर हरिश्चंद्र घाट पर चिताओं की लपटें स्पष्ट हो चली थीं। उनके बैठते ही बजरा चल पड़ा। अचानक बाबूजी दंग रह गए। बजरे पर तीसरा व्यक्ति सफ़ेद दाढ़ी, मूँछ और जटाओं में अपनी स्पष्ट पहचान बता रहा था- \"गुरूजी आप?\"
\"चकमा खा गए न? इसीलिए यह वेश रखा है।\" बाबा मिश्रीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा।
बाबूजी ने उनका चरणस्पर्श किया।
\"तुमने इसे कुछ बताया नहीं अभय?\"
\"नहीं मिश्री.....लेकिन अब समय आ गया है। सुनो समर.....मिश्री और मैं क्रांतिकारी दल के सदस्य हैं। अंतर यह है कि मिश्री अंग्रेज़ों का दुश्मन बन गया है। इसने कमिश्नर की अदालत में बम फोड़ा था। कम-से-कम दस अंग्रेज़ों का सफ़ाया हो गया तभी से ये वेश बदलकर घूमता है। सबने मान लिया है कि बम विस्फोट में यह भी मारा गया। तुम सोच रहे होगे समर कि मैं क्रांतिकारी दल का हूँ फिर अपने घर अंग्रेज़ क्यों आते हैं? इसलिए कि मैं उनका दोस्त बनकर उनके राज़ पता कर रहा हूँ.....\"
बाबूजी अवाक़ सुनते रहे.....जाने क्या सोचकर बोले- \"मैं भी क्रांतिदल में शामिल होना चाहता हूँ।\"
बाबा और मिश्रीनाथ एक साथ चौंके। बाबा मिश्रीनाथ ने बाबूजी का हाथ पकड़ लिया- \"नहीं समर, फिर प्रताप भवन की देखभाल कौन करेगा। तुम इकलौते बेटे हो अभय के। अपने ताऊ और ताई की हालत देख ही रहे हो। तुम्हारे सभी चाचाओं ने व्यापार सम्हाला है, प्रताप भवन तुम्हें सम्हालना है। हम लोगों का कोई भरोसा नहीं.....कब मौत आ जाए।\"
अचानक बाबूजी रो पड़े थे.....बजरा गंगा की लहरों पर डोलता रहा। अँधेरा खूब गाढ़ा होने पर बजरा दशाश्वमेध घाट पर आकर रुका। रास्ते में चलते हुए एक सुनसान जगह पर बाबा मिश्रीनाथ ने विदा ली और झाड़ियों में खो गए।
सुबहे बनारस। धीरे-धीरे अंगड़ाई लेती हुई, फूल की पंखुड़ी-सी खिलती वाराणसी जहाँ वरणा और गंगा का मिलन होता है और जहाँ के पंचगंगा घाट में यमुना, सरस्वती, किरणा और धूपताया नदियाँ गुप्त रूप से मिलती हैं।
अंग्रेज़ ऑफिसर्स ढूँढ-ढूँढ कर हार गए थे कि चारों नदियों की जलधारा आख़िर आती कहाँ से हैं परंतु जिस तरह यहाँ के संस्कृत विद्यालयों से निकले हज़ारों स्नातक एकता, बंधुत्व और \'वसुधैव कुटुम्बकम्\' की ज्योति पूरे विश्व में फैला रहे हैं उसी तरह ये नदियाँ वसुधैव कुटुम्बकम् की कल-कल जलधारा को अलग कैसे दरशा सकती हैं। अलग नहीं है भारत। मुस्लिम शासकों की अकर्मण्यता और विलासिता के कारण भले ही अंग्रेज़ों ने चालाकी से अपने पैर जमा लिये हैं यहाँ, पर कितने दिन? बाबा का मालवगढ़, मिश्रीनाथ का बनारस अब जाग उठा है। क्रांति की बारूद तैयार है, चिनगारी भर की देर है।
मंदिर की मूर्ति के पिछवाड़े चौकोर पत्थर सरकाकर पाताल में उतरती सीढ़ियों की अंधी खोह में बाबूजी बाबा के साथ गए थे। तड़के सुबह.....जब सुबहे बनारस की निर्मल ताज़गी फोटो के निगेटिव की तरह धुंधली थी और जब मणिकर्णिका कुंड से लगी गंगा तट तक जाती सीढ़ियों की लंबी कतार निपट सुनसान थी.....पाताल में पैर जमे तो अंधी खोह में दीया टिमटिमाया.....धीरे-धीरे तलघर स्पष्ट होने लगा। हथियार, बम, हथगोले, बारूद, नक़्शे.....मानो रणभूमि हो बाबा मिश्रीनाथ दीये की लौ तेज़ कर रहे थे। इस बार वे मारवाड़ी वेशभूषा में थे। गादी पर बैठने वाले सेठ की तरह।
\"इंतज़ाम पूरा है.....आज तुम मलावगढ़ लौट रहे हो अभय। तारीखें वही रहेंगी.....\"
उन्होंने बाबूजी को आँखें फाड़-फाड़कर सारा मंजर देखते पा अपने नज़दीक बुलाया, ज़मीन पर बैठने का संकेत किया।
\"आज तुमसे भी अंतिम मिलन है समर.....तुम्हारी पढ़ाई भी समाप्त हो चुकी है और तुम मालवगढ़ लौट रहे हो अपने पिता का कारोबार सम्हालने। लेकिन क्रांतिकारी नहीं बनना है तुम्हें.....वचन दो।\"
उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बाबूजी झिझके, बाबा की ओर देखा.....वहाँ अनेक ज्वालाएँ एक-दूसरे में समाहित हो दावानल बन रही थीं।
\"वचन दो समर।\"
बाबा मिश्रीनाथ ने पुनः कहा और बाबा की ओर संशय से देखा.....कुछ पल सन्नाटा रहा, अब की बाबा ने सख़्ती से पूछा- \"क्या सोच रहे हो समर?\" बाबूजी ने वेग से उठती रुलाई को अंदर ही अंदर ज़ब्त कर बाबा की गोद में अपना शीश नवा दिया- \"वचन देता हूँ मैं.....मेरा रणक्षेत्र घर होगा.....कर्त्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ होंगी।\"
दोनों ने बारी-बारी से बाबूजी को गले लगाया। बाबा मिश्रीनाथ ने झोले में से जलेबियों का दोना निकाला- \"हमारे भविष्य की कामयाबी की कामना सहित।\"
तीनों ने एक-एक जलेबी दोने में से उठाई। जलेबियाँ हलकी-हलकी गरम थीं।
\"इतनी सुबह जलेबियाँ कहाँ मिल गईं तुम्हें?\"
\"लल्लू ने रात तीन बजे बनाकर दीं। लालूराम क्रांतिकारी।\"
\"अब उसकी दुकान कौन सम्हालेगा? कल से तो तुम्हारे दल अपनी मुहिम पर रवाना हो रहा है।\"
\"उसका बेटा छेदीराम। अभय, लालू ने दूध भी औंटाया है और कचौरियाँ भी बनाई हैं ख़ास तुम दोनों के लिए। वहीँ बैठकर नाश्ता करेंगे।\"
तीनों अंधी खोह से मंदिर की ओर निकलती गुप्त सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए। चौकोर पत्थर के पास पुजारी खड़ा था और बाबूजी ने आश्चर्य से देखा कि उसने प्रणाम करने की जगह सेल्यूट मारा और वंदेमातरम् कहा।
लालूराम ने अपने हाथों बाबा, बाबूजी और मिश्रीनाथ के लिए जलेबियों, कचौरियों से प्लेट सजाकर दी। दोने में चटनी....मिट्टी के कुल्हड़ में औंटाया हुआ मलाई डला दूध। बाबूजी न उस सुबह को आज तक भूले हैं, न नाश्ते और दूध के स्वाद को और न लालूराम, पुजारी और बाबा मिश्रीनाथ को।
उषा बुआ ने प्रथम श्रेणी में इंटर पास किया और जब बी.ए.का फॉर्म भरना चाहा तो बड़ी दादी का ब्लड प्रैशर बढ़ गया। बिस्तर पर पड़े-पड़े वे बड़े बाबा पर चीखने लगीं जो गलियारे में तख़त पर ध्यानमग्न बैठे थे- \"अरे, साधू-संन्यासी होने से गिरस्ती नहीं चलती। छोरी बूढ़ी हो जाएगी तब चेतोगे?\"
बड़े बाबा का ध्यान तब भी नहीं टूटा तो बड़ी दादी ज़ोर-ज़ोर से हाँफने लगीं, हाथ-पैर पटकने लगीं, सारा शरीर ठंडे पसीने से नहा उठा। मारिया ने दौड़कर उन्हें सम्हाला..... इंजेक्शन दिया। दादी भी उनके पायताने बैठकर उनके तलुए सहलाती हुई ढाँढस देने लगीं- \"जीजी, चिंता से बीमारी और बढ़ेगी.....उषा की शादी इस साल ज़रूर हो जाएगी।\"
और दादी का कहा सच हो गया। जोधपुर में रियासती घराने में उनकी शादी तय हो गई। उनके ख़ानदान को महाराजाओं के समय सोने का कड़ा मिला था और जिस ख़ानदान को सोने का कड़ा मिल जाता उसके ठाठ का तो कहना ही क्या। ख़ानदानी महिलाएँ पैरों में सोने के बिछुए, पायल पहन सकती हैं.....उषा बुआ भी पहनेंगी। मेरे मन में सवाल उठा था कि हम लोग क्यों नहीं पैर में सोना पहन सकते पर यह उसी तरह तर्क देकर टाला गया था जिस तरह मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश। मेरे कुछ सवाल मेरे ज़ेहन में आज तक टँगे के टँगे हैं जो हवा में हिलती तोरन की तरह कभी-कभी मेरे अंदर खलबली मचा देते हैं। किंतु जवाब नहीं मिलता जैसे यह सवाल कि कोठी को हर आफ़त-मुसीबत के लिए दादी ही क्यों पहल करतीं, मन्नतें माँगतीं, और कोई क्यों नहीं?
दादी ने उषा बुआ की शादी के लिए यज्ञ कराने का संकल्प लिया था। उषा बुआ की सगाई की रस्म होते ही उन्होंने यज्ञ की घोषणा कर दी थी। शादी का मुहूर्त सवा महीने बाद का था तब तक यज्ञ निपट जाएगा। दादी का तर्क था कि शादी निपट जाने दो लेकिन दादी की मन्नत शादी पक्की होने की ही थी। लिहाज़ा कोठी में यज्ञ और शादी दोनों की तैयारियाँ शुरू हो गईं। पंडितजी बुलाए गए।
दादी ने चाँदी मढ़ी चौकी पर उन्हें बिठलाकर विधि विधान पूछे। पंडितजी ने भी यही कहा कि शादी निपट जाए, उसके पाँचवे दिन यज्ञ कराइए। कोई भी संकल्प कार्य संपन्न हुए बिना कैसे पूरा माना जाए? दादी नतमस्तक थीं, तर्क नहीं किया।
\"पंडितजी, क्या-क्या तैयारी करनी होगी बता दें। शादी तेईस तारीख़ की है, अट्ठाईस को पूर्णमासी के दिन यज्ञ करा लेते हैं।\"
महाराजिन पंडितजी के लिए चाँदी की तश्तरी में सूखे मेवे, काजू और पिश्ते की बर्फ़ी और चाँदी के गिलास में केशर मसाले वाला दूध रख गईं। पंडितजी ने बिना किसी तक़ल्लुफ़ के फ़ौरन ही नाश्ता करना शुरू कर दिया। दूध पीकर डकार ली और अँगोछे से मुँह पोंछते हुए बोले- \"सोने के लक्ष्मी-विष्णु बनवा लीजिये। रेशमी कपड़े बनेंगे उनके, गोटा किनारी लगेगी। छत्र बनेगा। चाँदी का पान, नारियल, सुपारी.....पंडितजी के जोड़े से कपड़े बनेंगे। यज्ञ पाँच दिन का होगा। आप पाँचवे दिन सबको भोजन करा सकती हैं।\"
कहकर पंडितजी पोथी पत्रा समेट चल दिए। मैं रजनी बुआ के कान में फुसफुसाई- \"ढोंगी बाबा गए।\"
\"ढोंगी क्यों?\"
\"यज्ञ में अपने कपड़ों की फ़रमाइश जो कर रहे थे।\"
जाड़ों के शुरूआती दिन। कोठी के आगे सड़क के उस पार नीम, कचनार के पेड़ों के साए में ऊँटों का काफ़िला ठहरा हुआ था। कपड़े के टेंट लगे थे.....इक्का-दुक्का। दादी ने घर में दर्ज़ी बैठा लिया था। सुबह निराहार रहकर पवित्र वातावरण में भगवान के कपड़े सिए जाते और दोपहर को शादी के लिए कपड़ों की सिलाई होती। हुक टाँकने, गोटा, किरन टाँकने और तुरपन करने के लिए दर्ज़ी अपनी दो लड़कियों को भी लाता था। दादी तीनों के लिए खाना बनवातीं....शाम को चाय नाश्ता कराकर ही उन्हें भेजतीं। पूरे दस दिन लगे कपड़े सिलाने में।
भगवान के कपड़े क्या शानदार बने थे। पीले रेशम पर चाँदी का गोटा, मोती, लाल पायपिंग। लक्ष्मीजी का दुपट्टा बहुत कीमती था। उसमें सोने के तार से कढ़ाई की गई थी। विष्णुजी की पगड़ी भी बड़ी प्यारी बनी थी। उषा बुआ के ब्लाउज़, पेटीकोट साड़ियों के संग तहकर रख दिए गए। उषा बुआ का लहँगा चोली और ओढ़नी भी बेहद कीमती बने थे। सोने-चाँदी और सच्चे मोतियों से उन पर बेल-बूटे काढ़े गए थे।
उषा बुआ की शादी के निमंत्रण कार्ड का डिज़ाइन मैंने तैयार किया था। रंगों का चुनाव भी असाधारण था और जब निमंत्रण पत्र की इबारत में दर्शनाभिलाषी और विनीत के नामों के बाद बीच की जगह में लाल सुनहरे अक्षरों में मैंने लिखा- \'बुआ के ब्याह में नन्हा वीरेंद्र बाट जोहे\' तो सभी चकित रह गए। बड़ी दादी बोलीं- \"होशियारी की गठरी है इसके दिमाग़ में, चाहे जब खोल लेती है।\"
दादी हँस दी, उन्हें तो दम मारने की फुरसत नहीं थी। राधो बुआ भी आ गई थीं। धीरे-धीरे मेहमान आने शुरू हो गए थे। उनके आने से काम में हाथ बँटाना तो ख़ैर मामूली-सा हुआ अलबत्ता उन्हीं के काम अधिक बढ़ गए। बड़ी दादी छड़ी के सहारे थोड़ा बहुत चल लेती थीं। शादी की तैयारियों में मीन-मेख निकालकर वे पैर दर्द से परेशान हो फिर बिस्तर पर ढह जातीं।
उनके बाल मात्र उँगली बराबर मोटी और लंबी चुटिया में सिमट आए थे। माँग के पास चाँद चमक रही थी। बड़ी दादी की ऐसी दुर्दशा में उनका अपना भी हाथ था। हमेशा आराम, दूसरों की बुराई और चिड़चिड़े स्वभाव के कारण ही बड़े बाबा उनसे विरक्त हो गए थे। नहीं तो बड़े बाबा जैसा सीधा सादा, इंसानियत से ओतप्रोत इंसान मिलना कठिन है।
पूरे मालवगढ़ में ख़बर फैल गई थी कि उषा बुआ की ससुराल रजवाड़ों से ताल्लुक रखती है। पैरों में सोना पहनती है। बारात देखने पूरा नगर उमड़ पड़ा था। क्या शानदार बारात थी उषा बुआ की। घोड़े, ऊँट कारें.....कोसों सड़क बारातियों से घिर गई थी। बाबा का इंतज़ाम भी क्या खूब था। मजाल है कि किसी की शान में गुस्ताख़ी हो जाए। स्वागत सत्कार, फूल माला, इत्र फुलेल से पाट दिया था सबको।
घोड़े से उतरते ही दूल्हे राजा के पैर लाल कालीन में धँसे पड़ रहे थे। कालीन पर फूल लिए स्त्रियाँ खड़ी थीं जो दूल्हे राजा पर फूल बरसा रही थीं। कोठी की भीतरी व्यवस्था अम्मा और दादी के ज़िम्मे। हॉल में ढोलक, मजीरे की धुन पर औरतों के द्वारा गाए गीतों की मधुर स्वर लहरी जादुई समा बाँध रही थी। आज मैंने भी लहँगा, चुनरी पहनी थी। बालों की चोटी गूँथकर उसमें मोगरे की माला पिरोई थी और मोतियों के गहने पहने थे। रजनी बुआ ने कुंदन के गहने पहने थे। संध्या बुआ कुछ उदास-सी दिख रही थी। राधो बुआ ने चुटकी ली- \"क्या बात है संध्या.....शादी का मन हो आया क्या?\"
संध्या बुआ शरमा गईं।
\"कहो तो दूल्हे राजा के छोटे भैया से छेड़ें बात?\"
\"जीजी\" संध्या बुआ ने आँखें तरेरकर राधो बुआ को देखा फिर दोनों खिलखिला पड़ीं। एक साथ कई कलियाँ बाहर बगीचे में खिल गईं। चाँद पूरणमासी का नहीं था फिर भी निरभ्र आकाश में निर्मल कांति बिखेर रहा था। हॉल में ट्रे में चाँदी के वर्क लगी गिलोरियाँ भेजी जा रही थीं। गानेवालियों के लिए चाय प्यालों में। राधो बुआ ने एक गिलोरी उठाकर संध्या बुआ के मुँह में ठूँस दी- \"उदास साली नए जीजाजी की अगवानी कैसे करेगी?\"
\"क्या राधो जीजी आप भी?\"
संध्या बुआ खुश दिखने के प्रयत्न में भी उदासी छिपा नहीं पा रही थीं। रजनी बुआ मुझे ऊपर की मंजिल में झरोखे के पास ले गईं। जहाँ उषा बुआ की सहेलियाँ उन्हें चुपके-चुपके दूल्हे राजा के दर्शन करा रही थीं। उत्तर दिशा का कोना सूना था। वहीँ रजनी बुआ धीमी आवाज़ में बताने लगीं-
\"संध्या जीजी का इश्क़ चल रहा है, उन्हीं के साथ पढ़ता है वह.....अजय नाम है उसका।\"
मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ...आज तक प्रताप भवन में इश्क़ शब्द का पदार्पण नहीं हुआ था। हमें जन्म घुट्टी में यह बात पिला दी जाती थी कि हम लड़कियाँ हैं जो मर्दों के साए के बिना साँस नहीं ले सकतीं। हमारा सबकुछ हमारा शौहर है.....इज्ज़त और सलामती से इस घर से बिदा ले हमें अपने-अपने घर जाना है और अपनी दुनिया बसानी है, जैसे उषा बुआ जा रही हैं। फिर संध्या बुआ ये क्या कर बैठीं? साफ़ दिखाई दे रहा है कि यह सरासर मुसीबतों और पीड़ाओं को न्योता देना था।
नीचे शहनाइयाँ बज रही थीं। उषा बुआ कितनी सुंदर लग रही थीं। दुल्हन के वेश में साक्षात् लक्ष्मी जैसी। सोने, हीरे, मोती से लकदक। सारा प्रताप भवन रोशनी, फूलों की खुशबू, कहकहे और अफ़रा तफ़री में डूबा था। जो जहाँ जिसे मिलता हँसी कहकहे में छेड़ने लगता..... उदास थे तो हम दोनों, हमउम्र, हममिजाज, सखियों जैसे मैं और रजनी बुआ।
हॉल से उठकर गानेवालियाँ शादी के मंडप तक पहुँच गईं- \'लाड़ल सासरिया न जासी, पीहर सूनो सो कर जासी.....म्हारी उषा राज दुलारी.....\'
पीहर सूना.....प्रताप भवन सूना.....कमरे, गलियारे, आँगन, चबूतरा.....उषा बुआ जब तक यहाँ रहीं गंभीरता और ख़ामोशी ही तो ओढ़े रहती थीं फिर उनके जाते ही सब कुछ सूना क्यों रहने लगा? क्यों उनकी पहचल सुनने को कान सजग रहने लगे? जग की यह कैसी रीत है.....इंसान की ग़ैरमौजूदगी ही उसकी मौजूदगी के लिए तड़पती है। उनकी बिदाई की रात कोई नहीं सोया।
दूसरे दिन से मेहमान बिदा होने लगे। केवल यज्ञ में शामिल होने वाले लोग ही बच गए। दादी तो मशीन बन चुकी थीं। उनका थका हुआ सौंदर्य उनके मन की दृढ़ता को स्पष्ट कर रहा था।
मारिया ने यज्ञ का पूरा विधान समझ लिया था और जब पाँच दिन के प्रसाद की योजना बाबा, दादी बना रहे थे तो वह एकदम निश्छलता से उनके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। उसकी हथेली में सौ-सौ के नोट दबे थे-
\"छोटी आंटी, आख़िरी दिन का प्रसाद मेरी ओर से।\"
दादी चौंक पड़ीं- \"लेकिन तुम तो ईसाई धर्म.....\"
उनकी बात अधूरी रह गई। मारिया बीच में ही बोल पड़ी \"तो क्या हुआ.....ईश्वर एक है.....हम सब उसी के बंदे हैं। मैं भी, आप भी। छोटी आंटी आपने संकल्प किया था उषा बुआ की शादी हो गई। अब मैं संकल्प कर रही हूँ जन सेवा के व्रत का.....ईश्वर मेरी मदद करे।\"
दादी इंकार नहीं कर सकीं, रुपए ले लिये जबकि बड़ी दादी सुनकर खीझी थीं- \"तुम तो दुलहिन, जात कुजात कुछ नहीं देखतीं.....वो ईसाई.....उनका और फिरंगियों का धरम एक ही तो है न।\"
दादी चुप रही थीं। उनके मन में कोई संशय न था। ईश्वर की शरण में आने वाला हर इंसान ईश्वरमय है। क्या कोढ़ियों के घाव धोते ईसामसीह देवतुल्य नहीं, क्या वेश्या के हाथ से भिक्षा ग्रहण करते गौतम बुद्ध देवतुल्य नहीं.....क्या अछूत शबरी के जूठे बेर राम ने नहीं चखे थे?
दादी ने मारिया के रुपयों से महाप्रसाद बनवाने का सोच डाला था।
उस रात मारिया ने मुझे बताया था- \"पायल बाई, मैं छोटी आंटी से थॉमस का ज़िक्र कैसे करती लेकिन मेरा संकल्प उसको लेकर है। उसने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे, अब हम दोनों मिलकर ज़िंदगी भर मानव सेवा करना चाहते हैं। मैं एक ऐसा सेवा केंद्र खोलूँगी जो दीन-दुखियों के लिए हो। अपने खेत-खलिहान बेच दूँगी इस सेवा केंद्र के लिए। मेरे बापू उस सेवा केंद्र की देखभाल करेंगे और मैं थॉमस के साथ मिलकर निरीह, असहाय और सताए हुए लोगों की सेवा करूँगी, यही संकल्प है मेरा।\"
शायद मारिया के पवित्र मन की चाहत थी जो अंतिम दिन की आहुतियाँ देखने भीड़ उमड़ी पड़ रही थी। यज्ञ मंडप में यज्ञ कुंड के सामने बाबा, दादी हाथ जोड़े बैठे थे। वातावरण में धूप अगरबत्ती की सुगंध बिखरी हुई थी। यज्ञ कुंड से सुगंधित लपटें उठ रही थीं और नेवैद्य की आहुतियाँ लकड़ी के बड़े चमचे से डाली जा रही थीं। दादी ने मारिया के नाम का महाप्रसाद बड़ी परात में यज्ञ कुंड के पास क्रोशिए से बने थालपोश से ढककर रखवाया था। जब दादी, बाबा ने आहुतियाँ देना समाप्त किया तो पंडितजी ने कहा- \"जो आहुति देना चाहते हैं, यहाँ आ जाएँ।\"
दादी ने मुझसे कहा- \"पायल, मारिया को बुला लाओ।\"
मारिया को खोजना नहीं पड़ा। वह फूलों के खंभे के पास ही थी।
\"आओ मारिया, आहुति दो.....अपना संकल्प दोहराओ।\"
पंडित चौंके- \"मालकिन।\"
दादी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। जब मारिया आहुति दे रही थी तो पंडितजी ने मंत्रों को पढ़ने से इंकार कर दिया.....दादी की आँखों में ज्वाला-सी भभकी और वे ज़ोर-ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगीं। मारिया आहुति देती रही। बाबा दंग रह गए। मालविका का यह रूप उन्होंने कभी देखा न था। मंत्र समाप्त होने पर उसने दादी बाबा के पैर छुए। दादी ने उससे संकल्प के इक्यावन रुपए पंडितजी के आगे रखवाए। रुपयों पर फूल, रोली, चावल.....
\"अगर आपको संकल्प भी नहीं ग्रहण करना है तो बता दीजिए, मारिया इन रुपयों को गरीबों में बाँट देगी।\"
पंडितजी कुछ न कह सके। सिर झुकाकर उन्होंने रुपए उठा लिये और मारिया के माथे पर रोली का टीका लगाकर कलाई में कलावा बाँधकर मंत्र पढ़ दिया।
अक्स हो गया था वह यज्ञ मेरे ज़ेहन में। दादी के शरीर में कोई शापग्रस्त दैवी आत्मा है वरना उन्हें मनुष्य रूप में क्यों जन्म लेना पड़ता। उनका निवास तो देवलोक होना चाहिए था। उसी दिन मैंने निर्णय लिया था हर ग़लत बात पर विरोध करने, आवाज़ उठाने का.....नहीं, ख़ामोशी से अत्याचार सहना भी पाप है.....उतना ही जितना अत्याचार करना।
दादी के मंत्रोच्चारण से बाबा इतने प्रभावित हुए थे कि उन्हें बाइबिल पढ़कर सुनाने लगे। घंटों समझाते रहते। दादी बहुत प्रभावित हुईं बाइबिल सुनकर लेकिन यह बात उनकी समझ में नहीं आई कि बाइबिल में ऐसा क्यों लिखा है कि कोढ़ियों और औरतों पर समान रूप से दया भाव रखो। आख़िर उन दोनों में समानता क्या है? क्या नारी इतनी निरीह, लाचार है.....क्या वह पुरुष समाज के लिए कोढ़ की तरह है? दादी ने मारिया से भी इस बात को लेकर बहस की। मारिया के तर्क उन्हें आश्चर्यचकित अवश्य करते रहे लेकिन संतुष्ट नहीं और जब बाबा ने कुरान की आयतें भी पढ़कर सुनाईं और बताया कि उसमें नारी को खेत और अंगूर का बगीचा कहा गया है तो दादी के मन की दीवार दरक़ गई.....मानो भूकंप आया हो।
नारी खेत है, इस बात को तो वे मानती हैं। पुरुष से बीज ग्रहण कर वक़्त आने पर उसे अंकुरित कर पल्लवों, डालियों में विकसित कर एक समाज रच डालती है। वह जड़ बनकर धरती के सारे रसों को अपने में समोकर इन वृक्षों को सौंपती है। वह ताक़त भी सौंपती है जो उन्हें छाया देने, आश्रय देने, रस देने, संतुष्टि देने और स्वास्थ्य देने के योग्य बनाती हैं। लेकिन यह अंगूर का बगीचा? यह तो विलासिता का प्रतीक है.....नारी को मात्र भोग्या सिद्ध करता हुआ। इस्लाम में ये दो विरोधी बातें एक साथ कैसे.....जहाँ एक ओर वह वसुंधरा बनकर मातृरूपा है वहीँ भोग्या भी.....पुरुष किस नज़रिए से उसे देखे जबकि वह उसी के शरीर में रचा, साँस पाया, रक्त पाया इंसान है?
पुराणों में नारी को उपासना में बाधक बताया है। वह नरक का द्वार है, संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त उसका सामीप्य नरक है..... नारी यदि नरक है तो पुरुष उस नरक की उत्पत्ति.....जो उत्पत्ति का स्रोत है उसे पुरुष कैसे नकार सकता है? उसे कोढ़ियों की श्रेणी में रखकर, अंगूर का बगीचा मानकर, नरक का द्वार कहकर आख़िर वह जताना क्या चाहता है? अपने पुरुषत्व की संतुष्टि के लिए उसने धर्म की आड़ क्यों ली?
क्यों नहीं खुलकर अपनी मानसिक प्रवृत्ति बिना किसी आड़ के सामने रखी? नहीं, इस आड़ में पांडित्य का ढोंग, कठमुल्लापन और केथोलिक नाटकीयता है। अधिक-से-अधिक लोकप्रियता पाने की, अधिक-से-अधिक शासन करने की, अधिक-से-अधिक कल्याणकारी सिद्ध होने की। दादी ने स्पष्ट कह दिया.....नहीं मान्यता देंगी वे इन ढकोसलों को। हाँ, वे मात्र इंसानियत का धर्म मानेंगी, जो धर्म मारिया मानती है।
मारिया न ईसाई है न मुस्लिम न हिंदू। वह एक इंसान है.....जो अंधकार की आँखों पर हथेली रख उज्ज्वलता की किरणों को फैलाएगी और जहाँ उजाला है वहाँ अँधेरा कैसा? अंधकार तो हमेशा सहारा लेकर ही फैलता है। शाखों और पत्तियों का सहारा लेकर ही तो वह धरती तक सूर्य की किरणें आने से रोकता है। वह साया बन जाता है लेकिन रोशनी उसको तब भी घेरे रहती है चारों ओर से.....रोशनी का हौसला बहुत विस्तृत है।
इतना मैं समझ गई थी उस छोटी वयस में ही कि नारी को किसी धर्म, किसी समाज में बराबरी का दर्ज़ा नहीं मिला है। वह निकृष्ट, हेय, भोग्या और सम्पत्ति मानी गई है। उसमें न आत्मा है न क़यामत तक मुर्दा बनकर सोते रहने का हौसला.....क़यामत आने पर केवल पुरुषों के मृत शरीर जीवित होंगे क्योंकि उनमें आत्मा है और मेरी कोमल सोच पर एक छाप पड़ गई विद्रोह की, आंदोलन की.....वह सब कुछ करने की जो पुरुष करता है और जो नारी के लिए अपराध माना जाता है। हाँ, बदलना है, परिवेश बदलना है अपना, भले ही वह इतने बड़े ब्रह्मांड में किया बूँद भर भी प्रयास क्यों न हो।
दादी को बहुत डर लगता है जब वे ईसाई और मुस्लिम धर्म के अनुसार मृत शरीर के दफ़नाए जाने की ख़बर सुनती हैं। एक बार प्रवचन देते हुए दादी के मथुरावासी गुरूजी ने बताया था कि \"समाधि की अवस्था में नाड़ी गुम हो जाती है, धड़कनें बंद हो जाती हैं और आदमी मृतप्राय-सा हो जाता है। महर्षि दधीचि ने समाधि की इसी अवस्था में इंद्र को वज्रास्त्र बनाने के लिए अपनी अस्थियों का दान दिया था।\"
\"समाधि की यह अवस्था कठिन तपस्या से प्राप्त होती होगी गुरूजी?\"
दादी के पूछने पर गुरूजी ने गंभीरता से अपनी शिष्या की ओर देखा। दादी के मुखड़े पर दृढ़ता और तेज फूट पड़ रहा था।
\"तुम विदुषी हो कल्याणी। तुम्हारी तर्क बुद्धि तुम्हारे मन को बेचैन किए रहती है। कल्याणी, तुम भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकती हो, कभी-कभी साधारण मानव की मृत्युपूर्व की अवस्था भी ऐसी ही हो जाती है। वह महामूर्छा में खो जाता है.....उस वक़्त डॉक्टर का आला और वैद्य की उँगलियाँ उसे मृत घोषित कर देती हैं लेकिन होती वह महामूर्छा है। वह चेतन अवस्था में पुनः लौट सकता है यदि उसका शरीर सुरक्षित रखा जाए।\"
गुरूजी के शब्दों ने दादी के अंतस् में उथल-पुथल मचा दी थी। तब क्या दफ़नाया हुआ इंसान पुनः चेतन अवस्था में नहीं लौट सकता? अगर उसे महामूर्छा में दफ़नाया गया हो मृत मानकर?
सिहर उठी थीं दादी। ज़मीन के अंदर दबे उस मृत मान लिये गए मानव की घुट-घुटकर मरने की हालत पर विचार करके। उन्होंने मारिया को अपने पास बिठाकर इस समस्या पर बहस की थी। मारिया भी काफ़ी जानकार और बुद्धिमान थी। उसने दादी के इस तर्क पर अपने अस्पताली अनुभव की मोहर लगा दी थी- \"छोटी आंटी.....अगर सभी मुर्दे जला दिए जाएँगे तो विद्यार्थी डॉक्टरी कैसे पढ़ेंगे? कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर की भीतरी रूप रचना कैसी है?\"
मैं वाह-वाह कर उठी थी- \"वाह मारिया, तुमने तो दादी को लाजवाब कर दिया।\"
मारिया के हाथ कानों को छूने लगे- \"ईश्वर क्षमा करें.....छोटी आंटी की बराबरी कौन कर सकता है? वो तो फ़रिश्ता हैं.....मैं तो ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलने वाली एक औरत भर.....मैंने तो अपनी ऑंखें.....अपना पूरा शरीर दान कर दिया है। मेरी आँखें किसी अंधकार में भटकते व्यक्ति को दृष्टि दें और मेरा शरीर मेडिकल छात्रों के काम आए बस यही चाहत है।\"
दादी अवाक़्- \"तुमने अपनी आँखें, अपना शरीर दान कर दिया?\"
\"हाँ छोटी आंटी, अब हर छह महीने में रक्तदान का नियम भी पालना है मुझे।\"
दादी के आगे पाताल से निकलकर एक अँधेरी सुरंग उजाले में तब्दील होती गई। उस सुरंग की दीवारों पर रंग-बिरंगे फूलों की लताएँ आच्छादित होती गईं। मारिया मानो फूल बन गई जिस पर क्षितिज से शबनमी बूँदों ने टपकना शुरू कर दिया। ओस भरी पंखुड़ियों की शीतलता में सारे संसार की अग्नि धीरे-धीरे शीतल, ठंडी होती गई.....हवा ने उन पंखुड़ियों को बिखरा दिया। अब मारिया चारों ओर फैल गई.....वह फूल बन गई, वह रंग बन गई, वह ओस बन गई, वह उज्ज्वलता बन गई।
अभिभूत दादी बाबा से कह बैठीं- \"मैं भी अपने नेत्र दान करूँगी।\"
बाबा की टकटकी बँध गई.....काफ़ी देर तक ख़ामोशी दोनों के दिलों में चीत्कार बन छाई रही। फिर बाबा का मौन टूटा-
\"पुराणों में लिखा है कि शरीर का कोई भी अंग कट जाने से दूसरे जन्म में वह अंग नहीं मिलता। फिर यह शरीर तुम्हारा नहीं है। यह धरती का है, पंचतत्व से बना.....धरती का शरीर धरती को ही लौटाना होगा साबुत।\"
\"फिर दधीचि का त्याग क्यों आज दिन भी याद किया जाता है?\" दादी का तर्क था।
\"उन्होंने अपनी हड्डियाँ देवताओं और मानव के कल्याण के लिए दान की थीं।\"
\"मैं भी अपनी आँखें मानव के कल्याण के लिए ही दान करूँगी।\"
बाबा निरुत्तर थे।
\"पायल मुझे लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी हैं। चलोगी साथ में?\" संध्या बुआ ने मुझसे पूछा। उषा बुआ की बिदाई के बाद का यह पहला वाक़या था और संध्या बुआ के साथ जाने का पहला मौका भी.....इसके पहले उन्होंने कभी मुझे साथ नहीं लिया था। दादी ने बग्घी तैयार करा दी थी। कोचवान बग्घी लिये इंतज़ार कर रहा था।
हम दोनों बग्घी की गुदगुदी सीट पर बैठे तो लगा दो चिड़ियाँ फुदककर घोंसले से बाहर आई हैं और उड़ने को डैने पसारे हैं। यों घर में किसी बात की सख़्ती नहीं थी पर कभी-कभी क़ायदे भी पाबंदी की तरह नज़र आते थे। संध्या बुआ के हाथ में रंगीन पोत से बना बैग था.....इतना बड़ा कि आठ-दस किताबें आ जाएँ। वे फ़ालसाई रंग की साड़ी में बड़ी प्यारी लग रही थीं। कानों में एक-एक मोती जड़े मोगरे की कली जैसे टॉप्स पहने थीं।
बग्घी चौड़े राजपथ से होकर गुज़री तो दो अंग्रेज़ घोड़ों पर सरपट भागते दिखे। घोड़ों की टाप सुनकर आसपास की हरियाली में से निकलकर कुत्ते भौंकने लगे। बग्घी अब टेढ़ी-मेढ़ी गलियों में उतर आई थी। गलियारों से लगे दो मंजिले मकान.....मकान के सामने आँगन..... आँगन में बड़े-बड़े बोर पहने, स्त्रियाँ बतिया रही थीं।
उनके घाघरे, रंग-बिरंगी चोलियाँ जिसमें से आधी छातियाँ अंदर, आधी बाहर.....पेट, कमर सब खुली। फिर भी सुना है घाघरे में चालीस गज़ कपड़ा लगता है। इतने कपड़े में बस दो टाँगें ढँकी हुई थीं। वे सूप में बाजरा फटक रही थीं, हाथ रुकते ही फूँक मारकर छिलके उड़ा देतीं।
बग्घी रुक गई। सामने लाइब्रेरी थी। संध्या बुआ लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर कमरे में पहुँची जहाँ बड़े-बड़े टेबिल, कुर्सियाँ और अलमारी में किताबें थीं। उन्हें आता देख सामने कुर्सी पर बैठा बेहद आकर्षक नौजवान खिल पड़ा- \"आओ संध्या.....तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था मैं।\" संध्या बुआ उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे भी बैठने का इशारा किया।
\"बहुत देर से बैठे हो अजय?\"
ओह!.....तो यह हैं अजय। संध्या बुआ की नींद, चैन हराम करने वाले महाशय।
\"अजय ये पायल है.....समर भैया की बेटी।\"
मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए।
\"आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है हमने संध्या से।\"
\"मेरी तारीफ़!\" मैं सकपका गई।
\"क्यों नहीं? जब आप पढ़ाई में इतनी होशियार हैं, जब आपमें तर्क-बुद्धि है, जब आप फोटोग्राफी और चित्रकारी में पारंगत हैं, कविताएँ भी लिखती हैं तो तारीफ़ नहीं होगी।\"
मुझे अजय की आवाज़ में सम्मोहन नज़र आया।
\"एक कला तो तुम भूल ही गए अजय, पायल ने कपड़ों पर बातिक करना भी सीखा है। मोम लगाकर इतने लाजवाब डिज़ाइन बनाती है ये कि पूछो मत।\"
अजय ने कुछ इस ढंग से मेरी ओर देखा कि मैं शरमा गई। वहाँ से उठकर मैं अखबारों-पत्रिकाओं के स्टैंड की तरफ चली गई। संध्या बुआ को अजय के साथ अकेला छोड़ने का मक़सद भी था इसमें। वे दोनों लगातार बातें करते रहे....संध्या बुआ ने अपने बैग में से एक नोटबुक निकालकर अजय को दी, बदले में अजय ने भी एक नोटबुक संध्या बुआ को दी जो उन्होंने जल्दी से अपने बैग में रख ली।
यह नोटबुक मेरी जिज्ञासा का केंद्र बन गई। लौटते वक़्त संध्या बुआ के चेहरे पर रौनक़ थी। उदासी मानो कोसों दूर बिला गई थी। मुझे अजय पसंद आए।
संध्या बुआ का कमरा मेरे और रजनी बुआ के कमरे से लगा हुआ था। बाहर बगीचे की तरफ खिड़कियाँ खुलती थीं जिसके रोशनदान में सतरंगी काँच लगी थी। लेकिन बड़ी दादी का हुक्म था, खिड़कियाँ हमेशा बंद रहेंगी और उन पर भारी परदे पड़े रहेंगे लेकिन आज संध्या बुआ ने खिड़कियाँ खोल दीं। ताज़ी हवा का एक महकता हुआ झोंका कमरे को बावला कर गया। चादर, परदे, गुलदान के फूल झुमने लगे। ये शायद उनका अपने भविष्य के लिए हलाल नहीं होंगी।
आसमान में बादलों की थिगलियाँ उस क्रांति का संकेत दे रही थीं जो बनारस में हो रही थी। कुछ इस तरह कि हम भले ही थिगलियाँ बनकर आएँ पर बरसेंगे तुम पर गर्जन-तर्जन से। बाबा तेज़ी से हर गतिविधि पर नज़र रखे थे। देव बाबा की मड़िया अब खाने के पैकेट नहीं भेजे जाते.....अब उन जंगलों से क्रांति वीरों का दल पूरी सजधज से लैस अपने मुहानों पर चल पड़ा था। घर में अंग्रेजों का आना इन दिनों कम था और बाबा का अधिकतर समय अपनी स्टडी में बीतता था।
संध्या बुआ इस बार रजनी बुआ को लेकर लाइब्रेरी गई थीं और मेरे हाथ वो सुनहरा मौका था जब मैं उनकी नोटबुक पढ़ सकती थी। मैं सधे क़दमों उनके कमरे में पहुँची और उनकी कोर्स की किताबों के बीच नोटबुक पा मैं खुशी से खिल पड़ी। अपने कमरे में आकर मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। नोटबुक खुलते ही अजय की शख़्सियत, उनके विचार, उनकी भावनाएँ मुझसे रूबरू होने लगीं। वह नोटबुक नहीं बल्कि डायरी थी, जिसमें तारीख़वार मन के तहखाने खोले गए थे। पहले पन्ने पर चार अक्टूबर की तारीख़ पड़ी थी। मैं तेज़ी से पढ़ने लगी।
४ अक्टूबर
आज सुबह से दिल उदास है, यह एहसास तेज़ी से मुझे घेरता जा रहा है कि मैं आसानी से संध्या को नहीं पा सकता। वह की निशानी है और मैं अपने अजय में बुज़दिली तो नहीं ही पा सकती। मैं ज़िंदगी के हर क़दम पर तुम्हारे साथ हूँ।\"
उसके इस हौसले ने मेरे मन में संघर्षों की साँकल खोल दी है। काँटे और कंकरों से भरे मार्ग पर मेरे क़दम अपने आप बढ़ने लगे हैं.....मैं अपने मन के संकल्प को पिघलने न दूँगा। हाँ संध्या, ये वादा है मेरा.....मैं इस साल अधिकतम अंक से पास होकर किसी कॉलेज में एप्लाई कर दूँगा और फिर पी-एच.डी. करूँगा। लेकिन संध्या, क्या हम शादी के बाद यहाँ रह पाएँगे?
६ अक्टूबर
कल मेरा जन्मदिन था.....माँ कहती है कि जब मैं पैदा हुआ था तब पिताजी इंग्लैंड में वक़ालत की पढ़ाई कर रहे थे। मैं ननिहाल में अपनी नानी के घर पैदा हुआ था और पिताजी ने अपने किसी अंग्रेज़ मित्र के हाथ मेरे लिए सौगातें भेजी थीं। मेरे जन्म के बाद पूरे साल भर माँ बीमार रहीं जब तक पिताजी लौट नहीं आए। यही वजह है कि मैं माँ को बेतहाशा प्यार करता हूँ, उनकी सेवा करने के लिए मेरे हाथ मचलने लगते हैं। हम पाँच भाई-बहनों में माँ का स्नेह सबसे छोटी बहन पर अधिक दिखाई देता है। यह मेरा भ्रम भी हो सकता है क्योंकि माँ ने कभी ज़ाहिर नहीं किया ये सब! उन्होंने सुबह से मेरे जन्मदिन की तैयारी कर रखी थी। वे मुझे मंदिर लेकर गई थीं, मेरे माथे पर तिलक लगाया था और मुझे खीर अपने हाथों से बनाकर खिलाई थी।
शाम को गाने बजाने का भी कार्यक्रम था। लेकिन मैं संध्या से मिलने के लिए उतावला हो रहा था। क्यों नहीं ऐसा होता कि हम रोज़ मिलते और अपनी आपबीती एक-दूसरे को सुनाते। हफ़्ते में दो दिन मिलना मिलने जैसा नहीं लगता। फिर भी मैं इंतज़ार करता हूँ इन दिनों का। मैंने आग के समंदर में अपने को झोंक दिया है लेकिन ख़त्म होने के लिए नहीं बल्कि उस आग से एक मशाल जलानी है जो परम्पराओं, मान्यताओं और सड़े-गले रिवाज़ों के अंधकार भरे मार्ग को रोशन कर सके। यह मशाल मेरी शख़्सियत का प्रतीक चिन्ह बन जाए। हाँ.....मुझे मशाल बनना है.....मुझे साँसों के चलते उन पलों को सार्थक करना है जो ज़िंदगी ने मुझे बख़्शे हैं.....एक निराला संसार.....गुलाम भारत.....कोड़े बरसाते अंग्रेज़ और कोड़े सहता किसान, मज़दूर.....उसका कसूर गरीब होना, उसका कसूर मेहनती होना, उसका कसूर लगान न दे पाना।
मुझे अंग्रेजों के कोड़े इतने नहीं टीसते जितने ज़मीनदारों के.....जो इस मिट्टी की संतानें हैं और जो अपनों को ही लहूलुहान किए हैं। संध्या भी ज़मींदार घराने की है लेकिन यह घराना अन्य घरानों से बहुत हद तक भिन्न है। यह घराना और इस घराने की ज़मींदारिन मालविका, संध्या की चाची दया का भंडार है। मालवगढ़ की रियाया मालविका के एहसानों को कभी भूलती नहीं बल्कि चर्चा छिड़ी रहती है। कुएँ, बावली बनवाना, शादी ब्याह में रुपए, अनाज, कपड़ों की मदद अस्पतालों में दान देना..... ग़रीब विद्यार्थियों की मदद.....इन सबके आगे मालविका का ख़ज़ाना खुला रहता है। एक ऐसा सदाव्रत जो घटने का नाम ही नहीं लेता। संध्या, तुम्हें ऐसा ही होना है.....क़ाश तुम उनकी पुत्री होतीं तो यह सब तुम्हारे खून में रचा-बसा होता।
९ अक्टूबर
मेरी आँखों में बुलंद इरादों की रोशनी है। हाथों में, पैरों में जुम्बिश आगे बढ़ते चले जाने की। मेरी अनामिका में संध्या के जन्मदिन पर भेंट की गई मोती जड़ी सोने की अँगूठी है। सुना है मोती जुदा कराता है.....तन से, या फिर विचारों से.....किसे जुदा कराएगा ये? मुझे और संध्या को? नामुमकिन.....शायद इसीलिए संध्या ने इस अंधविश्वास को चुनौती दी है। संध्या की आँखों में भोर की किरनें हैं, नर्म, कोमल.....मैं इन किरनों को दोपहर के सूरज में बदलकर अपने संसार के लिए धूप भरा आकाश जुटा लूँगा।
धूप में ऊर्जा है, सृजन है, धूप बन जाने देना और भाप को जलधाराओं में परिवर्तित करना धूप ही का काम है.....पत्ते-पत्ते को हरियाली, शाख़ों को फूल, खेतों की फसल.....सब कुछ धूप ही के वश की बात है.....धूप के बिना पर सूरज चाहे जितना तपे, इंसान सह जाता है। बहुत संभव है मेरी यह धूप भरी ज़िद मेरे प्रयासों के वृक्ष को झुलसा दे या ऐसी आँधी आए कि वह वृक्ष जड़ से समूचा उखड़ जाए पर उखड़ी जड़ें फिर भी तलाश करती रहेंगी धरती की कोख में अपने लिए एक हरी-भरी शिरा। संध्या, तुमने एक बार कहा था कि \'तुम मेरे लिए सारे जहाँ से लड़ सकती हो।\'
तो उठो संध्या.....यह जो रफ़्ता-रफ़्ता पिछले ढाई वर्षों से हम एक-दूसरे में रच बस गए हैं, इसी रचने-बसने की माँग है कि अब हमें उठ जाना चाहिए.....मंज़िल सम्मुख आन खड़ी है।.....मात्र एक क़दम, एक प्रयत्न, एक हौसला.....और सब कुछ हमारा। मैंने माँ से बात कर ली है। उन्हें बस डर है तो तुम्हारे चाचा का.....वे मानेंगे? उनकी स्वीकृति ही तो प्रताप भवन की स्वीकृति होगी। माँ कहती हैं मैं आग से न खेलूँ.....जानबूझकर मुसीबतों को आमंत्रण न दूँ, लेकिन आख़िर क्यों हम एक-दूसरे के नहीं हो सकते? कम-से-कम हममें इंसानियत तो है, जज़्बा तो है, कोशिश तो है.....क्या पद, शोहरत यही है इंसानियत की पहचान? और क्या सब हम स्वर्ग हासिल नहीं कर सकते? क्या पीढ़ियों का अतीत हमारे फैसले करेगा?
११ अक्टूबर
सुबह की गुलाबी ठंडक.....दिशाओं को भ्रमित करता आलोक, अँगड़ाई लेती भोर की किरण.....बबूल के फूलों की गंध आ रही है? लखनऊ में दर्शनशास्त्र पढ़ाते हुए सर (डॉ. मलिक) कहते थे कि किसी को इतना प्यार मत करो कि तुम्हारे सारे उद्देश्य फीके पड़ जाएँ कि और कुछ सोचने को रहे ही न! जीवन निस्सार, अर्थहीन, उदासी और ग़मों का ज़खीरा बन जाए लेकिन क्या अपने वश में है? ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, धूप छाँव जैसे बिना इल्म के, बिना कोशिश के सहना ही पड़ता है.....वैसा ही प्यार है। प्यार कर्म नहीं है जो प्रयास से किया जाए.....प्यार एक सोता है जो धरती की कोख़ से अनायास फूट पड़ता है।
उस पर अपना कोई वश नहीं। सारे संबंध, सख्य, आत्मीयता, भावनाओं का आलोड़न.....सभी में समाया है तो प्यार.....इस प्यार में ही बेबस हो जलधाराएँ किनारों की चट्टान पर उगी हरी, काली शैवाल को छूने के प्रयास में सिर पटकती रहती हैं.....लेकिन इससे भी बड़ा चुंबकीय खिंचाव उस सागर का है जिसकी ओर ये जलधाराएँ उमड़ी पड़ती हैं। गुफाएँ, जंगल, काँटे, झाड़ियाँ.....पथरीली ऊँची-नीची भूमि को पार करती सागर की विशाल छाती में समा जाती हैं.....समा जाने में ही सुख है.....सुख है इसीलिए चाह है।
संध्या, तुम्हारा उज्ज्वल मोहक चेहरा, चेहरे पर पंखुड़ी-से दो अधर.....मैं उस रस को नहीं भूल पाता.....निपट एकांत में मेरे हाथों की अंजलि में सिमटा तुम्हारा कमलमुख.....तुम्हारे होठों की हरारत से दहकते मेरे होंठ.....लरज गई थीं तुम- \"अजय, मैं मर जाऊँगी अजय, अब नहीं जिया जाता।\"
और तुम जलधारा-सी मेरे सीने में समाती चली गई थीं.....मुझे याद है दो दिन बाद उषा का तिलक जाने वाला था। मिलनी और गीत संध्या के दृश्य तुम्हारे नयनों में साकार हो रहे थे। तुम उदास थीं.....शायद इस शंका से कि अब उषा के बाद तुम्हारा नंबर है, कभी भी शादी का प्रस्ताव आ सकता है।
तुम्हारे पिता यूँ तो साधु स्वभाव के हैं पर हैं ज्वालामुखी। तुम्हारी इंकारी कहीं ज्वालामुखी को भड़का न दे और कहीं पिघलता लावा सब कुछ ले न डूबे। पंखुड़ी-पंखुड़ी बिखरा देता है। तुम झुकना नहीं- संध्या। ज़िंदगी की प्रत्येक साँस, प्रत्येक लम्हे में मैं तुम्हारे साथ हूँ।
आहट हुई। पन्ना ने दरवाज़े पर दस्तक दी- \"पायल बिटिया, मालकिन पूछ रही हैं तुम्हें।\"
मैंने फुर्ती से नोटबुक बंद कर संध्या बुआ के कमरे में ठीक उसी जगह रख दी जहाँ से निकाली थी। लेकिन मन बेचैन था। नोटबुक पूरी नहीं पढ़ पाई। फिर भी स्थितियाँ स्पष्ट थीं। संध्या बुआ और अजय पिछले ढाई वर्षों से इश्क़ की आग में जल रहे हैं। बड़ी विकट परिस्थिति थी। क्या होगा, सोचकर कलेजा काँप जाता था। संध्या बुआ मोम-सी पिघल रही हैं। उजाले में परछाइयाँ काँप रही हैं.....एक बड़े अंधकार के दायरे की रेखाएँ खिंचनी शुरू हो गई हैं। हवा हर दरीचे से अंदर घुसती चली आ रही है।
मारिया का संकल्प पूरा हो रहा है। सेवा केंद्र के लिए जगह की मंजूरी मिल गई है। मारिया ने ऐसी जगह चुनी है, जहाँ नयनाभिराम हरियाली है.....हरियाली में गुँथी बावलियाँ.....इधर-उधर चरते मवेशी। जगह खूब रौनकदार है। सामने ही पक्की सड़क है जो बाईं ओर मुड़कर राजपथ तक जाती है। लेकिन आसपास एक भी अस्पताल नहीं है। बीमार आदमी को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं।
उसे कंबल पर लिटाकर, कंबल के कोने मोटी लकड़ियों में फँसाकर दो आदमी उन लकड़ियों को कंधे पर रखकर अस्पताल ले जाते हैं। कंबल में झूलता आदमी वैसे ही अधमरा हो जाता है। मारिया ने यह सब देखा है, इसीलिए यह जगह उसे पसंद आई है। दादी की इच्छा है भूमिपूजन हो। मारिया को मानना पड़ता है। मुहूर्त परसों का है। कल थॉमस आ जाएगा। मारिया के बापू नहीं आ पाएँगे। अभी रोग की शिथिलता है।
दादी ने सेवा केंद्र के लिए एक लाख रुपयों का दान दिया है मारिया को। मारिया तो हतप्रभ रह गई। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका स्वप्न इतनी जल्दी फलित हो जाएगा।
\"छोटी आंटी, आप तो मेरे लिए देवदूत बन गईं।\"
उसने गद्गद हो दादी से कहा तो दादी अपनी निर्भीक सहज मुस्कान से उसे भिगोती मीठी झिड़की देने लगीं- \"बस-बस, मेरी शान में कशीदे मत काढ़ो। थे तो दिए, नहीं होते तो कहाँ से देती?\"
\"नहीं.....दिल है तो दिया, दिल नहीं तो आदमी कंजूस का कंजूस। छोटी आंटी, कल थॉमस आ जाएगा। अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक रहा है वह। आंटी, भूमि पूजन की तैयारी कैसे होगी, आप बता देना।\"
\"तुम चिंता मत करो मारिया, कंचन ने सारा इंतज़ाम कर लिया है।\" कहती दादी पलंग पर लेट गईं, मारिया उनके पैर दबाने लगी। दादी की आँखें धीरे-धीरे मूँदने लगीं.....दस नौकरों के होते हुए भी दादी के बिना किसी का काम नहीं चलता था। घर के प्रत्येक काम की शुरुआत, हर समस्या, हर मुसीबत केवल दादी के सामने बखानी जाती। कुछ इस विश्वास से कि वे हैं तो किसी का काम रुक ही नहीं सकता। मैं तो दादी के नख से शिख तक मोहित थी। उनकी सुंदरता, सादगी, स्वभाव का मीठापन, मृदुलता, बेहद सलीक़ा और साफ़गोई..... विचारों में तर्क और सोच की गहराई.....वे सचमुच विलक्षण प्रतिभा संपन्न थीं। दया और कल्याण की साक्षात् प्रतिमा।
भूमि पूजन के दिन थॉमस घर आया। ऊँचा, साँवला, पतली मूँछों का आकर्षक युवक। मारिया ने सबसे परिचय कराया। उसकी आँखों में मारिया के लिए जुनून भरा प्यार नज़र आया। सब तैयार थे। प्रताप भवन से चार बग्घियाँ और एक जीप रवाना हुई। जीप में पूजा का सामान, पंडितजी, कोदू और बंसीलाल थे। ड्राइवर के बाजू में बाबा और बाबूजी। महाराज ने पूरी सेंककर टोकरों में भर दी थीं, आलू की भुजिया, मिठाई के डिब्बे, थर्मस में चाय, बाबा का पानदान और पानी का जग। मारिया तो खुशी से खिली पड़ रही थी। यों लग रहा था जैसे सब जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हों। घर में बस बड़ी दादी थीं जसोदा के साथ। उनका तो चलना-फिरना ही मुश्किल था।
पंडितजी ने ज़मीन पर आसनी बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए भूमि पूजन किया। ये हमारे कुल के पंडितजी ही थे लेकिन इनके मन का कलुष यज्ञ वाले दिन धुल गया था। मारिया की जाति को लेकर इनके मन में अब कोई संशय न था। शगुन का कलावा उन्होंने मारिया और थॉमस दोनों को बाँधा। मारिया की ज़िद्द थी कि नींव के लिए पहली कुदाल दादी चलाएँ। दादी बाबा के सामने हिचक रही थीं लेकिन फिर उनकी आँखों से रज़ामंदी का संकेत पा दादी ने कुदाल चलाई। वह निर्जन भूमि प्रभु के समवेत नामोच्चारण से गुंजित हो चली। दूसरी कुदाल बाबा ने बड़े बाबा से चलवाई। फिर एक के बाद एक घर के सभी सदस्यों ने कुदाल चलाई। नारियल फोड़े गए और प्रसाद ग्रहण कर सब हरी भरी घास पर बिछाई गई दरियों पर बैठकर नाश्ता करने लगे। पंडितजी को अलग से परोसा गया। मारिया की आँखों में आंसू थे।
\"क्या बात है मारिया? बापू की याद आ रही है?\"
दादी के पूछने पर मारिया आँखें पोंछती हुई हँस पड़ी।
\"नहीं छोटी आंटी.....बापू का प्रतिरूप तो छोटे साहब हैं, मुझे तो अपने भाग्य पर यक़ीन नहीं हो रहा।\"
\"सच, आंटीजी.....सोचा भर था कि सेवा केंद्र खोलेंगे लेकिन इतनी जल्दी यह सपना सच होगा, ताज्जुब है! सब आपकी बदौलत.....\" थॉमस ने कहा।
बाबा ने थॉमस और मारिया को बधाई दी- \"तुम दोनों की लगन कारगर हुई.....जल्दी ही बिल्डिंग भी बन जाएगी।\"
थॉमस हफ़्ते भर रहा। मारिया लगातार उसके साथ रही लेकिन बड़ी दादी के प्रति अपने कर्त्तव्य को भी नहीं भूली। दवाई, इंजेक्शन, स्पंज, चादर, तकिए का गिलाफ़ बदलना, कंघी, चोटी..... सब नियमपूर्वक किया उसने। केवल खाने-नाश्ते का ज़िम्मा जसोदा ने ले लिया था। मारिया ने खाने नाश्ते के समय का चार्ट बनाकर जसोदा को समझा दिया था। घर के सभी सदस्यों के मन में मारिया को लेकर कोमल भावनाएँ थीं।
धीरे-धीरे थॉमस के बारे में भी सबको पता चल गया था अतः दोनों को घूमने में किसी को आपत्ति न थी। अलबत्ता बड़ी दादी अपनी आदतवश चीख़ती चिल्लाती रहतीं। जिस दिन थॉमस को जाना था, उनके अँगूठे की नस घुटने तक खिंची जा रही थी और वे दर्द से तड़प रही थीं। मारिया मालिश करती रही। सुकून मिला तो नींद आ गई। थॉमस की गाड़ी का समय हो गया था। उसे स्टेशन छोड़ने चली गई। इधर नींद खुलने पर मारिया को न पा उन्होंने घर सिर पर उठा लिया-
\"वो तो चाहती है मैं मरूँ तो टंटा ख़तम हो। अरे, उसे छोड़ने बंसीमल जा सकता था.....इसी को जाने की क्या ज़रुरत पड़ गई। अरी जसोदा, अँगूठे की नस तो पकड़.....मर जाऊँगी मैं तो दरद से।\"
बड़ी दादी की झुँझलाहट घर के हर प्राणी पर उतरा करती। उन्हें अगर कोई अच्छा लगता था तो भैया। भैया का नामकरण भी उन्होंने किया था- \"कुँवर वीरेंद्र सिंह। वीरों में इंद्र है मेरा पोता।\"
बड़ी दादी को बेटे की चाह थी। पर हुईं बेटियाँ ही बेटियाँ.....सो सारा लाड़ भैया पर..... भैया उनके कमरे में कुछ भी करने के लिए आज़ाद था। वह कालीन पर अपने खिलोने बिखेर सकता था। जूते पहने हुए उनके पलंग पर चढ़ सकता था। वह उनके सिरहाने बैठकर अपनी उँगली से उनके चेहरे पर काल्पनिक सिंगार करता..... कमेंट्री सहित.....ये लगाया बड़ी दादी को काजल, ये बिंदी.....नाक ऊपर करो दादी.....ये पहना दी नाथ.....और ये भर दी माँग।
\"तू मेरी माँग भरेगा, मेरा राज दुलारा। ज़रूर पिछले जन्म में मेरा प्रेमी है तू।\" बड़ी दादी लाड़ में भरकर उसे चूम लेतीं।
\"मैं प्रेमी नहीं.....कुँवर वीरेंद्र समरसिंह हूँ।\" कहता हुआ भैया बाहर दौड़ जाता। जसोदा और पन्ना हँसते-हँसते पेट पकड़ लेतीं।
भक्तिन थी जसोदा। हर सोमवार व्रत, हर एकादशी व्रत.....दिन भर निर्जला रहती, सूरज ढले ही व्रत का पारायण करती और व्रत का पारायण भी कैसा.....उबले आलू, दूध और केले.....अम्मा मावे की मिठाई मँगवाती। वह भगवान को चढ़ाती और चुटकी भर प्रसाद ग्रहण करती।
आज उसका एकादशी का व्रत था.....आज मारिया को भी रक्तदान के लिए जाना था। दादी ने सबेरे ही कंचन से कह दिया था कि निशास्ता बना ले। बादाम की गिरी और घी थोड़ा ज़्यादा डाले। मारिया को खून देने के बाद कमज़ोरी आएगी उसी के लिए टॉनिक था यह। पिछली दफ़े ओट बनाया था कंचन ने पर मारिया को पसंद नहीं आया था। थोड़ा-सा लेकर बाकी वापस लौटा दिया- \"हीक़ मारता है.....रहने दो न कंचन.....अभी खाना खाऊँगी तो सब ठीक हो जाएगा।\"
\"तुम जानो.....छोटी मालकिन गुस्सा हों तो हमें बीच में मत डालना। वे तो कहती हैं मारिया तप कर रही है। अपने शरीर का खून देना कोई मामूली बात नही है, तप है तप।\"
मारिया मन-ही-मन मुस्कुराई। अगर यह तप है तो वह इस तप को सलाम करती है। वह तो इतना जानती है कि परमात्मा का दिया यह शरीर मानव मात्र के कल्याण के लिए है, हर मानव में ईश्वर का वास है। उसके थॉमस में भी ईश्वर का वास है, बल्कि वह तो पूर्ण ईर स्वरुप है।
उसके हृदय में प्रेम ही प्रेम है। उसका दिल करता है वह चिड़िया की तरह उड़े और आसमान से धरती के ज़र्रे-ज़र्रे को देखे और जहाँ दुःख दिखाई दे वहाँ अपने पंखों की छाँव देती उतर जाए.....मारिया तलाशेगी, दुःख तलाशेगी औरों के और उन्हें अपने सेवा केंद्र की शीतल गोद में आश्रय देगी। यही व्रत है उसका और थॉमस का।
मारिया तैयार होकर निकली तो संध्या बुआ की बग्घी भी तैयार पाई। वह भी हाथ में किताबें लिये कमरे से निकल रही थीं- \"अस्पताल जाना है न! चलो छोड़े देते हैं।\"
संध्या बुआ और मारिया को लेकर बग्घी सड़क पर दौड़ने लगी। कतारबद्ध आम, जामुन के पेड़, नीम की हरी भरी शाखाएँ उस दौड़ से सहमकर पल भर डोलकर स्थिर हो गईं। नीम की डाल पर अपनी लंबी पूँछ लटकाए मोर ने आम के पेड़ तक की उड़ान भरी। उसके खुले सतरंगी पंखों का रंग माहौल में होली के रंगों-सा बिखर गया। संध्या बुआ निश्चय ही अजय से मिलने गई हैं और वो उनकी नोटबुक.....सधे क़दमों का शगल.....संध्या बुआ के कमरे में रैक पर सजी किताबों के बीच वह नोटबुक नहीं थी पर इस बार संध्या बुआ के हाथ से लिखी एक दूसरी मोरपिंच कलर की नोटबुक थी।
अंदर के पृष्ठों में एक मुलायम चितकबरा पंख रखा था.....उस पंख के निशान तक लिखा गया था। फिर वही धड़कते दिल और काँपते हाथों से हुआ कारनामा.....दरवाज़े की चिटकनी आहिस्ता से चढ़ाना और पलंग पर बैठकर जल्दी-जल्दी पढ़ना.....ओह, यह सब मेरी आदत क्यों बनता जा रहा था? क्यों जानना चाहती थी मैं संध्या बुआ और अजय के संबंधों को.....यह कैसी चाहत थी मेरी? पत्तों में छुपी दर्ज़ी चिड़िया जैसी जो जिस डाल पर बैठी होती उसी की पत्तियों की तिनकों से सिलाई कर अपने लिए घोंसला बना लेती.....उसे पता नहीं होता कि पत्तियाँ सूखकर पीली पड़ जाएँगी, डंठल कमज़ोर हो जाएगा और एक दिन उस पेड़ की नंगा झोली लेती पतझड़ी हवा उसे भी उड़ा ले जाएगी। संध्या बुआ ने लिखा है.....
तुम मेरे हो अजय और मैं वो नदी जो अनंत काल से सिर्फ़ तुम्हारे लिए बह रही है। मेरी निर्मल जलधारा ने तलहटी में पड़े हर गोल पत्थर को शिव बना दिया है। शिव ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। बेहद चरित्रवान, मात्र पार्वती को चाहने वाले। जब कामदेव ने अपने बाणों से उन्हें घायल किया तो पार्वती का सर्वांग प्रेममय बना दिया उन्होंने। इतना प्रेम! इतना अद्भुत प्रेम कि पार्वती शिवमय हो उठीं।
इस प्रेम में वे तीनों लोक भूल गए.....सुबह, शाम, रात.....बस प्रेम, प्रेम का अखंड विशाल तत्त्व इस ब्रह्मांड में समा सकता है भला? छोटा है यह संसार प्रेम के लिए। मैंने कालिदास का कुमारसंभव पढ़ा है। ओह.....पार्वती के समर्पण और शिव के द्वारा उस समर्पण को स्वीकार करना.....अद्भुत वर्णन है.....जब पार्वती के लिए कण-कण शिवमय था और शिव के लिए कण-कण पार्वतीमय। अजय, चाची की नौकरानी है जसोदा.....कहती है, प्रेम करने वाला पति चाहिए तो शिव की उपासना करो। मेरी माँ कहती हैं.....शिव-सा पति किस काम का? जटा-जूट धारी, श्मशान की राख मले शरीर पर.....नाग लिपटे.....मेरे बाबूजी ऐसे ही हो गए हैं।
साधु। साधुओं की संगत उन्हें भाती है.....वे घर में रहकर भी घर से पृथक् हैं.....उन्हें आसपास का कुछ औरता नहीं, कुछ सालता नहीं। मुझे डर लगता है अजय, तुम्हारे साथ अपने संबंधों को लेकर, संबंधों पर अपने बाबूजी की प्रतिक्रिया को लेकर। कल क्या होगा? क्या होगा जब घर में मेरी शादी की चर्चा चलेगी। उषा जीजी के बाद अब शादी का मुद्दा मेरी ओर मुड़ने ही वाला है। मैं आशंका से भयभीत हूँ। सब कुछ धुँधला-सा हो जाता है और आँखों के फोक़स में तुम्हीं नज़र आते हो, मेरे इतने क़रीब.....तुम्हारी साँसों की छुअन और मेरे शरीर में भड़कता लावा.....अजय, इस कगार तक निरापद तुम हो और बीच में टूटी किर्चों, काँटों और मुरम का चुभता फैलाव।
क्या यह प्रेम की परीक्षा है? हाँ.....मैं चल सकती हूँ इस दुर्गम मार्ग पर। क्या होगा? लहूलुहान होंगे न पैर। छाले और घावों से पट जाएँगे न तलवे! तो स्वीकार है मुझे, यह मार्ग स्वीकार है परंतु तुम्हारे बिना जीवन का एक लम्हा भी स्वीकार नहीं। तुम्हारी उदासीनता तो ज़रा भी नहीं स्वीकार है। जानते हो अजय, जो उदासीन होते हैं उन्हें चाहने वाले बिल्कुल टूट जाते हैं, जैसे मेरी माँ टूटी हैं.....वर्षों से पलंग की चौखट में एक तस्वीर की तरह जड़ चुकी हैं वे। वे अच्छा होना नहीं चाहतीं और जो अच्छा होना नहीं चाहता.....दवाइयाँ क्या असर करेंगी उस पर?
उनके अंदर की मरती जीवन आकांक्षा की वजह हैं मेरे बाबूजी। मेरे बाबूजी ने क्यों की शादी जबकि उनके अंदर गृहस्थ धर्म निभाने की इच्छा न थी। वे देह रहते हुए भी विदेह रहे.....न जाने कैसे हम तीनों बहनों ने जन्म लिया। वे माँ की इच्छाओं की पूर्ति न कर सके। मुझे याद है अजय। बता देने में कैसी शर्म? सच तो बेपर्दा होता है हमेशा। माँ का बुखार उतरा था.....मारिया ने उनके बाल धोए थे और उनका हाथ पकड़कर उन्हें घुमाने बगीचे तक ले गई थी। वहाँ आरामकुर्सी में उन्हें बैठाकर मुझे जताकर वह अस्पताल चली गई थी उनके लिए दवा और इंजेक्शन लाने।
पढ़ाई की धुन में मैं भूल ही गई कि उन्हें बगीचे से बिस्तर तक पहुँचाना है। रात की पदचाप को सुन.....अँधेरे में टिमकते जुगनुओं को देखती जब मैं तो देखा माँ कुर्सी से उठकर बाबूजी के तख़त पर बैठी उनके सीने पर झुकी जा रही हैं। प्रतिक्रिया में बाबूजी की निश्चलता ने उनमें उत्तेजना भर दी.....शायद अभिसार के अपमान की उत्तेजना.....वे ये भूल गईं कि वे बीमारी से ज़रा-सा ठीक हुई हैं.....रात का अँधेरा है, प्रताप भवन में रात्रिकालीन सरगर्मियाँ हैं। इधर-उधर घूमते नौकर, चाकर, दास-दासियाँ हैं। चाचा के अंग्रेज़ दोस्तों के आने का वक्त है और नौकरों को भी अपने-अपने काम पूरे करने की जल्दी पड़ी है।
हालाँकि बाबूजी के तख़त के पास, कमरे, बरामदे और बरामदे से लगी बोगनबेलिया की झाड़ी में अक्सर सन्नाटा रहता था। माँ ने बाबूजी के कुरते में नाखून गड़ा दिए.....कुरता जगह-जगह से फटने लगा। माँ ने उनके होंठ कचकचाकर काट डाले। बालों को मुट्ठियों में भर लिया। बाबूजी डर गए \'क्या हो गया है तुम्हें.....छोड़ो मुझे।\'
सहसा माँ फुँफकारती हँसी हँसी- \"डायन बन गई हूँ, ज़िंदा गाड़ दिया है न तुमने मुझे, इसीलिए डायन बन गई हूँ।\" और वे बाबूजी की धोती भी खोलने की कोशिश करने लगीं। अब सब कुछ बरदाश्त से परे था। ज़मींदार घराने की बड़ी बहू और ऐसा बर्ताव! उन्होंने माँ को ज़ोरदार धक्का दिया.....सँभलते-सँभलते माँ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उनके माथे पर खरोंचे डाल दीं.....वे एक हाथ से उनका सिर पकड़े थीं और दूसरे हाथ से नाखूनों से उनके माथे पर जाने क्या कर रही थीं। कुछ क्षणों के लिए बाबूजी भी अवाक़् हो गए। फिर बाँहों से पकड़कर उन्हें घसीटते हुए पलंग तक लाए, पटककर बाहर से साँकल चढ़ा ली.....मैं अपनी जगह खड़ी थरथर काँपने लगी, रुलाई मेरे अंदर समा नहीं रही थी। कुमारसंभव पढ़कर माँ के आवाहन और बाबूजी की उदासीनता ने मुझे आलोड़ित कर दिया था। प्रेम वीतराग बन गया था। झाड़ियों में उलझी अपनी ओढ़नी धीरे से छुड़ाकर मैं अपने कमरे में लौट आई। जब तक मारिया लौटी.....माँ को तेज़ बुखार चढ़ गया था और बाबूजी साधु की कुटिया की ओर पैदल निकल गए थे। उनके माथे पर माँ के नाखूनों का घाव झिलमिला रहा था।
अजय, समझ में नहीं आता कि उन दोनों के संबंधों में अलगाव क्यों है? कभी मैं दोनों को एक-दूसरे का दोषी पाती हूँ, कभी केवल माँ को जिनके ज़िद्दी स्वभाव और अहंकार ने बाबूजी को विरक्त कर दिया, कभी बाबूजी को, उनकी विरक्ति ने माँ को ज़िद्दी बना दिया, बीमार बना दिया, हम बहनों के जन्म होते गए और माँ छीजती रहीं.....हर बार पहले से कहीं ज़्यादा। हर बार बेटा न होने की वजह से वे प्रताड़ित होती रहीं मेरी दादी से, कुनबे की बुजुर्ग महिलाओं से। पुरुष उतना हस्तक्षेप नहीं कते जितनी चिल्लपों महिलाएँ करतीं। कुल मिलाकर सभी बातों ने हमें तटस्थ कर दिया.....ख़ाकर मुझे.....मैंने अपने आपको सीप में बंद मोती-सा समेट लिया।
यह हवेली मुझे संतप्त किए रहती है, बस सुख मिलता है तो तुमसे मिलकर। कई-कई दिन गुज़र जाते हैं मैं माँ के कमरे में नहीं जाती, बाबूजी से सामना नहीं होता। सुबह से शाम तक चहल-पहल में डूबी यह हवेली मुझे हर लम्हा वीरान लगती है। जानती हूँ तुम्हें पाना बड़ा दूभर प्रयास है पर अब एकमात्र वही उद्देश्य रह गया है मेरा.....तुम न मिले अजय तो मैं सांभर झील में जाऊँगी। नमक के पानी में गल-गलकर मर जाऊँगी.....जैसे जोंक पिघलती है.....नमक पड़ने से। अजय तुमने कहा था.....हम मिलकर ईश्वर के बनाए भाग्य को चुनौती दे सकते हैं।
चुनौती मार्ग खोलती है, मंजिल क़रीब आती है लेकिन मैं मार्ग में पड़े उन पैरों के निशानों का क्या करूँ जो लौट-लौटकर मुझे मेरे अतीत तक ले जाते हैं.....वहाँ तो चुनौती नहीं, वहाँ तो मंज़िल नहीं.....एक गोधूलि बेला है जहाँ न रात समझ में आती है न सवेरा। जहाँ बने उसूलों, नियमों को अपने जीवन की जीत समझ कुँवारा मन अपने पंजे आगे बढ़ा देता है उसे पाने को.....जैसे उषा जीजी ने पा लिया। लेकिन मायके की पहली ही विदाई में इस जीत की हकीकत खुलने लगी। जीजा सा मातृभक्त हैं। माता की आज्ञा के बिना वे हिलते नहीं। उषा जीजी केवल पूरक हैं.....विवाह बंधन की पूरक। उन्होंने मुझे बताया कि-
\"संध्या.....पहली ही बार में अपना कठपुतली होना तय पा लिया मैंने.....यहाँ तक कि आधी रात के समय जब सासूजी सो जाती हैं तभी वे कमरे में प्रवेश करते हैं और आते ही पूछते हैं- \"तुम जाग रही हो अब तक?\"
सर्वांग कुढ़ जाता है संध्या.....क्या मैं अपने मायके के लिए बोझ थी जो इस कैदखाने में लाकर पटक दिया मुझे। ससुराल के राजसी ठाठ मुझे आख़िर क्यों रोमांचित करेंगे जबकि मेरा जन्म ही एक समृद्ध आलीशान घराने में हुआ है। मुझे सालता है तो उनका अपने से अलगाव.....वे या तो व्यापार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं या सासूजी के साथ। उनके जीवन में मैं कहाँ हूँ?
कहते-कहते उषा जीजी का गला भर आया था। लेकिन प्रवाह रुका नहीं-बड़ी ननद ने बहुत ज़ोर दिया कि नई दुल्हन को घुमा लाओ.....पर उधर भी ये ज़िद्द करने लगे कि माताजी चलें तो कार्यक्रम बनाएँ। उन्हें कलकत्ता घूमना है, दक्षिणेश्वर घूमना है। ननद बिफ़र पड़ी थीं- \'कब तक माताजी के पल्लू से बँधे रहोगे.....अरे, अब तुम शादीशुदा हो, अपना जीवन खुद जियो और माताजी आप भी इन्हें पल्लू में समेटे रहती हैं.....थोड़ी आज़ाद भी छोड़िये।\'
\'लो, हम क्या पकड़े बैठे हैं। जहाँ मर्ज़ी हो जाएँ। घूम आएँ न कलकत्ता। हमारा क्या है सबर कर लेंगे।\'
उषा जीजी की बातें चौंकाने वाली थीं। फिर भी मैंने समझाया-\'जीजी, तुम ही हौसला रखो। धीरे-धीरे परिस्थितियाँ अपनी ओर मोड़ो। समय लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा।\'
\'क़ाश, संध्या ऐसा ही हो।\'
और वे पैरों में पहनी सोने की पाजेब गोल-गोल घुमाने लगीं, इन पाजेबों को देखकर कितनी ज़िद्द की थी पायल ने चाची से- \"अम्मा, तुम क्यों नहीं पहनतीं ऐसी पाजेब?\" उसके तर्क का चाची क्या जवाब देतीं? उषा जीजी इन्हीं पाज़ेबों के सम्मोहन में ही तो बिदा की गई थीं जिन्हें अब वे बेड़ियाँ मानने लगी थीं। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए उषा जीजी को.....
इसके बाद के पृष्ठ कोरे थे और वहीँ चितकबरा पंख रखा था। मैंने आहिस्ता-से नोटबुक बंद की, उसे यथावत् रखा और कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ गई। दादी और अम्मा सोफ़े पर बैठी क्रोशिया बुन रही थीं और पन्ना आरती की बत्तियाँ बना रही थी, रुई की फूलबत्तियाँ। तभी मारिया लौट आई। खून देने से उसका चेहरा कुम्हला गया था। कंचन उसके लिए बनाए ख़ास भोजन को थाली में परोसने लगी।
\"जसोदा, तुम भी खा लो, फिर सूरज अस्त हो जाएगा।\" दादी ने दिन भर एकादशी का व्रत रखे जसोदा से कहा।
व्रत तो दादी और अम्मा ने भी रखा था पर उनका फलाहार का समय दूसरा था..... शाम की आरती के बाद दादी बाबा और बाबूजी के खाने के बाद ही अम्मा के साथ जीमती थीं। सदा का नियम था उनका। वे एक अन्न खाती थीं। जसोदा अन्न को एकादशी के दिन हाथ भी नहीं लगाती थी। महराजिन ने जसोदा के लिए घी में भुने आलू और खूब गाढ़ा औटाया हुआ दूध तैयार किया था।
\"दूध में काजू किशमिश भी डाल दो.....जसोदा तो जान देने पर तुली है। मरेगी तो पाप हमारे सिर आयेगा।\"
अम्मा ने महाराजिन से कहा तो जसोदा हँस पड़ी- \"नहीं मरूँगी हुकुम.....आपकी ड्योढ़ी में जीवन मिलता है, मरूँगी क्यों?\"
\"चल-चल.....अब खा ले जाकर.....बहुत कसीदे काढ़ लिये तूने।\"
अम्मा की मीठी झिड़की सुन जसोदा भी मारिया के पास बैठकर खाने लगी। अंतर इतना भर था कि मारिया ने खाने के टेबिल पर थाली रखी थी और जसोदा ने आसनी पर बैठकर पीढ़े पर थाली रखी थी। पीढ़े के आसपास आचमन किए जल का घेरा था, मानो एक लक्ष्मण रेखा.....कि पारायण करते समय कोई उसे छुए न!
रात मारिया मेरे कमरे में आई। रजनी बुआ सो चुकी थीं और मैं बातिक की डिज़ाइन बुक से चादर में बातिक करने के लिए नमूना ढूँढ रही थी। इस बार मैं केवल काले और भूरे रंग का ही बातिक करूँगी। यह चादर अम्मा की शादी की सालगिरह तक बन जाना चाहिए, पूरा एक महीना है अभी।
\"पायल बाई.....आज सोने का इरादा नहीं है क्या?\" मारिया ने पलंग पर बैठते हुए कहा।
\"नींद तो तुम्हें भी नहीं आ रही मारिया।\"
\"कैसे आएगी नींद? दिल में धीरज नहीं कि इंतज़ार करूँ सेवा केंद्र बनने का। रोज़ जा-जाकर देखती हूँ.....अभी तो नींव भरी है।\"
मैं मारिया के चेहरे की चमक देख विस्मित हो गई। वहाँ केवल प्रेम की अलौकिक चमक के और कुछ न था। प्रेम से ही दया उपजती है, करूणा उपजती है। प्रेम शाश्वत है। धरती के कण-कण में समाया है। प्रेम न हो तो पतंगा शमा पर क्यों मंडराए जबकि जल जाना उसकी नियति है। जलती तो शमा भी है अपनी ही जगह पिघल-पिघलकर, लेकिन उसकी लौ को चूमने को आतुर पतंगे का प्रेम अलौकिक है.....\"
\"सेवा केंद्र बन जाएगा तो मैं और थॉमस साथ-साथ रहेंगे। देखो न पायल बाई..... कितना अपना लगता है अब थॉमस। उसके त्याग ने मेरे दिल को मथ डाला है। हम दोनों एक-दूसरे को बहुत प्यार करने लगे हैं.....अपने भाग्य से, विचारों से, कार्यों की समानता से हम एक हैं। प्रेम की भावना अब जो मेरे सामने उभरकर आई है.....उसका कोई दूसरा रूप हो ही नहीं सकता, हम दोनों ने बड़ी कठिन राह चुनी है.....अंधकार में कूदने जैसी.....बल्कि कूद ही पड़े हैं अंधकार में। न सुख पाने की चाह है, न घर बसाने की, न मौज करने की.....बस साथ-साथ संघर्ष करना है, अंधकार से जूझना है.....लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अगर मिट भी गए तो यह हमारा साझा समझौता है।\"
मारिया की आँखों में विश्वास की पौ फट रही थी। मैंने इस विदुषी महिला के आगे अपना माथा झुका लिया। एक विलक्षण तेज से युक्त.....त्याग और बलिदान की मूर्ति मारिया के चरणों को छू लेने की उद्दाम लालसा मैं कैसे रोक पाई,मैं ही जानती हूँ। एक ओर अपनी खुशियाँ बटोरती संध्या बुआ हैं.....प्यार वे भी करती हैं.....लेकिन उस प्यार में निजत्व है, व्यक्तिगत सुख की चाह है.....जबकि मारिया का प्यार पूरे समाज को लेकर है। एक विशाल मिशन.....सारे विश्व को एक कुटुम्ब मानकर कर्त्तव्य पालन की चाह.....धन्य हो देवी तुम!
मैंने बातिक के लिए चादर पर मोम लगाना शुरू कर दी। अप्रैल का महीना था.....हवाओं में चैत्र मास का तेवर था। होली के बाद से यूँ भी हवाएँ तेज़ चलने लगती हैं.....वन, कंदरा, घास के मैदान सभी को ये हवाएँ पागल कर देती हैं.....रेतीले मैदानों में ऊँचे-नीचे रेत के पठारों पर उँगली की पोर बराबर छेद हो जाते हैं और उनमें से हवाओं की बाँसुरी दूर-दूर तक अपनी तान छेड़ देती है।
पन्ना ने रात खूब बड़े पानी के बर्तन में गुलाब की पंखुड़ियाँ भिगोकर गुलाब जल तैयार किया था जो लगभग प्रतिदिन का शगल था पहले। लेकिन उषा बुआ की शादी के बाद हफ्ते में दो-तीन दिन ही गुलाब जल तैयार होता। हाँ, उबटन लगाने की परंपरा रोज़ ही निभाई जाती। पन्ना ज़िद्द कर रही थी- \"पायल बिटिया, उबटन लगवा लो.....फिर डिज़ाइन बनाना।\"
\"तू पहले बुआओं को लगा आ.....तब तक मेरा डिज़ाइन भी पूरा हो जाएगा।\"
मैंने चादर पर झुके-झुके पन्ना की ओर देखे बिना कहा- \"ज़रा-सी देर में तो मोम पपड़ा जाती है। अभी ही करना ज़रूरी है, नहीं तो दुबारा मोम पिघलाने की ज़हमत उठानी पड़ेगी।\"
\"नहा लीं वो दोनों तो.....संध्या बाई सा को कॉलेज जो जाना है.....अगले महीने से इम्तहान शुरू हो रहे हैं।\"
और पन्ना मेरे पाँवों में उबटन चुपड़ने लगी। फिर बाईं बाँह अपने घुटने पर टिकाकर उबटन लगाने लगी। उसकी कलाई की चूड़ियाँ एक लय में खनक रही थीं। पन्ना को मुझे उबटन लगाने, नहाते समय मेरी पीठ मलने, मेरी कंघी-चोटी करने में बहुत आनंद आता था। इस दौरान वह ज़माने भर की बातें मुझे बताती। पूरी कोठी की ख़बर रखती थी वो.....दिन भर डोलती रहती। हाथ में कच्ची कैरी और नमक की पुड़िया लिये कोठी का ज़र्रा-ज़र्रा खँगालती रहती।
\"नया फानूस लगा है बड़े हॉल में.....गलीचे, सोफ़े सब बदल दिए गए हैं। देखा नहीं तुमने पायल बिटिया इतना सुंदर शीशम का फर्नीचर आया है.....कल दिन भर बंसीमल और कोदू उसी में जुटे रहे.....रखने, सजाने में। आज शाम मेहमान आने वाले हैं उदैपुर से।\"
\"रुकेंगे क्या यहाँ?\"
\"इधर नहीं.....उधर डाक बंगले में रुकेंगे.....उधर भी खूब सजावट चल रही है। तुम तो अपने कमरे में बंद रहकर पढ़ती रहती हो दिन भर.....कोई खोज-ख़बर ही नहीं रखतीं।\"
\"अच्छा, अब मैं नहाऊँगी.....गुसलखाना तैयार है न।\"
मुझे पता था कि इस बातूनी के रहते मेरा कुछ काम नहीं हो पाएगा। यूँ भी मेरी परीक्षाएँ निपट चुकी थीं और फुरसत के दिन थे। अम्मा के लिए बतौर उपहार चादर भी तैयार कर लेनी थी।
पन्ना ने घंटा भर मुझे तैयार करने में लगाया। गुलाब जल से स्नान, कंघी, चोटी, तेल फुलेल.....छोटी-सी थी जब.....अम्मा बाबूजी की इकलौती लाड़ली बिटिया तो दाइयों का हुजूम साथ लगा रहता था। कोई मालिश करती, कोई नहलाती, कोई बाल सँवारती लेकिन नाश्ता, खाना मैं अम्मा के हाथ से ही करती। फिर वीरेंद्र के जन्म के बाद काफ़ी सारे काम मैं खुद करने लगी थी। हमेशा से मेरे पहनने के कपड़ों का चुनाव पन्ना ही करती थी।
संध्या बुआ बग्घी में बैठकर कॉलेज चली गई थीं और जसोदा भी जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज फिर उसका व्रत था और उसे राधा कृष्ण के मंदिर पूजा करने जाना था।
\"जसोदा तू सुबह ही मंदिर हो आया कर, फिर धूप चढ़ जाती है। इधर भी काम का समय हो जाता है.....आज तो ज़्यादा ही काम है। शाम चार बजे ही मेहमान आ जाएँगे।\"
अम्मा ने ताक़ीद की तो जसोदा ने पूजा की थाली में फूल रखते हुए तसल्ली दी- \"बस हुकुम, गई और आई।\"
लेकिन जसोदा का मंदिर से लौटना विस्फोटक था। आते ही वह तीर की तरह अम्मा के कमरे में चली आई। मैं अम्मा के पास ही बैठी थी। अम्मा के चेहरे पर थकावट के चिन्ह झलक आए थे। तीन-चार घंटों से जुटी थीं वे दादी के साथ तैयारी में। बाद में पता चला कि मेहमान उषा बुआ की ससुराल से आने वाले हैं.....फूफा सा के कोई दूर के मामा, मामी और उनके दो लड़के.....इसीलिए स्वागत का विशेष इंतज़ाम है। नौकरों को तो दम मारने की फुरसत नहीं। अम्मा ने जसोदा को कमरे में आते देखा तो पहले शरबत पीने की हिदायत दी-\"ख़श का शरबत पी ले जसोदा। आज तो काम में लगना ही पड़ेगा.....सब जुटे हैं।\"
\"चित्त तो ठिकाने हो।\" जसोदा नीचे फर्श पर बैठ गई।
\"क्यों.....क्या हुआ?\"
जसोदा ने सिर इधर-उधर घुमाकर कमरे का जायजा लिया, फिर थोड़ी देर मेरे चेहरे पर उसकी निगाहें थमीं.....न जाने कौन-सा राज़ बताने वाली है जसोदा, आशंका से मेरी धडकनें बढ़ गईं।
\"हुकुम, काट लो मेरी बोटी-बोटी जो एक शब्द भी झूठ बोलूँ। उपवास का दिन, मेरा तो चित्त ही ठिकाने नहीं आ रहा है। न प्यास सता रही है न भूख।\"
\"क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं?\" अम्मा ने परेशान होकर कहा तो जसोदा ने उनके पैर पकड़ लिये- \"हुकुम, मैं आपकी चेरी.....मेरा अपराध क्षमा.....बड़ी ग़लत बात देखी.....राधा कृष्ण मंदिर के रास्ते पर लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर संध्या बाई सा और एक अनजान लड़का दोनों खड़े थे। संध्या बाई सा का हाथ उनके हाथ में था। दोनों हँस रहे थे, बतिया रहे थे..... मेरा तो खून जम गया हुकुम, दौड़ी चली आ रही हूँ इधर।\"
मैं सन्न रह गई। तो जसोदा ने संध्या बुआ और अजय को साथ-साथ देख लिया। हे भगवान! अब क्या होगा? तभी मुझे पहचल-सी सुनाई दी। लगा, अम्मा के कमरे की बगीचे की ओर खुलती खिड़की के नीचे से कोई अभी-अभी गया है। खिड़की का परदा ज़रा-सा हटाकर मैंने देखा मारिया बड़ी दादी को बगीचे में धीरे-धीरे टहला रही है।
\"अम्मा.....बड़ी दादी।\" मैं आतंक से सिहरकर अम्मा के पास दुबक गई। डर अम्मा पर भी छा गया। उत्तेजना में जसोदा थोड़ा ऊँचा ही बोल रही थी। अगर जसोदा की बात बड़ी दादी ने सुन ली होगी तो? प्रश्न के काँटे मेरे और अम्मा के बीच तेज़ी से उग आए। न जाने ये काँटे किसे कब लहूलुहान कर दें? कब कहर बरस पड़े इस कोठी पर.....शाप.....साँप के रूप में बिल में घुसा ज़िंदा शाप.....केवल इस कोठी की स्त्रियों को मिला शाप, सुख दूर छिटका पड़ा है जिनसे, बस जलना है.....दुखों की भट्टी में सुलगना है.....यही नियति है हमारी। लेकिन मुझे इस नियति से इंकार है। मैं इस भट्टी में से मशाल जलाऊँगी और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चल पडूँगी। अंधकार से भरा मार्ग थोटी ड़ा तो रोशन होगा। मशाल की लपट में परछाइयाँ तो थरथराएँगी.....अपने होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास कराती.....फिर भले ही परछाईं मेरी अपनी हो.....
\"जसोदा, तूने कुछ नहीं देखा। समझी।\"
\"जी, हुकुम.....भूल गई सब। कुएँ में झौंक डाला सब कुछ.....लो, जीभ काट ली जो किसी से कहूँ तो।\"
और जसोदा ने जीभ निकालकर दाँतों के बीच दबा ली।
बड़ी दादी ने तो अपने कानों से ही सब सुन लिया था। उन्होंने फौरन दादी को बुलाया और लगभग घंटे भर तक उनका कमरा बंद रहा। दादी जब कमरे से बाहर निकलीं तो उनके चेहरे पर सफ़ेदी-सी पुती थी। चार बजे उषा बुआ के ससुराल वाले आ गए और हवेली सहमी-सहमी-सी अँगड़ाई लेने लगी। विशाल मेज पर चाँदी के बर्तनों से पकवानों की महक भूख जगाने लगी।
लेकिन भूख न मुझे थी न अम्मा को। दादी अलबत्ता बहुत संयम से समधियाने का स्वागत कर रही थीं। ये फूफा सा के वही मामा थे जिन्होंने द्वार पूजा के समय जब दादी ने दूल्हे का आरता उतारा था तो ठिठोली की थी। अलीगढ़ वाली मामी ने दूल्हे को काजल लगाकर जब शीशा दिखाया तो काजल की एक टिपकी गाल पर लगी देख इन्हीं मामा ने छेड़ा था- \"लो, अपनी नज़र से बचा रही हैं तुम्हें?\"
आज भी वे ठिठोली के ही मूड में थे। दादी ने भी अपने पर ज़ब्त कर रखा था.....न संध्या बुआ को एक शब्द कहा, न बड़ी दादी को कुछ कहने दिया.....न इस आफ़त को दूसरों पर प्रगट होने दिया।
रात ग्यारह-बारह बजे तक हँसी के ठहाके, चहल-पहल, गहमा-गहमी प्रताप भवन में चलती रही। बिदाई के समय दादी ने कपड़े लत्ते, मेवा मिश्री रुपए आदि देने की रस्म निभाकर पहले से तैयार जीप में उन्हें बिदा किया। बाबा गए छोड़ने, बड़े बाबा भी साथ गए और वीरेंद्र का जाना तो लाज़िमी था ही। क़रीब दो बजे जीप लौटी। मैं जाग रही थी और बिस्तर पर करवटें बदल रही थी।
एक भयानक विस्फोट की आशंका से मेरा दिल थर-थर काँप रहा था। परिस्थिति से अनभिज्ञ रजनी बुआ आराम से सो रही थीं। संध्या बुआ के कमरे की भी लाइट बुझी थी। ईश्वर ने मेरा दिल ही ऐसा बनाया है, घर का एक तिनका भी हिलता है तो विचलित मैं होती हूँ जबकि तय कर लिया है कि लीक से हटकर जीना है.....उन बातों को मानना ही नहीं है जिन्हें मानकर इस कोठी की औरतों ने पीड़ाएँ झेली हैं.....उन पीड़ाओं ने एक प्रतिध्वनि मुझमें जगा दी है जिससे मेरे अंतर् के शब्द दिशाओं, दिशाओं के दसों कोणों में गूँजने लगे हैं। मैं लहर बनकर जलधारा में उन्मुक्त बहना चाहती हूँ.....मैं पंख बनकर आसमान में उड़ना चाहती हूँ..... मैं उपेक्षित झाड़ी में फूल बनकर खिलना चाहती हूँ.....दुखों की गगरी में बूँद-बूँद समोए आँसूओं को मोती बना डालना चाहती हूँ। तभी तो बड़ी दादी बिस्तर पर पड़े-पड़े चीखती हैं- \"जिद्दन है छोरी.....औरत के शरीर में हिडिम्बा राक्षसी का अवतार!\"
हाँ, मैं हिडिम्बा हूँ.....भीम जैसे वज्र पुरुषों को झुका देने की ताब है मुझमें। यह बात दीगर है कि अपने लिए चुने वनवास में किसी भीम को कोई जगह नहीं देनी है मुझे।
सुबह संध्या बुआ की बड़ी दादी के दरबार में हाज़िरी हुई-
\"क्यों री, ख़ानदान का नाम डुबोने को कुछ बाकी छोड़ा है तूने?\"
बुआ अवाक्- \"माँऽऽऽ.....क्या हुआ?\"
बड़ी दादी की भट्टी में घी के छींटें पड़ गए- \"अच्छा, तो अब ये भी बताना पड़ेगा कि क्या हुआ! देख छोरी, सीधी तरह बता वो लड़का कौन है, तेरा क्या लगता है जो तू गलबहियाँ डाले उसके साथ खुलेआम घूम रही थी।\"
बुआ के काटो तो खून नहीं.....किसने ये आग लगाईं? किसने उन्हें अजय के साथ देख लिया?
\"अरी कुलबोरन.....आज तक जो इस ख़ानदान में नहीं हुआ वह तू करके दिखाना चाहती है। कुछ ख़याल है अपने बाप दादों की इज्ज़त आबरू का?\"
\"बस भी करो माँ! मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो ख़ानदान की इज्ज़त को बट्टा लगे।\" संध्या बुआ ने दरवाज़े की ओट में इकट्ठा हुई जसोदा, पन्ना, कंचन, महाराजिन को महसूस कर लिया था। बड़ी दादी बोलती हैं तो फिर इन सब बातों का ख़याल कहाँ रखती हैं? ऊँची आवाज़ को काबू करना उनके बस में नहीं।
\"तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना-अपना काम देखो।\" दादी ने दरवाज़ा बंद करते हुए सबको वहाँ से हटा दिया। ग़लती से मैं अंदर रह गई। जिसके लिए तसल्ली को बस एक कोना बचा था जहाँ सबकी नज़रों से बचाकर खुद को खड़ा किया जा सकता था वरना संध्या बुआ की छीछालेदर देखी नहीं जा रही थी। उनकी जुबान खुलनी थी कि दादी का लावा फूट पड़ा- \"अजी सुनते हो, सब तुम्हारे सीधेपन का नतीजा है।
देखो तो, गज भर की ज़बान है इस बदतमीज़ की। बड़े साधू बने बैठे हैं। जब औलाद पैदा करनी थी तो हरा-हरा सूझता था। मैं गौरी ब्याह करूँगा। लो, कर लो गौरी ब्याह.....कुछ उषा का कर लिया गौरी ब्याह.....कुछ संध्या का कर लो। धींगड़ी हो रही है छोरी, इधर रजनी भी तैयार हो रही है। नाथ लो बैल की जोड़ी.....धूनी रमाने से परिवार नहीं चलता।\" बड़ी दादी की ज़बान रुके-रुके कि बड़े बाबा झपाटे से तख़त से उतरकर कमरे में घुसे।
मैंने देखा उनके माथे पर सफ़ेद पड़ गई लकीरों में बड़ी दादी का नाम लिखा था चंद्रकांता। अचानक संध्या बुआ की नोटबुक के वे पृष्ठ याद आ गए जिस पर उन्होंने बड़ी दादी के आमंत्रण को बड़े बाबा द्वारा ठुकराए जाने पर उनके फुँफकारते व्यवहार का खुलासा किया था। बड़े बाबा के माथे पर उनके नाखूनों से बनाई लकीरें जिनकी पपड़ी उघड़कर संकेत दे रही थी कि वे एक ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नी चंद्रकांता को नहीं सम्हाल पाए और जो इस बात का ऐलान करती तलवार-सी उनके माथे पर लटकी है। वे तो अपनी लड़कियों तक को नहीं सम्हाल पाए। अब तैश दिखाने से क्या? कगार तो टूट चुके हैं।
बड़े बाबा ने संध्या बुआ की बाँह खींची और दूसरे कमरे में ले जाकर भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। कुंडी, काँच झनझनाए और थप्पड़ घूँसों की आवाज़ माहौल को थर्राने लगी। सब सकते में आ गए। किसी को सूझ नहीं रहा था कि क्या करें? सब अपनी-अपनी जगह पत्थर बन गए थे। लेकिन इन पत्थरों में एक अहल्या भी थी जो इसलिए पत्थर बनने का शाप ढो रही थी क्योंकि उसका नाता प्रताप भवन से था।
यह पत्थर मेरी दादी थीं..... उनके तमाम वजूद पर प्रेम की कोमल मख़मली काई उगी थी। अंदर का शापित पत्थर दीखता न था। बस ये काई मन मोहती थी। वे उठीं और जाकर बंद दरवाज़े की साँकल खटखटाने लगीं। कई लम्हे दस्तक बनकर बिखरते रहे, गूँजते रहे और जब दरवाज़ा खुला तो दादी ने संध्या बुआ को कलेजे में समेट लिया, लेकिन आश्चर्य। जो इतना पिटकर भी नहीं रोई थीं उनके नयन अश्रुधार की बाढ़ से भर गए.....भर गया उनके दिल का कोना-कोना और मेरे हाथ दुआ के लिए जुड़ गए।
दादी संध्या बुआ को अपने कमरे में ले गईं। मैं भी व्यकुलतावश बाहर बगीचे में निकल आई थी। नहीं जानती मन किन कगारों, पठारों से टकरा कर अपना सिर धुन रहा था। अगर प्यार करने का यही अंजाम है तो फिर कोई नफ़रत ही क्यों नहीं करता? क्या नफ़रत करने से बुजुर्ग खुश होंगे? क्या नफ़रत करने से मान-सम्मान बढ़ेगा? पन्ना ने आकर बताया कि मुझे दादी बुला रही हैं। मेरे पैरों में पंख लग गए थे। उड़ती हुई पल में दादी के सामने- \"जी दादी?\"
”बैठो पायल।\"
सोफ़े पर बैठते-बैठते मैंने देखा संध्या बुआ के आँसू तो थम चुके थे लेकिन सूखी सिसकियाँ रह-रहकर अब भी उठ रही थीं।
\"पायल.....मैंने तुम्हारे अंदर एक हिम्मती, शक्तिवान नारी के छुपे रूप को देख लिया है, परख लिया है। तुममें दकियानूसी सोच और रीति-रिवाज़ों से लड़ने की ताकत है। चुनौती स्वीकार करना और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना भी तुममें बखूबी भरा हुआ है। तुम जानती हो जब अक़बर तेरह वर्ष का था तो उसने अपने पिता के शत्रु से बदला लिया था और राजपाट के कामों को सम्हालने भी लगा था। तुम भी उसी उम्र से गुज़र रही हो। यह संध्या जुनून की हद तक पार कर चुकी है। बताओ मैं क्या करूँ?\"
\"जी दादी?\" मैं हकला गई थी। दादी ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? अपने इस रूप से तो मैं भी परिचित न थी।
\"मैं मर जाऊँगी चाची। मैं अजय के बिना नहीं रह सकती, आप मुझे ज़हर दे दो, मार डालो लेकिन अजय से जुदा न करो।\"
संध्या बुआ ने फिर रोना शुरू कर दिया था। दादी ने उनका सिर सहलाया।
\"देखो संध्या.....तुमने अपनी बात कह दी न? अब हमें सोचने दो। जानती हो न प्रताप भवन में प्यार-मुहब्बत की बात सोचना तलवार की धार पर चलने के समान है। लेकिन देखो, नट वह भी करके दिखा देता है.....तलवार की धार पर ऐसे चलता है ज्यों फूल बिछे हों वहाँ। इसलिए हौसला रखो, हमें वक़्त दो। तुम्हारे इम्तिहान सिर पर हैं। साल भर की मेहनत का सवाल है।\"
कहती दादी मेरी ओर मुख़ातिब हुईं- \"तुम्हें यहाँ बुलाने का मक़सद यही था कि तुम संध्या की पढ़ाई का ध्यान रखोगी। रजनी में ज़रा भी गंभीरता नहीं। उसे बनाव सिंगार, मेहँदी बूटे से फुरसत ही नहीं मिलती। केवल तुम ही विश्वास करने योग्य हो।\"
मैं हुलसकर दादी से लिपट गई-\"दादी, आपने मुझे कई बरस बड़ा कर दिया।\"
\"तुम हो ही कई बरस बड़ी। पिछले जनम में मेरी माँ.....तुम्हारे जन्म से तीन महीने पहले उनका स्वर्गवास हुआ था और जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे माथे पर वैसी ही लाल बिंदिया थी जैसी वे लगाती थीं। जानती हो पायल.....मेरी माँ ने मेरे बाबा की रियासत पर शासन भी किया था। दरबार में पिता की गद्दी की बगल में माँ की गद्दी भी लगती थी।\"
\"तो आज से आप मेरी बेटी.....मैं आपकी माँ।\" कहती हुई मैं हँस पड़ी। संध्या बुआ भी हँसी। माहौल हल्का हो गया।
लेकिन भ्रम था मेरा, माहौल हल्का नहीं हुआ था बल्कि आने वाली आँधी के पहले की निस्तब्धता थी जिसे सब शांति समझ बैठे थे। दूसरे दिन संध्या बुआ ने कॉलेज जाने की ज़िद्द की तो प्रताप भवन में तूफान आ गया।
\"हरगिज़ नहीं.....पढ़-लिखकर कौन से झंडे फ़हराने हैं, अब सांयसूती घर बैठो और पढ़ो। पर्चा देने जाने का इंतज़ाम करवा दिया जाएगा। बंसीमल साथ जाएगा, उधरी खड़ा रहेगा जब तक पर्चा चलेगा।\" बड़ी दादी ने फैसला सुना दिया।
\"तो पहरा लगेगा मुझ पर।\" संध्या बुआ ने तमककर पूछा।
बड़ी दादी देर तक बड़बड़ाती रहीं। नौकरानियों, दाइयों में फिर खुसर-पुसर शुरू हो गई.....शाम होते-होते प्रताप भवन में ज़लज़ला-सा आ गया। दादी ने कोदू को दौड़ाया-\"जाओ, डॉक्टर लिवा लाओ। संध्या की तबीयत बिगड़ गई है।\"
सबको यही बताया गया कि तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन हक़ीकत कुछ और थी संध्या बुआ ने शायद इसी दिन के लिए नीलाथोथा की पुड़िया संजोकर रखी थी सो चाट ली लेकिन गले के नीचे उतरने से पहले रजनी बुआ ने देख लिया और उनके मुँह में उँगली डालकर चीख़-चीख़कर रोने लगीं। मारिया ने सम्हाला।
अस्पताल ले जाना पड़ा उन्हें। चौबीस घंटे अस्पताल में रहीं वे.....इधर बड़ी दादी कोसती जाती थीं, रोती जाती थीं.....बड़े बाबा किंकर्तव्यविमूढ़ से रात भर सहन में चहलक़दमी करते रहे। अस्पताल में दादी बाबा थे। जब संध्या बुआ घर लौटीं तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वे अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थीं तभी बड़े बाबा आए और सिरहाने बैठकर नि:शब्द उनके बाल सहलाते रहे। उनकी आँखों से झरकर न जाने कितने आँसू संध्या बुआ के बालों विलीन होते रहे.....बहुत गहराई से महसूसा इसे बुआ ने और उतनी ही शिद्दत से बड़े बाबा का हाथ अपनी आँखों पर रख खुद भी रो पड़ीं वे।
अब मेरा ध्यान संध्या बुआ की ओर अधिक लगने लगा। उस दिन की घटना के बाद से उनका घर से निकलना बंद-सा हो गया था। वे लगातार अपने को कमरे में कैद रखने लगी थीं। सब समझते वे पढ़ रही हैं पर अक़्सर उनकी आँखें दीवार पर टिकी होतीं.....शून्य भेदन कर उसमें से नई राह बनाती संध्या बुआ.....बुआ, ये राह तुम्हें कहाँ ले जाएगी? किस काल में तुमने प्यार की कँटीली राह चुनी.....चैन खोया, शांति खोई? क्या यह वही काल था जब रानी सुंदरा ने पूरन जोगी की मुहब्बत में अपने आपको भुला दिया था, जब रांझा हीर की मुहब्बत में जोगी हो गया था और हीर जोगन.....घर समाज छोड़कर! क्या यह वही काल था जब लैला की मुहब्बत में दीवाने मजनूं को रेत के मरू ने अपने आगोश में ले लिया था और सोहनी को चनाब दरिया ने अपनी लहरों में पनाह दे दी थी.....तुम कहाँ जाओगी बुआ? इस काल दंश से कितना बचोगी?
मारिया का सेवा केंद्र लगभग तैयार हो गया। केवल दरवाज़े-खिड़कियाँ जड़नी बाकी थीं। अठारह कमरों, गलियारों और बड़े से अहाते वाला यह सेवा केंद्र लाल ईंटों से बना था, बहुत कुछ गुप्तकालीन टच देता। बगीचे की रूपरेखा थॉमस ने तैयार की थी। मुख्य फाटक के दोनों ओर बोगनबेलिया की रोपी जाएँगी। अहाते की दीवार से लगे आम, अशोक, नीम और पीपल के झाड़ होंगे। माता मरियम की मूर्ति सेवा केंद्र की मुख्य इमारत की दीवार पर काँच के शो केस में रखी जाएगी। नरम लचीली घास के लॉन पर लोगों के बैठने के लिए पत्थर की बेंचें, फूलों की क्यारियाँ और फ़व्वारे होंगे। बाबा कुछ महीनों के लिए बनारस जा रहे हैं इसलिए मारिया बिना खिड़की दरवाज़े जड़े सेवा केंद्र का उद्घाटन करा लेने को उतावली हो रही है। उसने तो थॉमस और बापू को भी बुला लिया है।
\"छोटी आंटी आप और छोटे साहब के हाथों ही उद्घाटन होगा सेवा केंद्र का।\"
मारिया की आस्था से दादी अभिभूत थीं। वे खुद उद्घाटन की तैयारियों में जुट गईं। निमंत्रण पत्र की रूपरेखा संध्या बुआ ने तैयार की। उद्घाटन के बाद जलपान का भी आयोजन है, निमंत्रण पत्र के साथ मारिया का विज़िटिंग कार्ड भी रखा गया।
मारिया का उत्साह तो देखने लायक था। चम्पा के फूल-सी खिली पड़ रही थी वह, साथ में उसकी श्रद्धा, सेवा और आस्था की महक थी। दादी खुद जाकर उसके लिए कोसे की सफेद साड़ी लाई थीं जिस पर पतली सुनहरी किनार थी। मारिया सचमुच आकर्षक लग रही थी उस दिन। उसके बापू भी गाँव से आ गए थे। दुबले-पतले, साँवले से.....लेकिन जिजीविषा से पूर्ण। मारिया का सेवा केंद्र देख उन्होंने कई बार अपनी आँखें पोछीं। मारिया ने दादी-बाबा से उनका परिचय कराया तो वे गद्गद हो नतमस्तक हो गए।
\"आप तो जाने-पहचाने लगते हैं। मारिया ने अजनबियत रहने ही कहाँ दी। गाँव आती तो केवल आपके किस्से।\"
मारिया हाथ पकड़कर मुझे भी उनके सामने ले गई- \"बापू.....पायल।\"
मारिया के शब्द अधूरे रह गए। वे तपाक़ से बोले- \"पायल बाई.....\"
और मारिया की ओर देख हँस दिए।
उद्घाटन समारोह में मानो पूरा शहर ही उलट पड़ा था। अंग्रेजों की बग्घियाँ भी क़तार से खड़ी हुई थीं। बड़ी दादी को छोड़कर कोठी का हर व्यक्ति मौजूद था। गेट पर बँधे लाल रिबन दादी-बाबा ने मिलकर एक साथ काटा। कंचन, जसोदा और पन्ना ने फूल बरसाए। तालियों की देर तक गूँजती गड़गड़ाहट थमी तो एक अकेली ताली ने सबको चौंका दिया। सबकी नज़रें आवाज़ की दिशा में उठीं और पलभर को अनझिप रह गईं। कोदू और बंसीमल बड़ी दादी को व्हील चेयर पर बैठाए हुए थे और बड़ी दादी के दोनों हाथ धीरे-धीरे ताली बजा रहे थे।
अचानक मारिया ने लोगों को संबोधित किया-\"हुज़ूर.....मेरे पूज्य मेहमान, यह जो क़रिश्मा आप देख रहे हैं, यह प्रभु यीशु की मर्ज़ी है। आज वर्षों बाद जनाब अमरसिंह की धर्मपत्नी चंद्रकांता देवी घर से निकली हैं, प्रताप भवन धन्य हुआ है। बिना ईश्वर के यह सेवा केंद्र चल भी नहीं सकता और मेरे ईश्वर का स्वरुप हैं छोटी आंटी और अंकल.....\"
कहते हुए मारिया की आँखें चू पड़ीं। बाबा ने सम्हाला।
\"मारिया ने जो यह तप किया है.....ग़रीब, असहाय और सताए हुए लोगों की सेवा करने का जो संकल्प लिया है, उसके इस कार्य का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। हाँ, यह सच है कि भाभी सा वर्षों से बीमार हैं। उनका यहाँ आना.....वर्षों बाद प्रताप भवन की ड्योढ़ी फलाँगना मारिया की सेवा भावना का सबूत है। आइये, हम सब स छोटी-सी तपस्विनी को नमन करें।\"
एक साथ कई हाथ जुड़े, कई आँखें भीगीं, कई दिल हिले। थॉमस के जज़्बातों के फूल माला बनकर मारिया के गले में सज गए। मारिया नववधू-सी लजा गई। उस शाम खुशियों का सागर उमड़ा पड़ रहा था। अब थॉमस और बापू सेवा केंद्र में ही अलग से बने अपने निवास स्थानों पर रहेंगे। अब मारिया भी हमारे साथ नहीं रह पाएगी, अलबत्ता बड़ी दादी की देखभाल वह नियमित हाज़िरी देकर जारी रखेगी।
बड़ी विचलित कर गई मारिया की जुदाई। प्रताप भवन में मारिया बेटी की हैसियत से रहती थी.....अब उसके साथ रहने की सबको आदत-सी पड़ चुकी थी। मेरी तो कई सूनी रातों में मेरा साथ दिया है। कभी उपदेशक बनकर, कभी अपने अनुभवों का ख़जाना खोलकर.....अब कौन मेरे सूने कमरे में पहचल बनकर आएगा; मेरी चित्रकारी, बातिक डिज़ाइनों पर अपनी क़ीमती सलाह देगा।
मेरी फोटोग्राफ़ी के नुक्स निकालेगा और कविताएँ सुनकर सपनों में खो जाएगा; मारिया एक सपना अक़्सर सुनाती थी। एक मकान है, एकदम खंडहरनुमा.....चील, कौवों का बसेरा.....खंडहर के पीछे दहकते शोले.....सूखी लकड़ियाँ, पत्ते बटोरकर थॉमस उन शोलों को और भड़का रहा है.....उनकी आँच मारिया तक पहुँचती है और वह स्वयं आग बन जाती है। बिल्कुल ककनूस पक्षी की तरह जो आग के गीत गाते-गाते स्वयं जलने लगता है। पंख लपटें छोड़ने लगते हैं। जैसे-जैसे आग बढ़ती जाती है, गीत के सुर भी बढ़ते जाते हैं और फिर.....मात्र चंद लम्हों में वहाँ राख की छोटी-सी ढेरी होती है। ककनूस ढेरी में बदल जाता है और बदल जाते हैं ज़मीन आसमान।
\"पायल बाई.....आग विद्रोह की प्रतीक है न?\"
\"नहीं, सृजन की। आग सब कुछ राख कर देती है और उस राख में से नए अंकुर निकलते हैं।\"
आज उन अंकुरों को कोमलता से सम्हाले मारिया बिदा ले रही है। दादी ने ठीक बेटी की बिदाई जैसी रस्म अभी-अभी पूरी की है और मारिया सबके गले लगकर अंत में मेरे पास आई है-\"पायल बाई, अपने अंदर की आग बुझने न देना। भले ही उसे अभी दबाकर रखना पड़े.....\"
और मुझे मारिया की ही सुनाई वह बात याद आ गई। उसने बताया था कि उसके गाँव में चूल्हे की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती, उसे चावल के भूसे में दबा दिया जाता है। जब ज़रुरत होती है फुँकनी से भूसा उड़ाकर आग भड़का ली जाती है.....
मैं उसके कान में फुसफुसाई-\"निश्चिंत रहो मारिया। मैं देवताओं से आग छीनकर ही धरती पर आई हूँ। यूनान के प्रमेथ्यू की तरह।\" उसने संतुष्टि में मेरी ओर देखा और न जाने उसे क्या हुआ कि मेरे चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर उसने मेरे गालों को चूम लिया..... वह थरथराहट भरा उसका चुंबन मेरे हृदय के तारों को झंकृत करता दिशाओं में गूँज उठा.....मैंने देखा ढलती साँझ में उसका ताँगा धीरे-धीरे गायब होता जा रहा है।
न जाने कहाँ लेकर गई हैं दादी संध्या बुआ को। मुझे बताया नहीं पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि आजकल अधिकतर समय दादी संध्या बुआ के कमरे में ही बिताती हैं.....घंटों बातें होती हैं दोनों में।
\"खूब दोस्ती हो गई है चाची और संध्या जीजी में।\" रजनी बुआ ने बताया-\"मैं तो माँ तक के कमरे में नहीं जाती, संध्या जीजी की पिटाई के बाद उनके कमरे की दहलीज़ लाँघना मैंने खुद के लिए वर्जित कर लिया है। उस दिन भूले से मैं उनके कमरे में चली गई थी, मारिया ने ही मुझे थर्मामीटर में उनका बुखार देखने के लिए बुलाया था। उसका चश्मा नहीं मिल रहा था कहीं.....\"
\"चलो भागो यहाँ से? नहीं ज़रुरत है मुझे किसी लड़की की। कोई यहाँ मत आया करो। मैंने तो कोख से नागिनों को जन्मा है सो डँस रही हैं मुझे।\"
फिर भी तुम जाया करो बुआ....बड़ी दादी अकेलापन महसूस करती होंगी।\"
\"नहीं पायल.....वहाँ जाकर उनकी झिड़की सुनना मेरे वश की बात नहीं। मैं तो होश सम्हालते ही उन्हें बिस्तर पर देखती आ रही हूँ। झिड़कियाँ सुनती आ रही हूँ। और कितना सुनूँ? उन्हें भी समझना चाहिए कि अब हम बड़े हो रहे हैं पर उन्होंने अपनी औलाद को कभी औलाद समझा ही नहीं.....तिरस्कार.....झिड़की.....अपमान.....उफ़.....\"
कोई अनुभव अपने आप में पूर्ण नहीं होता.....धीरे-धीरे वक़्त उसमें और सूत्र जोड़ता जाता है.....तब अनुभव की रस्सी गँठकर तैयार होती है। तीन बुआओं की रस्सी गँठ चुकी है अब उसके रेशे नहीं उधेड़े जा सकते। बड़ी दादी की यह दूसरी हार थी। पहली बार पति को खोने की, दूसरी औलाद को खोने की। कितनी लाचार थीं बेचारी। मारिया के हाथों रोगों के निदान में उलझी.....उलटे तमाम रोगों को पोसतीं पलंग की चौखट में कैद एक ज़िंदा एहसास.....
संध्या बुआ का मन अब पढ़ाई में लगना कठिन था। बेहद विचलित थीं वे.....दादी को चिंता थी कहीं साल न बिगड़ जाए उनका। साल भर की मेहनत पर पानी न फिर जाए..... उनके क़दमों को वापस लौटाना मुश्किल था.....प्यार के जज़्बे ने उनके अंग-अंग को अपने मादक रस में डुबो लिया था। ज़्यादा सख़्ती बरती तो सब कुछ खत्म हो जाने की आशंका थी।
चिलचिलाती धूप अभ्रक के समान चमक रही थी। माली ने लॉन के बीचोंबीच एक क्यारी में अफ़ीम के पौधे लगाए थे जिनके सतरंगी फूल सूरज की सतरंगी किरणों को दोगुना रंगीन बना रहे थे। बाबा इन दिनों बनारस गए हुए थे और बड़े बाबा कीना बाबा आश्रम में साधुओं के जमघट के बीच किसी तंत्र-मंत्र में डूबे थे। कीना बाबा बनारस के सिद्ध तांत्रिक थे, उन्हीं के शिष्य ने यहाँ भी वैसा ही खजूर के पेड़ों से घिरा आश्रम बनवाया था जहाँ तंत्र साधनाएँ होती थीं। खजूर के अलावा अन्य जाति के छतनारे पेड़ों की वजह से यहाँ काफ़ी ठंडक रहती थी।
सामने ही मीठे पानी का कुआँ, कुएँ पर महिला प्रवेश वर्जित था जबकि तांत्रिकों की सारी साधनाएँ बिना महिला के संभव न थी। क्या इनकी सिद्धदेवी भैरवी के अस्तित्व से इंकार किया जा सकता है? और दादी का साहस इतना कि इसी आश्रम के पीछे एक छोटी-सी टेकड़ी पर बने रास बिहारी के मंदिर में मुझे और संध्या बुआ को बग्घी में बिठाकर ले गईं। वहाँ अजय पहले से आकर खड़े थे। उन्होंने झुककर दादी के पैर छुए.....हमें मंदिर के फर्श पर बैठने का संकेत कर दादी ने मंदिर की परिक्रमा की। अच्छी तरह पूरे मंदिर का मुआयना कर वे अजय से बोलीं-\"वीरान रहता है यह मंदिर। एक तो सुनसान में है दूसरे तांत्रिकों के आश्रम के पास होने की वजह से कोई आता-जाता नहीं है यहाँ। इक्का-दुक्का लोग शाम तक आएँगे।\"
उन्होंने संध्या बुआ को हाथ में पकड़ा मख़मली कत्थई बटुआ खोलने को बटुए में दो अँगूठियाँ और डिब्बी में सिंदूर था।
\"अजय और संध्या.....भगवान को साक्षी मानकर एक-दूसरे को पति-पत्नी रूप में स्वीकार करो।\"
मेरे तो होश उड़ गए......दिल की धड़कनें आँधी-तूफ़ान की गति से बढ़ने लगीं। कल्पना से परे था सारा मंजर। मेरी आँखों में एक-एक क्रिया गहरे खुबती चली गई। पहले अजय ने बुआ को अँगूठी पहनाई फिर बुआ ने अजय को। अजय ने उँगली की पोर सिंदूर की डिब्बी में छुआकर संध्या बुआ की माँग में बिल्कुल हल्की सिंदूर की रेखा खींच दी। दोनों ने झुककर पहले रास बिहारी की मूर्ति के, फिर दादी के पैर छुए। दादी ने दोनों को गले से लगा लिया-\"ईश्वर तुम दोनों को हिम्मत दे, प्यार के अंजाम को सहने की ताकत दे, घर-परिवार का सामना करने का हौसला दे।\"
मुझे लगा सूरज की सतरंगी किरनों में से एक किरन जुदा हुई और दादी के वजूद में समा गई.....और वजूद और किरन मिलकर आग का शोला बन गए। इस शोले ने उन अँधियारों को रोशन कर दिया जहाँ कभी अकेली किरन पहुँच नहीं सकती थी। यह उस शोले का जज़्बा था जो अंधियारे की बर्फ़ को बूँद-बूँद पिघलाकर हम सब पर शीतलता की बौछार कर रहा था।
दादी ने बूँदी के लड्डू का पैकेट खोलकर सबको लड्डू खिलाए। फिर मुझे अपने क़रीब खींचकर चूमा-\"तुम गवाह हो इस गंधर्व विवाह की। जानती हो गंधर्व विवाह गुप्त होता है। तुम्हें भी सब कुछ गुप्त रखना है। वक़्त आने पर सबको बता दिया जाएगा।\"
\"अजय और संध्या, मैंने यह विवाह करके समझो साँप के मुँह में हाथ डाला है। आज अपना भविष्य बनाकर दिखाओ कि प्रताप भवन खुद तुम दोनों के इस विवाह पर रज़ामंदी की मोहर लगाए।\"
अजय ने दादी के हाथ भरपूर विश्वास से थपथपाए। उन हाथों की मर्दानी गर्मी ने दादी को विश्वस्त किया होगा कि उन्होंने जो इतना बड़ा ख़तरा उठाया है उसे वे जग हँसाई बनाकर नहीं छोड़ेंगे। अजय ने मेरी ओर भी मुस्कुराकर देखा। मैंने उनके नज़दीक जाकर उन्हें बधाई दी तो दोनों ने एक साथ मुझे आलिंगन में भर लिया। दादी ने हम तीनों को ही अपने हाथ से लड्डू खिलाया तो अजय ने भी दादी के मुँह में लड्डू का टुकड़ा रखते हुए जेब से लाल काग़ज़ में लिपटी कोई चीज़ निकालकर उन्हें भेंट स्वरुप दी।
\"चाची, आप हमारी नई ज़िंदगी की ब्रह्मा हैं। इतनी कूवत तो नहीं कि कुछ दे सकूँ आपको, यह केवल निशानी है आज के दिन की।\"
दादी ने पुड़िया खोली तो उसमें माणिक जड़ी बहुत खूबसूरत अँगूठी थी जिसे अजय ने स्वयं अपने हाथों दादी को पहना दिया।
\"जानती हैं चाची, \'भृगु संहिता\' में क्या लिखा है मेरे और संध्या के बारे में? लिखा है प्राचीन काल में मैं राजा दुष्यंत था और संध्या कण्व के आश्रम में पली शकुंतला। इसीलिए तो इस जनम में भी हमारा गंधर्व विवाह हुआ। हम दोनों के मिलन में यह अँगूठी अब दोबारा रूकावट न डाले इसीलिए बहुत सुरक्षित हाथों में सौंप रहा हूँ इसे।
दादी हँस दीं। सांध्यतारा निकल आया था और मंदिर की सीढ़ियों पर इक्का-दुक्का भक्तों का आगमन होना शुरू हो चुका था। दादी ने संध्या बुआ से अपनी सिंदूर भरी माँग को बालों की लट से ढँक लेने के लिए कहा। अजय को वहीँ छोड़कर हम तीनों बग्घी में बैठकर घर लौट आए।
अब संध्या बुआ स्थिर चित्त थीं और प्रताप भवन में यह ख़बर फैल गई थी कि दादी मंदिर से संध्या बुआ को किसी पंडित-ओझा से झड़वा फुँकवाकर लाई हैं.....और अब सब ठीक है।
संध्या बुआ के गुप्त विवाह के बाद की यह पहली करवा चौथ थी। नाश्ते की टेबिल पर उनका इंतज़ार हो रहा था। मैं आँखें झुकाए धीरे-धीरे नाश्ता कर रही थी, डर था कहीं दादी से आँख न मिल जाए और अन्य लोगों तक उन नज़रों का भेद न खुल जाए। जब से मारिया गई है बड़ी दादी व्हील चेयर पर पूरी कोठी में आती-जाती रहती हैं। इस काम के लिए पन्ना को नियुक्त किया है कि वह उनकी चेयर चलाए। दादी और अम्मा तो निर्जला व्रत रखती थीं लेकिन बड़ी दादी के व्रत इतने कठोर न थे। बीमारी के कारण उन्हें दवाएँ लेते समय फलाहार लेने की छूट थी। पन्ना उनकी चेयर खाने की टेबिल तक लाई तो बड़ी दादी ने पूछा-\"संध्या कहाँ है?\"
\"संध्या जीजी को नहीं खाना है।\" रजनी बुआ तपाक़ से बोलीं।
\"क्यों? उसे तो सुबह उठते ही भूख सताने लगती है, आज क्या हुआ?\"
\"शायद तबीयत ठीक नहीं है, कल रात सिरदर्द की शिकायत कर रही थी।\"
दादी ने झूठ नहीं कहा था, संध्या बुआ को सचमुच कल रात सिर में तेज़ दर्द था। लेकिन मुझे लगा कि दादी ने इस बहाने उनके करवा चौथ के व्रत की रक्षा कर ली है। जैसे कोहरा अपनी धुँध की चादर में फूलों को समेट ले। फूल भी सुरक्षित रहें और दुनिया की नज़र से बचे भी रहें।
दिन भर चौके में तरह-तरह के पकवान बनते रहे। जसोदा और कंचन भी व्रत से थीं। दोनों के पति भी रात का खाना कोठी में ही खाने वाले थे। जसोदा ने सबको मेहँदी लगाई। मुझे शुरू से ही मेहँदी अच्छी नहीं लगती। बड़ा अजीब लगता है हाथों में चित्रांकन.....जबकि दूसरों के हाथों में मैं खुद मेहँदी के चित्र बना देती हूँ.....बहुत बारीक और घने.....शगुन के लिए जसोदा ने हथेली के बीचोंबीच मेहँदी की एक बिंदी-सी लगा दी।
\"राजपूतों में तुम जाने कहाँ से पैदा हो गईं पायल बिटिया.....तुम-सी हमने दूसरी नहीं देखी।\"
\"दूसरी हो भी न जसोदा.....मैं पहली ही बनी रहना चाहती हूँ।\"
कंचन करवे ख़रीद लाई थी। मिट्टी के टोंटीदार। ऊपर छत पर रंगोली सजाई जा रही थी। गेरू भिगोकर सुंदर चित्रकारी की जा रही थी। घर की सभी महिलाओं ने रेशमी रंग-बिरंगी साड़ियाँ, लहँगे पहने। बालों में जुही की कलियाँ सजाईं, भारी-भारी सोने, हीरे, कुंदन के आभूषण पहने। दादी ने संध्या बुआ को इतना खूबसूरत असली रेशम का लहँगा और ओढ़नी पहनाई कि मैं देखती ही रह गई। हलके-हलके हीरे के आभूषण, हाथों में मेहँदी भी खूब रची थी। संध्या बुआ पे सुहाग का सत खूब चढ़ा था.....आज अजय उन्हें देखते तो कहते धरती पर चाँद कैसे?
\"ऊपर जब हम सब चाँद को अर्घ्य दें तो तुम मन-ही-मन उन्हें पूज लेना। फिर नीचे अपने कमरे में आकर खिड़की से अर्घ्य दे लेना। कोई नहीं देख सकेगा।\"
और ऊपर छत पर जाने से पहले मेरे मन में फुसफुसाईं-\"तुम संध्या का ध्यान रखना।\"
मैंने दादी के कथन पर हामी में सिर हिलाया तो उन्होंने मेरे सिर पर हलकी-सी चपत मारी और हँस दी।
संध्या बुआ छत पर आ गईं। व्रत के कारण उनका चेहरा कुम्हला गया था। रेशमी लहँगे और आभूषण तो मैंने और रजनी बुआ ने भी पहने थे इसलिए किसी का ध्यान संध्या बुआ की सजावट पर नहीं गया लेकिन उनके कुम्हलाए चेहरे को देख अम्मा चिंतित हो गईं-\"संध्या बाई तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है?\"
\"नहीं भाभीसा.....कल रात सिर दर्द की हालत में देर तक पढ़ती रही न.....इसीलिए.....\"
चाँद निकल आया था। खूब बड़ा, गाढ़ा गुलाबी-सा.....जब तक पूजा चली, सबने अर्घ्य दिया तब तक चाँद शीतल, ठंडी रोशनी से भर चुका था। दादी सोलहों श्रृंगार किए बेहद खूबसूरत लग रही थीं। रूप तो उनका बेमिसाल था ही, ऊपर से श्रृंगार। मैं तो लट्टू हो गई उन पर। पूजा के समापन पर दादी को छोड़कर सब नीचे उतर गईं तो मैंने बाबा को सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जाते देखा। कौतुहलवश मेरे पैर ठिठक गए। कनखियों से देखा दादी ने खड़े-खड़े ही बाबा के माथे पर तिलक लगाया, उन पर फूल बरसाए, आरती उतारी और झुककर उनके पैर छुए। उठते-उठते सिर पर से उनका आँचल सरक गया। बाबा ने उन्हें गले से लगा लिया और कुरते की जेब में इसी क्षण के लिए बड़े जतन से रखी जुही की वेणी उनके जूड़े में टाँक दी। आसमान में चाँद मानो थम-सा गया। तब तक संध्या बुआ आखिरी सीढ़ी से भी ओझल हो गई थीं।
पन्ना ने कंचन से शर्त बदी थी कि इस बार बारिश अच्छी होगी और जो अच्छी हुई तो वह कंचन से चाँदी की पाजेब लेगी। राजस्थान में बारिश की शर्तों का चलन बहुत अधिक है। बारिश होगी या नहीं इस बात की शर्त पर अच्छा ख़ासा सौदा तय होता है। कितने ही लोग इन शर्तों में तबाह हो गए। दिसंबर भी बीता जा रहा है और कंचन ने अभी तक पाजेब ख़रीदकर पन्ना को नहीं दी। इस बात की शिकायत लेकर वह दादी के पास गई तो दादी ने हँसकर उसे पान के बीड़े लगाने का हुकुम दिया। ऊपर से चाँदी की तश्तरी में सभी बीड़ों को रखकर गुलाबजल छिड़कने की ताक़ीद भी की। पन्ना ने बड़ी खूबसूरती से बीड़े सजाए.....वह हौले-हौले कोई गीत गुनगुनाती जा रही थी। कोठी पर आज फिर अंग्रेज़ों का जमघट था। घोड़े, बग्घी और जीप बाहर खड़ी थीं। बड़े हॉल में व्हिस्की के दौर चल रहे थे। दादी ने पूर्ण शाकाहारी खाना बनवाया था। जब से यज्ञ हुआ है इस घर में मांसाहार पकने पर पाबंदी लग गई है। दादी की इस इच्छा के आगे बाबा नतमस्तक हैं। भोजन के बाद दादी पान के सुगंधित बीड़े भी भिजवाएँगी।
\"पन्ना, तुझे चाँदी की पाजेबों के साथ मैं सोने के कर्णफूल भी दूँगी।\"
पन्ना ने आश्चर्य से दादी को देखा। दादी हँस पड़ीं-\"अरी बावली, मन्नत माँग..... मन्नत.....उषा के लड़का हो.....फिर देखना तेरा मुँह लड्डूओं से भर दूँगी।\"
पन्ना एकदम किलकारी मारकर खड़ी हो गई और नृत्य की मुद्रा में गोल घूम गई।
\"बाईसा के घर जाकर मैं तो खूब गाऊँगी, खूब नाचूँगी.....मैं तो उनसे करधनी भी लूँगी।\"
\"ठीक है जा.....तैयारी कर ले। तेरे साथ संध्या और रजनी भी जाएँगी जोधपुर।\"
\"छूछक लेके।\"
\"तू तो सच में बावली हो गई है। अभी जचकी हुई नहीं और छूछक ले जाने लगी।\"
इतने में बंसीलाल पान लेने आ गया.....पान की तश्तरी उसे पकड़ाकर पन्ना अंदर के कमरे में दौड़ गई।
अंग्रेज़ों को बिदा कर बाबा जब दादी के पास आए तो कुछ थके से दिख रहे थे। आते ही पलंग पर लेट गए। जाड़ों में वैसे ही रात जल्दी गहराने लगती है.....राजस्थान का मरू खूब ठंडाता है रात में.....ठंडी-ठंडी रेत माहौल भी ठंडा कर देती है।
रजनी और संध्या बुआ जोधपुर के लिए रवाना हो रही थीं। दादी ने ढेर सारी सौगातें पैकेटों में बँधवाईं, मिठाई से भरी टोकरियाँ जिन पर लाल काग़ज़ लिपटा था.....दादी के हाथ में कुछ ऐसी बरक़त थी कि किसी को कहने को कुछ रहता ही न था। साक्षात् अन्नपूर्णा का भंडार.....तृप्ति का स्रोत। दादी ने पूरी बाँह का नीला ब्लाउज़ और नीले बॉर्डर की गुलाबी सूती साड़ी पहनी थी.....न जाने क्यों जैसे-जैसे दादी की उम्र बढ़ रही थी उनका सौंदर्य भी बढ़ता जा रहा था। यह शायद उनके अंदर के गुणों का चमत्कार है। मेरी अपनी समझ से दादी हमेशा दूसरों के लिए ही समर्पित रही हैं.....सीढ़ी-सादी लेकिन बेहद ताकतवर आत्मविश्वास लिये। अम्मा ने एक बार मेरे तर्कों का शमन न होने पर मुझे उदास देखकर कहा था-\"अपने को कभी कमजोर मत समझना पायल। जानती हो, धुल जैसी पैरों तले रौंदी जाने वाली चीज़ में भी कितनी ताकत होती है? जब वह गुबार बन जाती है तो पूरे आसमान को अपने आगोश में ले लेती है। फिर नारी तो वह ताकत है जो अपनी कोख से लाखों वर्षों का इतिहास पैदा करती है। जल प्रलय के बाद मानव को इस धरती पर अवतरित होने में लाखों वर्ष लगे और नारी की कोख से केवल नौ महीने में मानव पैदा हो जाता है।\"
अम्मा के इस ज्ञान पर मैं दंग रह गई थी। दादी मुझे ऐसे ही चमत्कारिक ज्ञान से भरी लगती है।
प्रताप भवन सूना हो गया दोनों बुआओं के जाने से। रजनी बुआ शौकीन और चंचल हैं लेकिन संध्या बुआ जिज्ञासाओं का भंडार। उनका हर कार्यकलाप मुझे बड़ा रोचक लगता है। अब कैसे बीतेंगे पंद्रह दिन। बाबूजी गए हैं पहुँचाने..... तय हुआ है कि फूफासा आएँगे छोड़ने। उषा बुआ भी साथ आएँगी। जचकी यहीं होगी। तब तक आषाढ़ लग जाएगा। फिर तो तीजों के बाद ही लौटेंगी उषा बुआ। मैं अकेलेपन से जूझती कोठी के बाहर के बगीचे में आ गई। हरसिंगार फूलों से लदा था और सुगंध हवाओं में रच-बस गई थी। बहुत सारे फूल लॉन की लचीली दूब पर बिखर गए थे। नारंगी डंडी वाले शंख श्वेत कोमल फूल.....नन्हे-नन्हे.....सितारों जैसे। मैं अंदर से अम्मा की पूजा की डलिया उठा लाई, जालीदार ताँबे की। एक-एक फूल चुन-चुनकर उसमें रखने लगी। हरसिंगार मुझे रोमांचित कर जाता है। जाने क्या आकर्षण है इन फूलों में कि मैं बस बँधकर रह जाती हूँ। डलिया फूलों से भर गई लेकिन फूल उतनी ही मात्रा में दूब पर बिछे हुए थे। रात भर टपकते रहते हैं ये फूल। गेट पर पहचल सुन मैंने मुड़कर देखा-\"नमस्ते बाई जी।\"
पोस्टमैन था.....पीले रंग का लंबा लिफाफा लिये। ऊपर संध्या बुआ का नाम लिखा था। मैंने न जाने क्या सोचकर लिफाफे को अपने दुपट्टे में छुपा लिया और तेज़ी से अपने कमरे में आ गई। फूलों की डलिया कमरे में बिछे कालीन के बीचोंबीच रखी छोटी-सी गोल मेज पर रख दी और पलंग पर लेटकर लिफाफा खोलने लगी। अजय का ख़त था, संध्या बुआ के नाम.....
मेरी संध्या
तुम्हारे पत्र ने एहसास कराया कि हमें बिछुड़े दो महीने बीत चुके हैं। इस एहसास की वजह जानना चाहोगी? मैंने कभी तुम्हें अपने से जुदा माना ही नहीं, तुम धड़कन बनकर मेरे अंदर धड़क रही हो। आज तुम्हारे पत्र ने मालवगढ़ से जुदाई का एहसास तेज़ी से कराया। जुलाई में मैंने कलकत्ता के डिग्री कॉलेज में लेक्चररशिप ज्वाइन की थी और तब से पी-एच.डी. के लिए अच्छे गाइड की तलाश में था। शांतिनिकेतन के एक विद्वान प्रोफेसर का अचानक मिलना इस तलाश का ख़ात्मा था। अब बाकायदा पी-एच.डी. के काम में जुटा हूँ।
तुम जोधपुर जा रही हो.....जाओ, परिवर्तन स्वस्थ और स्फूर्तिवान बना देता है। जोधपुर मेरा देखा हुआ है। कुछ वर्ष पहले नागपंचमी के दिन मैं वहीँ था। जानती हो वहाँ नाग देवी, देवताओं को आधा मनुष्य, आधा सर्प माना जाता है। उनकी इस प्रकार की मूर्तियाँ पूरे शहर में घुमाई जाती हैं। जब मैं लखनऊ में था और गोमती के किनारे एक दिन घास पर लेटा था तो न जाने कहाँ से एक नाग ने आकर मेरे सिर पर अपना फन काढ़ लिया था। मैं आँखें मूँदे लेटा था। सामने भेड़-बकरियाँ चराते चरवाहे लड़के की चीख से आँखें खोलीं तो नाग का फन देख बिजली की फुर्ती से खड़ा हो गया और आश्चर्यचकित हो उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह झाड़ियों में गुम हो गया। जब यह क़िस्सा माँ को बताया तो कहने लगीं-\"तुम पर नागदेवता की कृपा रहेगी हमेशा।\"
उस रात माँ पीपल के नीचे नागदेवता के लिए नरेटी में दूध रखकर दीया जला आई थीं। संध्या, तुम्हारी कोठी के नाग से अब हमें कोई ख़तरा नहीं है। तुम कहती थीं न कि महिलाओं का शाप है तो उस शाप से हमें मुक्ति मिल गई.....नाग का वरदान बहुत पहले मिल गया था हमें।
चाची कैसी हैं, चाची के उपकारों को भुला पाना कठिन है। उन्होंने हमें एक समर्थ दिशा दी वरना हम भटकते ही रहते और भटकन से कभी मंजिल नहीं मिलती। कल रात यूँ ही सुनसान सड़क पर घूमते हुए जब थककर लौटा और अपने पलंग पर लेटा तो नींद लग गई। लगा, तुम आ रही हो धीरे-धीरे। तुम्हारे हाथों में ढेर सारे हरसिंगार के फूल हैं जिन्हें तुम मेरे सिरहाने रखकर अपने गुलाबी आँचल से मेरे माथे का पसीना पोंछ रही हो। तुम कह रही हो-\"हारना नहीं.....मंजिल की राह बढ़ते जाना, अगर तुम रूककर अपने पैरों के काँटे निकालोगे या छाले सहलाओगे तो तुम्हारे संकल्प ठंडे पड़ जाएँगे। मैं बिछी हूँ न मख़मल बनकर तुम्हारी राहों पर और तुम्हारी आँखों से दो बूँद आँसू टपक पड़े थे। संध्या, यह स्वप्न किस ओर इंगित कर रहा था? तुम्हारे अथाह प्यार और समर्पण की ओर या.....संध्या, तुमने कभी न रोने का वादा किया था मुझसे दीपावली के दिनों की मेरी मालवगढ़ यात्रा के चौथे दिन.....उस दिन भी तुम्हारी आँखें डबडबा रही थीं.....संध्या, क्या ये इंतज़ार मिलन की तड़प बढ़ा नहीं रहा और.....और ज़्यादा। अच्छा.....ये तो बताओ तुम्हें दीपावली का उपहार पसंद आया या नहीं? चाची के लिए शॉल भी मैं शांतिनिकेतन से ख़रीदकर लाया था। उस दिन तो शॉल ओढ़कर मुस्कुराती हुई तुम्हारे साथ बग्घी में बैठकर वे प्रताप भवन चली गई थीं.....पर मैं देर तक सोचता रहा.....प्रताप भवन की इतनी समृद्धि में वह शॉल कहाँ समाएगा? आजकल चिंतक भी होता जा रहा हूँ। अक़्सर बेलूड़ मठ चला जाता हूँ जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में बनवाया गया है। सामने शांत, मंथर हुबली नदी पर मछुआरों की नावें खड़ी रहती हैं। अक्सर मैं नाव किराए पर लेकर खुद ही चप्पू चलाता हुबली के गहरे जल की ओर बढ़ जाता हूँ। गहराई में वह अधिक शांत स्थिर नज़र आती है। शाम की सिंदूरी रंगत लहरों को सुहागिन बना देती है। हुबली के तट पर बिना ब्लाउज़ के काली-सफेद धारियों वाली लाल बॉर्डर की बंगाली साड़ी पहने बंगालिनें कपड़े धोती रहती हैं, या अपने लंबे-लंबे बाल। एक लड़की के बाल तो बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। बेचैन होकर मैंने नाव मठ की ओर मोड़ दी थी और मठ के प्रांगण में लगे उस के नीचे देर तक बैठा रहा था जो है तो बरगद का पर पत्ते अजीब किस्म के हैं। इन पत्तों में एक पॉकेट-सा बना है। उँगली की पोर बराबर जगह हैं उसमें। कहते हैं कृष्ण यशोदा के डर से मक्खन छुपाकर रखते थे। कृष्ण कैसे वृंदावन से यहाँ तक मक्खन छुपाने आते होंगे और कैसे इतने नटखट कृष्ण को राधा ने प्यार किया? लेकिन राधा का प्यार अद्भुत था.....वह मानिनी थी.....कभी अपने बरसाने गाँव को छोड़कर कृष्ण के पीछे नहीं भागी। कृष्ण जहाँ-जहाँ गए, जिन-जिन नारियों से उनका संपर्क हुआ, राधा ने अपने आपको उन-उन नारियों में समाहित कर लिया पर अपना गाँव कभी नहीं छोड़ा। वह धीर, गंभीर, मानिनी राधा मेरे मन पर प्रेम का लैंडमार्क बनकर प्रतिष्ठित है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रेम से कहीं अधिक ऊँचा और महान था।\"
संध्या, अनुसंधान कार्य के तेज़ी से चलने के बावजूद अकेलापन बहुत सालता है। यह विवशता है.....चाहे इसे आग्रह मानो.....लेकिन इतना तय है कि तुम्हारे बिना जीवन की राह पर चलना, पाना, तृप्त होना कठिन है। तुम्हारे पत्र इस कठिनाई में सहायक बनेंगे इसलिए पत्र लिखने का क्रम जारी रखना। चाची को चरण स्पर्श और पायल को प्यार.....अपना ख़याल रखना।
तुम्हारा
अजय
पत्र तहाकर मैंने लिफाफे में रख दिया। अचानक बहुत सारे रहस्य खुल गए कि अजय कलकत्ते में लैक्चरर हैं कि वे दीपावली में यहाँ आए थे और दादी संध्या बुआ को उनसे मिलवाने ले गई थीं। कौन-सी ऊर्जा दादी में रची बसी है, कौन-सी हिम्मत कि वे सबका मनचाहा कर डालती हैं, सबका ध्यान रखती हैं.....सहसा मैं अपराधबोध से ग्रसित हो उठी। मुझे नहीं खोलना चाहिए था लिफाफा.....मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था अजय का पत्र। पति-पत्नी की अंतरंगता जानने का मुझे कोई हक़ नहीं। पति! संध्या बुआ के पति! तो फिर मैं उनका नाम क्यों लेती हूँ? क्यों नहीं उन्हें फूफासा कहकर संबोधित करती? अपने हृदय के आलोड़न में डूबी मैं पत्र लिये दादी के कमरे में आई। दादी सोफे पर आराम की मुद्रा में बैठी कोई किताब पढ़ रही थीं। मैं अपराधिनी-सी सीधी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। आँखें झुका लीं, मुँह से कुछ नहीं कह सकी।
\"पायल, क्या हुआ? इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी है?\"
मैंने लिफाफा आगे कर दिया। दादी ने लिफाफा हाथ में लिया.....उस पर संध्या बुआ का नाम पढ़ फौरन ख़त बाहर निकाला।
\"हे भगवान!.....यह क्या नादानी की अजय ने?\"
फिर मेरा हाथ पकड़ अपने नज़दीक बिठा लिया-\"तुम्हें कहाँ मिला ये ख़त?\"
\"मैं बगीचे में थी तभी पोस्टमैन आया था। दादी, मैं अपराधी हूँ, मैंने ख़त पढ़ लिया है।\" मैंने रुक-रूककर कहा।
\"लाख-लाख शुक्र है भगवान का जो बगीचे में उस वक्त तुम थीं। कहीं यह ख़त कोठी के किसी मर्द के हाथ पड़ जाता तो लेने के देने पड़ जाते।\"
फिर मेरे चेहरे को देख मेरी ठोड़ी उठाते हुए दुलार से कहा-\"तुम तो सब जानती हो मेरी माँ! पढ़ लिया तो इतना परेशान होने की कोई ज़रुरत नहीं। ऐसा इसमें क्या लिखा होगा जो तुम नहीं जानतीं।\"
\"लिखा है।\"
\"क्या?\"
\"लिखा है कि तुम दीपावली के लिए उनके आने पर अकेली ही बुआ के साथ उनसे मिलने गई थीं।\"
दादी की हँसी छूट पड़ी-\"अरे मेरी लाड़ल.....मेरी माँ.....पूरी पुरखिन हो गई तू तो।\"
मुझे अपने आलिंगन में लेकर उन्होंने मुझे खूब चूमा और मेरे बाल सहलाते हुए बोलीं-\"संध्या की बहुत चिंता है मुझे। जब यह राज़ खुलेगा तो न जाने कौन-सा कहर ढहेगा कोठी पर।\"
\"आप हैं न दादी! फिर तो सब ठीक ही होगा।\"
सुबह-सुबह बाबा ने दादी को सूचना दी कि उन्हें अगले हफ्ते बनारस के तूफानी दौरे पर जाना है। वहाँ समय लग सकता है क्योंकि बलिया, मुज़फ्फरपुर, इलाहाबाद और भी न जाने कहाँ-कहाँ वे जाएँगे। पार्टी का काम है। अगस्त क्रांति की योजना बनानी है इसलिए बाबूजी को भेजकर बुआओं को बुलवा लिया जाए जिससे उनकी ग़ैर हाज़िरी में बाबूजी प्रताप भवन की देखरेख कर सकें। बड़े बाबा तो किसी मक़सद के ही नहीं है.....उन्हें तो अभी से वानप्रस्थी मान लिया जाए तो बेहतर है।
\"समर क्यों जाएगा? कुँवर राजा खुद आएँगे पहुँचाने, यही तय हुआ है।\"
\"कब तक पहुँचा जाएँगे?\"
\"एकादशी को आ रहे हैं, ख़बर तो यही आई है।\"
बाबा आश्वस्त हुए.....वे भी एकादशी के दिन जा रहे हैं। बुआ लोग सुबह आ जाएँगी, बाबा शाम को जाएँगे।
\"चलो अच्छा है, मिलना हो जाएगा।\" बाबा ने बेफ़िक्र हो कहा तो दादी को शंका हुई।
\"ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या वहीँ रहने का इरादा है?\"
बाबा हँस दिए-\"फिर भी अगस्त तक रुकना पड़ेगा। तब तक उषा तो लौट ही जाएगी न जोधपुर।\"
दादी जानती थीं, इस बार लंबे अर्से के लिए जा रहे हैं.....देश की आज़ादी के लिए उठे उनके क़दमों को वे रोकना नहीं चाहती थीं फिर भी मोह तो होता ही है। सिर पर क़फ़न बाँधकर निकले हैं सारे क्रांतिवीर.....लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है और इन क्रांतिवीरों ने बहुत कुछ त्यागा है। अपना घर, बीवी, बच्चे.....बस चाह है तो गुलामी की बेड़ियों को काट डालने की, फिर चाहे फाँसी का फंदा चूमना पड़े, बंदूक की गोली झेलनी पड़े या काले पानी की सज़ा। अंग्रेज़ों के दिन लद गए अब। इसीलिए वे मधुमक्खी-से हर ओर छाए रहते हैं.....जैसे सूर्यास्त होने पर बौनों की परछाईं लंबी होकर अधिक जगह पर छा जाती है। बाबा ने अपनी विदेश यात्रा के किस्से बताते हुए एक दिन किसी फ़ीनिक्स पक्षी का ज़िक्र किया था जो हज़ार साल तक जीता है और फिर शाखों से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर अपनी चिता स्वयं बनाता है। धीरे-धीरे चिता में जलकर वह राख हो जाता है और उस राख में से एक नया फ़ीनिक्स पक्षी जन्म लेता है। अपने रंग-बिरंगे पंख पसारे, खूबसूरत और आकर्षक.....क्रांतिवीर भी क्रांति की चिता में स्वयं को जलाकर, राख कर देश को नए रंग-बिरंगे पंख सौंपेंगे आज़ादी के, उन्नति के, खुशियों के।
बुआ लोग आ गई हैं। उषा बुआ का पेट ढोलक-सा बाहर निकल आया है लेकिन उनके चेहरे पर रौनक भी खूब आ गई है। फूफासा पैंट-शर्ट में बड़े स्मार्ट लग रहे थे। रह-रहकर रजनी बुआ को छेड़ रहे थे.....रजनी बुआ झल्ला जातीं-\"क्या जीजसा.....आप भी बस.....\"
\"हम सब जानते हैं, मन-ही-मन तो लड्डू फूट रहे हैं।\"
फूफासा ने फिर छेड़ा तो उषा बुआ मुस्कुराकर बोलीं-\"जाने भी दीजिए न, क्यों मेरी छोटी-सी बहन को तंग कर रहे हैं।\"
बाद में पता चला उषा बुआ की ससुराल में उनके दूर के रिश्ते के किसी पड़ोसी ने अपने बेटे के लिए रजनी बुआ को पसंद कर लिया है। मैं हँसते-हँसते दोहरी हो गई-\"हाय राम.....तेरह साल की उमर में ही? अभी तो स्कूल भी पास नहीं किया बुआ आपने।\"
\"स्कूल क्या.....मैं तो कॉलेज भी पास करूँगी, लॉ पढूँगी। शादी-वादी मुझे नहीं करनी और वो भी उषा जीजी की ससुराल में.....ना बाबा, कान पकड़े।\"
\"क्यों?\" मैंने उत्सुकता से पूछा।
रजनी बुआ गंभीर हो गईं-\"है कोई आज़ादी उषा जीजी को। सब कुछ उनकी सास के इशारे पर चलता है। सास के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता.....ससुर तक पूछकर जाते हैं। अंदर कमरे में जाने क्या खटर-पटर चलती है। उनके कमरे से लगा भंडार घर है जिसकी चाबियाँ उनकी कमर में खुँसी रहती हैं। मेवा मिष्ठान्न सब उनके कब्ज़े में। भूख लगे तो पहले उनका मुँह तको और जीजासा तो बिल्कुल उनके पल्लू में छुपे रहते हैं।\"
फिर मेरे कान के पास मुँह लाकर बोलीं-\"सोने की पाजेब तो मिली जीजी को पर सुकून नहीं.....कठपुतली बन गई हैं वो जिसकी डोर उनकी सास के हाथ में है।\"
अचानक संध्या बुआ को लिखी अजय की चिट्ठी याद आ गई मुझे और याद आ गया वह साँप जो प्रताप भवन की बहू, लड़कियों का शाप बनकर उसकी नींव में दुबका रहता है।
बाबा बनारस चले गए और दादी का अधिकतर समय उषा बुआ की देखभाल में बीतने लगा। वे सोहर के गीत हल्के-हल्के गुनगुनाती जातीं और कंचन से सौंठ मसाले कुटवाती जातीं। गोंद की बर्फी, सौंठ गुड़ के लड्डू.....मखानों का सरौते से सुपारी की तरह कतरा जाना.....हरीरे में डाले जाने वाले मसालों, मेवों की काट छाँट.....एक हलचल भरा माहौल बना रहता। मैं सोचती शादी तो मुझे करनी नहीं है और जचकी में दिए जाने वाली ये सारी चीज़ें मुझे इस क़दर पसंद हैं.....मेरे मन का ऐसा संयोग क्यों है आख़िर? मारिया रोज़ आकर उषा बुआ का चेकअप कर जाती। दवाएँ लाकर दे देती और दिलासा भी कि सब नॉर्मल है। अगले महीने के पहले हफ्ते में जचकी हो जाएगी।
अब संध्या बुआ का रूटीन हो गया था। सुबह पोस्टमैन के आने के समय में बाग में टहलना। लेकिन जाने क्यों पंद्रह दिन से पोस्टमैन झाँका तक नहीं। अलबत्ता उन्हें वहाँ खड़ी देख सड़क से जाते हिजड़े ज़रूर रुक गए। सबके सब तालियाँ बजाते कोठी के बाहर चबूतरे पर मटक-मटककर नाचने लगे। क्या गा रहे थे एक पंक्ति भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन कोठी के नौकर-चाकर वहाँ इकट्ठे होकर हँसे जा रहे थे। दादी ने कंचन के हाथ पुराने कपड़े, मिठाई का डिब्बा और न्योछावर के रुपए भिजवाकर उन्हें रुख़सत किया।
जसोदा ने मदिर से लौटकर दादी के कमरे में बैठी अम्मा और दादी को बताया कि मंदिर के पीछे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। उसकी जड़ में थड़ा (गोल चबूतरा) बना है। पूरा थड़ा गेरू से पुता है। अगर बरगद की जड़ में गर्भवती औरत कलावा बाँध दे और गेरू चढ़ाकर दीया जला दे तो लड़का होना पक्का-\"हुकुम, मैं ले जाऊँ उषा बाईजी को?\"
दादी उस वक़्त क्रोशिए से लेस बुन रही थीं, हँस पड़ीं-\"दो दिन में जचकी हो जाएगी। बरगद में कलावा बाँधने से क्या पेट का बच्चा बदल जाएगा। अब तो जो होना है वह पेट में आ चुका है। जा, अपना काम देख।\"
जसोदा खिसियाई हँसी हँसकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अम्मा गंभीर हो गईं-\"सुना है उषा बाईजी की ससुराल वाले लड़का ही चाहते हैं?\"
\"सुना तो बहुत कुछ है कि ख़ानदानी ज़ेवरात और सोने की पाजेबों से बड़ा रुतबा है उनका जोधपुर में। उषा के ससुर पक्के ज़मींदार हैं.....शराब, नाच-गाना सब चलता है।\"
दादी के द्वारा दी इस ख़बर से अम्मा चौंक पड़ीं-\"और कुँवर राजा?\"
\"जब बाप नाच-रंग में सना है तो क्या बेटा अछूता रहेगा? यहीं कह रहा था संध्या से कि जब उषा जोधपुर लौटेगी तो वो जश्न मनाया जाएगा कि सब देखते रह जाएँगे। दूर-दूर के मेहमानों को न्यौता जाएगा, रात भर महफिलें सजेंगी, तवायफ़ें नाचेंगी।\"
अम्मा ने अपने कानों को हाथ लगाया-\"हाय राम।\"
ज़मींदार घराना तो प्रताप भवन में भी बसा है लेकिन बाबा-दादी की सादगी और पवित्रता के क़िस्से दूर-दूर तक मशहूर हैं और सादगी की यह परंपरा पड़बाबा प्रतापसिंह के समय से चली आ रही है। इस कोठी ने हमेशा सबकी मदद की, कभी किसी को सताया नहीं.....ईमानदार, बेदाग और नम्रता, इंसानियत के लिए मानी जाती है यह कोठी। न जाने बड़ी दादी का स्वभाव ऐसा कैसे हो गया?
सूरज की पहली किरण ने जब धरती को छुआ और बगीचे के सारे फूल जब शबनम से नहा चुके तो अम्मा के कमरे के पिछवाड़े बने सोहर घर के बच्चे के रोने की आवाज़ पूरी कोठी में फैल गई। प्रताप भवन जाग गया। मैं और रजनी बुआ दौड़ी-दौड़ी नीचे आईं तो पन्ना को फुर्ती से रसोईघर की ओर जाते देखा। वह वहीँ से चिल्लाई-\"भाई आया है पायल बिटिया, तुम्हें छेड़ने।\"
सचमुच मानो खुशियों का जखीरा खुल गया था.....सब इधर से उधर दौड़ रहे थे। अफ़रातफ़री मची थी। रसोईघर में महाराजिन मोतीचूर के लड्डू और घेवर बना रही थी। पन्ना कोठी के गेट पर बड़ी-सी रंगोली सजा रही थी और उषा बुआ पर फूलों की वर्षा करने के लिए जसोदा गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़कर चाँदी की थाली में रखती जा रही थी। दस बजे तक शहनाई वाले आ गए और कोठी पर बधाई देने आने वालों का ताँता लग गया। अंग्रेज़ पुलिस कमिश्नर ने अपने सिपाहियों को भेजकर कोठी के अहाते में बंदूकों से सलामी दागी। अनुपम दृश्य था।
मैं देख आई थी अपने भैया को। छोटे से पालने में मख़मली बिछावन पर आँख मूँदे सो रहा था। एकदम गुलाबी, पूरे चेहरे, माथे पर सिकुड़नें.....छूकर देखा तो रुई के बंडल जैसा लगा.....मैंने बुआ को बधाई दी-
\"बुआ.....आपने मुझे बबुआ दिया इसका शुक्रिया।\"
उषा बुआ मुस्कुरा दीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, एकदम कमज़ोर, बेजान-सी लग रही थीं वे। धीमे से बोलीं-\"तुम्हें भाई मुबारक हो.....बहुत प्यारा नाम दिया तुमने इसे बबुआ।\"
और पूरी कोठी में ख़बर फैल गई कि पायल ने नामकरण भी कर दिया.....प्यारा-सा गुड्डा जैसा बबुआ।
दोपहर होते-होते नृत्यमंडली आ गई। ख़ास राजपूती पहनावे में पगड़ी बाँधे मर्द और बड़े-बड़े घाघरे पहने औरतें.....खूब सजी-धजी। माथे पर लड्डू जैसे बोर बँधे थे चाँदी के। बौर की डोरी के साथ मेंढ़ी भी गूँथी गई थी। कोहनी तक चूड़ियाँ, बाजूबंद,कड़े। नाच दो घंटे चला। जब खाने-पीने से सब निपट गए.....मेहमानों की ख़ातिर-तवज्जो हो गई तो बड़ी दादी ने नर्तकियों को कोठी के अंदर बड़े आँगन में बुलाया। खुद व्हील चेयर पर बैठ गईं। मारिया, कंचन, जसोदा, पन्ना ने घर की सभी महिलाओं के लिए कुर्सियाँ रखीं। दादी ने सौ का नोट जसोदा को न्योछावर करने को दिया तो उनमें से एक नर्तकी उनके पास आकर घुटनों के बल बैठ गई-\"हम खुद ही आ जाते हैं बड़ी मालकिन।\"
बड़ी दादी ने सौ का नोट उसके सिर पर घुमाया-\"अब नाचो तुम लोग।\"
नाच क्या था.....करतब था सर्कस जैसा। छोटी-सी परात के किनारों पर दोनों पैर जमाकर वह नाचने लगी, चकरघिन्नी-सी। न परात मुड़ी न वह गिरी। जब उसका नाच ख़तम हुआ तो दूसरी कुलाटियाँ खाने लगी और मुँह में उंगलियाँ फँसाकर अजीब-सी आवाज़ें निकालने लगी, तीसरी ने सात घड़े एक के ऊपर एक सिर पर जमाए और ठुमक-ठुमककर नाचने लगी। सबने तालियाँ बजाईं। कंचन, जसोदा साथ-साथ गीत गाने लगीं, पन्ना नाचने लगी। नाचते-नाचते दादी के पास गई-\"हुकम.....मेरे सोने के कर्णफूल.....चाँदी की पाजेब?\"
\"सब तैयार हैं, आज तू जी भर कर नाच।\"
कहती हुई दादी ने कंचन को अंदर भेजकर गहनों का डिब्बा मँगवाया और पन्ना को थमा दिया। नीले मख़मल के डिब्बे को पन्ना ने बड़ी उतावली से खोला तो उसका चेहरा फूल-सा खिल पड़ा। मीना जड़ी चाँदी की पाजेब और मोगरे के फूल जैसे सोने के कर्णफूल। वह बावरी हो गई और कमर को ठुमके दे-देकर लचकाने, मटकाने लगी।
सावन के काले कजरारे मेघ झम-झाम बरस रहे थे.....इस साल अच्छी बरसात हो रही थी। सूखे मरू न जाने कब के प्यासे थे जो सारा पानी सोखते चले जा रहे थे। गर्मी से पपड़ाई ज़मीन मुलायम होकर घास के अंकुर उलीचे दे रही थी। रह-रहकर बिजली चमकती और पल भर में बादल कड़कड़ाने लगते। उषा बुआ तीज़ों तक नहीं रुक रही हैं। फूफासा लेने आ गए हैं। बता रहे हैं कि कल नहीं लिवा ले गए तो फिर महीनों के लिए मुहूर्त टल जाएगा। मुहूर्त तो बस बहाना है, सच्चाई तो यह है कि उनकी सास का हुकुम है तीजों के पहले बहू घर आ जाए.....जश्न मनाने को उतावले हो रहे होंगे सब। तवायफें दम साधे होंगी कि कब बुलावा आए और कब जाएँ? जश्न का कुछ-कुछ हवाला तो मैंने फूफासा से सुन ही लिया था। मुझे लगता है, इंसान को.....ख़ासकर अमीरों को अपने धन की ताकत दिखाने का मौका भर मिलना चाहिए। मैं इस धन के मोह से अपने को दूर रखूँगी। मेरे लिए ज़िंदगी में और भी दो चीज़ें ज़रूरी हैं। प्यार और ज्ञान की खोज। इसीलिए मेरे दिल में संध्या बुआ और अजय का महत्व ज़्यादा है। भले ही उनका प्यार तूफान बनकर उन्हें यहाँ-से-वहाँ भटका रहा है पर मुझे यक़ीन है एक दिन तूफान थमेगा और उन्हें किनारा मिलेगा।
बाबा ने बनारस से लौटकर बताया कि आज़ादी की क्रांति तेज़ी पकड़ रही है। पूरा देश सुलग रहा है। बनारस में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने तिरंगा हाथ में लेकर फौजदारी अदालत पर उसे फहराने के संकल्प में पुलिस के हंटर खाए। लाठियाँ खाईं। उन्हें सड़कों पर घसीटा गया लेकिन लालूराम फौजदारी अदालत पर झंडा फहराने में कामयाब हुआ। उसकी कामयाबी के पीछे भी अंग्रेज़ों की चाल थी वरना गोलियों से भून दिया जाता वह। ब्रिटिश साम्राज्यवाद जनता को खुश देखना चाहता था और अगर एक खिलौने के फहराने से जनता खुश होती है तो इसमें हर्ज़ ही क्या है? वह कोई खज़ाना तो माँग नहीं रही। मिश्रीनाथ और लालूराम के नेतृत्व में दशाश्वमेध घाट से जुलूस निकला और तब अंग्रेज़ों ने लाठी, बंदूक से काम लिया। बहुत सारे व्यक्ति शहीद हो गए। मिश्रीनाथ और लालूराम बाल-बाल बच गए। उत्तेजित भीड़ ने टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए, खंभे उखाड़ डाले, क़रीब-क़रीब सभी स्टेशन लूट लिये और ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ डालीं। राजवाड़ी और बाबतपुर के हवाई अड्डे भी नेस्तानाबूत कर दिए। डाकखाने, पुलिस चौकियाँ, गोदाम वगैरह लूट लिये। जी.टी.रोड पर फौज के जाने पर रूकावट डालने के लिए गड्ढे खोद दिए गए। पुलिस ने छिपकर गोलियाँ चलाईं तो क्रांतिकारी ज़मीन पर लेट गए लेकिन पुलिस के हाथ एक घायल तक नहीं लगा। इन लेटने वालों में बाबा भी थे लेकिन बदले हुए वेश में। बौखलाई हुई पुलिस ने राजामें काफ़ी तूफान मचाया। महिलाओं पर भी अत्याचार किया। उन्हें नंगी करके पीटा गया। सुनकर दादी उत्तेजित हो गईं- रौरव नरक भी न मिलेगा इन राक्षसों को।
\"और जानती हो, इन पुलिस वालों में अधिकतर तो भारतीय ही थे जो घोड़े पर चढ़े अंग्रेज़ अफसर के इशारे पर यह सब कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से ज़बरदस्ती हॉस्टल खाली करवाए और उनका सामान भी लूट लिया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मिश्रीदत्त के पास काफ़ी तादाद में देवमड़िया से ट्रेंड क्रांतिकारी मैंने भेजे हैं और हथियारों का ख़ासा जख़ीरा भी।\"
\"ले कैसे गए इतने हथियार तुम?\" दादी ने आश्चर्य से पूछा-\"जाते समय तो ऐसे गए थे तुम जैसे किसी के घर मेहमान बनकर जा रहे हो?\"
\"यही तो ख़ासियत है महारानी कि साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम अंग्रेज़ की जड़ें भी हिलाते रहें और उनके दोस्त भी बने रहें। देवमड़िया के क्रांतिकारी ही गुप्त रूप से रिवॉल्वर, कारतूस के टिन, राइफल, दोनाली बंदूकें, करौलियाँ, बारूद, बम, हथगोले वगैरह ले गए.....बस, अब देश की आज़ादी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।\"
बाबा ने मेरी ओर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर शपथ दिलवाई कि प्रताप भवन की सरगर्मियों और आज़ादी के प्रयास न नौकर-चाकरों को पता चलें, न प्रताप भवन के बाहर किसी को, रिश्तेदारों तक को नहीं।
दादी मुस्कुराईं-\"अरे.....उससे कैसा डर?.....वह तो पुरखिन है पूरी.....\"
बाबा भी मुस्कुराए लेकिन फिर तुरंत फुसफुसाकर बोले-\"अब हमें खूब सतर्क रहना है। आंदोलन ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। मालवगढ़ इस दृष्टि से थोड़ा शांत है फिर भी कहाँ, कब, क्या घटित हो जाए कहना मुश्किल है।\"
अचानक.....रोमांच से भरे माहौल में कुछ हलचल-सी हुई। सबने चौंककर दरवाज़े की तरफ देखा। बाबूजी थे।
\"आओ समर, बैठो।\" बाबा ने अपने बाजू में उन्हें बैठने का इशारा किया। बाबूजी ने बाबा, दादी के पैर छुए और बाबा के पास बैठ गए।
\"देवमड़िया का सब काम निपट गया।\" बाबूजी ने बताया।
\"बहुत अच्छा.....उस जगह को बिल्कुल नॉर्मल करवा दिया है न? कोई सुराग न मिले अंग्रेज़ों को वहाँ से।\"
\"सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक ख़तरनाक बात हो गई है।\"
सबने चौंककर बाबूजी की ओर देखा। सन्नाटा-सा खिंच गया माहौल में.....वक्त ही ऐसा था। किस पल क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। मुझे तो अंग्रेज़ों के घोड़ों की टाप ही लगातार सुनाई देती थी। जबकि सड़क निचाट और सूनी थी।
\"ताऊजी के उस अघोरी साधू की कुटिया से कुछ हथियार बरामद हुए हैं। जहाँ उसकी जलती थी उसके नीचे खोदने पर कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। असल में वह साधू के वेष में क्रांतिकारी था। हफ्ते भर से फ़रार है वह। पुलिस उसकी फ़िराक में है। कहीं ताऊजी पर मुसीबत न आ जाए।\"
बाबा चिंता में पड़ गए। देर तक बाबूजी से मशविरा चलता रहा। पहले तो यह पता किया गया कि बड़े बाबा घर पर हैं या नहीं। बड़े बाबा, बड़ी दादी के कमरे में बैठे उन्हें भागवत पढ़कर सुना रहे थे। फिर कोदू को अंग्रेज़ कलक्टर के बंगले पर भेजा गया कि ज़रूरी काम है, फौरन प्रताप भवन तशरीफ़ लाएँ।
बाबा बड़े हॉल में आ गए.....थोड़ी ही देर में अंग्रेज़ जीप से आ पहुँचा। अगवानी हुई.....कांधारी अनार का रस पेश किया।
\"आपको तकलीफ़ नहीं देते.....पर यह सब क्या हो रहा है? बड़े भाई साहब जिस साधु के यहाँ जाते थे वह भी साला क्रांतिकारी निकला।\"
अंग्रेज़ ने मूँछों की क्लीन जगह पर उँगली फेरी-\"वह भी गिरफ्तार हो जाएगा, जेल में चक्की पीसेगा।\"
बाबा की मुट्ठियाँ सोफे के हत्थे पर भिंच गईं।
\"आप चिंता न करें। मि. अमरसिंह (बड़े बाबा) को होशियार कर दें। वे दोबारा उस साधु की कुटिया में न जाएँ और अगर कहीं कोई सुराग मिलता है तो हमें तुरंत बताएँ।\"
\"बल्कि हम तो कहते हैं भाई साहब को आपकी मदद करनी चाहिए उसे ढूँढने में।\"
\"इसकी ज़रुरत नहीं है। हम प्रताप भवन की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ईमानदारी और वफादारी को अच्छी तरह समझते हैं।\"
बाबा ने अपनी बातों की तरकीब से अंग्रेज़ कलेक्टर के दिल में अपनी ईमानदारी का सिक्का जमा लिया। तब तक बंसीमल ने व्हिस्की, सोडे की बोतलें वग़ैरह टेबिल पर लाकर रख दी थीं। काफ़ी देर तक शराब का दौर चलता रहा। आश्वस्त होकर जब कलेक्टर उठा तो उसके पैर डगमगा रहे थे।
अगस्त क्रांति पूरे देश में वन में लगी आग की तरह फैल चुकी थी। बाबा के जरिए और कोठी में आने वाले अखबारों के जरिए सभी प्रांतों की ख़बरें मिल रही थीं। हालाँकि अखबार वही छप रहे थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार से ग्रीन सिग्नल मिला था। आधी सच्ची, आधी झूठी ख़बरों वाले अंग्रेज़ों के पिट्ठू अखबार मैं तो छूती तक नहीं थी। सभी जगह की क्रांति के किस्से सुने पर कलकत्ता की ख़बर नहीं सुनाई दी। संध्या बुआ बेचैन थीं और बाबा के आगे-पीछे घूम रही थीं। क्या बाबा को पता था कि अजय कलकत्ते में हैं? क्या जान-बूझकर वे कलकत्ते की ख़बरें छुपा रहे थे? नहीं.....भ्रम था मेरा.....ख़बरें शाम को मिल गईं। हम सब दादी के कमरे में दम साधे बैठे थे। बड़ा रोमांचक माहौल था.....मालवगढ़ में भी मिलिट्री लॉरियाँ घूमने लगी थीं। बाबा ने बताया-\"अब तक तो कलकत्ता शांत-सा था। लेकिन अचानक ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के वक्तव्य ने भड़का दिया। बंगाली विद्यार्थी यह सुनकर भड़क गए कि बंबई के अगस्त क्रांति मैदान में नेताओं के जोशीले भाषण, नारे और गिरफ्तारियों के बाद कलकत्ते में आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने शंकर घोष लेन और कार्नवालिस स्ट्रीट के संगम पर ट्राम गाड़ियाँ जलाईं। सभी जगह अंग्रेज़ों ने गोलियाँ बरसाईं। कई लोग शहीद हो गए।
\"विद्यार्थी आंदोलन में शरीक़ हैं तो.....प्रोफेसर, लैक्चरर भी.....और संध्या बुआ का चेहरा उतर गया। दादी भाँप गईं लेकिन बाबा के आगे कुछ कह न सकीं।
\"ज़बरदस्त उपद्रव किया क्रांतिकारियों ने। रेल यातायात, डाकखाने सब ठप्प कर दिए। टेलीफोन के तार काट दिए। सबसे भयंकर तो पंद्रह अगस्त का दिन रहा जब चित्तरंजन एवेन्यू से सैनिक लॉरियों ने उत्तेजित भीड़ पर लगातार गोलियाँ बरसाईं। हाथीबगान बाज़ार की मिठाइयों की दुकानों को लूटा। बड़ा भयंकर कांड रहा लेकिन सही-सही ख़बरें नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि अंग्रेज़ पुलिस ने संवाददाताओं, पत्रकारों को रिपोर्टिंग के लिए जाने नहीं दिया। केवल \'बंगला भारत\' अखबार से ही कुछ ख़बरें मिल पा रही हैं।\" संध्या बुआ रुमाल से माथे पर झलक आए पसीने को दबा-दबाकर पोंछने लगीं।
प्रताप भवन चिंता की गिरफ्त में था। बाबा दिन-रात चिंता से घिरे रहने लगे। खाना-पीना मानो छूट-सा गया था। दादी ज़बरदस्ती कुछ खिला देतीं तो चुपचाप खा लेते, फिर गहन सोच में डूब जाते। इन दिनों उनका काफ़ी सारा वक़्त तलघर में बीतने लगा था। वहाँ केवल दादी जा सकती थीं.....बाकियों के लिए तलघर की जानकारी नहीं के बराबर थी। बनारस की ख़बरें लाने का काम बाबूजी को सौंपा गया था। हालाँकि इस बात की पूरी सतर्कता रखी गई थी कि बाबूजी इस संग्राम में शामिल न हों वरना प्रताप भवन अनाथ हो जाएगा। रात दस बजे बुझे हुए चेहरे सहित बाबूजी ने बाबा को ख़बर दी कि बनारस में लालूराम सहित देवमड़िया के सत्रह क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें हंटर मारते हुए, सड़कों पर घसीटते हुए जेल ले जाकर ठूँस दिया गया है और बाबा.....मिश्रीदत्त.....
\"क्या हुआ मिश्रीदत्त को?\" बाबा उतावले हो गए।
\"बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने.....\"
\"हाँ-हाँ.....बोलो समर.....क्या हुआ उनको?\"
\"वे शहीद हो गए।\"
बाबा ने आँखें ज़ोर से बंद कर हाथ ऊपर उठा दिए-\"हे ईश्वर.....\" लेकिन तुरंत ही सम्हलकर जोशीले स्वर में बोले-\"भारत माता की जय।\"
हम सभी एक स्वर में बोल पड़े-\"भारत माता की जय।\"
\"मिश्री, तुम अमर हो गए.....शहीद.....अमर शहीद.....लेकिन इतनी जल्दी मुझे अकेला छोड़कर तुम चले गए कि.....\"
और बाबा फूट-फूटकर रो पड़े। बाबा को मैंने पहली बार रोते देखा। मेरी भी आँखें भर आईं.....आँखें सभी की भर आईं थीं। दादी, बाबूजी, रजनी बुआ, संध्या बुआ.....सभी सकते में थे। अचानक बाबा उठे.....अपने टेबिल के पास गए। किताबों में दबी मिश्रीदत्त की तस्वीर निकाली और सामने रखकर धीरे-धीरे बुदबुदाने लगे-
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः .....उस रात बाबा ने मुँह तक नहीं जुठारा.....मुँह तो प्रताप भवन में किसी ने नहीं जुठारा। यहाँ तक कि नौकरों तक ने नहीं। दादी गीता पाठ करती रहीं और बिस्तर पर लेटे बाबा सुनते रहे। बाबा बुरी तरह टूट गए से लग रहे थे। मानो महीनों से बीमार हों.....दूसरे दिन उन्हें बुखार आ गया। दादी ने एक पल के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वे बुदबुदाते रहते। \"क्या हुआ जो मेरा सब चला गया। मेरे वीर सैनिक, हथियारों का ज़खीरा, लालूराम जैसा देशभक्त और मेरा यार मिश्री.....लेकिन यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत आज़ाद होगा और मालविका तब तुम घी के दीये जलाना और आतिशबाज़ी छोड़ना।\"
\"मैं ही क्यों? तुम भी। हम सब मिलकर खुशियाँ मनाएँगे।\"
तभी रजनी बुआ ठुनकती हुई आईं और आकर सीधे बाबा के सामने खड़ी हो गईं-
\"चाचा सा.....मैं वकालत पढूँगी।\"
बाबा फीकी हँसी हँस दिए, दादी उनके तलवे सहला रही थीं।
\"आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं न्याय का साथ दूँ।\"
बाबा ने अपना हाथ बढ़ाया और रजनी बुआ का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया-\"क्यों नहीं चाहते हम? तुम्हें वकालत पढ़ना है.....ज़रूर पढ़ाएँगे।\" और दादी की ओर देखते हुए ठहाका लगाकर हँसते हुए बोले-
\"सुना तुमने.....हमारी चिरैया वकील बनेगी, काला कोट पहनेगी.....अदालत में जिरह करेगी.....एँऽऽऽ.....\"
और हँसते-हँसते उन्हें ठसकी लग गई। दादी पीठ सहलाने लगी, रजनी बुआ दौड़कर पानी ले आई.....ठसकी भयंकर थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आँखें लाल हो गईं, आँसू निकल पड़े, माथे की नसें फूल गईं और सारा शरीर पसीने में नहा उठा। इधर बाबूजी घबराकर डॉक्टर लाने दौड़े.....नौकर-चाकर सब भाग-दौड़ करने लगे.....बिजली की गति से पूरे प्रताप भवन में ख़बर पहुँच गई बाबा की तबीयत ख़राब होने की। बाबा ने खाँसते-खाँसते खून की उल्टी की और कटे पेड़-से पलंग पर गिर गए। दादी रो पड़ीं-\"हे ईश्वर.....यह क्या हो गया इन्हें?\"
कोठी में हड़कंप मच गया। मिनटों में बाबूजी डॉक्टर को ले आए। जांच के दौरान कोठी में ऐसा सन्नाटा था कि सुई भी गिरे तो आवाज़ हो। दम साधे सब डॉक्टर की ओर देख रहे थे। डॉक्टर ने दवाई दी.....इंजेक्शन लगाया और उनके सिरहाने कुर्सी पर बैठ गए। बैठने से पहले बाबूजी को अलग ले जाकर बता दिया कि \"हार्ट अटैक है.....अभी ख़तरा टला नहीं है। हम ख़तरा टलने तक यहीं बैठेंगे। अप ये दवाएँ मँगवा लें।\"
तुरंत बंसीमल को दवा लाने दौड़ाया। दादी सीधी मंदिर में जा बैठीं और प्रार्थना करने लगीं। बाबूजी ने हम सबको भी सोने के लिए कहा। बेमन से हम कमरे की ओर जा ही रहे थे कि बाबा की लंबी-लंबी साँसों की आवाज़ फिर सुनाई देने लगी। मैं दौड़कर दादी को मंदिर से बुला लाई। लेकिन उनके आते-आते बाबा तेज़ी से छटपटाकर शांत हो चुके थे। डॉक्टर ने नाड़ी देखी.....और अंतिम प्रयास में जुट गया लेकिन वह शांति चिर शांति थी। बाबा हमें छोड़कर जा चुके थे। दादी की लंबी चीत्कार से प्रताप भवन सहम उठा। दीवारें, फ़र्श, छत, दरवाज़े, बरामदे, सहन.....हर जगह, हर इंच धरती पर मातम छा गया। सभी स्तब्ध थे। यह क्या हुआ? कहीं यह डरावना, झूठा स्वप्न तो नहीं लेकिन स्वप्न के बाद आँख भी खुलती है और जब आँख खुलती है तो सच्चाई सामने आती है। बाबा देश की आज़ादी का ख़्वाब लिये चल दिए। शायद वे अपने दल का बलिदान, मिश्रीदत्त का बलिदान सह नहीं पाए, शायद उन्होंने एक साथ जीने-मरने की क़समें खाई थीं। इसीलिए बिना देर किए वे भी चल दिए। पूरी कोठी मातम और रुदन में डूब गई। दादी ने अपना सिर दीवार पर दे मारा.....मैं और रजनी बुआ दादी से लिपट गईं और रोने लगीं। खूब रो चुकने के बाद दादी ने आहिस्ता से अपने को हम लोगों से छुड़ाया और बाबा के शव के पास जाकर अपना चूड़ियों भरा हाथ फर्श पर पटकने को उठाया ही था कि तेज़ी से व्हील चेयर लुढ़काती बड़ी दादी आईं-\"क्या अपशगुन करती हो दुलहिन.....तुम तो सती हो सती.....\"
उनके मुँह से ये शब्द सुनकर सब सकते में आ गए। बाबा के देहांत के सदमे से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि ऐसी चुभती बात!
\"क्या कह रही हो माँ?\" संध्या बुआ ने उनके दोनों कंधे पकड़कर झकझोर दिए-\"जानती भी हो क्या कह दिया अनजाने में.....\"
\"अनजाने में क्यों? पूरे होशोहवास में कहा है। क्या हमारे ख़ानदान में कोई सती नहीं हुई? क्या गुलाब कुँवर मासी सा को सब इतनी जल्दी भूल गए?\"
और मेरे तलुवों के नीचे पसीना छूटने लगा.....यह कैसी करुणा जताई बड़ी दादी ने? यह कैसा मरहम लगाया दादी के ताजे घाव पर कि घायल को ही मिटा डालने का बीड़ा उठा लिया। मेरी रग-रग उत्तेजित हो उठी। मेरे कलेजे में एक बवंडर-सा उठा और मैंने देखा कि मैं हाथ में तलवार लिये एक बहुत बड़े महल के प्रांगण में खड़ी हूँ। जहाँ जौहर की आकाश चूमती लपटें उठ रही हैं और राजपूत स्त्रियाँ सोलहों श्रृंगार किए ओम् का उच्चारण करती उसमें कूदने को तत्पर हैं और जब मुझे जौहर की अग्नि में ढकेला जाने लगा तो मैं चीख पड़ी-\"ख़बरदार जो किसी ने भी मुझे हाथ लगाया। मैं रणभूमि में शहीद होऊँगी। मैं इस तलवार से दुश्मनों को मारकर वीरता भरी मौत को गले लगाऊँगी। तुम लोगों की तरह कायरता भरी मौत नहीं.....छोड़ दो मुझे.....मत जलाओ.....मत जलाओ दादी को..... दादीऽऽऽ\"
जब होश आया तो देखा अम्मा और जसोदा मेरे कमरे में थीं। और मेरा सिर अम्मा की गोद में था। अम्मा मुझे देखती रहीं। जाने कब हम दोनों लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़े। जसोदा बिलख रही थी-\"अरे मोर मैया.....अरे परमेसर.....ये सब क्या हो गया? कोई भूत प्रेत का साया लग गया रे.....\"
बाबा की मौत से कहीं अधिक बड़ा सदमा था बड़ी दादी का दादी के प्रति लिया निर्णय। प्रताप भवन के हर शख़्स की आँखों में सन्नाटा था लेकिन वो सन्नाटा चीखकर कह रहा था कि ये अन्याय है.....अत्यंत दयालु, सब पर प्रेम की वर्षा करने वाली, सबकी मददगार मेरी दादी के लिए ये लोमहर्षक निर्णय सबको झँझोड़े डाल रहा था। बाबा का ग़म तो सब भूल गए.....अब सीने में सिसकियाँ थीं तो दादी के लिए। मेरे शरीर में चिन्गारियों का तूफान उठ रहा था जिसे आग बनने से मैं रोके थी.....क्योंकि मेरा अस्तित्व अभी छोटा था और मेरी बात में वज़न नहीं था कि मैं बड़ी दादी के निर्णय पर युद्ध छेड़ सकूँ।
पूरे इलाक़े में ख़बर फैल गई कि दादी सती हो रही हैं। दादी तब अड़तालीस वर्ष की थीं.....लेकिन पैंतीस से ज़्यादा की नहीं लगती थीं। ईश्वर ने उन पर दोनों हाथों से रूप का ख़जाना लुटाया था। दादी के महान कल्याणकारी कार्यों ने इस सौंदर्य में और इज़ाफा कर दिया था। अब तक उन्होंने बाबा की मौत के हादसे को स्वीकार कर लिया था। आँसुओं की लकीरें और होंठ पपड़ा गए थे.....हिम्मत करके वे बड़ी दादी के क़दमों पर गिर पड़ीं-\"नहीं जीजी.....इतनी कठोर न बनो.....मैं सती होना नहीं चाहती।\"
अभी उनके मुख से शब्द पूरी तरह निकले भी न थे कि बड़ी दादी का भरपूर हाथ उनके होठों पर आ गया। घुट गए उनके शब्द। बड़ी दादी ने घोट डाला दादी को जीते जी..... दुश्मन थीं वे पिछले जन्म की.....सारी उम्र कोसती-काटती बिस्तर पर पड़ी-पड़ी सेवा कराती रहीं। नौ वर्ष की थीं दादी जब बालिका वधू बनकर इस कोठी में आई थीं। शादी का अर्थ तक नहीं जानती थीं तब वे और बड़ी दादी पहले से ही कोठी की चाबियाँ समेटे राजरानी बनी बैठी थीं। बीमार, ज़िद्दी, चिड़चिड़ी बदमिज़ाज।.....पलंग पर ही हगना, मूतना, स्पंज, दवादारू.....दादी ने कभी घिन न जताई.....नौकर-चाकर समय पर नहीं आ पाते तो खुद ही कर देतीं उनका काम, कलेजे से लगाकर रखा उनको और वक़्तका मज़ाक कि आज वही उनको ज़िंदा जलाने को चिता सजाए बैठी हैं।
दोपहर तक प्रताप भवन सगे-संबंधियों, नाते-रिश्तेदारों से खचाखच भर गया। ख़ानदान की तमाम ममेरी, फुफेरी मामियों, चाचियों, चाचा, फूफा, ताऊ और जाने कौन-कौन से देखे अनदेखे रिश्तों की भीड़ ने दादी को सती होने को उकसाया।
\"मालविका को सती हो जाना चाहिए.....ये पुण्य का काम है। सीधे मोक्ष मिलेगा। यही तो हम राजपूतों की आन-बान-शान का प्रतीक है।\"
\"हाँ.....हाँ.....हमारे शेखावाटी के झुँझुनू नगर में नारायणी देवी का मंदिर भी इसी बात की गवाही देता है।\"
\"अरे महासती नारायणी देवी के सत का तो कहना ही क्या.....खुद ही बैठ गई थीं वो तो चबूतरे पर अपने पति का सिर गोद में रखकर और किसी ने चिता को अग्नि नहीं दी थी बल्कि खुद ही अपने सत् के बल पर अपने हाथ के चुड़े से अग्नि प्रगट कर देवसर की पहाड़ी पर महासती हो गई थीं।\"
जितने मुँह उतनी बातें। सुन-सुनकर मेरा दिमाग भन्नाने लगा। मन में आया कि कहूँ कि खुद अपनी मर्ज़ी से सती होने और ज़बरदस्ती सती कराने में ज़मीन-आसमान का फर्क है.....हत्या है हत्या.....पर.....होंठ बंद थे मेरे.....कुछ भी कहना छोटा मुँह बड़ी बात होती। मुझे तो ताज्जुब था अम्मा बाबूजी पे.....वे क्यों नहीं कहते कुछ?
\"क्यों आप सब चाहते हैं कि मैं सती हो जाऊँ? मेरे बाद इस कोठी का क्या होगा? कौन देखभाल करेगा इसकी? उनके अधूरे कामों को कौन पूरा करेगा?\"
दादी उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थीं जिनके दुखों में दादी एक फौजी की तरह डटी रहती थीं.....लेकिन उन लोगों पर क्या असर होना था जो स्वयं ठंडे पायदानों पर खड़े आग में जलने का तमाशा देखने को उतावले थे। बड़ी दादी ने दादी को कृष्ण के मंदिर में बैठा दिया।
रजनी बुआ और संध्या बुआ रो-रोकर बेहोश-सी हो गई थीं। संध्या बुआ को तो बुखार चढ़ने लगा था.....सिर दर्द से फटा जा रहा था और वे रह-रहकर उल्टियाँ कर रही थीं। उषा बुआ अपने डेढ़ महीने के बबुआ को दूध तक नहीं पिला पा रही थीं। वह चिंघाड़-चिंघाड़कर कोठी सिर पर उठाए ले रहा था। अम्मा और बाबूजी का कमरा अंदर से बंद था.....शायद अपने भीरूपन की ग्लानिवश.....शायद हम सबसे नज़रें न मिला सकने की अपनी मजबूरीवश।
मैं जसोदा के आँचल में दुबकी बैठी लगातार सिसक रही थी.....बाबा की मृत्यु का समाचार सुनकर मारिया और थॉमस आए थे.....मगर यहाँ तो नज़ारा ही दूसरा था। मारिया ने जो कुछ देखा, सुना.....उससे वह घृणा से भर उठी बड़ी दादी के प्रति। वह निडर, साहसी लड़की सीधी बड़ी दादी के पास गई-\"आप हत्यारी हैं.....छोटी आंटी की सबसे बड़ी दुश्मन..... मनुष्यता और दयालुता से कोसों दूर.....इसीलिए आप बीमार हैं.....आप कभी अच्छी हो ही नहीं सकतीं। छोटी आंटी की हत्या तो आप बाद में करेंगी पहले मेरे सिर फूटने का तमाशा देखकर तो खुश हो जाइए.....\"
और मारिया दीवार पर ज़ोर-ज़ोर से अपना सिर पटकने लगी। खून उबाल खाकर माथा, चेहरा भिगोने लगा.....उषा बुआ चीखीं-\"अरे, कोई बचाओ।\"
चीख सुनकर दासियाँ दौड़ी आईं.....मारिया ने किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। वह तेज़ी से यह कहती हुई प्रताप भवन के गेट से बाहर निकल गई कि अब वह कभी इस कोठी में क़दम नहीं रखेगी। उसे छोटी आंटी की शपथ है।
आकाश जब खून से रंग उठा, भुतहा अँधेरा धीरे-धीरे मनहूस कोठी को लीलने लगा। हवा सहमी-सी बहने लगी और सड़क के उस पार ठूँठ आम की जड़ों पर जब सियार सिर पटक-पटककर रोने लगे तब मंदिर की कोठरी से दादी को बाहर निकाला गया। दादी पीपल के पत्ते-सी थर-थर काँप रही थीं। कैसा क्रूर समाज है ये जो पतिव्रत धर्म के नाम ज़िंदा इंसानों को जला देता है और स्वयं रोम के नीरो बादशाह की तरह विनाश का उत्सव देख-देखकर रोमांचित होता है।
दादी का सोलहों श्रृंगार किया गया। बीच-बीच में जो वे रो-रोकर गिड़गिड़ाती जा रही थीं उसे बंद कराने के लिए बड़ी दादी ने उन्हें नशा करा दिया था।
\"कुकर्मी.....अगला जनम भी खटिया पर ही बीतेगा।\"
बड़ी दादी को कोसती कंचन दाँत पीसती जा रही थी और सुबकती जा रही थी।
अब तक दादी पत्थर हो उठी थीं। उनकी आँखें नशे के कारण लाल हो गईं। कोठी के आगे लोगों की विशाल भीड़ खड़ी थी। ढोल, नगाड़े, ताशे बज रहे थे। बैलगाड़ियों पर घी के कनस्तर लादे जा रहे थे। चंदन की लकड़ियाँ लादी जा रही थीं। हर आगंतुक के हाथ में फूलों की माला और नारियल थे। बाबा का शव शानदार राजसी ठाठ से सजाया गया था। शव कोठी के बाहर चबूतरे पर रखा था। जो भी दर्शन करने आता मुट्ठी भर फूल चढ़ाकर परिक्रमा करता। पूरा मालवगढ़ उलट पड़ा था। कोठी के सामने दरबान, कोदू, माली, महाराज, बंसीमल और रामू फूट-फूटकर रो रहे थे। अब न उनके मालिक रहे न मालकिन। अनाथ हो गए वे सब। अब कौन उनके आँसू पोंछेगा? कौन उनकी मुसीबतों में दौड़ा आएगा? मालकिन के सती होने के निर्णय पर वे विरोध करें भी तो कैसे? धर्म ने उनके पैरों में बेड़ियाँ डाल रखी थीं? और बाबूजी? अपनी जन्मदात्री के ज़िंदादाह के लिए होंठ सिये शव के पास खड़े थे.....न विरोध..... न बगावत.....एक मौन स्वीकृति.....मैं उनकी इस लिजलिजी हार से टूटकर बिखर चुकी थी और.....और जुलूस चल पड़ा। सहसा मैं पागलों की तरह दौड़ी-\"मत ले जाओ मेरी दादी को..... बाबूजी.....ताऊजी.....अरे बुआ.....रोको इन्हें.....बचा लो दादी को.....\"
और चीख़ते-सिसकते दहशत और डर से मेरी पेशाब निकल गई। मेरी सलवार पूरी भीग गई। लेकिन भीड़ पर कुछ असर नहीं हुआ और मेरे घिग्घी बँधे शब्द हवा में टूटे पत्ते की तरह भटकते रहे। लावारिस.....
दादी को ढकेल-ढकेलकर शवयात्रा के साथ सब ले जाने लगे। कोठी से जब शवयात्रा शुरू हुई, समवेत स्वरों में गगनभेदी नारा गूँज उठा-\"सती माता की जै.....जै सती भवानी की.....छोटी मालकिन जैसी तपस्विनी कौन होगी? शुद्ध पवित्र सती आत्मा है, हमारी तारनहार.....पूरे मालवगढ़ को तार दिया सती मैया ने.....जय हो.....\" कहते लोग शवयात्रा में शरीक़ हो रहे थे। मुझे और रजनी बुआ को अम्मा अपने गले से लगाए रो-रोकर पागल हुई जा रही थीं। क्या बाबा को कंधा देकर ले जाते हुए बाबूजी का दिमाग, आत्मा, सोच सब सुन्न हो गई थी? क्या नाते-रिश्तेदारों ने उनके पैरों में बेड़ियाँ डाल दी थीं.....क्या जल्लाद ने उनकी ज़बान खींच ली थी.....क्या उन्हें मालूम नहीं था कि यह हत्या है.....कोई उत्सव नहीं?.....नहीं, मैं बाबूजी को कभी माफ़ नहीं करूँगी और इस काल कोठरी में अब साँस लेना मेरे लिए पाप है।
लगभग चार-पाँच घंटों में अकेला कोदू दौड़ता आया.....हाँफता हुआ अम्मा के चरणों में गिर पड़ा।
\"गजब हो गया हुकुम।\"
अम्मा ने कुछ नहीं कहा.....वे उस वेदना से उबर नहीं पा रही थीं.....मेरी आँखों के आगे तो दादी को भस्म करती लपटें तांडव कर रही थीं।
\"सब लोग लौटकर आ रहे हैं। मालिक का दाह संस्कार हो गया। लेकिन.....\"
\"लेकिन क्या?\"
\"लेकिन.....छोटी मालकिन सती होने से बच गईं।\"
\"क्याऽऽऽ.....\"
अब सबके शरीर में चेतना आई। मैं खुशी से उतावली हो चीख-सी पड़ी-\"विस्तार से बताइए न कोदू काका।\"
कोदू हम सबको खुश देखकर आश्वस्त हुआ। उसने पूरी शवयात्रा का मानो चित्र-सा खींच दिया-
\"श्मशान भूमि के फाटक पर थोड़ी देर को शवयात्रा रुकी। एक बड़ी-सी थाली में महावर उँडेलकर उसमें दादी की हथेलियाँ रंगी गईं और फाटक पर उनकी दोनों हथेलियों की छाप उकेरी गई। बड़ी शानदार चंदन की चिता पहले से तैयार थी। सारे अंतिम कर्म करके मालिक को चिता पर लेटाया गया और जब मालकिन को चिता पर बैठाने लगे तो कुँवर सा (बाबूजी) ने अपना सिर पत्थर पर पटक लिया.....खून की धारें फूट पड़ीं.....पर किसे परवाह? सबका ध्यान तो छोटी मालकिन पर था। उन पर फूल और नारियल का ढेर-सा लग गया। ढोल, नगाड़े, ताशे ज़ोर-ज़ोर से बजने लगे। बीच-बीच में चमचों से उनके सिर पर घी उँडेलते हुए लोग चिता को छूते हुए सती माता की जय बोलते जा रहे थे। तभी हवा में बंदूक की गोलियाँ चलीं, लोग सहमकर पीछे हटने लगे। श्मशान घाट में सन्नाटा छा गया.....क्रांति की दहशत ने वैसे ही लोगों को सहमा रखा था.....अचानक चिता के पास एक घोड़ा आकर रुका और उस पर से अंग्रेज़ ऑफीसर जिम उतरा.....लोगों ने साँस रोककर देखा कि जिम ने एक हिकारत भरी निगाह भीड़ पर डाली और झटके से दादी को चिता पर से फूल की तरह उठा लिया..... हवा में फिर गोलियाँ दगीं और जिम ने दादी को घोड़े पर बैठाकर सरपट घोड़ा दौड़ा दिया..... बड़ी देर बाद भीड़ में हरकत आई.....आधे लोग तो डर के मारे चुपचाप खिसक लिये.....बाकी ने झटपट मालिक की चिता को आग दी। कुँवर सा के सिर से खून निकलने के कारण वे अर्धमूर्छित-से चिता के पास लाए गए थे और चिता की जलती लकड़ी उनके हाथ में पकड़ा चिता में छुला दी गई थी। तभी मारिया और थॉमस पुलिस लेकर वहाँ पहुँच गए। लेकिन हम तो हुकुम छोटी मालकिन के घोड़े के पीछे भाग रहे थे। हम उन्हें दिखाई थोड़ी दे रहे थे। पगडंडी से गए थे न हम।
छोटी मालकिन जिम की बाँहों में अचेत थीं। घोड़ा एक शानदार बंगले के सामने आकर रुका। बंगले के बाहर बरामदे में बिछे तख़त पर जिम ने मालकिन को लेटाया और अपनी नौकरानी से कहा कि वह उन पर लगा घी, सिंदूर सब स्पंज से साफ़ कर दे। फिर ख़ानसामे को डॉक्टर लाने दौड़ा दिया। हम तो पास की झाड़ी में दुबके सारा नज़ारा साफ़-साफ़ देख रहे थे। घंटा भर छुपे रहे झाड़ियों में हम। जब मालकिन अच्छी हो गईं तो सामने बैठे जिम को देखकर चौंक पड़ीं-\"मुझे आप क्यों ले आए यहाँ? क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। अब मैं कहाँ जाऊँ? प्रताप भवन मुझे क्यों स्वीकारेगा? समाज भी ठुकराएगा.....मैं अपराधिन हो गई.....पापिन हो गई।\" और वे रोने लगीं। जिम उनके पास आया। जेब से रुमाल निकालकर उनकी ओर बढ़ाया-\"लीजिए, आँसू पोंछ लीजिए। मैं हूँ न। मेरे रहते आपको रोने की ज़रुरत नहीं।\"
\"आप! आप कौन हैं मेरे? बोलिए.....\"
\"मैं आपके पति मिस्टर अभयसिंह का दोस्त हूँ। आपकी कोठी पर कितनी बार मैंने आपके हाथ का बना खाना खाया है। आप नहीं जानतीं.....मैं उसी दिन आपके रूप का दीवाना हो गया था जिस दिन अपने नौकर के हाथ सब्ज़ी का डोंगा पकड़ाते हुए बीच में पड़ा परदा उड़ गया था। वो पल भर का दर्शन मेरे जीवन की साध बन गया था.....मालविका.....कोहरे में लिपटी चाँदनी-सी आप नशा बनकर मेरे अंग-अंग पर छा गई थीं।\"
मालकिन ने कानों पर हाथ रख लिये-\"बस करिए.....मेरे लिए यह सुनना भी पाप है।\"
जिम अचानक उत्तेजित हो उठा-\"और वो पुण्य था जो आपके परिवार वाले आपके संग कर रहे थे? आपका मर्डर कर रहे थे सब मिलकर। मैं चाहूँ तो सबको फाँसी पर चढ़ा दूँ। है कोई ऐसा कानून जहाँ इंसान को ज़िंदा जलाना धर्म है? सच कहिए.....अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर कहिए कि आप अपनी मर्ज़ी से जलने को तैयार थीं? क्या आपके साथ जबरदस्ती नहीं की गई?\"
मालकिन ने सिर झुका लिया और फूट-फूटकर रो पड़ीं। फिर हमसे वहाँ रुका नहीं गया हुकम! मालकिन का रोना देखा नहीं जा रहा था।
कहते-कहते कोदू खुद भी रो पड़ा। आँसू तो हम सबके भी बहे जा रहे थे पर हमें उनका एहसास नहीं था। जो कुछ हुआ वह मेरे लिए सुखद था लेकिन अविश्वसनीय भी। पुलिस को खबर करके दादी को बचाने की मारिया की कोशिश ने मेरी नज़रों में उसके प्रति मान और बढ़ा दिया था।
जैसे ही श्मशान घाट से सब वापस लौटे, बड़ी दादी कलपने लगी-\"हे ईश्वर.....इस ख़ानदान की इज्ज़त मिट्टी में मिल गई। अब कैसे पार लगेंगे हम सब? अब कैसे बेटियाँ ब्याही जाएँगी? ऐसे कैसे हिम्मत पड़ी उस मुए फिरंगी की? मुझे तो दाल में काला नज़र आता है। आता तो था.....मुआ.....सींग उठाए रोज़ मिलने.....अब मैं बीमार। शरीर से लाचार। देखने वाला कौन? लो, कर लो देश को आज़ाद। अपनी दुलहिन तो सम्हाली नहीं गई। और रहो महीनों-महीनों घर से गायब.....कट गई न नाक।\"
\"चुप भी रहो माँ.....इतने रिश्तेदारों के सामने क्या अच्छा लग रहा है ये सब।\" संध्या बुआ ने उन्हें चुप कराना चाहा तो वे उसी पर बरस पड़ीं-\"तू भी उसी रंग में रंगी है, वैसे ही लच्छन हैं तेरे भी। घुसी रहती थी न चाची.....चाची करके उसके कमरे में।\"
उषा बुआ संध्या बुआ का हाथ पकड़कर ले जाने लगीं तो संध्या बुआ \'जीजी\' कहकर उनसे लिपटकर रोने लगी।
प्रताप भवन को जैसे साँप सूँघ गया। किसी की किसी चीज़ में रूचि नहीं रही थी। सब मानो ज़िंदगी ढो रहे थे और मैं पागल बनी प्रतीक्षा कर रही थी दादी के लौटने की, जबकि कोठी के दरवाज़े उनके लिए बंद हो चुके थे। कितना निर्मम था सब कुछ। हृदयहीन बड़ी दादी के उठे एक क़दम ने इंसानियत को कुचल डाला था.....हाँ मेरी दादी इंसानियत की पर्याय थीं। इस घर की देखरेख और रौनक उनसे थी। मुझसे तो उनके कमरे की ओर देखा भी नहीं जा रहा था। जहाँ हमेशा दादी की उपस्थिति छत्र बनकर सब पर छाई रहती थी वहाँ अब जानलेवा सन्नाटा पसरा था। जानती थी, उनके बिना अब इस कोठी को भुतहा तब्दील होने में समय न लगेगा। मैंने पहली बार कोठी से बाहर अकेले घूमने का सोचा.....निरुद्देश्य.....शायद कुछ तसल्ली मिले। नहीं, किसी से मैंने जाने के लिए पूछा नहीं.....हाँ, अम्मा को जता दिया था कि एक-दो घंटे में लौटूँगी। बग्घी तैयार थी। थोड़ी देर यूँ ही सड़कों पर बग्घी दौड़ती रही फिर मैंने मारिया के सेवा केंद्र जाने का आदेश दिया। सेवा केंद्र खूब हरा-भरा हो गया था। गेट पर लगे बोगनबेलिया में पीले, सफेद और मजंटा फूल खिले थे। बग्घी गेट पर रुकी। उतरते-उतरते मैंने चकित होकर देखा, सेवा केंद्र के गुम्बद के नीचे बहुत बड़ा बोर्ड लगा है-\"मालविका स्मृति केंद्र।\"
अभिभूत और आलोड़ित थी मैं.....मालविका के लिए प्रताप भवन के गेट पर ताला लगा है किंतु जन-जन के मानस में अंकित हैं वे.....मारिया.....मारिया.....मैंने खुशी में भरकर चीखना चाहा। सामने थॉमस दिख गया।
\"मिस पायल! आप!!\" और वह मुझे मारिया के केबिन में ले गया। मारिया कुर्सी पर बैठी रजिस्टर में कुछ लिख रही थी।
\"आइए.....पायल बाई।\"
उसने उठकर मुझे गले से लगा लिया। उसके माथे की चोट पर काली खुरंट जम गई थी। मुझे अपने माथे की ओर देखते पा वह हँस पड़ी-\"ये आपके प्रताप भवन की निशानी है जिसे मैं कभी मिटने नहीं दूँगी क्योंकि ये मुझे याद दिलाती रहेगी कि वहाँ शैतान भी बसते हैं।\"
मैंने सिर झुका लिया।
\"छोटे साहब की डेथ का मुझे बहुत अफसोस है लेकिन इस बात की भी खुशी है कि छोटी आंटी सुरक्षित हैं। आपको पता है मैंने पुलिस बुला ली थी वहाँ। अगर मिस्टर जिम नहीं आते तो मैं छोटी आंटी को पुलिस की मदद से यहाँ ले आती। ओह.....भयानक! भयानक दृश्य था वह.....चिता के बीचोंबीच ज़िंदा इंसान का बैठे होना और जलने की प्रतीक्षा.....\"
\"मारिया.....प्लीज़.....कंट्रोल करो.....ये समय पायल बाई को सांत्वना देने का है।\" थॉमस ने कहा।
\"ओह.....सॉरी! मैं.....मैं बहक गई थी.....कुछ पिएँगी आप?\"
\"मैं कुछ लेकर आता हूँ।\"
और थॉमस फुर्ती से चला गया।
\"तुमने तो मारिया.....शपथ ले ली है वहाँ न आने की?\" अब बड़ी दादी का क्या होगा?\"
\"अच्छा! उन्हें है ज़रुरत तीमारदारी की?\" मारिया ने व्यंग्य से कहा।
मैं कटकर रह गई।
\"पायल बाई.....मेरा व्रत ग़रीब, लाचार और शारीरिक तौर पर असहाय लोगों की मदद करना है और बड़ी आंटी ऐसी तो नहीं हैं.....बड़ी कठोर शक्ति है उनमें। एक हँसती-खेलती ज़िंदगी को राख कर देने की शक्ति है उनमें। बल्कि अब तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे मरीजों पर उनकी छाया भी न पड़े।\"
मेरा दिल कतरा-कतरा हो गया और हर कतरे से खून रिसने लगा। मैं बिना खून की होने के लिए तड़प उठी। सुना है.....बिना खून का इंसान पल भर भी जी नहीं पाता।
\"पायल बाई.....छोटी आंटी के साथ जो कुछ हुआ उसे मैं भूल नहीं सकती। मैं उनसे मिलने मिस्टर जिम के बंगले पर गई थी। पता चला उन्होंने छोटे साहब की डेथ के बाद से भोजन को हाथ भी नहीं लगाया है। रो-रोकर बुखार चढ़ा लिया है। माथे में भयंकर दर्द.....आँखें शोलों जैसी दहक रही थीं। जिम ने डॉक्टरों की भीड़ इकट्ठा कर ली थी पर न वे दवाई खा रही थीं, न इंजेक्शन लगवा रही थीं। मेरे पहुँचते ही टकटकी बाँधकर मुझे देखने लगीं। मैं उनसे लिपट गई तो उनकी आँखों से जैसे आँसुओं का सोता फूट पड़ा-\"आंटी, प्लीज़ मत रोइए।\"
\"मारिया, मैं मर क्यों न गई.....इस तिल-तिल जलने से तो एक साथ, एक बार में ही जल मरना अच्छा था। क्या तुम्हारे साहब मुझे माफ़ करेंगे? उनकी आत्मा कलपती होगी।\"
\"आंटी.....आपको तसल्ली रखनी होगी। आंटी सब ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे।\" मैंने झूठी तसल्ली देनी चाही तो वे बिफर पड़ीं-\"नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा.....छूट गया मुझसे सब कुछ.....मेरा घर द्वार.....मेरे बच्चे.....पायल, संध्या.....क्या बिगाड़ा था मैंने जीजी का जो मुझे सती करना चाहा उन्होंने? मैंने तो अपनी तरफ से उन्हें कोई दुःख नहीं दिया कभी! इनकी मृत्यु के बाद मेरे आँसू पोंछने की जगह मुझे मार डालने की साजिश?\"
कहते-कहते उनका सारा शरीर पत्ते-सा काँपने लगा और पूरा चेहरा आँसुओं से भर गया। पायल बाई.....इतने सारे गाँवों के ज़मींदार ख़ानदान की छोटी आंटी की ऐसी दुर्दशा की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं अपने रुमाल से उनके आँसू पोंछती रही।
\"मारिया.....पल के पल में सब कुछ ख़तम हो गया मेरा। कल तक मेरा संसार आसमान की ऊँचाई तक था.....आज पैरों के नीचे की धरती भी छिन गई। त्रिशंकु बनी मैं निर्वासन झेलने को विवश हूँ।\"
अब मैं भी अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। देर तक उनके साथ मैं भी रोती रही। थोड़ा नॉर्मल होने पर मैंने अपना मुँह धोया, उनका चेहरा गीले तौलिए से पोंछा और अपनी कसम दिलाकर दो-चार निवाले ज़बरदस्ती उनके गले के नीचे उतारे। फिर दवा खिलाई, इंजेक्शन लगाया। थोड़ी राहत मिलने पर वे सबके बारे में पूछती रहीं। आप बहुत याद आती हैं उन्हें पायल बाई.....बस यही बोलीं-कि \'न जाने क्या होगा संध्या का?\' और चुपचाप लेट गईं। मैं उनका सिर सहलाती रही। जब वे सो गईं तो मैं आहिस्ता से उठकर बाहर आ गई। मिस्टर जिम कार से मुझे सेवा केंद्र छोड़ गए। रास्ते में बताने लगे कि किसी भी तरह सम्हल नहीं रही हैं मालविका.....डरता हूँ, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। अगर प्रताप भवन उन्हें वापस बुला ले तो मैं खुद बड़े सम्मान के साथ उन्हें वहाँ छोड़कर आऊँगा। मैं आशंका से भर गई, कहीं प्रताप भवन में उन्हें प्रवेश नहीं मिला तो वह स्थिति छोटी आंटी के लिए बड़ी शर्मनाक होगी ख़ासकर मिस्टर जिम के सामने। मैंने कहा-
\"नहीं, ऐसा सोचिए भी मत। अब वे आपके साथ ही रहेंगी, मैं उन्हें मना लूँगी। मैं रोज़ उनकी देखभाल के लिए आऊँगी। आप चिंता न करें। थोड़ा वक़्त गुज़रने दीजिए। सब ठीक हो जाएगा।\" जिम के चेहरे पर चमकती आस मैंने साफ़ देखी। पायल बाई.....मैं रोज़ जाती हूँ बिला नागा उनके पास। मिस्टर जिम तो फरिश्ता हैं, मैंने इतना भला इंसान छोटी आंटी के बाद यह दूसरा देखा।
जाने कब मारिया चुप हो गई, कब उसने मेरे बहते आँसू पोंछे, मुझे तसल्ली दी, कॉफी पिलाई और दादी की ख़बर देते रहने का वादा कर बग्घी में मेरे साथ मुझे कोठी तक छोड़ने आई। मेरे लाख इसरार करने पर भी बग्घी से वह नहीं लौटी.....पैदल ही आगे बढ़ गई.....उस सड़क पर जो जिम के बंगले की ओर जाती थी।
रात को मैंने अम्मा बाबूजी से कहा-\"मैं बनारस जाकर पढ़ना चाहती हूँ।\"
बाबूजी चौंके-\"बनारस?\"
अम्मा सहम-सी गईं-\"वह तो आंदोलन का गढ़ बना है और ज़्यादातर क्रांतिकारी विद्यार्थी ही हैं।\"
\"तो क्या हुआ? मैं भी क्रांति में भाग लूँगी। देश को आज़ाद करूँगी। बाबा के अधूरे काम को कोई तो पूरा करे।\"
थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। बाबूजी ने समझौते का रुख अपनाया- \"ठीक है, ये साल निकाल लो, अगले साल चली जाना।\"
\"नहीं बाबूजी मेरा मन नहीं लगता यहाँ.....मैं दादी को भूल नहीं पाती.....हर घड़ी मन में कचोट मची रहती है। अगर इसी तरह की हालत रही तो.....हो चुकी मेरी पढ़ाई।\"
मेरी गंभीरता पर दोनों सोचने पर मज़बूर हो गए। अपनी बात कहकर मैं उठने ही वाली थी कि बाबूजी बोले-\"बेटी अगर तुम बनारस की बजाय शांतिनिकेतन जाकर पढ़ो तो कैसा रहे? शिक्षा की उससे अच्छी व्यवस्था और कहीं नहीं है।\"
मुझे इंकार न था, मुझे बस यहाँ से हटना था। नहीं मन लगता मेरा यहाँ।
\"ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें।\"
\"हम तुम्हें कल बताएँगे वहाँ जाने के बारे में।\"
मैं मन-ही-मन आश्वस्त थी लेकिन विस्फोट तो होना था मेरे शांतिनिकेतन जाकर पढ़ने का। बाबा और दादी के चले जाने के बाद से फैला कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा इस विस्फोट से थर्रा गया। बड़े बाबा निर्विकार थे। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले-\"पायल बेटे, मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी फैसला करने की पूरी छूट है। तुम समझदार हो, अच्छा ही सोचोगी।\"
लेकिन बड़ी दादी के दाँतों की आरी चल पड़ी-\"तो अब इस घर के फैसले छोरियाँ करेंगी। वो भी बित्ते भर की छोरी.....नाक पोंछने तक का तो शऊर नहीं.....शांतिनिकेतन जाकर पढ़ेंगी.....अपने बाप की बराबरी करना चाहती हैं, हम सब मर गए हैं क्या तेरे लिए?\"
कोई कुछ न बोला। मेरे अंदर क्रोध की ज्वालाएँ भड़क उठीं। बड़े बाबा मुझे अपने सीने में दबोचे थे और लगातार पीठ थपथपा रहे थे।
\"उलटी करनी तुम सब करते हो और भुगतती हूँ मैं। ये सब तुम लोगों की करनी का नतीजा है जो खटिया तोड़ रही हूँ मैं। वो कुलबोरन तो कुल को बोर कर चली गई.....एक-एक कर तुम सब चली जाओ, फिर आ जाना मेरे कीड़े बीनने।\"
सहसा बड़े बाबा ने मुझे झटके से छोड़ा और जाकर बड़ी दादी के बाल झँझोड़ डाले-\"एक शब्द भी और कहा तो घोंट डालूँगा गला। जीना हराम करके रखा है सबका।\"
\"हाँ.....हाँ.....घोंट डालो। ऐबी तुम्हीं हो.....तुम्हारे ही कारण मेरी ये दुर्गत हुई है।\" और वे चीख-चीखकर रोने लगीं। पर वहाँ कोई झाँका तक नहीं.....न कंचन, न जसोदा, न पन्ना.....सब तटस्थ-से थे जैसे। संध्या बुआ ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गईं-
\"देख पायल, तू शांतिनिकेतन ज़रूर जाएगी। भाईसा से मैं खुद बात करूँगी। पर एक बात मत भूलना.....जब मुझे तेरी ज़रुरत पड़ेगी तो तुझे आना होगा।\"
मैं समझ गई। संध्या बुआ का इशारा उनके गुप्त विवाह की ओर था।
\"हाँ बुआ, सिर के बल आऊँगी।\"
उन्होंने मुझे सीने से लगाकर मेरा माथा चूम लिया-\"यूँ भी मेरा मन डरता रहता है। कलकत्ता भी आंदोलन से सुलग उठा है। बुद्धिजीवी वर्ग.....पत्रकार, संपादक, लेखक, प्रोफेसर सब आंदोलन में कूद पड़े हैं। पुलिस खुफिया भंडार का पता लगाने के लिए आम जनता को टॉर्चर कर रही है। अजय के लिए सोचकर काँप उठती हूँ.....मैं उनके साथ होती तो चिंता नहीं थी.....यहाँ चाची भी नहीं है, कौन साथ देगा मेरा। बस, तुम पर भरोसा है और एक प्रार्थना, थोड़ा रुक जाओ पायल, अभी परिस्थितियाँ कहीं जाने लायक नहीं हैं।\"
\"ठीक है बुआ.....सैकेंड सैशन दिवाली के बाद शुरू होता है, मैं तब चली जाऊँगी।\"
संध्या बुआ आश्वस्त हुईं-\"शुक्रिया पायल, तुमने मेरी बात रख ली।\"
अक्टूबर की एक शाम मारिया ने थॉमस के हाथ ख़बर भिजवाई कि फौरन आकर मिलिए। वैसे तो कभी लाइब्रेरी, कभी स्कूल, कभी मंदिर में मारिया आती थी और दादी के समाचार सुना जाती थी। वे अब काफ़ी सम्हल चुकी हैं और सभी परिस्थितियों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मेरा मन उनसे मिलने को तड़पता रहता था पर जाना नामुमकिन था.....वैसे भी प्रताप भवन में पत्ता भी हिलता है तो सबको ख़बर हो जाती है। अब मैं भी सम्हल-सम्हलकर पाँव रख रही थी। वक़्त से पहले बचपन बिदा ले चुका था और प्रौढ़पन ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी।
मुझे तैयार होते देख संध्या बुआ भी साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। अम्मा को हमने बता दिया था कि हम लोग सेवा केंद्र जा रहे हैं। जब बग्घी गेट पर रुकी तो देखा मारिया बेचैनी से हमारा इंतज़ार कर रही है। उसने बहुत ख़ूबसूरत सिल्क की साड़ी पहनी थी और हलके-हलके मोती के ज़ेवर भी।
\"मेरे कमरे में चलिए, बताती हूँ सब।\"
हम तीनों तेज़ी से कमरे में आए.....उसने हमें कुर्सियों पर बैठाया और पहले से तैयार शरबत गिलासों में उँडेलकर सामने रख दिया।
\"कुछ बताओ भी तो मारिया, बात क्या है?\"
\"आज मिस्टर जिम की शादी है।\"
\"शादी? किसके साथ?\" संध्या बुआ ने आशंकित हो पूछा।
मारिया एक पल रुकी लेकिन फौरन ही उसने स्थिति स्पष्ट कर दी-\"मिस्टर जिम छोटी आंटी से शादी कर रहे हैं। चर्च में, कैथोलिक तरीके से। मैं वहीँ जा रही हूँ। छोटी आंटी ने ख़ास आप दोनों को लेकर आने की प्रार्थना की है।\" संध्या बुआ को जैसे अंगारा छू गया-\"क्याऽऽऽ चाची शादी कर रही हैं?\"
\"क्यों नहीं.....इस तरह कब तक दोनों साथ रह सकते हैं? और कोई चारा भी तो नहीं है।\" मारिया ने निर्भीकता से कहा।
\"चलिए, वरना देर हो जाएगी।\"
\"नहीं मारिया.....हमारा जाना मुमकिन नहीं है।\" संध्या बुआ ने कहा तो मैं झल्ला पड़ी-\"मगर मैं जाऊँगी.....मैं ज़रूर जाऊँगी।\"
\"बचपना मत करो पायल! हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। भावावेश में तुम आगे तक का बिगाड़ कर लोगी। ज़रा सोचो, शादी में हमारा शामिल होना कितनी बड़ी बात रखता है। वह वजह बन जाएगा पूरे ख़ानदान के शामिल होने का।\"
संध्या बुआ की बात में वज़न था। मारिया को भी यही ठीक लगा। उसने दूसरे दिन लाइब्रेरी में आकर सब कुछ बताने का आश्वासन दिया और चली गई।
रात बीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। करवटें बदलते-बदलते मैं थक गई। पूरा प्रताप भवन रात की चादर में दुबका था। हलका-हलका जाड़ा पड़ना शुरू हो गया था। मुझे दादी के फैसले पर ज़रा भी अफसोस न था। आख़िर वे कर भी क्या सकती थीं इसके सिवा.....ऐसे ही जिंदगी नहीं बीत जाती! यहाँ तो उन्हें दूध की मक्खी सी निकालकर फेंक दिया गया था जैसे इस कोठी में उन्हें कोई जानता ही न हो, जबकि सारी घटनाओं के लिए केवल बड़ी दादी ज़िम्मेदार थीं। क्या दोष था दादी का? क्या गुनाह किया था उन्होंने? कैसे मर-मरकर जी रही होंगी वे वहाँ? क्या हक़ था बड़ी दादी को उन्हें चिता की आग में झोंकने का? बाबा के बाद उनकी बगिया को सँवारने का क्या दादी का हक़ न था? क्या कोठी के कोने-कोने में बसी बाबा की आत्मा उनसे जवाब नहीं माँगती कि मेरे बाद तुम्हीं सब कुछ सम्हालने वाली थीं और तुम्हीं जीवन से पलायन कर रही हो? क्या अम्मा-बाबूजी के सुखी संसार को देख उनकी इच्छा न होती कि अपने तिल-तिल श्रम से उपजे सुख को वे भोगें? पर समाज ने ऐसा होने न दिया। दादी के लिए इस कोठी की देहरी पराई हो गई। बिरादरी बेगानी हो गई और वे स्वयं हव्य सामग्री बन गईं। कैसे स्वीकार किया होगा दादी ने उस विदेशी संस्कृति वाले माहौल को.....कैसे भूल पाई होंगी कोठी के कोने आतड़ को, तीज, करवाचौथ को.....पापड़, अचार को.....बाबा के एहसास को। सोचते-सोचते मुझे ध्यान आया कि कब से मेरा तकिया आँसुओं से भीग रहा है, यह तो सुबह भी हो गई।
इंतज़ार था शाम होने का.....लेकिन वह शाम हाथ से फिसल गई और मैं और संध्या बुआ मुँहबाए खड़े रह गए। ख़बर पूरे मालवगढ़ में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि छोटी मालकिन ने जिम से शादी कर ली है। ईसाई हो गई हैं वे। सफेद फ्रॉक में दुल्हन बनी उन्हें कईयों ने चर्च में देखा था और यह भी ख़बर थी कि रात अंग्रेज़ों के डांसिंग फ्लोर पर अफ्रीकी ड्रम बजा था, शैम्पेन खुली थी और देर रात तक मौज मस्ती की गई थी।
सारी बिरादरी थू-थू करने लगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर जिसने हिंदू धर्म की मर्यादा को ताक पर रख दिया। जिसने पति की चिता की आग ठंडी भी न होने दी और सुहाग सेज सजा ली। ईश्वर कभी उस कुल कलंकिनी का अब मुँह न दिखाए।
बड़ी दादी दोहत्थड़ मारकर रोईं-\"डायन निकली वो तो। ऐसे चलित्तर थे तभी तो जवानी में देवरसा उठ गए। चली थीं सती होने.....देवी कहलाने।\"
कैसी ढुलमुल मानसिकता है लोगों की। जब वे सती हो रही थीं तो पवित्र आत्मा, देवी और कुलवधू थीं और जब आज उन्होंने ज़िंदा रहने की मजबूरी में अपने को एक पवित्र रिश्ते में बाँधा तो कुलच्छिनी हो गईं, डायन हो गईं? लेकिन मेरे लिए दादी उस महावृक्ष की तरह हैं, जिन्होंने न जाने कितने बसंत, कितने पावस के झंझावातों को झेलकर इस कोठी को सँवारा है। उनके विचारों की गहराई, ऊँचाई और सच्चाई समझने के लिए उन लोगों को उतना ही गहरा होना पड़ेगा। ऊँचाई क्या बिना शिखर पर चढ़े जानी जा सकती है?
दादी, तुम तो वह बूँद हो जिसे बादल ने मात्र पानी समझकर अपने से विलग कर दिया किंतु जो सीप में पकड़कर मोती बन गई। तुम मेरे मन में मोती-सी जड़ गईं दादी..... तुम्हारे साहस ने अब मुझे किसी भी अन्याय के आगे न झुकने के लिए मजबूत बना दिया है। अब मैं शान से अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीयूँगी और किया भी मैंने वही।
द्वितीय सत्र आरंभ होते ही मेरा शांतिनिकेतन के छात्रावास में दाख़िला हो गया। जाने से पहले मैं दादी से मिलना चाहती थी पर पता चला वे यूरोप घूमने के लिए गई हैं और महीने भर बाद लौटेंगी, यह भी पता चला कि अब शायद वे यहाँ न रहें, शिमला जाकर रहें.....वहाँ पहले से ही जिम का कॉटेज है और सेबों का बगीचा भी। अच्छा ही है। यहाँ रहेंगी तो कोठी की याद सताएगी। इस सड़क से गुज़रेंगी तो कोठी के कंगूरों पर बाबा की निगाहें मुस्कुराती देखेंगी.....शायद अब इतना साहस उनमें बचा न हो। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिम की जिसने देवदूत-सा आकर मेरी दादी को बचाया। जीवन सागर की एक लहर ने दादी के साथ बगावत कर दी थी। वे डूब ही जातीं अगर तिनके की तरह जिम न आते। उन्होंने दादी को नई ज़िंदगी दी। उनसे शादी करके अपने प्यार को सम्मान दिया।
शांतिनिकेतन के आम्रकुंजों में, आकाश की छत के नीचे लगी कक्षाओं में पढ़ते हुए मैं रोमांचित थी। लगता था जैसे मैं प्राचीन काल में गुरुकुल आश्रम की कोई तपस्विनी शिष्या हूँ। ऐसा अद्भुत स्कूल मैंने पहली बार देखा, सबसे ज़्यादा प्रभावित किया मुझे नंदलाल बोस और रामकिंकर बेज की मूर्तिकला और भित्तिकला ने। काली मिट्टी से बने कला भवन की दीवारों पर काली मिट्टी से ही उभारी गई प्राचीन लास्य नृत्य में लीन अप्सराओं और देवताओं की मूर्तियों ने मेरा मन मोहित कर लिया। मैंने यहाँ बातिक कला भी बाकायदा सीखनी शुरू कर दी जिसकी कक्षाएँ ताल कुटीर में होती थीं। ताड़ के वृक्ष को घेरकर बनाया गया ताल कुटीर। मैं नियमित विश्व भारती प्रकाशन विभाग पुस्तकालय भी जाने लगी। मन ऐसा रम गया था कि कुछ दिनों के लिए मालवगढ़ का ख़याल तक न आया लेकिन तभी अम्मा का ख़त आया कि \"क्रिस्मस की छुट्टियों में तुम्हें लेने तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं.....फौरन चली आओ।\"
फौरन! क्यों? दो महीनों में ही मेरी क्या ज़रुरत आन पड़ी वहाँ? मेरा इरादा तो इन छुट्टियों में शांतिनिकेतन शिक्षा केंद्र को पूर्णतया समझने का था। यह केवल स्कूल नहीं है बल्कि इंसान को इंसानियत में खरा करने की एक विशाल कसौटी है और यह तय है कि इस कसौटी पर परीक्षित किया इंसान कभी भटक नहीं सकता।
मुझे जाना पड़ा। बाबूजी आए थे लेने और बगैर एक दिन भी रुके वे मुझे फौरन ले गए। रास्ते में पढ़ाई के विषय में औपचारिक बातें होती रहीं। मैं भाँप गई थी कि कोई गंभीर मसला ज़रूर है पर पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मुझे मालवगढ़ आने तक धैर्य रखना पड़ा लेकिन कोठी में प्रवेश करते ही मानो स्थिति स्पष्ट हो गई। संध्या बुआ की आँखें लाल थीं और अम्मा ने मुझे उनसे उस वक्त कुछ भी पूछने को मना कर दिया था। अम्मा मुझे अपने कमरे में ले गईं। जसोदा मेवों वाला दूध और घेवर ले आई और अपने हाथ से मुझे खिलाने लगी। अम्मा ने उसी के सामने मुझसे पूछा-\"संध्या बाई और अजय की शादी के समय मंदिर में तुम थीं न?\"
मेरे काटो तो खून नहीं.....तो राज़ खुल गया।
\"बताओ पायल, एकमात्र तुम्हीं चश्मदीद गवाह हो उस शादी की क्योंकि तुम्हारी दादी तो यहाँ हैं नहीं.....मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ।\"
\"हाँ पायल बिटिया, बता दीजिए सब क्योंकि संध्या बाई सा ने अपने मुँह से ही हुकम के आगे शादी की बात कबूल कर ली है।\" जसोदा ने इसरार किया तो मैं दंग रह गई। संध्या बुआ ने पूरे घर के सामने खुद ही अपनी शादी का ऐलान कर दिया था और अब वे चाहती थीं कि उनकी बिदा कर दी जाए।
बड़ी दादी ने माथा पीट लिया था।
\"अरे, ये क्या उलटी-सीधी बातें सिखाती रही मालविका इन सबों को।\"
बड़ी दादी अब उन्हें दुल्हन नहीं कहती थीं। जसोदा, कंचन और पन्ना की तरह उन्हें भी नाम से संबोधित करती थीं।
\"हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। न कुछ बताया गया और उधर शादी भी कर आई जाकर। खुद के बेटी होती तो क्या इसी तरह टारती उसे।\"
\"हाँ पायल, बताओ क्या-क्या हुआ था।\"
बड़ी दादी के कमरे में दरबार लगा था। संध्या बुआ अपराधी के कठघरे में थीं और मैं गवाह के.....अम्मा, बाबूजी, बड़े बाबा, रजनी बुआ और तमाम सेविकाएँ भी वहाँ मौजूद थीं। संध्या बुआ ने चुनौती भरी नज़रों से मुझे देखा कि देखें कितनी कूबत है तुममें सच उगलने की। मेरे सामने एक संपूर्ण जीवन था.....सिर्फ़ मेरी गवाही संध्या बुआ को उस जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दिला सकती थी। दादी शिमला चली गई थीं और जिम के बंगले में ताला था। और यहाँ थीं बड़ी दादी, पितृसत्ता की पक्षधर.....उनकी नज़र में विधवा का शादी कर लेना गुनाह था, लड़कियों का मर्दों की बराबरी से चलना गुनाह था.....फिर संध्या बुआ ने तो मर्दों तक को मात दे दी थी। उन्हें डूब जाने का डर नहीं था इसीलिए बड़े आराम से उन्होंने अपने लिए घरौंदा बना लिया था।
\"अरी, गूँगी बनी क्यों खड़ी है?\"
मुझे मानो चिंगारी छू गई-\"हाँ, बुआ की मंदिर में शादी हो चुकी है। माँग में सिंदूर भी भर दिया अजय ने जयमाला पहनाकर.....\"
\"अरी कुलच्छिनी, कुलबोरनी.....मर जाती तू सोबर में तो मैं गंगा नहा लेती। देख..... देख.....ये पाँव मेरे कितने सूज गए हैं.....सब तेरी करनी से.....अरे. कब तक भुगतूँ मैं.....शाप लग गया इस कोठी को.....कहते थे मेरे मायके के पंडितजी कि मत करो इस ख़ानदान में शादी, भुगतेगी लड़की ज़िंदगी भर।\"
\"माँ, क्यों कोसती रहती हो खुद को और सबको, क्या मिलता है तुम्हें।\"
\"मिला न, कुलतारिनी होने का प्रसाद मिला न मुझे। अरे वाह! मुँहजोरी तो देखो इस धींगड़ी की। करतूत करके अब मुझी पर चढ़ी जा रही है।\"
\"हाँ, मैंने करतूत की.....पाप किया.....सब पापी हैं इस घर में.....चाची भी पापी हैं.....सब पापी हैं.....सब पापी हैं.....पर तुम तो पुण्यात्मा हो, तो लो, रोओ मेरी लाश पर।\"
और संध्या बुआ ने सामने रखी फलों की डलिया से चाकू उठाकर अपनी कलाई की नसों को काटने के लिए कलाई पर ज़ोर से मारा। अम्मा और मैं उन्हें रोकने दौड़े तो चाकू हमारी ओर तान दिया-\"कोई आगे मत बढ़ना वरना पेट में भी भोंक लूँगी ये चाकू।\"
उनकी आँखों में अपने को स्वाहा करने की वहशत सुलग उठी थी। हम जहाँ के तहाँ रुके थे पर कंचन और जसोदा ने दबे पाँव पीछे से जाकर उन्हें दबोच लिया और चाकू छीन लिया। संध्या बुआ की कलाई लहूलुहान थी पर नसें नहीं कट पाई थीं। सब हक्का-बक्का थे इस कांड से। कलाई से बहता लहू फर्श पर टपक रहा था पर दर्द की एक लकीर भी उनके चेहरे पर न थी। बड़ी दादी ख़ामोश थीं और मुँह में पल्ला ठूँसे रो रही थीं। बड़े बाबा बाहर चले गए थे और बाबूजी संध्या बुआ को अपने से चिपटाकर उनके कमरे तक ले आए थे। जो देखा वह मेरे दिल में खुद गया हमेशा के लिए.....हमेशा के लिए आँखों के आगे बिछ-सा गया..... लगता है जैसे ये धड़कते हुए पल धीरे-धीरे आकार लेकर एक विशाल आग का गोला बन गए हैं और फिर उस गोले में विस्फोट हुआ है और एक जला हुआ टुकड़ा उसमें से गिरा है, यह टुकड़ा प्रेम था और वह प्रेम मेरी संध्या बुआ हैं। धीरे-धीरे आग ठंडी पड़ गई और सारी कायनात अँधेरे के आगोश में समा गई।
सुबह बाबूजी ने फैसला सुनाया कि संध्या बुआ की शादी हम सबको स्वीकार है और चूँकि बाबा को गए अभी पूरा साल नहीं हुआ है लेकिन फिर भी शुद्धि कराके एक सादे समारोह में शादी का ऐलान करके उन्हें बिदा कर दिया जाए। जब देश के हालात ऐसे चल रहे हैं कि कभी भी वक़्त क्रांति की आग प्रताप भवन को भी छू सकती है.....देशभक्तों में सिर कटाने की होड़ लगी है, खून की नदियाँ बह रही हैं ऐसे में हम अपनी परंपराओं, मान्यताओं से चिपके रहें, यह शोभा नहीं देता।
बाबूजी अचानक बाबा की जगह ले चुके थे। वैसी ही सोच, गंभीरता उनमें आ गई थी। जिम्मेदारियों के बोझ ने उन्हें बुजुर्ग बना दिया था।
मैंने दादी की मारिया की मार्फत ख़त लिखा था-
\"दादी, आप यहाँ नहीं हैं और संध्या बुआ बिदा हो रही हैं। एक भयानक कांड होते-होते रह गया और संध्या बुआ बच गईं, हमें वापस मिल गई वरना क्या से क्या हो जाता। आपके जाते ही प्रताप भवन पर दुर्भाग्य के घने बादल छा गए हैं। ऐसा होगा ही.....जब कोई पुण्यात्मा कलपाई जाए तो ऐसा होगा ही। अपने दुखों को खुद ही निमंत्रण दिया प्रताप भवन ने.....वजह बड़ी दादी बन गईं। ख़ैर, संध्या बुआ की बिदाई के साथ ही मैं शांतिनिकेतन लौट जाऊँगी इस फैसले के साथ कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। मैं शादी करने के बाद ज़िंदा चिता में जलने, किसी के हाथों की कठपुतली बनने, बिस्तर पर सड़ने और कलाई की नसों को काटने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा जीवन एक चुनौती बन गया है और मैं इस चुनौती का वरण करने जा रही हूँ। बहरहाल मैंने पूरी हिम्मत से बुआ की शादी का आँखों देखा विवरण सुनाकर अब उस पर प्रताप भवन की रज़ामंदी का ठप्पा लगवा लिया है। बुआ के साथ ही मैं भी शांतिनिकेतन चली जाऊँगी। दादी, आप मुझसे वहाँ मिलने आइए न। मैं आपके लिए छटपटा रही हूँ, प्रताप भवन खाने को दौड़ता है इसीलिए मैंने शांतिनिकेतन में पढ़ना शुरू किया है और इसीलिए संध्या बुआ भी जा रही हैं, बाबा की बरसी के पहले ही। आपसे मिलने की प्रतीक्षा में।
आपकी माँ पायल\"
धार्मिक अनुष्ठानों, शांति पाठ, तर्पण, हवन आदि कराके बाबूजी ने बाबा के शोक से भरे पूरे साल को समेटकर चार महीने का कर दिया और प्रताप भवन में दबी-दबी शहनाइयाँ बज उठीं.....ज़ाहिर था लोग उँगलियाँ उठाएँगे.....उठीं भी-\"आज तक राजपूतों में ऐसा तो हुआ नहीं कभी जैसी चलन प्रताप भवन चला रहा है। अपने गौरवशाली अतीत को धूल में मिलाने पर तुला है वरना एक समय वो भी था कि ज़मींदार प्रतापसिंह का नाम लेकर लोग कसमें खाते थे। क्या ज़माना आ गया है।\" लेकिन बाबूजी के पास ठोस तथ्य थे। एक तो देश की डाँवाँडोल परिस्थिति, बड़ी दादी की निरंतर गिरती जा रही शारीरिक हालत और फिर अगले दो वर्षों तक अशुभ ग्रहों का कुंडली में रहना हमें मजबूर करता है शादी के लिए।
लिहाज़ा फुसफुसाहटें दब गईं और मालवगढ़ समारोह में शामिल हो गया। फिर भी अजय की ज़िद्द थी कि ज़्यादा धूमधाम न हो.....बहुत कम रिश्तेदार आ पाए। उषा बुआ और राधो बुआ आ गई थीं। कुछ रिश्तेदार शादी की तैयारी से निकले भी तो क्रांति के अंदेशे से वापस लौट गए। भारत ने आज़ादी पाने के लिए जो करवट बदली थी वह देशव्यापी थी।
सबने महसूस किया मानो संध्या बुआ की इस तरह शादी करके बला टाली गई है। माना, बाबा के देहावसान के बाद प्रताप भवन भी तमाम घटनाओं का केंद्र बन गया था लेकिन उषा बुआ की शादी की धूमधाम जैसा एक अंश तो होता। सब यही कह रहे थे कि दादी जैसा इंतज़ाम करना किसी के बूते की बात नहीं है। बिना दादी के प्रताप भवन चरमरा गया था और उसकी चरमराहट की पहली गूँज थी मेरा शांतिनिकेतन प्रस्थान.....और दूसरी संध्या बुआ की बेरौनक शादी।
बिदा होकर संध्या बुआ अजय फूफा सा के घर पूरे क्रिस्मस वेकेशन रहीं और छुट्टियाँ समाप्त होते ही हम साथ-साथ कलकत्ता लौटे। चलते समय अम्मा ने कहा था-\"पायल, इधर वीरेंद्र की पढ़ाई की डाँवाँडोल स्थिति है.....उसे भी शांतिनिकेतन भेजने का सोच रहे हैं तुम्हारे बाबूजी।\"
\"लेकिन इस साल नहीं.....अगले साल! तुम हर हफ्ते पत्र लिखना बेटी.....मेरा मन ही नहीं लगता यहाँ। लेकिन रजनी बाई के कारण मैं हिल भी तो नहीं सकती यहाँ से।\"
मैं अम्मा की मजबूरी समझती थी। यह भी जानती थी कि अभी तो स्थिति सुधरने में सालों लगेंगे। दस साल तक तो रजनी बुआ की शादी का सवाल ही नहीं उठता। फिर उन्हें तो वकील बनना है।
\"क्यों जलाती हो यह कहकर मुझे.....पायल! मेरी वकील बनने की ज़िद्द ने ही चाचा सा की जान ली.....चाची सा के लिए ये घर पराया हो गया। सारे बवाल की जड़ मैं ही हूँ।\"
और वे रो पड़ीं। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। नि:शब्द वे अपनी तेज़ धड़कनों से बड़ी देर तक अपनी मनःस्थिति उजागर करती रहीं। फिर आँसू पोंछे-
\"सब चले गए.....दोनों जीजियाँ, चाची सा.....तुम भी जा रही हो पायल। घर काटने को दौड़ता है अब। सबने अपने-अपने ठिकाने खोज लिये, मैं कहाँ जाऊँ?\"
अब की अम्मा ने उन्हें हुलसकर लिपटा लिया-\"मैं हूँ न! और फिर तुम तो मेरी बेटी जैसी हो.....ननद तो बस रिश्ते भर की हो। अब पायल जा रही है तो क्या तुम मेरी देखभाल नहीं करोगी?\"
\"भाभी सा.....\" रजनी बुआ के कातर शब्द उनकी हिचकियों में दब गए।
हावड़ा स्टेशन पर हम जैसे ही उतरे मेरा मन खुशी से और आश्चर्य से भर गया। दादी और जिम हमारी ओर तेज़ी से आ रहे थे। दादी के हाथ में फूलों की मालाएँ थीं और वे बेहद सुंदर ढाका सिल्क की साड़ी और पूरी बाँह का ब्लाउज़ पहने थीं। उसी रंग का पश्मीने का शॉल। उनके माथे पर सिंदूर की बिंदी जगमगा रही थी। कोट, पतलून और टाई में जिम को मैं पहली बार देख रही थी। नहीं.....पहली बार नहीं.....धुँधला-धुँधला याद आया.....यह चेहरा कोठी पर भी देखा है मैंने। हाँ, बाबा के समय जिम आते रहे हैं वहाँ। मैं \'दादीऽऽ\' कहती तेज़ी से उनसे लिपट गई। उनका भी पूरा शरीर सिसकियों से हिल उठा। मैंने महसूस किया दादी काफ़ी दुबली हो गई हैं। उन्होंने अजय फूफा सा और संध्या बुआ को भी अपने से लिपटाकर मालाओं से सजा दिया। सब रो रहे थे.....कहता कोई कुछ भी न था। मानो वक़्त थम गया था, ठिठककर हमारी बरबादी और क्षणिक खुशहाली पर वह ठगा सा खड़ा था। न जाने कितने लम्हों, घंटों, दिनों, महीनों का ज्वार हमारे दिलों को आलोड़ित किए था। हमसे छूटा हमारा वक़्त, निर्वासित हुए हम सब और सामने पड़ा ज़िंदगी का लंबा रास्ता जिस पर चलना हमारी मजबूरी थी। हमें देख जिम ने भी चश्मे के अंदर बहते अपने आँसुओं को पोंछा और कहीं और देखकर जैसे ही इशारा किया, बैंड बज उठे। प्लेटफार्म पर ही दादी ने बैंड का इंतज़ाम किया था। जब हम नॉर्मल हुए तो दादी ने जिम से हम सबका परिचय कराया। फिर हम फूलों से सजी कार में बैठकर दादी के द्वारा अरेंज किए बेहद आलीशान होटल में आए जहाँ जिम के अंग्रेज़ दोस्तों का जमघट, शानदार डिनर और रिकॉर्ड प्लेयर हमारा इंतज़ार कर रहा था। दादी ने, शादी में जो कसर रह गई थी वह पूरी कर दी।
\"संध्या.....तुम्हारी शादी कोई मामूली घटना नहीं है.....ये दो ऐसे दिलों का मिलन है जो सिर्फ प्रेम करने के लिए ही दुनिया में आए.....मेरी तुम दोनों ही से प्रार्थना है कि अपने दिल की आवाज़ पहचानने का, सुनने का अपने में माद्दा पैदा करो। शादी तो सभी करते हैं पर कोई एक शादी ही मिसाल बनती है।\"
संध्या बुआ का सिर झुका था.....दादी ने उन्हें पुनः गले से लगाया और मेरी ओर मुख़ातिब हुईं-
\"और तुम पायल! तुमने जो संध्या के लिए गवाही दी है उसने मेरा सिर ऊँचा कर दिया.....इसीलिए तो मैं तुम्हें साथ लेकर आगे बढ़ी थी क्योंकि तुममें साहस की परछाई मैंने देख ली थी। और संध्या, तुम्हें पायल का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। जानती हो इसी के ख़त से मुझे तुम्हारी शादी की बात और यहाँ आने की तारीख पता चली।\"
\"आपकी माँ जो है ये.....फिर भूल कैसे सकती है?\" संध्या बुआ ने मेरे गाल दबाए। जिम दूसरे कमरे में बैठे अपने दोस्तों के पास अजय फूफा सा के साथ चले गए तो एकांत होते ही दादी ने कोठी का हाल विस्तार से पूछा। बीच-बीच में रोती भी जा रही थीं वे। लेकिन आश्वस्त भी थीं। बताया-
\"मिस्टर जिम बेहद भले और सभ्य इंसान हैं बल्कि तुम्हारे बाबा के बाद यही मुझे पूर्ण इंसान नज़र आए। इन्होंने किसी बात का दबाव मुझ पर नहीं डाला। अगर मैं कोठी में जाना चाहती तो ये भेज देते पर मैं ही नहीं गई। जहाँ से जलाने के लिए निकाली गई वहाँ मेरा ज़िंदा होना कैसे कबूला जाता? मिस्टर जिम मुझे कुछ भी याद नहीं करने देते। उनका मानना है कि बीते हुए लम्हे इंसान के क़दमों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन्हें वक्त की कब्र में दफ़न कर देना चाहिए।\"
\"दादी.....मुझे माफ़ करें लेकिन न जाने क्यों मन बेताब है यह जानने के लिए कि आप खुश तो हैं न?\" मैंने हिम्मत करके पूछा।
\"ये बात जिम से पूछो क्योंकि मेरा तो यह दूसरा जन्म है। पहले जन्म के दुःख दूसरे जन्म में सालें, ऐसा कहाँ संभव है?\"
\"मैं शिमला आऊँगी दादी।\"
वे मुस्कुरा दीं.....शायद उनके मन की भीतरी परतों में कोई नासूर था जिसने उनकी ज़बान खुश्क कर दी थी।
रात भर जश्न होता रहा। सुबह दादी और जिम मुझे कार से शांतिनिकेतन पहुँचा गए। अजय फूफा सा और संध्या बुआ भी मुझे पहुँचाने आए थे।
\"लौटते हुए हम संध्या और अजय को उनके बंगले पर छोड़कर रात की फ़्लाइट से दिल्ली चले जाएँगे। दिल्ली में हमें थोड़ा काम है.....वहाँ से दो दिन बाद शिमला.....\"
\"इतनी ठंड में शिमला.....वहाँ तो खूब बर्फ़बारी हुई है।\"
मुझे लगा दादी अपने उसी अंदाज में कहेंगी-\'पुरखिन, सब ख़बर रखती है।\'
लेकिन वे चुप रहीं.....बस, मुझे लिपटा लिया और पीठ थपथपाती रहीं।
१५ अगस्त १९४७ की मध्यरात्रि, जब सारा संसार सो रहा था, आज़ाद भारत धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य का यूनियन जैक दिल्ली के लाल किले से उतार दिया गया था और भारत का तिरंगा झंडा अपनी पूरी शान से लहरा रहा था। कलकत्ता की सड़कों पर इस वक़्त सन्नाटा रहता है और ज़रा-सी आहट पर कुत्ते भौंकने लगते हैं। सारा वातावरण रात की काली चादर ओढ़ निष्क्रिय और सुशुप्त रहता है किंतु उस मध्यरात्रि की चहल-पहल का कहना ही क्या था। सड़कें कोलाहल में डूबी थीं, प्रकाश और उज्ज्वलता दीपों में साकार थी, हलवाइयों ने अपनी दुकानें खोल दी थीं और संदेश, रसगुल्ले लुटाने शुरू कर दिए थे। रात दुल्हन-सी सज उठी थी। और क्यों न सजे.....ये स्वतंत्र भारत की पहली रात थी। वर्षों की गुलामी का एक ऐसा दस्तावेज जिस पर शहीदों ने अपने रक्त से हस्ताक्षर किए थे और जो हमारा वसीयतनामा था.....क़ाश। आज बाबा होते.....तो देखते कि जिन अंग्रेज़ों की भीतर-ही-भीतर जड़ें खोदने में वे लगे थे.....उस अंग्रेज़ी साम्राज्य का महावृक्ष जड़ से उखड़कर धरती पर गिर पड़ा था।
मैं संध्या बुआ के बंगले पर थी। उस रात घर में काफ़ी मिठाइयाँ होने के बावजूद संध्या बुआ ने घी में सूजी भूनकर हलवा बनाया था और हलवे की प्लेट कतरे हुए मेवों से ढककर, वर्क लगाकर द्वारकाधीश श्रीकृष्ण को भोग लगाया था। अजय फूफा सा ने देशभक्ति के गीतों का रेकॉर्ड लगाया था और बंगले की बाउंड्री वॉल के बाहर पटाखे, अनारदाने छोड़े थे। दादी ने भी दीपक जलाए होंगे.....कृष्णजी को भोग लगाया होगा.....क्या पता, सत्ता की समाप्ति से जिम उदास हों या.....
तभी फोन की घंटी बजी। फोन बुआ ने उठाया और उस तरफ की आवाज सुन चहकीं-\"चाचीसा!.....बधाई, बहुत-बहुत बधाई.....इस दिन का इंतज़ार वर्षों से था। चाचासा की तपस्या फलीभूत हुई। हम आज़ाद हो गए.....हाँ देती हूँ पायल.....चाचीसा का फोन है.....\"
मैंने झपटकर फोन लिया-\"ओह दादी.....आप सामने होतीं आज.....सच्ची.....मैंने इतनी खुशी आज तक कभी महसूस नहीं की। लेकिन दादी, अब तो आप लंदन चली जाएँगी.....और फिर कभी नहीं मिल पाएँगी।\" मैं रो पड़ी थी। दादी भी रो रही थीं.....दोनों ओर से सन्नाटा था। दोनों ओर भावातिरेक में भरे गलों की चुप्पी थी। तभी रिसीवर जिम ने लिया और अंग्रेज़ी में बधाई देकर तुरंत साफ़, स्पष्ट हिंदी में कहा-\"हम लंदन नहीं जाएँगे पायल, डोंट वरी, लंदन में हमारा क्या है? मेरा जन्म यहीं हुआ, भारत की मिट्टी में पल-बढ़कर मैं बड़ा हुआ। भारत मेरा है, मैं यहीं रहूँगा। खुश।\"
और मारे खुशी के मेरे आँसू निकल पड़े। फोन का रिसीवर रखकर मैं चीखी-\"बुआ..... दादी लंदन नहीं जाएँगी। यहीं रहेंगी।\"
वह रात हमारी दोहरी खुशी में जागरण करते बीती।
भले ही मैं दादी से मिल नहीं पाती थी लेकिन मेरे लिए ये तसल्ली काफ़ी थी कि वे भारत में हैं और जिम के साथ प्यार और समझौते से भरी खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। कई बार चाहा शिमला जाऊँ.....दादी के पास थोड़ा वक़्त गुज़ारूँ लेकिन जाना नहीं हो पाया। मैं अपनी पढ़ाई में तन-मन से आकंठ डूबी थी हालाँकि अम्मा के ख़त मुझे विचलित कर जाते.....
पायल.....मेरी गुड़िया,
पढ़ाई के प्रति तुम्हारे रुझान ने वर्षों से कसमसाते मेरे मन को राहत पहुँचाई है। मैं भी पढ़ना चाहती थी, जीवन में कुछ कर दिखाना चाहती थी लेकिन वक़्त की मज़बूरी और मेरी अपनी कमजोरी.....कुछ कर न सकी मैं.....जीवन के उतार-चढ़ाव में बिंधती चली गई..... लेकिन तुम पर मेरा भरोसा है.....तुम अपनी ज़िंदगी उसी ढंग से जी पाओगी जैसी मैं अपने लिए चाहती थी। ईश्वर तुम्हारे साथ है। इधर प्रताप भवन पर मँडराते दुर्भाग्य के स्याह बादल छँटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बड़ी अम्माजी पूर्णतया बिस्तर से लग चुकी हैं। उनके अंग-अंग में बीमारी ने डेरा डाल लिया है लेकिन ज़बान की अकड़न वैसी की वैसी है-\'दूसरों का किया बच्चियाँ भुगत रही हैं। रजनी की कहीं शादी ही नहीं लगती। उधर पायल भी जवान हो रही है।\' उनका कोसना सुनते-सुनते मन अथाह दर्द से भर उठता है। तुमने अच्छा किया जो कोठी से कोसों दूर पढ़ने चली गईं वरना तुम्हारा मन इन बातों से दुर्बल हो उठता। लेकिन पायल, मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी योग्यता, मनोबल को तुम कभी कम नहीं होने दोगी।
अम्मा के ख़त की आख़िरी पंक्तियों ने मेरे मन को अधिक मज़बूत कर दिया। हाँ.....मैं दृढ़ रहूँगी अपने इरादे में और अपनी औरत होने की नियति से भी लडूँगी।
एम. ए. करने के बाद मैं कलकत्ते में ही कॉलेज में लैक्चरर हो गई और संध्या बुआ के साथ रहने लगी। मेरी नौकरी करने की ख़बर सुनकर बहुत हंगामा किया था बड़ी दादी ने। बोल-कुबोल बोले थे। नाते रिश्तेदारों ने भी नाक-भौं सिकोड़ी थी। मगर उन बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ बल्कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं और अधिक दृढ़ संकल्प हो गई। रजनी बुआ की शादी भी बड़ी मुश्किलों से तय हो गई थी। दिक्कतें तो बहुत आईं। जहाँ भी शादी लगती, दादी और जिम के रिश्तों का हवाला पहले पहुँच जाता। उस घर में कौन संबंध करना चाहेगा जहाँ ऐसा कांड होकर चुका हो किसी को भी गहराई से उस घटना का तो पता नहीं था। दोष पूरा दादी पर.....न जाने कैसे.....शायद सिंगापुर में बसा होने के कारण इस परिवार से रजनी बुआ की शादी तय हो पाई थी। हीरे का व्यापार था उनका। स्वाभाविक दिन होते तो उतनी दूर शादी करना किसी को गवारा न होता लेकिन अब तो जैसे-तैसे हाथ पीले करने थे। अम्मा ने ही शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाई। देवउठनी एकादशी के बाद का मुहूर्त निकला। तय हुआ कि संध्या बुआ पंद्रह दिन पहले चली जाएँगी, मैं और अजय फूफासा ऐन वक़्त पर ही पहुँच पाएँगे। तमाम रिश्तेदार आ ही जाएँगे, काम की किल्लत नहीं होगी।
अभी सूरज पूरी तरह निकल नहीं पाया था.....मैं बरामदे में बैठी आज दिया जाने वाला अपना लैक्चर तैयार कर रही थी लेकिन मन नहीं लग रहा था। रह-रह कर मैं प्रताप भवन पहुँच जाती.....तो बन गईं रजनी बुआ गृहस्थन.....अब वकील कैसे बनेंगी वे? खा गईं न मात परिस्थितियों से? बाबा ठीक कहते थे रजनी बुआ कभी वकील नहीं बन सकतीं।
नौकर ट्रे में चाय की केतली और प्याले लाकर रख गया। प्रायः हम तीनों सुबह की चाय साथ बैठकर पीते थे। संध्या बुआ तरोताजा और खिली-खिली-सी लग रही थीं। रजनी बुआ की शादी से वे बेहद खुश थीं और चाहती थीं कि जल्दी-से-जल्दी मालवगढ़ पहुँच जाएँ। चाय प्यालों में डालकर उन्होंने फूफासा को आवाज़ दी-\"आइए\" फूफासा के हाथ में अखबार और एक लिफाफा था। लिफाफा उन्होंने मेरी ओर बढ़ाया-\"पायल, ये तुम्हारा पत्र।\"
पत्र लेकर जैसे ही मेरी नज़र लिफाफे पर पड़ी मन तेज़ी से उसे खोलने को बेताब हो उठा क्योंकि उस पर इटली की मोहर लगी थी। रोम यूनिवर्सिटी से पत्र आया था और इस जानकारी से भरा कि मेरा आवेदन पत्र मंजूर कर लिया गया था और मुझे पी-एच.डी. के लिए स्कॉलरशिप पर तीन वर्षों के लिए बुलाया गया था। मैं खुशी से लगभग चीख-सी पड़ी थी-\"बुआ.....फूफासा.....\"
\"हाँ.....क्या हुआ?\"
\"देखिए तो ये पत्र.....ओह गॉड.....यक़ीन नहीं हो रहा।\"
उन्होंने मेरे हाथ से पत्र लेकर बारी-बारी से पढ़ा। संध्या बुआ ने तो मेरे कंधे पकड़कर उठाते हुए मुझे चूम ही लिया-\"मुझे तुम पर गर्व है पायल।\"
\"संध्या.....तुम्हारी भतीजी तो कमाल की निकली।\"
\"ओह.....मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रही हूँ। अजय, तुम खुद जाकर इसके लिए रसगुल्ले लेकर आओ.....पहले मैं द्वारकाधीश को भोग लगाऊँगी.....रसगुल्ले भी, और राजभोग भी।\"
\"सच पायल.....बहुत बड़ी जीत है तुम्हारी। हम इसे ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे।\" अजय फूफासा ने मेरी ओर हाथ मिलाने को बढ़ाया लेकिन मैंने उनके गले में अपनी दोनों बाँहें डाल दीं-
\"अब बुआ, कहने मत लगना कि बड़ी दादी नहीं मानेंगी।\"
\"इसी का तो डर है पायल.....सबसे ज़्यादा विरोध माँ से ही मिलेगा। बाबूजी तो तटस्थ हैं, साधु स्वभाव है उनका।\"
\"कुछ भी हो.....अब मेरा जाना तो निश्चित है।\" चाय का आख़िरी सिप लेकर मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने उठ पड़ी।
\"तुम किसी बाद का तनाव मन में न लाना पायल, हम लोग सब सम्हाल लेंगे।\" उठते-उठते बुआ ने मेरा मन तसल्ली से भर दिया।
मेरी इच्छा रोम यूनिवर्सिटी से ही पी-एच.डी. करने की थी। आज मेरा रोम-रोम मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति का शुक्रगुज़ार है जिसकी बदौलत मेरा सपना साकार हुआ। अब मैं निश्चय ही अपनी मंजिल पा लूँगी। अम्मा सुनेंगी तो बेहद खुश होंगी। बड़ी दादी की मुझे परवाह नहीं, वैसे ही वे मुझे समाज विद्रोहिणी समझती हैं बल्कि समाज विद्रोहिणी, रीति रिवाज़ विद्रोहिणी क़रार दे चुकी हैं। क्योंकि न मैं गृहस्थी की गुलामी कर सकती, न गृहस्थी के लिए समर्पिता बन देवी कहला सकती। उनकी नज़रों में औरत के यही दो रूप हैं....यही दो रूप उन्होंने दादी पर भी थोपे। वे जब नौ वर्ष की बालिका वधू बनकर प्रताप भवन आई थीं तो उन्हें अपनी और अपने साथ पूरी गृहस्थी की गुलामी सिखला दी थी उन्होंने। इतनी समृद्धि, दास दासी, नौकर-चाकर सब के होते हुए वे गुलाम ही बनी रहीं.....जब बाबा चल बसे तो उन्हें सती बनाकर देवी का दर्जा दिलाने की कोशिश की उन्होंने। नाकामयाब रहीं यह बात दीगर है। लेकिन मुझ पर उनका वश नहीं चलेगा। मुझे तो अपने मानव स्वरुप का चुनाव करना है और वो मैंने कर लिया.....पदार्थ बनकर.....पुरुष की संपत्ति बनकर नहीं जीना है मुझे बल्कि गति बनकर जीना है।
प्रताप भवन रोशनी के लट्टुओं से जगमगा उठा था। रजनी बुआ की शादी में अम्मा का इंतज़ाम काबिले तारीफ था.....घर मेहमानों से खचाखच भरा था। हँसी, ठिठोली, गाना बजाना, हल्दी उबटन का आलम था लेकिन मुझे दादी के बिना सब कुछ सूना और फीका-फीका लग रहा था। हालाँकि मेरे इटली जाकर पी-एच.डी. करने की ख़बर ने पूरे प्रताप भवन में तहलका-सा मचा दिया था। सबकी अपनी-अपनी तरह की प्रतिक्रियाएँ.....
तो अब डॉक्टरी पढ़ेंगी बन्नो.....हमारे खानदान में तो किसी लड़की ने डॉक्टरी पढ़ी नहीं.....ऊँह.....होता क्या है.....ज़माने भर की किताबें बाँच लो.....दूल्हा मिलेगा व्यापारी ही..... हमारे पुश्तान पुश्त की यही तो ख़ासियत रही है। लेकिन पायल.....विदेश जाना कोई ढंग की बात लगती नहीं हमें.....
कहने वालों को अपनी ही बात की फूहड़ता रजनी बुआ के कारण तुरंत महसूस होने लगी.....कोई बुजुर्ग सी महिला ने बात ढँकी-\'विदेश जाना तो तब सोहे जब घरवाला साथ हो।\'
\"अरे मामीसा, आप यहाँ बैठी हैं? उधर मेहँदी मांडने में आपका इंतज़ार हो रहा है।\"
हँसी.....खिलखिलाहट.....व्यंग्य.....बरसों से चली आ रही वैवाहिक परंपरा में कहीं कोई बदलाव नहीं.....
रजनी बुआ की शादी में प्रताप भवन से संबंध रखने वाला मालवगढ़ का हर घर शामिल हुआ था। बस नहीं आई तो मारिया.....बड़ी मानिनी निकली। अपनी शपथ को दृढ़ता से निभा रही है। हालाँकि बड़ी दादी को उसकी कमी बहुत खलती है। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई है भी नहीं। दो-चार नर्सें आई थी पर बड़ी दादी के कर्कश स्वभाव ने उन्हें टिकने न दिया।
रजनी बुआ की बिदा होते ही मैं मारिया से मिलने मालविका स्मृति केंद्र गई। मुझे देखते ही वह हुलसकर मुझसे लिपट गई-\"अरे पायल बाई.....आप?\" उसने मुझे माथा, गाल, पलकें और हाथों पर प्रेम भरे चुम्बनों से नहला दिया-\"अच्छे से निपट गई न रजनी बाई की शादी?\"
\"तुम तो आईं नहीं मारिया? प्रताप भवन की लड़कियों में से यह आख़िरी शादी थी?\" मैंने उलाहना दिया।
\"मैं तो वनवास भोग रही हूँ बड़ी आंटी का दिया।\" उसने पलकें झुकाकर उत्तर दिया।
थोड़ी देर ख़ामोशी रही। कहते हैं जब दर्द बराबर-बराबर अपनी तासीर हर दिल में बाँटता है तो कहने को कुछ शेष नहीं रहता। एक शून्य चारों ओर फैल जाता है जो उस दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। मारिया ने ही ख़ामोशी तोड़ी-
\"छोटी आंटी मुझे बराबर शिमला से ख़त लिखती रहती हैं.....प्रताप भवन मैं जाती नहीं लेकिन वहाँ की हर घटना से उन्हें वाकिफ़ कराती रहती हूँ। एक बार.....हाँ, पिछले जाड़ों में ही वे मिस्टर जिम के साथ यहाँ आई थीं। किसी से मिली नहीं.....चुपचाप मुझे बंगले पर बुलवा लिया था। अरे, क्या बताऊँ पायल बाई, नूर बरस रहा था उनके चेहरे से। वे सचमुच महान आत्मा हैं क्योंकि उनके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं है और जिनके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होती उन्हें ही क्रूसीफ़ाई होना पड़ता है.....प्रभु यीशु क्षमा करें।\"
उसने सीने पर क्रॉस बनाया।
हमारी बातों के दौरान थॉमस ने कॉफी और बिस्किट मँगवा लिये थे। कॉफी का प्याला मेरे हाथ में देते हुए उसने पूछा-\"आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है पायल बाई।\"
\"वही तो बताने आई हूँ। मैं तीन साल के लिए इटली जा रही हूँ पी-एच.डी. करने। स्कॉलरशिप मिली है मुझे।\"
\"अरे वाह.....यह तो बहुत बढ़िया ख़बर है। मैं आज ही छोटी आंटी को ख़त लिखूँगी। पायल बाई.....आपमें कुछ बात ज़रूर है तभी तो छोटी आंटी बहुत सीरियसली आपको अपनी माँ कहती हैं। गुणों का भंडार हैं आप।\"
\"बस.....बस.....मुझे अपना सेवा केंद्र नहीं घुमाओगी?\" मैंने कॉफी ख़तम कर उठते हुए कहा।
\"क्यों नहीं.....और यह सेवा केंद्र आपका भी तो है, केवल मेरा नहीं।\"
वह भी उठ खड़ी हुई और बड़े उत्साह से एक-एक जगह की जानकारी मुझे देने लगी। अब तो और विस्तार कर लिया है उसने कमरों का और अधिक लोग नियुक्त कर लिये हैं। मारिया और थॉमस के प्रेम ने मिलकर जो यह मानव सेवा केंद्र का घरौंदा सजाया है वह किसी ताजमहल से कम नहीं। प्रेम का ऐसा गतिमान रूप जो बीमारी, रुकी हुई ज़िंदगी को जीने लायक बनाता है। बल्कि मेरी नज़रों में तो ताजमहल से बढ़कर है। ताजमहल सिर्फ़ मक़बरा बनकर रह गया। वहाँ ज़िंदगी की रवानी नहीं है, गीत नहीं है.....एक निराशा है..... उदासी है.....तनहाई है और मारिया और थॉमस के इस ताजमहल में आशा है, त्याग और समर्पण है। मैंने मन-ही-मन इस प्रेम के प्रतीक को नमन किया।
विदा के समय मैंने मारिया के दोनों हाथ अपने माथे को छुलाए। ताँगे में बैठते हुए मैंने देखा वे दोनों रुमाल से अपनी आँखें पोंछ रहे थे।
प्रताप भवन रजनी बुआ की बिदा के बाद एकदम सूना हो गया था। मेहमान भी एक-एक कर बिदा हो गए थे। वैसे भी इस बार मैं पूरी शादी से तटस्थ-सी रही। नेग दस्तूर निभाने के बावजूद मन कहीं और लगा रहा। दादी के बिना प्रताप भवन ज़रा भी नहीं सुहा रहा था। ऊपर से बड़ी दादी बिस्तर पर पड़ी-पड़ी कोसती रहतीं-\"तुम पायल, चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, विदेशियों की धरती पे सिर पटक आओ लेकिन एक बात गाँठ बाँध लो कि विधवा दूसरी शादी करके अपना सतीत्व खो देती है। मालविका का किया तो तुम्हें भोगना ही होगा। रजनी तो जैसे-तैसे निपट गई लेकिन तुम्हारी गृहस्थी बसना मुश्किल है।\"
मन हुआ कहूँ गृहस्थी बसाकर आपको क्या मिला बड़ी दादी? लेकिन जहाँ ज़िद्द हो कि किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी वहाँ कुछ कहने से फ़ायदा भी क्या?
लेकिन अम्मा नहीं रोक पाईं अपने को-\"आप क्यों कोसती रहती हैं दिन-रात उसे।\"
\"सच्ची बात तुम लोगों को कोसना लगे है। उलटी रीत हो गई है इस खानदान की अब तो। तू ही बता पायल बिट्टो, क्या मिला तुझे? घर की चौखट पार करके क्या न्याय मिलता है, क्या बाहर की दुनिया अपनी हो जाती है?\"
ज़िंदगी में पहली बार बड़ी दादी के मुँह से सटीक बात सुनने को मिली। कहना चाहा, न्याय तो नहीं मिलता लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत आ जाती है लेकिन चुप ही रही। बड़ी दादी से कुछ भी कहना मुझे दोहरा दुख दे जाता था क्योंकि मैं देख रही थी धीरे-धीरे उनकी देह का घुलना.....मृत्यु निश्चित है लेकिन इतनी दूर कि पदचाप तक नहीं.....लेकिन उसके इस ओर चल पड़ने की सूचना घुलती देह स्पष्ट दे रही है.....आह, ज़िंदगी का इतना कड़वा यथार्थ!!
वे बड़बड़ाती रहीं-\"रजनी को उधर विदेश में ससुराल मिली जाके.....मालविका का किया भुगता तो भई उसने भी। अब उसके साथ कुछ ऊँच-नीच हो तो न कोई देखने वाला.....न सुनने वाला। तुम भी परदेस जा रही हो.....पूरे घर की मत मारी गई है। अरे अब शादी-ब्याह करके अपनी गृहस्थी सम्हालो तो वो बात तुम्हारी अम्मा को रुचती नहीं.....करो, जिसके जो जी में आवे।\"
भारी मन से अम्मा मेरे इटली जाने की तैयारी में जुट गईं। कुछ हलकी-फुलकी पोशाकें बनवा दीं उन्होंने और स्वेटर, शॉल, पुलोवर, मफ़लर से अटैची भर दी।
\"सम्हालकर रहना.....ज़्यादा-से-ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाना। रिसर्च का काम तपस्या है पूरी। खाने-पीने तक का होश नहीं रहता। अब तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा।\"
अम्मा अटैची जमाती जाती थीं और सीख भी दिए जाती थीं। न जाने अम्मा कब ये मानेंगी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। शादी की भाग-दौड़ में बाबूजी बीमार पड़ गए थे वरना वे भी मेरे साथ कलकत्ता चलते। उनके लिए वीरेंद्र कुर्सी ले आया था। मैंने उन्हें कुर्सी पर बिठाकर शॉल अच्छी तरह उढ़ा दिया-\"किसी बात की चिंता न करें बाबूजी, बस आशीर्वाद दें।\" और मैंने उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने गद्गद हो मुझे गले से लगा लिया-\"हमारा नाम रोशन करना बेटा।\"
तभी वीरेंद्र आ गया। जीप में मेरा सामान रखते हुए कहने लगा-\"मैं तो बनारस जाने की सोच रहा हूँ जीजी.....वहीँ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ।\"
मैंने उसे बाँहों में भरकर चूम लिया-\"तुम जो भी करोगे, अच्छा ही करोगे। बस, अम्मा-बाबूजी को अकेलापन महसूस मत होने देना।\"
अम्मा संध्या बुआ की गोद भराई रस्म कर रही थीं। बुआ के आँचल में चावल, मेवे मिश्री, पान सुपारी डालकर उन्होंने उनकी माँग में सिंदूर लगाया और गले लगाकर भेंट भरी। उन्होंने मेरे माथे पर भी रोली लगाईं और संध्या बुआ के साथ मेरे भी मुँह में पेड़ा ठूँसते हुए छलछलाई आँखों से आशीर्वाद दिया। मैंने भी छलछलाई आँखों सहित अम्मा के सीने में मुँह गड़ा दिया। अब मिलना तो तीन वर्षों बाद ही होगा। बिदाई के क्षण भारी थे.....ज्यों बदली बरसने की चाह में झुकी पड़ रही थी। मैंने जीप के पायदान पर पैर रखा ही था कि भीतरी कमरों से बड़ी दादी की तेज़ आवाज आई-\"अरी कंचन.....पायल गई क्या?\"
पैरों में पंख उग आए जैसे। मैं भागती हुई गई और लेटी हुई बड़ी दादी की दुर्बल काया से लिपटकर रो पड़ी। उन्होंने भी निर्बाध बहते आँसुओं को गालों पर से पोछा और मुट्ठी में दबा शगुन का नोट मेरी हथेलियों में दबा दिया-\"ले रख.....जब जिद्दिया गई है उधर जाने को तो इसे लेकर जा.....\"
फिर कंचन से बोलीं-\"थाली इधर ला न, खड़ी है भुच्च-सी।\"
और कंचन के हाथ से रोली चावल की थाली ले मेरे माथे पर शगुन का रूचना लगा दिया-\"पोता बिदा हो रहा है मेरा तो.....जा.....ईश्वर तेरा भला करें।\"
अब की बार मुझसे किसी की ओर देखा नहीं गया। नज़रें नीची किए होंठों से उबलती रुलाई रुमाल से दबाकर मैं संध्या बुआ के बाजू में जीप में बैठ गई। स्टार्ट होते ही ढेर सारी धूल और धुएँ के गुबार की आड़ में तमाम चेहरे अपने आप ही छिप गए।
कलकत्ता पहुँचकर कॉलेज के कितने अधिक काम निपटाने थे। नई लैक्चरर को चार्ज हैंडओवर करना था। कुछ करेक्शन के बंडल थे प्रथम वर्ष के छात्रों के.....उन्हें रात-दिन जागकर जाँचा। प्रिंसिपल मुझे फ़ेयरवेल देना चाह रही थीं और प्राध्यापक वर्ग दावत माँग रहा था मुझसे। सो दोनों काम सम्मिलित हुए.....अच्छा लगा।
सबकी ओर से दी गई भावभीनी बिदाई ने मुझमें ये चुनौती तो जगा ही दी थी कि अब मुझे सफल होकर लौटना है।
बिदाई की आख़िरी रात संध्या बुआ और फूफासा रात भर मेरे साथ जागते रहे। प्रताप भवन की कितनी सारी बातें याद कीं हमने लेकिन दादी का सती होने के लिए जाने वाला दिन याद कर हम भीतर तक हिल गए और उसी उदासी में सवेरे ने दस्तक दी।
अब कैसे बयाँ करूँ अपने जाने की सुबह.....ऐसी तैयारी हो रही थी मेरे जाने की कि जैसे अब लौटूँगी ही नहीं। बुआ, फूफासा को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। बंगले के हर कमरे में उनका आना-जाना लगा था.....यह अफ़रा-तफ़री तब रुकी जब एयरपोर्ट जाने का वक़्त नजदीक आन पहुँचा।
\"तैयार हो पायल?\" फूफासा के पूछने पर मैं हँस पड़ी।
\"मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। आप ही लोगों की तैयारी ख़त्म नहीं हो पा रही है।\"
दोनों हँस दिए। संध्या बुआ के कुंदकली-से शुभ्र दाँतों की हँसी को मैंने मुट्ठी में समेट लिया जैसे अनजान पथ पर चल पड़ने वाला राही अपनी निधि समेटता है।
एयरपोर्ट की ओर जाते हुए बादलों का झुक आना अजय फूफासा को चिंतित कर गया था-\"कहीं फ़्लाइट न कैंसिल हो जाए।\"
लेकिन मेरे मन में तमाम खुशियों की दस्तक हो रही थी। हवा कार की खिड़की को छूती और फिर सड़क की बाईं ओर बाँस के झुरमुट में छुपकर बाँसुरी बजाने लगती। मौसम में वैसे भी खुनकी थी।
\"इटली तक पहुँचते-पहुँचते प्लेन की सूँ-सूँ आवाज से तुम्हारे कान सुन्न हो जाएँगे पायल.....रुई जरूर लगा लेना कानों में और जिस भी समय पहुँचो, पहला फोन मुझे.....समझीं?\" संध्या बुआ की हिदायत पर मैं मुस्कुराना चाहती थी पर दादी की याद ने मुझे कचोट-सा लिया। इसी तरह दादी मेरी हर बात का ख़याल रखती थीं। न जाने कैसे एक ही वक़्त में वे कोठी के हर शख़्स की ज़रुरत महसूस कर लेती थीं और जुट जाती थीं। उन्हें अगर पता लगे कि मैं पढ़ाई के लिए विदेश जा रही हूँ तो कितनी अधिक खुश हों वे.....बल्कि खुश हो भी चुकी होंगी अब तक मारिया के मार्फत लिखे मेरे पत्र से। हमारे पास तो उन्हें सूचना देने का कोई साधन ही नहीं है.....न उनका पता, न फोन नंबर.....मारिया भी माँगने पर टाल जाती है। न जाने क्यों.....!
गाड़ी ढलान पर आ गई थी। ठंडी हवा ने मेरे बालों की लटों को उड़ाकर माथे पर बिखरा दिया था। मैंने बैग से स्कार्फ़ निकालकर कसकर बाँध लिया। बुआ का मेरे माथे पर लगाया हल्दी चावल का तिलक धुँधला पड़ गया था लेकिन मुँह में केसरी राजभोग का स्वाद बरकरार था। बुआ मुझे अपनी बेटी की जगह मानने लगी थीं क्योंकि शादी के इतने सालों बाद भी उन्हें औलाद नसीब नहीं हुई थी। दोनों के चेहरों की मुस्कुराहट व्यथा में परिवर्तित थी जबकि दोनों ने सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहा था। अजय फूफासा में गंभीरता का पुट घुलता जा रहा था और बुआ तनहा महसूस करने लगी थीं। क़ाश, कोई किलकारी उनकी तनहाई का भेदन कर पाती!
एयरपोर्ट में ख़ासी चहल-पहल थी.....मेरी फ़्लाइट लगभग तैयार थी और सौ-सौ हिदायतों के साथ मैं प्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी.....जाने क्यों दूर खड़े हाथ हिलाते अजय फूफासा को देख मुझे बाबूजी की याद आ गई जो तबीयत ख़राब होने के कारण मुझे पहुँचाने नहीं आ पाए थे लेकिन मुझे लेकर आश्वस्त भी बहुत थे। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रताप भवन के इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी लड़की ने इतना साहस किया था.....कोठी की चहार-दीवारी से निकल तमाम रीति रिवाज़ों को नकारते हुए अपने लिए एक नई सृष्टि की रचना करने चली थी। हाँ.....यह सृजन विप्लव साबित होगा लेकिन दिशाओं को उज्ज्वल भी यही सृजन करेगा.....अब औरत के मोम-सा पिघलने के दिन गए।
रोम की धरती पर क़दम रखते ही एक अपरिचित एहसास ने मुझे चौंका दिया.....क्या यही है नीरो बादशाह का राज्य.....राजधानी रोम.....ऑल रोड्स लीड टु रोम.....सारी सड़कें रोम की ओर जाती हैं। मैं कहाँ जाऊँ.....कैसे?
अजय फूफासा ने अपने एक परिचित स्कॉलर को, जो रोम यूनिवर्सिटी में पी-एच.डी. कर रहा था, मेरे वहाँ पहुँचने की इत्तिला दे दी थी। वही मुझे लेने आया था और उसी के द्वारा मेरे रहने का प्रबंध होना था। मैंने एयरपोर्ट पर उसके नाम की घोषणा करवाकर उसे अपने पास बुलवाया। ऊँचे कद के, साँवले रंग के बेहद शिष्ट बंगाली युवक को अपनी ओर तेज़ी से आता देख मैं समझ गई.....दो क़दम आगे बढ़ी कि उसने मेरा अभिवादन किया-
\"मैं हूँ मिहिर सेन.....\"
\"परिचित हूँ आपके नाम से। मिलने का सौभाग्य आज मिला।\" मिहिर ने मेरा सामान कार की डिक्की में रखा और मेरे लिए शिष्टतावश कार का दरवाज़ा खोला-\"बैठिए.....मिस पायल सिंह।\"
\"अरे!\" मैं हँस पड़ी-\"इतनी फॉर्मेल्टी में विदेशी जगह में कैसे रह पाऊँगी?\"
\"मज़े से.....एक बेहतरीन कमरा आपके लिए किराए पर ले लिया है। बाजू में ही मेरा भी कमरा है।\"
\"वाह, यह तो बहुत अच्छा है।\"
कार की खिड़की से मैं पत्थरों से बने घर और मल्टीस्टार बिल्डिंगों का नज़ारा देखने लगी। बड़ी-बड़ी खिड़कियों वाले पत्थरों से बने घर रोमन स्थापत्य की तस्वीर पेश कर रहे थे। एक तंग-सी पत्थरों से जड़ी गली में मिहिर ने कार रोक दी। घुमावदार सीढ़ियों को पार कर हम जिस कमरे में पहुँचे वह कई और कमरों वाले बड़े से घर का एक ठंडा कमरा था। शायद पूरा घर बंद था। मिहिर ने स्टीम हीटर चला दिया। धीरे-धीरे कमरा गर्म होने लगा। एक ओर बड़ा-सा तख़्त था जिस पर मोटा गुदगुदा बिस्तर, कंबल, लिहाफ़, तकिया था। तख़्त के नीचे ऊनी पाँवपोश। दीवार पर ठुकी लकड़ी की आलमारी जिसमें कई हैंगरों वाला वॉड्रोब था। कमरे की छत काफ़ी ऊँची थी।
\"आप अपना सामान वग़ैरह ठीक-ठाक कर लीजिए। तब तक मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। कल से तो फिर यूनिवर्सिटी चलना ही है।\"
भूख तो लगी थी पर एकदम अकेली होना भी नहीं चाहती थी मैं। लेकिन मिहिर को रोकना बेकार था। उसके जाते ही मैंने सारा सामान खोल डाला और सलवार कुरता पहनकर स्वेटर, मफ़लर, मोज़े पहन लिये। बेतहाशा ठंड थी। पानी तो छूना भी कठिन था।
मिहिर पीज़ा और रेड वाइन लेकर जल्दी ही लौट आया। मैं उस अद्भुत खाद्य पदार्थ को देख रही थी कि मिहिर हँस पड़ा-\"ये यहाँ की विशेष डिश है पीज़ा.....बहुत स्वादिष्ट होता है यह। ये एक तरह से पूरा भोजन है.....आटा और सब्ज़ियों का अद्भुत मेल.....चीज़, सॉस सब कुछ होता है इसमें।\"
उसने पीज़ा के टुकड़ों को काग़ज़ के पैक में से प्लेटों में परोसा-\"लीजिए, खाइए। और ये रेड वाइन भी थोड़ी ले लीजिए। शरीर में गर्मी लाने के लिए यह ज़रूरी है वरना अकड़ जाएँगी।\"
मैं ताज्जुब से मिहिर को देखने लगी जो कुछ ही घंटों में अपरिचय का दायरा तोड़ चुका था और यूँ लग रहा था जैसे हम वर्षों से परिचित हों। मैंने हँसते हुए पीज़ा का टुकड़ा उठाया-
\"मिहिर जी, अभी मुझे समझने तो दीजिए रोम को। इतनी ठंड तो हमारे मालवगढ़ में भी पड़ती है, जब पाला पड़ता है.....फसलें ठिठुर जाती हैं। आप संकोच मत करिए.....आराम से पीजिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी मैं खाने-पीने के मामले में ज़रा भी झंझट नहीं करती। जो मिल गया, खा लिया।\"
मिहिर हँस पड़ा-\"यानी स्वभाव से तपस्विनी। पायल जी, दुनिया में मैंने दो तरह के इंसान देखे; एक वे जो भोजन खाते हैं, दूसरे वे जिन्हें भोजन खाता है। मुझे खुशी है आपको भोजन नहीं खाता।\"
कहते हुए वह ठहाका लगाकर हँसा और एक ही घूँट में वाइन का गिलास ख़त्म कर पीज़ा खाने लगा। पीज़ा सचमुच स्वादिष्ट था या भूख में ज़्यादा अच्छा लग रहा हो।
हम देर तक रिसर्च वर्क पर चर्चा करते रहे। दोनों के विषय, गाइड और यूनिवर्सिटी एक ही थे और विदेश में ऐसा होना बहुत बड़ी बात है.....जबकि हम पहले बिल्कुल अपरिचित थे। मिहिर के जाते ही मैं बिस्तर में दुबक गई। बाहर तेज़ हवा चल रही थी और अजनबी जगह में तरह-तरह की पदचाप मुझे सहमा रही थी। शायद इसीलिए कि इस कमरे में मेरी पहली रात थी। मुझे अम्मा की बेतहाशा याद आई.....संध्या बुआ और फूफासा मानो नज़दीक ही खड़े नज़र आए.....अरे हाँ, उन्हें तो फोन भी करना है पर अब इन सुनसान सड़कों पर मैं कहाँ ढूँढने जाऊँ फोन की सुविधा? कल मिहिर से कहूँगी। या शायद अजय फूफासा खुद ही यूनिवर्सिटी फोन कर लें।
काफ़ी देर बाद मुझे नींद आई। और इतनी गहरी कि सुबह मिहिर के दरवाज़ा खटखटाने पर ही नींद टूटी। अपने देर तक सोने के कारण मैं शरमा भी गई। वह तरोताज़ा दिख रहा था और उसके हाथ में कॉफी का थर्मस था।
\"सॉरी मिहिर जी, मैं अभी तैयार हुई जाती हूँ। असल में नींद काफी देर से आई।\" कहकर मैं बाथरूम में घुस गई।
अजय फूफासा ने सचमुच यूनिवर्सिटी में फोन करके मेरा हालचाल जाना.....संध्या बुआ रूठी हुई हैं.....मैं फोन करके मना लूँ उन्हें.....उनका आदेश था। मैंने कहना चाहा कि यहाँ तो अभी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या है? सब कुछ नया-नया है। पाँवों के नीचे की धरती तक अजनबी है पर बुआ समझें तब न! वे तो जब तक मेरी आवाज़ नहीं सुन लेंगी उन्हें यक़ीन ही नहीं होगा कि मैं रोम पहुँच गई हूँ। और यह ज़िद्द भी लिये बैठी हैं कि फोन मैं ही करूँ। तय हुआ कि मिहिर भी अपना काम जल्दी ख़त्म कर देगा ताकि हम इन कामों के लिए वक़्त निकाल सकें। यूनिवर्सिटी तो मुझे इतनी पसंद आई थी कि वहाँ रह जाने का मन कर रहा था।
मिहिर और मैं जिस इलाक़े में रहते थे वहाँ अधिकतर विद्यार्थी ही रहते थे विभिन्न देशों से आए थे। मेरे पड़ोस में एक जापानी विद्यार्थी ठहरा था जो अपने फुरसत के समय गिटार बजाया करता था। वह भी रोम यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर था। वह जब भी मिलता अपने देश की यशोगाथा में डूब जाता। यहाँ से पढ़ाई समाप्त कर वह अपने देश लौटेगा और ओसाका यूनिवर्सिटी में अध्यापन करेगा। जब मिहिर, मैं और यह जापानी साथ होते तो वह अपने देश के गर्म पानी के सोतों, चीड़, देवदार के जंगलों और चक्करदार पहाड़ी सड़कों का ज़िक्र करता। मेरा देश भी तो गर्म पानी के सोतों और चीड़, देवदार के जंगलों वाला है। फिर हम कहाँ से अपरिचित हैं और क्यों और जब देश की सीमाएँ हर दूसरे देश से जुड़ी हैं तो रजनी बुआ की शादी विदेश में होने पर प्रताप भवन इतना उदास क्यों था? क्यों बड़ी दादी पीड़ा से सराबोर थीं?
समय गतिशील है। वह किसी का इंतज़ार नहीं करता। न समय, न सागर की लहरें। लेकिन लहरों का क्रम लगातार तट को छूकर वापस लौट जाने और फिर दुबारा आने का दस्तूर निभाता चलता है और समय दस्तूर नहीं निभाता। वह बीतता चलता है। रोम में आए पूरा एक बरस बीत गया। इस एक बरस में मिहिर ने मुझे रोम के चप्पे-चप्पे से परिचित करा दिया। यहाँ का सूर्यास्त.....इटली के देहातों का भ्रमण, पहाड़ियों का प्राकृतिक दृश्य, ठंड, कोहरा, धुंध.....एक-एक क्षण जी चुकी हूँ मैं। मैंने देखे हैं यहाँ के फुटपाथ जिन पर भिखारी मक्खियों-से भिनभिनाते हैं.....ढाबे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं.....टाइबर नदी का किनारा जहाँ अक़्सर आवारा कुत्ते भौंकते रहते हैं। पत्थरों के घर, मल्टी स्टोरीज़ बिल्डिंग.....तंग गलियाँ। कभी-कभी ऊब जाती हूँ इनसे तब अपना मालवगढ़ बहुत याद आता है। आलिशान प्रताप भवन..... चहुँओर बिखरी समृद्धि। मिहिर मेरे मूड्स समझ लेता है और मुझे ज़बरदस्ती घुमाने ले जाता है जंगलों की ओर। खुली फैली हरियाली। मीलों फैले अंगूर, संतरे और जैतून के बगीचे। तराई में इनके जंगल ही जंगल हैं। मैं यूनिवर्सिटी की टीम के साथ क्रेट आयरलैंड भी देख चुकी हैं। जहाँ ज्वालामुखी हैं और उनमें से हर समय लावा निकलता रहता है। लावे की खूबसूरत झालरें रात की रोशनी में बहुत खूबसूरत लगती हैं। बहुत आकर्षित करती हैं।
बचपन से ही मुझे नीरो बादशाह ने बहुत डिस्टर्ब किया है। उसकी निर्ममता और शैतानी प्रवृत्तियों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है कि आख़िर क्यों रोम ने इतना सहा? क्या सारी व्यवस्था गूँगी-बहरी हो रही थी? क्या किसी के कान पर जूँ तक नहीं रेंग रही थी जब रोम जल रहा था और नीरो अपना गिटार बजा रहा था? यह सवाल रेंगता है मेरे मन में और मैं विचलित हो जाती हूँ। कोलोसियम पैलेस देखकर भी मैं तड़प उठी थी। उस विशाल पैलेस के झरोखे में बैठकर वह भूखे शेर के सामने असहाय आदमी की तड़प देखता था। इतना सैडिस्ट! ओह!
इस बार २५ दिसंबर को बेतहाशा बर्फ़ गिरी थी और उस बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने हम पोप पॉल की सिटी वेटिकान गए थे। मिहिर ने बताया कि यहाँ पोप पॉल के नाम के सिक्के भी चलते हैं।
मैंने आश्चर्य से मिहिर को देखा था। भीड़ लाखों की तादाद में थी, बर्फ़बारी के बावजूद, क्योंकि पोप अपने पैलेस की गोल बाल्कनी से सबको दर्शन देते थे। धर्म में आस्था अमूमन पूरे विश्व में है।
हम पूरा पैलेस नहीं घूम पाए। पूरा पैलेस घूमने में सात दिन लगते हैं। पैलेस के अंदर बड़े-बड़े दीवार तक ऊँचे कालीनों में ईसा मसीह के जीवन की प्रत्येक घटना अक़्स है।
लेकिन मैं ट्रिवोली फाउंटेन ज़रूर गई और पीठ के पीछे से सिक्का भी उछाला क्योंकि मिहिर ने कहा था कि इस फ़व्वारे के पानी में सिक्का डालने से आदमी दुबारा यहाँ आता है।
.....हाँ, मैं दुबारा यहाँ आना चाहती हूँ.....एकदम निश्चिंतता में.....जब पढ़ाई का बोझ सिर पर न हो और जब मैं इस बात पर रिसर्च कर सकूँ कि नीरो ऐसा क्यों था? वैसे रोम की आबोहवा में निश्चिंतता तो मैंने महसूस की। लापरवाही और हर क्षण को भरपूर जी लेने की हर व्यक्ति में साध। मिहिर भी इतनी पढ़ाई के बावजूद कितना एन्जॉय करता है। बता रहा था कि एक बार उसने एक अंग्रेज़ लड़के के साथ खूब नाचा, गाने गाए और चुल्लू में बोतल से धार बनाकर वाइन पी। चिंतामुक्त लोग, चिंतामुक्त शहर जहाँ नीरो बादशाह गिटार बजाता था जिसे सुनने की मजबूरी में उसका वज़ीर एन्टीनो बोर होता रहता था। शायद इसी निश्चिंतता में वह जलते हुए रोम को देखकर गिटार बजा रहा होगा लेकिन मेरी चिंताएँ समाप्त नहीं होतीं। घर से मिली ख़बरें मुझे तनाव से भर देती हैं। अम्मा के ख़तों में इतना विस्तृत हवाला होता है हर एक बात का कि लगता है सिनेमा की रील आँखों के आगे खुलती जा रही है। वीरेंद्र ने बनारस में अपना सिल्क उद्योग शुरू कर दिया है। और अम्मा-बाबूजी भी वहीँ जाकर रहने लगे हैं। वीरेंद्र ने कालीन और बनारसी सिल्क की मिलें ख़रीदकर अच्छा-ख़ासा अपना व्यापार शुरू कर दिया है। वह तीक्ष्ण बुद्धि का है और कपड़ों का व्यापार तो ख़ानदानी है ही। शहर के बाहरी इलाक़े में बहुत बड़ा हरा-भरा प्लॉट ख़रीदकर एक विशाल बंगला बनवाया है उसने और फार्म हाउस की तरह तमाम फलों, सब्ज़ियों के बगीचे। उसकी इच्छा तो गाय ख़रीदने की भी थी पर अम्मा ने मना कर दिया। यह सब अपने वश की बात नहीं.....न कभी हमने मवेशी पाले हैं। घोड़े ज़रूर रखे पर अब तो कारों का ज़माना आ गया है। नित नए मॉडल बदलते रहो कार के। जसोदा भी अम्मा के साथ ही बनारस आ गई है और पन्ना के बापू ने पन्ना की शादी कर दी है। कंचन के ज़िम्मे है बड़ी दादी की चाकरी। वह भी भुन्नाती रहती है। दादी की दासी होने के कारण ज़ाहिर है कि वह दादी से स्नेह करती थी और उनके संग हुए अत्याचार के कारण बड़ी दादी से नफ़रत। बड़े बाबा अक़्सर बनारस में ओझा तांत्रिकों की संगत में रहने लगे थे। वे वहाँ के जंगलों में रहने वाले भीलों से धनुष बाण चलाना सीख रहे थे। कभी-कभार किसी उड़ते परिंदे का शिकार कर लाते और जसोदा से बिनती करते कि इसे पका दे। जसोदा परहेज़ तो करती पर उनकी बात टाल भी नहीं पाती। उस रात वे बंगले के पिछवाड़े बने कमरे में, जो वीरेंद्र ने अपने व्यापारी मिलने-जुलने वालों के लिए बनवाया था चले जाते और बीड़ी पीते हुए गिलास में शराब डालकर अँधेरे में टकटकी बाँध लेते। इतनी समृद्धि, कोठी, ज़मीन, खेत, खलिहान, कपड़ों के कारखाने छोड़कर बड़े बाबा क्यों सधुक्कड़ी पथ पर अग्रसर हैं? क्यों बड़ी दादी को तनहा छोड़ दिया है? यह प्रश्न मुझे मथ डालता। लड़कियाँ कब तक अपनी घर-गृहस्थी छोड़कर उनकी सेवा टहल को आती रहेंगी? उषा बुआ जाती हैं तो संध्या बुआ आ जाती हैं.....रजनी बुआ जल्दी-जल्दी नहीं आ पातीं। वैसे भी वे सिंगापुर में हैं। सातवाँ महीना चल रहा है उनका। तक़लीफ़ ज़्यादा है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है।
वसंत में जब चिनार के पत्ते रक्तिम हो उठे और जब बर्फ़ पिघलकर धरती में छुपे फूलों को खिलने का मौक़ा देने लगी तो अम्मा का ख़त आया कि वीरेंद्र की शादी तय हो गई है। अगले महीने की अट्ठाइस तारीख़ को तिलक चढ़ेगा। मैं जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाऊँ।
तो अम्मा ने मेरे शादी न करने के प्रस्ताव पर अपनी रज़ामंदी की मोहर लगा ही दी। वरना बड़ी बहन के कुँवारी रहते छोटा भाई शादी करे यह कहाँ संभव था। कम-से-कम प्रताप भवन में तो बिल्कुल नहीं। अम्मा ने मुझसे कभी किसी बात के लिए ज़िद्द नहीं की। उन्होंने मेरे अंतर्मन को विकसित होने का पूरा मौका दिया। वे हमेशा कहती हैं-\'पायल, अपने को पहचान लो। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है वरना आत्मा हमेशा धिक्कारती है और आत्मा की धिक्कार बड़ी चुभती है।\'
यही प्रश्न तो मैं अपने से करती हूँ अक़्सर कि मेरी लड़ाई किस बात को लेकर है? या कि मैं अपने उद्देश्यों को व्यवस्थित नहीं कर पा रही हूँ। फिर यह भटकाव जैसी सोच क्यों हो जाती है कभी-कभी। होती है और फौरन सम्हल भी जाती हूँ.....नहीं, मुझे अपनी सोच सतही नहीं रखनी है वरना क़दम डगमगा जाएँगे।
शादी की ख़बर से मन खुशी से भर उठा था। मेरा भैया इतना बड़ा हो गया कि अब दूल्हा बनेगा। बचपन में तीज त्यौहारों पर मुझ पर थोपे गए रीति रिवाज़ों को लेकर मैं हमेशा जिरह कर बैठती थी कि भैया ऐसा क्यों नहीं करता। आज तमाम रीति रिवाज़ों से अपने को फ़ारिग कर लिया है मैंने लेकिन आज मेरा वीरू रीति रिवाज़ों का पालन करता बंधनों में बँध रहा है। जी चाहा पंछी की तरह उड़कर पहुँच जाऊँ उसके पास और उसके पगड़ी सेहरा बँधे सिर की बलैया ले लूँ.....लेकिन.....मैं तो शादी में भी नहीं जा पाऊँगी। इस परदेस में पढ़ाई का तक़ाज़ा मेरे पैरों को रोक रहा है। हँसी-खेल नहीं है उतनी दूर जाना। लेकिन अम्मा के अनुसार शादी का मुहूर्त टाला भी नहीं जा सकता। वीरेंद्र ने आतुर होकर लिखा-
\'क्या करूँ जीजी? तुम्हीं बताओ.....शादी रुक नहीं सकती क्योंकि फिर लंबे समय तक अशुभ ग्रहों का योग है प्रताप भवन पर।\'
पढ़कर मन में बरसों पहले की संध्या बुआ की शादी के समय की घटना दरक़ गई। यही बात कहकर तो बाबूजी ने मालवगढ़ के लोगों के सामने जल्दी शादी करने की दलील पेश की थी जो महज़ एक बहाना थी। आज वही बात सत्य हो रही है। मैंने वीरेंद्र को लिखा-
\"अशुभ ग्रह तो भैया मेरे, बरसों पहले लग गए थे प्रताप भवन पर.....जब दादी को बाबा की चिता पर जलाने के लिए जीवित बिठाला गया था। अब उस अशुभ ग्रह को तुम्हें और तुम्हारी दुल्हन को शुभ बनाना है। कमर कास लो। मैं मन-प्राण से तुम्हारे पास हूँ।\"
और सचमुच जब भी थीसिस की किताबें खोलती.....कानों में शहनाई गूँजने लगती..... एक-एक दृश्य खुली आँखों से देखने लगती। रोम की पतझड़ की ऋतु भी मेरे मन में बहारों जैसी गमक उठी थी। सजे हुए आरता के थाल, बंदनवारें, रंगोली, मेहँदी, ढोलक की थाप पर बन्ना-बन्नी के गीत मेरे आसपास सीप के मुँह से खुलने लगे। सब कुछ साफ़-साफ़ और स्पष्ट दिखाई देने लगा। लौंग, इलायची, दालचीनी की महक़ कमरे को झकझोरने लगी। दाल, बाटी, चूरमा, साँगर की चटपटी सब्ज़ी, टैंटी का अचार.....लगता न जाने कब से सब कुछ छूट चुका है और जो नहीं है वही मानो मथ रहा है।
शादी के महीने भर बाद तस्वीरें भी आ गईं। मैंने मिहिर को दिखाईं। बताया, छोटे भाई की शादी की तस्वीरें हैं.....इसमें देखो पगड़ी बाँधे मेरा भोला-भाला नटखट वीरेंद्र कितना प्यारा लग रहा है.....और ये सोलहों श्रृंगार किए उसकी दुल्हन उर्मिला.....मिहिर को पता था मैंने शादी नहीं करने का फैसला कर लिया है तो ताज्जुब करने लगा था-\'राजस्थानियों में ऐसा रेयर देखने को मिलता है।\'
मुझे रेयर ही तो बनना है.....अनुउपलब्ध.....बचपन से ही विद्रोहिणी जो हूँ।
रजनी बुआ को जुड़वाँ लड़कियाँ हुई हैं। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी कि पूरा घर तनाव में आ गया था। ब्लड प्रैशर हाई हो गया था। ऐसे में ऑपरेशन करना भी ख़तरनाक था और नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं रही थी। बड़े-बड़े डॉक्टरों का जमघट कुछ कर नहीं पा रहा था। जैसे-तैसे सुबह पाँच बजे फॉरसेफ़ ऑपरेशन से लड़कियाँ पैदा हुईं.....बड़ी दादी मृत्यु से लड़ रही रजनी बुआ को तसल्ली देना तो दूर उल्टे कोसने लगीं कि जी का जंजाल लड़की जनी हैं वो भी दो-दो.....और पायल.....सभी आँचल में मुँह दबाकर हँसने लगीं क्योंकि बड़ी अम्माजी ने खुद भी तो जी का जंजाल लड़कियाँ जनी थीं.....वो भी तीन-तीन.....
पत्र पढ़ते हुए मैं ज़ोरों से हँस पड़ी। मेरी हँसी मेरे एकांत कमरे को मुखर कर गई। अम्मा को तो लेखिका होना चाहिए था। इतना जीवंत वर्णन करती हैं कि लगता है आँखों के सामने ही सब घट रहा है। वैसे भी बड़ी दादी बहुत बीमार रहती हैं। बीस साल से बिस्तर पर पड़े-पड़े उनके स्वभाव में अब ज़रा भी नम्रता नहीं रही.....शायद पहले भी नहीं थी। लेकिन तब दादी सम्हाले थीं पूरा घर तो पता नहीं चलता था। अब बहुत बिसूरती हैं उनके लिए वे-\"खोट मेरे नसीब में थी। मेरे ही मन में मंथरा आ बसी थी जो उजड़ गई मेरी अजुध्या। अपनी दुलहिन को वनवास दे दिया।\"
रोते-रोते वे पानी के एक गिलास तक को तरस जातीं। घंटों बाद कंचन पानी लाकर देती। अम्मा भड़क उठी थीं ये देखकर-\"यह क्या कंचन, जब मेरे सामने तुम ऐसा कर रही हो तो मेरे बनारस जाते ही तुम तो तँगा डालोगी इन्हें? तुम्हें यहाँ इन्हीं की देखभाल के लिए रखा गया है।\"
\"लो, पूतना ने दूध पिलाया और मैं पूतना को पोसूँ? अब मुझसे नहीं होती चाकरी।\"
लेकिन चाकरी उसे करनी पड़ी थी। भले ही रो-रोकर। अम्मा के बनारस लौटते ही कोठी में कंचन और बड़ी दादी ही रह गई थीं। वैसे तीनों बुआएँ बारी-बारी से आती थीं लेकिन अपनी ही सौ झंझटों में उलझी रहतीं। तीमारदारी खुद की करनी पड़ती। उषा बुआ अक़्सर रश्क़ करतीं-\"पायल अच्छी निकली.....न गृहस्थी का जंजाल न किसी बाल-बच्चे की ज़िम्मेदारी.....यहाँ तो तीन-तीन हो गए हैं। उन्हीं की किल्ल पों में दिन खप जाता है।\"
\"भगवान हो तुम तो जो तीन बाल गोपालों की माँ हो। पायल को तो ऐसा होना ही था.....किताबों ने उसका दिमाग़ ख़राब कर रखा है। भला, बिना घर गृहस्थी के औरत भली लगती है कभी?\"
क्या मानसिकता है? ज्ञान की खोज सिर्फ पुरुषों के हक़ में ऐसी ही औरतों ने रखी है। औरत की इसी मानसिकता का फ़ायदा उठाया है विश्व भर के धर्मों ने और धार्मिक कठमुल्लाओं ने। रोमन कानून तक में है कि औरत को पुरुषों के संरक्षण में रखना चाहिए ताकि उसकी मूढ़ता पर लगाम लगाईं जा सके। सच है जो मूढ़ होगा, लगाम उसी पर लगेगी इसीलिए तो लगाम के ख़िलाफ़ मैं युद्ध छेड़े हूँ। इसीलिए तो औरत के प्रति भयानक उपेक्षा रखने वाले कुरान, औरत को निकृष्ट वस्तु मानने वाली मनु संहिता और आदम के एकाकीपन को दूर करने के लिए उसी के शरीर से रची गई ईव को प्रमाणित करता ईसाई धर्म मैंने खंगाल डाला है और इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि औरत अपनी तमाम स्थितियों के लिए उतनी ही ज़िम्मेदार है जितने कि पुरुष। शायद यह मेरा अपना अनुभव है.....अपने जीवन से लिया गया।
थीसिस पूरी हो चुकी है। तीन वर्ष देखते-ही-देखते गुज़र गए। यह अंतिम सप्ताह है रोम में हमारा। वैसे मिहिर तो रोम में ही रहेगा। वह परुजिया यूनिवर्सिटी में लैक्चरर हो गया क्योंकि उसका एक खूबसूरत रोमन लड़की से इश्क़ हो गया था और दोनों जल्द शादी करने वाले थे। मेरे लिए उसकी शादी तक रुकना असंभव था।
यह अंतिम सप्ताह है रोम में हमारा। मैं, मिहिर और जापानी (बहुत कठिन है उसका नाम) शाम साथ में गुज़ारना चाहते हैं। पढ़ाई के तनाव के बाद मुक्ति के एहसास के लिए यह ज़रूरी भी था। जापानी ने अपनी अंग्रेज़ गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में दावत का आयोजन किया। भोजन के साथ वाइन भी थी। हम उन्मुक्त होकर गाने गा रहे थे और एक-दूसरे को छेड़ रहे थे। अंग्रेज़ लड़की लगातार सिगरेट पी रही थी और जापानी से लिपटी बैठी थी। काफ़ी रात गए जब थकान से हमारी आँखें मुँदने लगीं तो जापानी और अंग्रेज़ तो बाजू वाले कमरे में चले गए.....मैं सोफ़े पर लेट गई। मिहिर ने कालीन पर ही लंबी तानने का फैसला कर लिया था। वह एक पत्रिका के पन्ने पलटता हुआ सिगरेट पी रहा था।
\"पायल.....क्या तुम सचमुच कभी शादी नहीं करोगी?\"
मैं उसके सवाल से चौंकी-\"क्यों मिहिर, यह सवाल क्यों आया तुम्हारे मन में?\"
\"बस.....ऐसे ही.....यह एकांत.....सुहानी, स्वप्निल रात.....बाजू के कमरे में चल रहा रोमांस.....पायल, क्या तुम्हें अपने अंदर से कोई आवाज़ आती महसूस नहीं होती?\"
मेरे अंदर छन्न से कुछ तिड़का.....क्या मिहिर के प्रति मेरा अथाह विश्वास! नहीं..... वह इतना सतही नहीं है। फिर!!
\"पायल.....देखो मेरी ओर, और बताओ कि तुम ज़िंदगी के इस अहम हिस्से से खुद को क्यों वंचित रखना चाहती हो। माफ़ करना.....अगर मैं खुलकर सैक्स का नाम लूँ.....पर क्यों?\"
अब की बार मैं उठकर बैठ गई-\"जानते हो मिहिर.....कुछ आत्माएँ अभिशप्त होती हैं.....जिनके लिए दुनिया के सब सुख नहीं होते। कुछ के हाथ से मिलते-मिलते भी सुख फिसल जाते हैं और कुछ तमाम उम्र सुख की तलाश में भटकते हैं। मैं एक अभिशप्त आत्मा हूँ.....अपना शाप ढो रही हूँ मिहिर।\" मिहिर मेरे नज़दीक आया। अपने दोनों हाथों में मेरा चेहरा भरकर मेरे होंठ चूम लिये-\"पायल, मैं तुम्हारे लिए सुख की कामना करता हूँ।\"
मैं कुछ नहीं बोली। वह देर तक मेरी हथेलियाँ सहलाता रहा फिर मुझे लेटाकर कंबल ओढ़ा दिया।
मिहिर के इस व्यवहार ने मेरे मन में उसके प्रति सम्मान और बढ़ा दिया।
अपने दोस्त मिहिर से अलविदा कहकर मैं पी-एच.डी. की उपाधि लिये नई उमंग से भरी अपने देश लौटी। एयरपोर्ट पर मेरे ताज्जुब की सीमा नहीं थी जब मैंने देखा कि मुझे लेने अम्मा, बाबूजी, संध्या बुआ, अजय फूफासा, वीरेंद्र और उर्मिला सभी आए थे। वीरेंद्र के हाथों में बड़ी-सी गुलाब के फूलों की माला थी और उर्मिला के हाथों में कैमरा। उसने मुझे माला पहनाकर अपनी गोद में फूल की तरह उठा लिया-\"मेरी ग्रेट डॉक्टर जीजी मिस पायल.....इटली रिटर्न.....देखा उर्मिला मेरी जीजी को.....जैसा मैं वर्णन करता था वैसी ही हैं न?\"
उर्मिला ने मेरे पैर छुए और मेरी बाँहों में समा गई।
कार में बैठकर संध्या बुआ के बंगले तक आते हुए रास्ते में ही अम्मा ने बता दिया कि उर्मिला जल्द ही मुझे बुआ बनाने वाली है और इसके पैर इतने शुभ हैं कि संध्या बाई भी उम्मीदों से हैं।
\"अरे वाह....\" मैंने आगे की सीट पर बैठी संध्या बुआ के गले में पीछे से बाँहें डाल दीं और उनके गाल चूम लिये-\"यह हुई न बात।\"
\"ये क्या हो रहा है मेरी बीवी के साथ?\" अजय फूफासा ने शरारती लहज़े में कहा तो संध्या बुआ ने तुरंत मेरे गाल पर हल्की-सी चपत लगाई-\"पूरी बिगड़कर लौटी है।\"
रोम से मैं सभी के लिए सौगातें लाई थी। बड़ी दादी के लिए फर का मुलायम शॉल। हँस पड़ा वीरेंद्र शॉल देखकर-\"सूखकर छुआरा हो गई हैं बड़ी दादी.....ये शॉल ओढ़कर पहाड़ी चूहा लगेंगी।\"
हम सब हँस पड़े थे। अम्मा हफ़्ते भर रुकी थीं। मुझे अगले महीने की पहली तारीख़ से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी। सीधे हैड ऑफ़ दि डिपार्टमेंट के पद पर। अम्मा चाहती थीं मैं तब तक मालवगढ़ रह आऊँ। बड़ी दादी का कोई भरोसा नहीं.....डॉक्टरों तक ने उम्मीद छोड़ दी है। मेरे पास पूरे पंद्रह दिन थे। मैं आराम से दस दिन तो मालवगढ़ में रह ही सकती थी। अम्मा, वीरेंद्र और उर्मिला बनारस लौट गए।
शाम को अजय फूफासा दो ख़बरें एक साथ लेकर घर लौटे। एक तो यह कि मेरी मालवगढ़ जाने की टिकट आ गई है और दूसरी कि वे यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ़ फ़ैकल्टी हो गए हैं। पूरा घर खुशियों से जगमगा उठा। मेरे तो पैर ही थिरक उठे। लगता था जैसे पूरा आसमान मुट्ठी में आ गया है.....दिशाएँ लुप्त होती जा रही हैं और एक बड़ी चौड़ी-सी राह आँखों के आगे खुलती चली जा रही है जिसके दोनों किनारों पर दीपक जगमगा रहे हैं। दूर सड़क के छोर से एक नन्हा-सा बच्चा घुँघराले बालों वाला दौड़ता आ रहा है, किलकारी भरता कि सहसा जलते दीपक पर उसका पैर पड़ गया और लौ उसके कपड़ों को सुलगाने लगी। तभी फोन बज उठा। फोन शिमला से था जिम का और सूचना बवंडर से भरी.....कि दादी नहीं रही। मानो आकाश मुट्ठी से फिसलकर टुकड़ा-टुकड़ा हो ज़मीन पर गिर पड़ा हो.....संध्या बुआ के पैर चौखट पर ऐसे टकराए कि वे पेट के बल फ़र्श पर गिर पड़ीं। गिरते ही ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। अजय फूफासा डॉक्टर को बुलाने दौड़े.....फ़ोन मैंने अटैंड किया-जिम कह रहे थे कि कल रात दादी अच्छी-भली डिनर लेकर सोईं। रात के क़रीब सवा दो बजे पानी माँगा जबकि वे प्यास लगने पर खुद ही सिरहाने रखे थर्मस से पानी लेकर पी लेती थीं। लेकिन जिम को जगाकर उन्होंने पानी माँगा.....बताया, सीने में दर्द है, घुटन-सी हो रही है। जब तक डॉक्टर आया, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जिम की आवाज़ अथाह दर्द में डूबी थी। फ़ोन बेआवाज़ हो गया।
आँखों के आगे घिरते अंधकार और सीने से उबल-उबलकर निकलती रुलाई के बीच आँसू भरी आँखों से मैंने देखा.....संध्या बुआ के पलंग के पास बैठी डॉक्टर ने फूफासा को बताया कि आपकी पत्नी का एबॉर्शन हो गया है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि बेबी चार माह का था। मैं ऐंबुलेंस बुलवाती हूँ। खुली आँखों से देखा मेरा स्वप्न इस रूप में फलित होकर सामने आएगा मैंने सोचा भी न था। सचमुच दीपक की लौ ने मेरे नन्हे भाई को गर्भ में ही जला डाला। वह संध्या बुआ की पहली और आख़िरी अजन्मी संतान थी।
बुआ सुबह नर्सिंग होम से लौट आईं पीली, मुरझाई हुई सी। मैं उनकी गोद में गिरकर बुक्का फाड़कर रो पड़ी। अजय फूफासा डाइनिंग टेबल पर अपना सिर पटकने लगे। सदमा दोहरा था। एक तो कभी पिता न बन सकने की पीड़ा, दूसरे उनकी शादी में अहम भूमिका निभाने वाली, समाज के आगे उनकी शादी को चुनौती मानने वाली दादी नहीं रहीं-
\"चलिए बुआ, दादी के अंतिम दर्शन के लिए हम शिमला चलते हैं।\"
पर बुआ जड़ थीं-\"क्या होगा उधर जाकर? पायल, मरने वाला तो चला गया।\"
मैं हक्की-बक्की बुआ को देखने लगी-\"बुआ, क्या हुआ बुआ.....ऐसे क्यों कह रही हैं बुआ?\"
\"ठीक ही कह रही हूँ.....जाने वाला तो चला गया। चाची चली गईं.....सबका उपकार करके, ममता, प्रेम, स्नेह, दया.....धन खुले हाथों लुटा कर। अच्छी आत्मा थीं.....फट से जान निकल गई, पाँच मिनिट भी नहीं लगे। इधर माँ भुगत रही हैं.....बीस-पच्चीस सालों से अपनी मौत बिस्तर पर.....है कल का भरोसा? कल तक मैं माँ थी, आज मेरी ममता लुट गई..... बताओ, है ज़िंदगी का भरोसा? एक पल का भी तो ठिकाना नहीं।\"
अजय फूफासा तेज़ी से आए। बुआ का चेहरा सीने में भींच लिया-\"मत दुखी हो संध्या.....हम दोनों एक-दूसरे का सहारा बनेंगे.....फिर पायल है न हमारी बेटी।\"
संध्या बुआ रोने लगीं-\"ज़िद्द करती है अजय तुम्हारी बेटी कि शिमला चलो। बताओ क्या ये सही होगा? क्या हम अंग्रेज़ी रीति रिवाज़ के अंतिम संस्कार सहन कर पाएँगे? और क्या चाची की आत्मा सहन कर पाएगी कि हम लोग उनके शरीर को इस रूप में देखें? उन्हें भी तो दुख होगा अजय।\"
वज़न था बुआ के तर्क में.....हाँ, यह सही है कि दादी सांसारिक तौर पर भले ही प्रताप भवन से रिश्ते तोड़ चुकी थीं पर मन से वे उसके चप्पे-चप्पे में मौजूद थीं। तो अंत हो गया एक सदी का.....इतिहास रच गईं दादी जिसमें त्याग भी था, समर्पण भी.....चुनौती भी थी.....जोश और दृढ़ता भी। मैंने धीरे-धीरे आँखें मूँदकर उन्हें याद किया और फिर उमड़ते आँसुओं को बेतहाशा बहने दिया।
चारों ओर धुँधलका.....ढलती रात के थमे हुए क़दमों में व्यतीत होते जाने की आहट जागने लगी। तो यह होता है अवसान। सारी ज़िंदगी का कलुष, पराजय, नफ़रत, तिरस्कार। अपनों का बेगाना हो जाना और इतने बर्दाश्त का यह अंत। तो फिर ज़िंदगी के क्या मायने? क्यों व्यर्थ की कड़वाहट और संबंधों का ढोना। क्यों रिश्तों के बीच पनपी खाई को देख बिसूरना? आज अगर दादी होतीं तो मेरे हर सवाल का जवाब देतीं।
मुझे जवाब दो दादी।
दादी की मृत्यु का धक्का इतना तीव्र था कि मेरा मन खंडहर हो गया। उनका होना ही मेरे लिए काफ़ी था भले ही हम मिल नहीं पाते थे लेकिन अब.....अब चीख़ते सन्नाटे हैं और कचोटती यादें। कितना जोश था मन में कि एक दिन पहुँच जाऊँगी शिमला और उनके कंधे पर सिर रखकर संतुष्टि से आँखें मूँद लूँगी-\"देखो दादी, तुम्हारी पायल माँ अब रोम रिटर्न डॉक्टर बन गई है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ दि डिपार्टमेंट हो गई है। अब उसे अपने पैरों पर खड़ा होना आ गया है। उसने ज़िंदगी के सभी चैलेंजों को स्वीकार कर लिया है-घर, गृहस्थी, सैक्स-इन सबसे परे उसकी अपनी एक अलग दुनिया है जहाँ सर्वोच्च सिंहासन पर आप विराजमान हैं क्योंकि आप ही ने उसे हिम्मत दी। आपसे और अम्मा से प्रेरणा पाकर ही पायल इस मुकाम तक पहुँच पाई है। लेकिन उड़ने की आकांक्षा मन में उठते ही पंखों का टूट जाना महसूस किया मैंने दादी के न रहने से। अब चाहे खंडहरों में सिर पटकूँ या बियाबाँ में भटकूँ, कौन है देखने वाला। दादी तो अशेष में शेष हो गईं।
जानती हूँ कि कुछ बातें बहुत मुश्किल होती हैं। कुछ बातों के लिए चाहकर भी अवरोध सहन करना पड़ता है। मैं दादी की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाई, मैं वीरेंद्र के ब्याह में भी शामिल नहीं हो पाई। शुभ-अशुभ दोनों प्रसंगों से मैं किस क़दर जुड़ी थी.....मानो मेरे शरीर का अंग ही थे दोनों प्रसंग पर मेरी मजबूरी.....मैं बड़ी दादी से मिलने भी नहीं जा पा रही हूँ.....मैं संध्या बुआ के शिशु का न जन्म देख पाई न उसकी किलकारियाँ सुन पाई। उजाड़ हो गई बुआ मातृत्व से। उस समय जबकि अजय फूफासा डीन बन चुके हैं। ज़िंदगी में ऐसा होना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है फिर भी हम इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। ये कैसा जीवन है.....इस क़दर धूप-छाँव से भरा कि न धूप पहचानी जा रही है न छाँव। हर घटना प्रताप भवन से जुड़ी होते हुए भी घट रही है कहीं ओर। मानो घटनाओं की पोटली प्रताप भवन की सीढ़ियों पर रखी थी जो मेरे वहाँ से हट्टे ही खुली तो सही पर घटित कहाँ-कहाँ हुई-चकित हूँ- शोक है और पीड़ा है-और यही प्राप्य है जीवन का।
अम्मा लिखती हैं कि बड़ी दादी को बहुत पछतावा है दादी के संग किए अपने व्यवहार का-\"पुण्यात्मा थी मालविका, विधवा होकर भी सधवा मरी.....न खटिया न बिस्तर, पट्ट से चल दी और मैं सधवा होकर भी विधवा जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ, बरसों से खटिया भोग रही हूँ पर मौत आती नहीं।\"
छ: महीने और गुज़र गए। मैं यूनिवर्सिटी में रम गई। अध्यापन, विद्यार्थी, पुस्तकालय और घर। बस, यहीं तक सिमट आया संसार। मुझे सरकार की तरफ़ से बंगला एलॉट हुआ। अजय फूफासा और संध्या बुआ की ज़िद्द थी कि वे मुझे अलग नहीं रहने देंगे। जब एक ही शहर में रहते हैं तो अलग रहने में क्या तुक है। मैंने कोमलता से कहा-\"बुआ, फूफासा! मुझे सहारा देकर मेरे निश्चय से मत डिगाइए। बेटी का तो धर्म है विदा होना। आशीर्वाद सहित विदा करिए।\"
संध्या बुआ जानती थीं मुझे मेरे निश्चय से कोई नहीं डिगा सकता। फिर एक ही शहर में हैं तो रोज़ ही मिलेंगे। मुश्किल से दस मिनिट की दूरी पर तो है बंगला, बुआ के बंगले से। बुआ ने बंगला ऐसा शानदार सजा दिया कि मुझे डर लगने लगा, मैं ठीक तरह से सार सम्हाल कर पाऊँगी? वीरेंद्र और उर्मिला भी आए। उर्मिला अपने माह भर के बेटे को लेकर आई। गोरा गदबदा, गप्पू-सा जैसे मुलायम रुई से बना हो। उतने दिन हम सब संध्या बुआ के घर रहे। संध्या बुआ तो गुड्डू को देखकर खुद को भूल गईं। उसका हर काम अपने हाथों से करने लगीं। वह बिटर-बिटर उनका मुँह ताकते हुए हँस पड़ता तो कहतीं-\"देखो अजय, पूर्वजन्म का रिश्ता है इससे मेरा।\"
\"पूर्वजन्म का ही क्यों, इस जन्म में भी तो तुम उसकी दादी हो।\"
\"नहीं अजय.....यह मुझे माँ पुकारेगा। क्यों रे शैतान, पुकारेगा न।\"
कितना दर्द था उनके हृदय में। अजय फूफासा की तो आँखें छलछला आईं। वे बहाने से उठे और रीडिंग रूम में चले गए। फिर जब डिनर के लिए मैं बुलाने गई तभी बाहर आए।
पूजा की छुट्टियों में प्रोग्राम बना कि पहले हम सब बनारस जाएँगे फिर अम्मा-बाबूजी को लेकर मालवगढ़ बड़ी दादी के पास। अजय फूफासा का यूनिवर्सिटी में काम अधिक था इसलिए मैं और संध्या बुआ ही बनारस गए। बनारस से मालवगढ़.....बड़ी दादी सख़्त बीमार थीं। सूनी, वीरान-सी कोठी में वे अकेली बिस्तर पर पड़ी मोम-सी घुल रही थीं। हमें आया देख कोदू, रामू, कंचन सभी कोठी के इंतज़ाम में जुट गए। कमरे सँवारे गए.....रसोईघर में खाने की तैयारियाँ शुरू हो गईं। मैं बड़ी दादी के सिरहाने बैठकर उनके बाल सहलाने लगी-\"कैसी हैं बड़ी दादी?\"
उन्होंने हवा में अपने निर्बल नस उभरे हाथ यूँ हिलाए जैसे उन्हें नहीं पता वे कैसी हैं। फिर टकटकी बाँधे मुझे देखने लगीं। मैं उनकी आँखों की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनसे लिपटकर रो पड़ी। बड़ी देर बाद वे धीमे से बोलीं-\"तू तो बहुत बड़ी अफ़सर हो गई है-है न-\"
\"नहीं बड़ी दादी, मैं तो पायल ही हूँ, आपकी वही तुनक मिजाज पायल।\"
\"चल! बहलाती है मुझे, मैं जानती हूँ तू अफ़सर हो गई है, मुझसे लाख छुपा ले।\" वे हँस पड़ीं-कमज़ोर, फीकी हँसी-\"क्यों री.....अफ़सर क्या शादी नहीं करते?\"
मैंने उनके हड्डीहा गालों को चूमा-\"फिर वही शादी। मैं शादी के लिए जन्मी ही नहीं।\"
\"हाँ री शिखंडी-महाभारत से उठकर सीधी आ गई कलजुग में।\"
बड़ी दादी की उपमाएँ होती बड़ी सटीक हैं। कंचन उनके लिए दवा और फल ले आई। उन्होंने नाक-भौं सिकोड़ी। संध्या बुआ ज़बरदस्ती सेब की फाँकें उनके मुँह में ठूँसने लगीं तो वे भड़क गईं। पूरी फाँक नीचे फर्श पर उगल दी-\"मार बकबका सवाद है इसका.....संध्या तू तो मुझे गट्टे की चटपटी तरकारी और बघारे हुए केसरिया चावल खिला दे। जैसे हमारी मालविका दुलहिन बनाती थी।\"
दवा खाकर बड़ी दादी को हलकी-सी झपकी आ गई। हालाँकि प्रताप भवन के कमरे हॉल के झाड़फानूस रोशन थे उस रात। बगीचे में पानी के सिंचाव से भीनी, सौंधी महक भी उठ रही थी लेकिन एक सन्नाटा भी था जो सभी को निगल जाने को आतुर था। मैं अपने उदास कमरे में स्वयं को सहज नहीं पा रही थी।
संध्या बुआ ने कटोरी में गट्टे की सब्ज़ी, फूली नरम रोटियाँ, केसरिया चावल, पापड़ आदि परोसे और बड़ी दादी के कमरे की ओर जा ही रही थीं कि बड़े बाबा आ गए। मैं तो उन्हें देखकर सकते में आ गई। बाल लंबे-लंबे जटाओं जैसे, मटमैली धोती और नारंगी कुरता, गले में रुद्राक्ष की मालाएँ और माथे पर भभूति की तीन रेखाएँ खिंची हुईं। प्रताप भवन की अपार संपत्ति को ठुकराकर उनके साधू हो जाने के लिए क्या केवल बड़ी दादी ज़िम्मेदार हैं या पच्चीस सालों से बिस्तर भोग रही बड़ी दादी के लिए बड़े बाबा ज़िम्मेदार हैं? दुर्गति दोनों की हुई.....मगर क्यों? क्यों ज़िंदगी भर के रिश्ते शूल बन जाते हैं।
बड़े बाबा को देखकर दादी कोहनियों के सहारे बिस्तर पर उठंग-सी हो गईं-\"आ गए?\" और उनके हाथ काँपे.....वे बिस्तर पर गिर गईं.....साँस उलटी चलने लगी.....बदन पत्ते-सा काँपने लगा। संध्या बुआ ने हाथ में पकड़ी थाली मेज पर पटकी और बड़ी दादी के तलुवे सहलाती हुई ज़ोर से चीखीं-\"कोई डॉक्टर को बुलाओ।\"
कोठी में नौकर, दासियाँ इधर-उधर भागने लगे। बड़े बाबा तटस्थ से बने सिरहाने खड़े थे। बड़ी दादी ने इशारे से भाग-दौड़ करने को मना किया। फिर जीभ निकालकर अपने सूखे हलक़ को दिखाया.....मैं चम्मच से उनके मुँह में पानी डालने लगी तो छटपटाहट और बेचैनीवश उन्होंने हाथ से चम्मच को परे ढकेल-सा दिया। उनकी तक़लीफ़ बढ़ती जा रही थी। अचानक बड़े बाबा उनके सिरहाने पर घुटनों के बल बैठ गए-\"हरि ओम् जपो.....बोलो हरि ओम्।\"
बड़ी दादी ने डबडबाई आँखों से उनकी ओर देखा। उन आँखों में इतनी पीड़ा समाई थी कि मानो अब उस पीड़ा का विस्फोट होने ही वाला है.....कि जैसे वो कहना चाहती हैं बड़े बाबा से कि देख लो.....पराए घर से मुझे लाकर क्या दुर्गत की है तुमने मेरी.....मैं सारी उमर धीरे-धीरे अगरबत्ती-सा सुलगती रही लेकिन तुमने वो सुलगना नहीं देखा.....बस उसकी खुशबू में ही मस्त रहे.....किस काम का तुम्हारा साधू होना जब कर्तव्यों को ही नहीं निभा सके..... मुँह फेर लेने से क्या ज़िम्मेवारियाँ ख़त्म हो जाती हैं?
उन नज़रों ने अपनी मौन भाषा में पत्थरदिल बड़े बाबा से बहुत कुछ कहना चाहा था लेकिन वह केवल इतना कह पाईं-वो भी बाबूजी से.....उनका हाथ कसकर पकड़कर-\"समर..... तुम्हारी अम्मा मुझे माफ़ तो कर देंगी न?\" और क्षण भर में उनका शरीर पत्ते-सा काँपकर निश्चल हो गया।
\"अरे हुकम.....बिना कुछ खाए-पिए ही चल दीं।\" कंचन की चीख और रुलाई ने प्रताप भवन की नींवें हिला डाली थीं। अचानक बड़े बाबा ने उनके पलंग के पाए पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। वे रोते जा रहे थे और होंठों ही होंठों में कुछ बुदबुदाते जा रहे थे। ज़िंदगी भर बड़ी दादी को तड़पाया.....उसकी कुछ तो टीस, चुभन सालनी चाहिए उन्हें! जानती हूँ उन्होंने बड़ी दादी को न शारीरिक सुख दिया न मानसिक। बल्कि उनकी ज़िंदगी के रफ़्ता-रफ़्ता घुलते रहने और गलते रहने के लिए ज़िम्मेवार भी वही हैं। उनकी बीमारी में उन्होंने डॉक्टर, नर्स, वैद्य, हक़ीम के हुजूम ज़रूर खड़े कर दिए थे पर बीमार को अच्छा होने के लिए प्यार की भी आवश्यकता है। दवाइयाँ तभी असर करती हैं जब बीमार को पता हो कि उसकी किसी को ज़रुरत है। बड़े बाबा ने कभी ये ज़रुरत नहीं जताई.....हाँ.....अब मैं कह सकती हूँ कि जब उनका शरीर भोगने योग्य नहीं रहा तो वे तांत्रिक साधू हो गए। भोग वासना से असंतुष्ट व्यक्ति ही तांत्रिक होते हैं और ईश्वर से प्रेम करने वाले, हर मनुष्य में ईश्वर का रूप देखने वाले व्यक्ति मांत्रिक-तपस्वी होते हैं। बड़े बाबा ने किसी से प्रेम भी किया है मुझे तो इसी बात पर संदेह है।
उषा बुआ तो आ गई थीं पर रजनी बुआ कल सुबह ही आ पाएँगी ऐसा वीरेंद्र और उर्मिला ने बताया था क्योंकि जब ये दोनों बनारस से यहाँ के लिए रवाना हो रहे थे तो रजनी बुआ की इन लोगों से फोन पर बात हुई थी। रजनी बुआ की फ़्लाइट ही रात की है।
मुट्ठी भर बची बड़ी दादी की देह को सोलहों श्रृंगार करके सजाया गया। बड़े बाबा ने उनकी माँग भरी और सुहागिन औरतों ने उनकी माँग से सिंदूर ले अपनी माँग से छुआया..... अमर सुहाग के लिए.....। ईश्वर ने उन्हें कम-से-कम सुहागिन मरने का तो वरदान दिया।
मारिया को नहीं आना था, नहीं आई। थॉमस आया। दादी के शव पर फूल चढ़ाए और शमशान भी गया। शाम तक कोठी वीरान हो चुकी थी। रह गए थे केवल वे संबंधी जो तेरहवीं तक रुकने वाले थे। बड़े बाबा पूरे तेरह दिन उस जगह आसन जमाये रहे जहाँ बड़ी दादी ने प्राण त्यागे थे। उनका पलंग, बिस्तर सब दान कर दिया गया और वहाँ दीप जलाकर उनकी फोटो रखी गई थी जिस पर रोज़ सुबह संध्या बुआ ताज़े फूलों की माला पहनातीं। उन्होंने कौल ले लिया था कि अब वे कभी गट्टे की तरकारी और केसरिया चावल नहीं खाएँगी क्योंकि इन चीज़ों को वे बड़ी दादी को खिला नहीं पाई थीं।
तेरहवीं के बाद सब कुछ तितर-बितर हो गया। अम्मा वग़ैरह बनारस लौट गईं। कंचन रोती-सुबकती अपने गाँव चली गई और हम लोग कलकत्ता लौट आए। रजनी बुआ कुछ दिनों के लिए उषा बुआ के घर जोधपुर गई थीं। कोठी की देखभाल के लिए रामू और कोदू रह गए। जहाँ कभी चहल-पहल, शान शौकत और ऐश्वर्य के झरने बहते थे अब वहाँ सूखे सन्नाटे अपनी चिटखी दरारों से झाँक रहे थे।
कलकत्ता लौटकर मैं अपने बंगले नहीं लौटी। इस वक़्त संध्या बुआ को मेरी ज़रुरत है। वे टूट चुकी थीं बड़ी दादी की मृत्यु से। उनका मायका बियाबाँ में बदल चुका था। और यह एहसास तेज़ी से उनके अंदर समाता जा रहा था कि उनका जीवन असुरक्षित-सा हो गया है। माँ नहीं बनीं वे.....उनका अपना अधूरापन उन्हें मथे डालता था।
रात मैंने ख़्वाब देखा। मैंने देखा, दिल हिला देने वाले सन्नाटे में तमाम बोलते उल्लुओं, चमगादड़ों से भरे खंडहर हैं और भयानक अँधेरा है और उस अँधेरे और खंडहर में चलती हुई मैं देखती हूँ उन खंडहरों का एक-एक पत्थर अपने महल होने के सबूत दे रहा है। सबूत ही नहीं बल्कि उन धड़कनों का भी हवाला दे रहा है जो ज़िंदगी बनकर धड़की हैं यहाँ लेकिन अब वे धड़कनें पत्थर बनकर रह गई हैं। और अचानक मुझे ठोकर लगी-देखा, कोठी के चबूतरे पर किसी की चिता जल रही है और चिता के सिरहाने बैठे बड़े बाबा मंत्र पढ़ रहे हैं और तभी कोठी की दीवार में छिपा काला साँप निकला और उसने जलती चिता में छलाँग लगा दी.....पसीने में तरबतर घबराकर मेरी नींद खुल गई। हालाँकि साँप का जल मरना इस बात का संकेत था कि प्रताप भवन की औरतों के शाप ख़त्म हो गए.....पर कब? जब सब कुछ स्वाहा हो गया?
यह ख़्वाब आड़े दूसरे आ-आकर सारी रात मेरी नींदों को जागरण में बदल देता। भय के मारे मैं सो नहीं पाती थी। महीनों लगे थे मुझे कोठी की वीरानी स्वीकार करने में और महीनों लगे थे संध्या बुआ को सम्हालने में। लेकिन गुज़रता वक़्त वह चंदन का लेप है जो ज़िंदगी से मिली चोट, घावों को आहिस्ता-आहिस्ता पूरता चलता है। मैं अपने बंगले लौटकर अध्यापन में व्यस्त हो गई और संध्या बुआ ने एक ईसाई महिला के साथ जुड़कर जानवरों के संरक्षण का कार्य शुरू कर दिया। वे सड़क के आवारा, भूखे और घायल कुत्ते, बिल्लियों की तीमारदारी करतीं.....उन्हें दूध, बिस्किट, खिचड़ी आदि खिलातीं। जब वे घर से बाहर निकलतीं तो तमाम कुत्ते पूँछ हिलाते कूँ-कूँ करते उनके पैरों में लोटने लगते। उनकी इच्छा थी एक वेटरनिटी हॉस्पिटल खोलने की जिसके लिए वे और उनकी सहयोगी मिसेज़ लीना सरकारी अनुदान के लिए प्रयत्नशील थीं। संध्या बुआ ने अपना जीवन गुज़ारने की राह पा ली थी जिसमें उनका मन बहुत रमता था। अजय फूफासा ने उन्हें कभी नहीं रोका इस काम से।
अम्मा ने लिखा था कि बड़ी दादी की मृत्यु के बाद बड़े बाबा अब पक्के संन्यासी हो गए हैं और अघोरियों के बीच हरिश्चंद्र घाट पर रहते हैं। ऐसे भयंकर अघोरियों के बीच जो मुर्दे की जली खोपड़ी पर गांकड़-बाटी पकाकर खाते हैं। उनका यह हश्र तो होना ही था। मुझे तो न दुख हुआ न उनके प्रति सहानुभूति जागी। अगर यही सब उन्हें करना था तो शादी क्यों की? क्यों अपने से बाँधकर बड़ी दादी को ज़िंदगी भर हलाल करते रहे। बड़ी दादी ज़िंदगी भर उनसे मिली उपेक्षा, तिरस्कार का बदला हम सबसे लेती रहीं। भले ही उनके अंतर्मन को यह पता न हो कि हम सबके साथ क्यों करती हैं?
कलकत्ता शीतलहर की चपेट में था। दो दिन से लगातार शिमला और उसके आसपास की घाटियों में भारी हिमपात हो रहा था। लेकिन बावजूद हिमपात के न जाने कैसे ये ख़बर हम तक पहुँची कि शिमला में जिम की मृत्यु हो चुकी है। यह बड़ी दादी की मृत्यु के डेढ़ साल बाद की घटना थी। अम्मा का पत्र संध्या बुआ के पास आया था कि वीरेंद्र कुछ दिनों के लिए मालवगढ़ गया था तो पता चला कि जिम की मृत्यु हो चुकी है और उनका शव दफ़नाने के लिए हवाई जहाज से मालवगढ़ लाया गया था। ख़बर सुनकर वीरेंद्र भी रामू के साथ कब्रिस्तान गया था। पता चला कि दादी की इच्छा को सम्मान देते हुए उनका भी शव जिम ने मालवगढ़ लाकर ही दफ़नाया था। दादी की कब्र के बाजू में ही जिम की कब्र भी बना दी गई थी।
उफ़! प्रेम की इस परिभाषा ने मुझे आलोड़ित कर दिया। मेरा मन जिम के प्रति श्रद्धा से भर गया जिन्होंने दादी की इच्छाएँ एक-एक कर पूरी कीं और उनकी बेतहाशा क़द्र की।
जिम की मृत्यु के महीने भर बाद मेरे नाम एक सरकारी लिफफा आया जो जिम के वकील द्वारा भेजा गया था। लिफाफा खोलते ही मैं विस्फारित नेत्रों से जिम के द्वारा लिखा वसीयतनामा पढ़ने लगी। शिमला का कॉटेज, सेब के बाग, मालवगढ़ का बंगला, दादी के सारे कीमती आभूषण, बैंक में जमा धनराशि सब मेरे नाम थी। अपनी ज़िंदगी भर की कमाई मुझे सौंप दी थी जिम ने.....शायद दादी की इच्छा से.....हाँ, दादी की ही इच्छा रही होगी ऐसी। शाम को मैंने वसीयतनामा ले जाकर संध्या बुआ और फूफासा को दिखाया। हम सभी इस वसीयतनामे से आश्चर्यचकित थे.....यह कैसा अनाम रिश्ता था जो ज़िंदगी भर निभाया जाता रहा बिना किसी अपेक्षा के, मिलन के। न हम कभी शिमला गए न वे दोनों कभी यहाँ आए फिर भी ऐसा अटूट बंधन। इतना प्रगाढ़ प्रेम। त्याग की ऐसी विशालता! मुझे पूर्वजन्म में विश्वास नहीं इसीलिए इस रिश्ते को पूर्वजन्म के रिश्तों से नहीं जोड़ा जाता मुझसे। या शायद ऐसा हुआ हो कि मैं दादी के गर्भ में से आई और किसी दैवी शक्ति ने मुझे उनके गर्भ से निकालकर अम्मा के गर्भ में रख दिया हो। जैसे स्वामी महावीर को देवआनंदा के गर्भ से निकालकर कुंडग्राम की रानी त्रिशला के गर्भ में रख दिया था। क्योंकि देवआनंदा ब्राह्मण थी और जैन धर्म के सभी तेईस तीर्थंकर क्षत्रिय के घर जन्मे थे.....परंपरा का खंडन इतनी आसानी से कैसे हो सकता है?
वसीयतनामा पढ़कर फूफासा गंभीर हो गए-\"पायल! तुम्हें जाना चाहिए शिमला। सब कुछ आँखों से देखभाल आओ। उनकी जायदाद को सम्हाली।\"
\"हाँ पायल, नहीं तो जिम और चाची की आत्मा को तक़लीफ़ होगी।\" संध्या बुआ ने भी यही कहा।
मैं सोच में पड़ गई। जितना दूर भागती हूँ ज़मीन जायदाद, धन ऐश्वर्य से, उतना ही पीछे पड़ी रहती है ये संपत्ति। उधर प्रताप भवन वीरेंद्र के नाम है लेकिन सोने चाँदी के बर्तन, ज़ेवरात और बैंक के फिक्स्ड डिपाज़िट और प्रताप भवन के पिछवाड़े की ज़मीन मेरे नाम है। हालाँकि उस ज़मीन पर वह एक फॉर्म हाउस बनवा रहा है पर मेरी इच्छा है वहाँ दादी के नाम से एक बालिका विद्यालय खोला जाए पर वीरेंद्र और उर्मिला तैयार नहीं हैं कि इतनी झंझट कौन पाले। बार-बार मीटिंग करनी पड़ेगी, विद्यालय प्रबंधन की ज़िम्मेवारी उठानी पड़ेगी, ज़िंदगी चरखी बनकर रह जाएगी।
\"अब तुम तो बैरागिन हो पायल लेकिन देने वाले तो बैरागी नहीं थे। सभी चाहते हैं कि उनका कमाया गाढ़ा धन उनके बाद सही हाथों में जाए।\" संध्या बुआ ने मेरी उपेक्षा देख कहा तो मैं मुस्कुरा दी।
\"यही तो दिक्कत है बुआ.....सही हाथ कहाँ हैं मेरे? सड़ जाएगी सारी संपत्ति पड़े-पड़े।\"
\"तुम मार्च में छुट्टी लेकर अपनी बुआ के साथ शिमला हो आओ, देख आओ सब। मालिकाना हक़ जताना पड़ेगा वरना लूट लेंगे लोग।\"
यही बात अजय फूफासा ने वीरेंद्र को भी लिखी कि वीरेंद्र भी साथ जाए। यह ज़रूरी है। अम्मा तो चकित थीं सब सुनकर। रात फोन पर बात हुई। बोलीं-
\"इतना तो सगे भी नहीं सोचते जितना जिम ने सोचा। जिम ने अम्माजी से सच्चा प्यार किया था। प्यार की ख़ातिर उन्होंने उनकी हर इच्छा पूरी की।\"
\"हाँ अम्मा ऐसे लोग बिरले होते हैं।\" मेरी आवाज़ भावुक हो रही थी। दादी और जिम की याद से आँखें भरी जा रही थीं। संध्या बुआ ने रिसीवर मेरे हाथ से लेकर कहा-\"फिर पक्का रहा भाभीसा! हम लोग इधर से शिमला पहुँचते हैं और उधर से वीरेंद्र आ जाए। चाहे तो उर्मिला को भी साथ ले आए।\"
\"नहीं संध्या बाई, गुड्डू छोटा है अभी और उधर ठंड का मौसम तो मार्च-अप्रैल तक रहा ही आता है। वीरेंद्र आएगा, फिर उधर कॉटेज है ही, उर्मिला कभी भी घूम आएगी।\"
\"ठीक है।\" संध्या बुआ ने एक-दो मिनिट और बात की और फोन रख चहकती-सी उठीं, \"आज तो मैं अपनी लखपति बिटिया के लिए गाजर का हलवा बनाऊँगी।\"
अजय फूफासा कुछ अलग ही मूड में थे-\"छोड़ो हलवा-शलवा.....कोई बढ़िया-सी पिक्चर देखते हैं और बाहर ही डिनर ले लेते हैं।\"
ये हुई न बात।\" कहती संध्या बुआ ने मेरे गाल मसल डाले और मुझे गले लगाते हुए चूम लिया।
दिल्ली में राधो बुआ के जेठ रहते हैं। वे ही हम लोगों को एयरपोर्ट से घर तक लाए, एक दिन उनके घर रुकना पड़ा क्योंकि वीरेंद्र दूसरे दिन आने वाला था। फिर कार से हम सब शिमला गए। शिमला पहुँचकर कार से उतरते ही ठंडी हवा ने बदन कँपा दिया। संध्या बुआ जल्दी-जल्दी स्वेटर, शॉल निकालकर हमें देने लगीं और खुद भी अपने को ढँकने लगीं-\"कैसे रहती होंगी चाची यहाँ, मेरी तो कुल्फ़ी जमी जा रही है।\"
वीरेंद्र ऐसे ठठाकर हँसा कि चारों ओर सूनी घाटी में उसकी हँसी गूँज उठी। देवदार, ओक, चीड़ के ऊँचे-ऊँचे दरख़्तों के सुई जैसे पत्तों के बीच गुज़रती हवा सिसकारियाँ भर रही थी। सर्पिल पहाड़ी सड़क के एक ओर जंगली लाल, गुलाबी, सफ़ेद गुलाब इतने अधिक खिले थे कि पत्ते तक दिखाई नहीं दे रहे थे। घाटी में दूब की तरह छिछली स्ट्रॉबेरी की लतरें दूर-दूर तक फैली थीं। उनका उलझाव जीवन के उलझाव के कितना नज़दीक लगा। उलझाव में भी पुष्पित, पल्लवित, फलित होने का अपना धर्म था।
वकील साहब बताए हुए समय पर पहुँच गए थे। औपचारिक परिचय के बाद वे हमें जिम के कॉटेज ले आए। कॉटेज इतना शानदार और इतना सुंदर सजा हुआ था जैसे अभी-अभी कोई यहाँ से उठकर गया हो। पूरी सजावट में सुरुचि का आभास था। चॉकलेटी कालीन पर बेंत के सोफे, दरवाज़ों पर पड़े परदों में चाँदी की घंटियाँ लगी हुईं जो हवा के स्पर्श से टुनटुनाने लगती थीं। परदे के पीछे से ही एक पहाड़ी नौकर प्रगट हुआ। आते ही हमें सैल्यूट मारा। वकील साहब ने बताया कि यह बरसों से मिस्टर जिम की तीमारदारी करता रहा। मिसेज़ जिम इसे अपने बच्चे जैसा प्यार देती थीं।
कैसा लगता है दादी के लिए यह संबोधन और यह तस्वीर जो ड्राइंगरूम की दीवार पर टँगी है जिसमें जिम के साथ दादी अंग्रेज़ दुल्हन की सफ़ेद पोशाक में बिल्कुल परी-सी नज़र आ रही थीं।
\"ये मेम साब हैं हमारी.....बहुत अच्छी बहुत दयालु-ईश्वर के जैसी-हम आज भी उनके लिए रोते हैं।\" कहता हुआ नौकर जल्दी-जल्दी अपने टपकते आँसुओं को पोंछने लगा। संध्या बुआ ने उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे पुचकारा।
\"आप लोग आराम करिए, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ आपके लिए फिर खाना पकाऊँगा-बढ़िया आलू-मटर की तरकारी।\" कहता हुआ वह किचन में चला गया।
संध्या बुआ तो पलंग पर लेट गई थीं। वीरेंद्र वकील साहब को छोड़ने गेट तक आया था और मैं पूरा कॉटेज घूम-घूमकर देखने लगी। ड्राइंगरूम, लिविंगरूम, स्लीपिंगरूम, रीडिंगरूम, डाइनिंगरूम, मेहमानों का कमरा-किचन, स्टोररूम-बड़ी-बड़ी बाल्कनियाँ जिनके नीचे घाटी की ओर उतरा जा सकता था। घाटी में पहाड़ी चश्मा छलछल बहा जा रहा था। रेत के मैदानों से हरी-भरी घाटियों तक का दादी का सफ़र-एक पूरा जीवन जिसमें समर्पण था, स्वप्न थे, पीड़ा थी, आकांक्षा थी, आस्था थी, पराजय थी और प्रेम के उन्माद में गहरे डूब जाने का अपार सुख था। बाल्कनी से लगा छोटा-सा पूजाघर जहाँ कृष्ण की मूर्ति थी। पूजाघर देखकर मैं अभिभूत थी। लगा दादी आकर कानों में कह रही हैं-\"देख लिया पायल मेरा दूसरा जन्म? यह दूसरा जन्म मेरा ईश्वर का दिया वरदान था।\"
मुझे न जाने क्या सूझा कि अपने दुपट्टे से कृष्ण की मूर्ति पोंछने लगी। फिर वहीँ रखे डिब्बे में से घी में डूबी और ठंड के कारण जमे हुए घी में कठोरता से जुड़ी बत्तियों में से बड़ी मुश्किल से एक बत्ती निकालकर कलश पर रखे दीये में जला दी। बत्ती आँच पाकर धीरे-धीरे पिघलने लगी। मन मेरा भी पिघल रहा था।
संध्या बुआ ने आवाज़ दी-\"आओ पायल, खाना लगा दिया है।\"
सुबह हम ब्रेकफ़ास्ट से निपटे ही थे कि वकील साहब कुछ ज़रूरी काग़ज़ात लेकर आ गए। कई जगह मुझे हस्ताक्षर करने थे। उसके बाद वे हमें सेब के बाग दिखाने ले गए। वकील साहब जिम के ख़ास दोस्त थे और बाक़ायदा पच्चीस वर्षों की दोस्ती थी उनकी। एक-दो बार तो वे जिम और दादी के साथ लंदन भी जा चुके थे। रोज़ उठना-बैठना था। हँसते हुए बताया-\"हमारी तो अंग्रेज़ी की शिष्या थीं मिसेज़ जिम।\"
हम एक साथ चौंके।
\"भाषा पर उनकी पकड़ बहुत मज़बूत थी। महीने भर में सीख गईं अंग्रेज़ी बोलना।\"
ओह, गर्व से मेरा सिर ऊँचा हो गया। दादी ने दिखा दिया कि औरत किसी भी काम में मर्दों से पीछे नहीं है। संध्या बुआ ने मेरी ओर देखा और हम दोनों ने आँखों ही आँखों में एक-दूसरे से कह दिया और मान भी लिया कि दादी के लिए यह कोई कठिन बात न थी। वे बेहद विदुषी थीं।
कई एकड़ भूमि पर सेब के बगीचे थे। मौसम के समय इन्हें ठेके पर उठा दिया जाता था-\"आप बिल्कुल परेशान न हों, पूरी देखभाल करूँगा मैं इन बगीचों की। आप और वीरेंद्र जी समय-समय पर आते ही रहेंगे।\"
वकील साहब ने तसल्ली दी थी। सुनकर मुझे अच्छा ही लगा था। मैंने वीरेंद्र को बगीचा घूमने के बहाने अलग ले-जाकर कहा कि इधर की देखभाल का पूरा चार्ज वकील साहब को वेतन सहित दे दिया जाए तो कैसा रहे? वे मन लगाकर देखभाल करें इसके लिए ये ज़रूरी है। संध्या बुआ को भी मेरा प्रस्ताव पसंद आया। लिहाज़ा उन्हें इस काम के लिए नियुक्त कर दिया गया। कॉटेज पहाड़ी नौकर सम्हालेगा और साथ में एक-दो बार ख़ासकर गर्मियों में कलकत्ता या बनारस से ट्रिप लगती रहेंगी हम लोगों की। सारी व्यवस्था के बाद वकील साहब ने रात्रि भोज के लिए हमें अपने घर आमंत्रित किया। दूसरे दिन हमें लौट जाना था।
रात्रि भोज के बाद वकील साहब हमें कालीबाड़ी रोड पर चहलकदमी कराने ले गए। पूरा शिमला रात की बाँहों में ख़ामोशी से दुबका था। टिमटिमाती बत्तियाँ नीचे घाटियों में बसे घरों में रोशन थीं।
\"ये काली मंदिर है.....जागृत देवी हैं.....जो माँगो वही मिल जाता है।\"
\"अच्छा!\" संध्या बुआ मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर चली गईं। उनका बजाया पीतल का घंटा देर तक प्रतिध्वनि में गूँजता रहा। दर्शन करके बुआ बाहर आईं-\"तुम दोनों दर्शन नहीं करोगे.....माँग लो भई आज तो।\"
मैं हँस दी-\"क्या माँगूँ बुआ.....सब कुछ तो है।\"
और वीरेंद्र के साथ मैं दर्शन कर आई पर माँगा कुछ नहीं। मंदिर की छत पर हम बहुत देर तक खड़े रहे, यहाँ से शिमला की रौनक देखते ही बनती है मानो पूरा आसमान घाटी पर उतर आया हो। जब हम ढलवाँ सड़क से अपने कॉटेज की ओर लौट रहे थे तो मैं और बुआ पीछे रह गए। बुआ आहिस्ता-आहिस्ता चल रही थीं।
\"पायल, मन की शांति सबसे बड़ा धन है जो तुम्हारे पास नहीं है। यही माँग लेतीं काली माँ से?\"
मैं चुप रही। दुख भी हुआ, बुआ की बात मुझे बुरी लगी, लेकिन उनका कहना भी सही है। शांति तो वास्तव में नहीं मिली मुझे। प्रताप भवन में घटी सभी घटनाओं को लेकर मन बहुत अशांत रहा हमेशा। अभी तक कई सवाल मथे डालते हैं.....इन्हीं सवालों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। बहुत घना बुना हुआ अंधकार का जाल है और उस जाल में कैद प्रताप भवन। मैंने अंधकार से बगावत कर आलोक को तलाशा लेकिन वह आलोक इतना नन्हा था कि उस बुने जाल को काट नहीं पाया और मैं स्वयं को आलोकित समझ मन-ही-मन संतुष्ट होती रही जबकि वह संतुष्टि थी नहीं.....महज भ्रम था।
संध्या बुआ और वीरेंद्र गहरी नींद में थे। पहाड़ी नौकर ने फ़ायर प्लेस में लकड़ियाँ सुलगाकर कमरा ख़ासा गरम कर दिया था.....मेरी आँखों में नींद का दूर-दूर तक पता न था। मैं दादो के कमरे में आकर उनकी चीज़ों को देख रही थी। हर चीज़ में उनकी मौजूदगी समाई थी। बस वे ही नहीं थीं। सामने रैक पर किताबों का भंडार जमा था। अंग्रेज़ी-हिंदी की किताबें! अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे बहुत अधिक अध्ययन में डूब गई थीं। अध्ययन तो वे प्रताप भवन में रहते हुए भी करती थीं और प्रतिदिन डायरी लिखने की आदत भी बाबा ने डाली थी उनमें। वे डायरी लिखती थीं और रात को बाबा को सुनाती थीं। बाबा हँसते-\"डायरी मन का दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी सही तस्वीर दिखाता है, यह आत्मयोग है, आत्मा के दर्शन कराने वाला योग-इसलिए इसे लिखो और गुनो।\"
अचानक मेरी खोजी दृष्टि ने उनकी डायरी खोज ही ली। शायद इसी की तलाश में मेरी नींद उड़ी थी। हाँ, मैं जानना चाहती थी कि प्रताप भवन छोड़ने के बाद दादी की मनःस्थिति क्या थी। शायद उनके प्रति प्रगाढ़ लगाव वजह हो लेकिन डायरी पाकर अपार खुशी ने मेरे मन को चैन दे दिया। बादामी रंग की डायरी का प्रत्येक पन्ना दादी की लिखावट से भरा था। पन्ने पलटती हुई एक-दो लाइनें पढ़ती हुई मैं कमरे में आकर पलंग पर लेट गई और बहुत देर तक डायरी को सीने से लगाए रही। मानो दादी के पास ही लेटी हूँ मैं। मैंने आँखें मूँद लीं। सुबह घाटी में उतरते हलके-हलके आलोक में जब नींद खुली तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि डायरी को अपने सूटकेस में कपड़ों की तह के नीचे दबा दिया। फिर खिड़की पर पड़ा परदा हटाया.....खिड़की की बंद काँच पर रात को गिरे कोहरे ने अपनी चादर चढ़ा रखी थी जो सूरज की किरणों के गुनगुने स्पर्श से लकीरों में बह रहा था। मैंने खिड़की खोल दी। ठंडी हवा की छुअन बदन सिहरा गई।
दूसरे दिन हम दिल्ली लौटे। हमसे मिलने राधो बुआ आ गई थीं सो उनके साथ दो दिन बिताकर वीरेंद्र बनारस चला गया और हम कलकत्ता लौट गए।
मार्च के वासंती दिन। ठूँठ पेड़ों पर फूल, रस और गंध की मस्ती छाई है। पतझड़ ने पेड़ों की नंगाझोली ले ली थी। वसंत ने उन्हें फिर बसा दिया। लेकिन मेरा मन बसता नहीं, हालाँकि यूनिवर्सिटी में बेहद व्यस्तता है। इम्तहान, पेपर सैटिंग, पेपर करेक्शन, पी-एच.डी. के विद्यार्थियों का वायवा लेना। थककर घर लौटती और मिनटों में नींद घेर लेती। बीच में नींद टूटती तो डायरी पढ़ने का लालच सिर उठा लेता। पर कड़ूआई आँखें इजाज़त नहीं देतीं। आजकल मेरी बंगालिन नौकरानी हफ़्ते भर की छुट्टी लेकर गाँव गई है और संध्या बुआ रंगरूट की तरह एकदम डिनर के टाइम पर खाना लेकर आ जाती हैं। आज वे ज़िद्द कर रही थीं कि मुझे खिलाकर और सुलाकर ही जाएँगी और आज ही मेरा मन उतारू था डायरी के पृष्ठ खोलने को। उनके जाते ही मैंने टेबिल लैंप जलाया और टेबिल की दराज़ से डायरी निकाल उसे सहलाया मानो दादी का कोमल स्पर्श हो। डायरी का हर पन्ना उनकी ज़िंदगी का खुला दस्तावेज था।
पहला पन्ना
इस दुनिया में इंसान का जन्म माँ की कोख से होता है लेकिन मेरा जन्म चिता से हुआ.....और जन्म होते ही जिस देवपुरुष ने मुझे सम्हाला वे हैं जिम.....इंसान के रूप में देवपुरुष। नहीं, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी बिल्कुल याद नहीं करूँगी। वह तो मेरे कर्मों का भुगतान थी। मैं ज़िंदगी भर अपनी सीप-सी मुट्ठी में जिस मोती को सहेजे रही वह बूँद निकली और फिर चालीस मन लकड़ियों की चिता पर बूँद का अस्तित्व ही क्या? मैंने बहुत तर्क किए थे उस बूँद के लिए जिम से लेकिन मेरे हर तर्क़ का काट उनके पास मौजूद है। उन्होंने मेरी उन बातों के प्रति भी आँखें खोलीं, प्रताप भवन में रहते हुए जिन बातों की ओर मेरा कभी ध्यान भी नहीं गया। तब मैंने महसूस किया कि त्याग भी उसी के लिए करना चाहिए जो तुम्हारा त्याग समझे। उसी क्षण हमने शादी का फैसला कर लिया और यह सही भी था क्योंकि जिम की मुहब्बत जुनून की हद पार कर चुकी थी।
शादी की रात मुझे जिम की बहनों ने जिम की पसंद से सजाया था। दूध-सी सफेद पोशाक में ऐसी शांति बसी थी जैसी मैंने और कहीं नहीं पाई। मेरे हाथों में मेहँदी नहीं, सफ़ेद रेशम के कोहनी तक के दस्ताने थे। पाँवों में महावर नहीं, मोती टँके सफ़ेद चमड़े के खूबसूरत जूते थे। गले में सफ़ेद शनील के नेकलेस पर हीरा जगमगा रहा था। शादी की क़समों के बाद जब जिम ने मेरी उँगली में अँगूठी पहनाकर मुझे चूमा तो ऐसा लगा कि जाने कब से मैं जिम के प्यार के इंतज़ार में थी। सदियाँ गुज़र गईं.....तूफानों ने बार-बार झकझोरा लेकिन शायद मैं इसी दिन के लिए बचती चली आई। हालाँकि अहल्या गौतम के धोखे में इंद्र की बाँहों में समाकर पत्थर होने का शाप झेलती रही.....लेकिन एक दिन उस पत्थर को पिघलना ही था। मैं चिता की राख़ में अपने पत्थर होने के शाप को तोड़कर अपने गौतम के आगोश में समा गई। मुझे इंतज़ार था पायल और संध्या का। लेकिन मारिया अकेली ही आई। उसने और थॉमस ने फूलों का गुच्छा मुझे भेंट किया और बधाई दी। मेरे ख़ामोश प्रश्न पर उसने तसल्ली दी-\"नहीं आ पाईं दोनों, मैं तो आ गई न छोटी आंटी। उनके साथ प्रताप भवन के कायदे-कानून हैं, उन्हें तो उसी समाज में रहना है।\" मारिया के मुँह से इस कड़वे सच को सुन थोड़ी देर को मैं विचलित हो गई थी। स्थिति समझकर जिम ने मेरे कंधे थपथपाए और फ़्लोर पर थिरकते जोड़ों को दिखाने लगे जो अफ्रीकी ड्रम की लय के साथ नाच रहे थे। अंग्रेज़ी विवाह गीत के लरजते बोल मालवगढ़ में दूर-दूर तक गूँज रहे थे।
दूसरा पन्ना
जानती हूँ इस विवाह की ख़बर से पूरा मालवगढ़ थू-थू कर उठेगा। इसीलिए जिम से ज़िद्द की कि हम शिमला चलकर रहेंगे। जिम समझ गए, यह आशंका उनकी आँखों में भी तैर रही थी। बोले-\"मैं ट्रांसफर करवाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मालवगढ़ के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। क्रांति कब यहाँ सुलग उठे, कहा नहीं जा सकता।\"
जिम ठीक कह रहे थे। क्रांति पूरे देश में लावा बनकर फूट रही थी। एक-एक गाँव तक एकजुट होकर उस लावे में कूद पड़ने को तैयार था। मारिया हर हफ़्ते आती और क्रांति की ख़बरें और प्रताप भवन की ख़बरें सुना जाती। मुझे केवल संध्या की चिंता थी.....पता नहीं, अजय और संध्या के रिश्ते को प्रताप भवन कबूल भी कर पाएगा? तब क्या होगा? क्या करेगी वो.....कहीं आत्महत्या न कर ले? कहीं घर से न भाग जाए। दोनों ही कलंक हैं.....एक प्रताप भवन के लिए और दूसरा खुद संध्या के लिए। गुप्त विवाह ही सही पर शादी कोई गुड़ियों का खेल नहीं। पूरी ज़िंदगी समर्पित कर देनी पड़ती है। मैंने जिम को सब कुछ बता दिया था। उन्होंने हमेशा की तरह मुझे धीरज ही बँधाया-\"सब ठीक हो जाएगा। इन सब बातों को कबूल करने में वक़्त लगता है पर कबूल हो जाता है। कोठी को भी दोनों की शादी को मान्यता देनी ही होगी।\"
देश उलटफेर के कगार पर था। ऐसे में किसी भी प्रकार की तसल्ली व्यर्थ लग रही थी।
तीसरा पन्ना
कल रात हम डिनर लेकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि किसी ने दो बार दरवाज़ा थपथपाया। जिम ने रिवॉल्वर हाथ में ली और बाहर के कमरे में आकर दरवाज़ा खोला। ऊँट पालने वाले की वेशभूषा में एक व्यक्ति अंदर आया। जिम से रात भर के लिए शरण देने की विनती की.....कहा कि वह ब्रिटिश विरोधी है और भारत की आज़ादी चाहता है। उसने सीने में रिवॉल्वर छिपा रखी थी, जेब में फ़ोल्डिंग पर्स था जिसमें ज़रूरी काग़ज़ात, नक़्शे आदि थे।
\"क्या चाहते हो?\" जिम ने रिवॉल्वर ताने हुए पूछा।
\"सिर्फ़ आज रात के लिए आश्रय। पुलिस मेरे पीछे है।\"
\"क्रांतिकारी हो! जानते हो मैं अंग्रेज़ हूँ।\"
क्रांतिकारी ने मुझे देखा और हथियार डाल दिए-\"तो मार दें गोली, कहीं-न-कहीं तो मरना ही है, यह भी तो शहीदी मौत कहलाएगी। क्या ग़लत कर रहे हैं हम? अपना ही देश तो माँग रहे हैं आप लोगों से। बापूजी की अहिंसा आपको रास नहीं आती, हिंसा पर उतर आते हैं। हमारी ज़मीन, धन-दौलत छीनकर हमीं पर रुआब?\"
युवक हाँफ़ने लगा। जिम की रिवॉल्वर नीची हो गई। उन्होंने आगंतुक को अंदर बुलाकर दरवाज़ा लगा लिया और बत्ती बुझाकर उसे आराम करने का इशारा किया। बाहर पुलिस के भारी बूटों की आवाज़ देर तक माहौल थर्राती रही। अपने कमरे में आकर जिम ने मुझसे कहा, \"उसे कुछ खाने-पीने को दे दो।\"
मैं आशंकित थी। जिम के व्यवहार ने मेरे अंदर खलबली मचा दी थी। नहीं रहा गया तो पूछा-\"ऐसा क्यों किया आपने, क्या ये देशद्रोह नहीं है?\"
जिम ने चकित हो मुझे देखा। न जाने कितने तूफ़ान छुपे थे उन आँखों में-\"भारतीय सिपाही भी तो भारतीय क्रांतिकारियों को टॉर्चर करते हैं, क्या वे देशद्रोही नहीं हैं?\"
\"लेकिन वे तो गुलाम हैं, जैसा हुक्म होगा पालन करेंगे।\"
\"मालविका!\" जिम ने मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा-\"मैं ईस्ट इंडिया कंपनी में उच्च पद का ऑफ़ीसर ज़रूर हूँ लेकिन मेरा जन्म भारत में हुआ है। सच पूछा जाए तो मैंने अपने देश को जाना ही नहीं कि कैसा होता है अपना देश! मैं अपने को भारतीय मानता हूँ। और तहेदिल से चाहता हूँ कि भारत आज़ाद हो जाए।\"
मैंने अपना सिर धीरे-धीरे जिम के उन्हीं हाथों पर झुका दिया जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आश्वस्त कर रहे थे।
चौथा पन्ना
लंदन में जिम की थोड़ी-बहुत पैतृक संपत्ति है। एक मिल है और एक फार्म हाउस भी जिसकी देखभाल जिम के चचेरे भाई करते हैं। उस संपत्ति में जिम की ज़रा भी रूचि नहीं है। हालाँकि उस संपत्ति से होने वाली आय का जिम के हिस्से का धन हर साल बैंक में जिम के नाम जमा हो रहा है लेकिन वह धन कितना है यह भी जिम नहीं जानते। ऐसे निर्विकार इंसान का क्या कीजै?
पाँचवाँ पन्ना
महीने भर की यूरोप यात्रा कराके जिम मुझे मालवगढ़ वापस नहीं लाए, सीधे शिमला ले आए। अच्छा ही हुआ। मालवगढ़ रहने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी। मैं कोई ऐसी नई जगह रहना चाहती थी जहाँ पहले न आई होऊँ। जहाँ मेरा अतीत दबे पाँव मुझ पर हावी न रहे, जहाँ कोई सवाल न हो, संशय न हो, बस ज़िंदगी का भरा पूरा छतनारा वृक्ष हो जिसके नीचे मैं बकाया उमर गुज़ार सकूँ। वैसे अतीत हर वक़्त धूप के उस ज़िद्दी टुकड़े-सा धप्प-से मेरे आगे आ धमकता है जिसे ढकते तोपते थान के थान कपड़े ख़र्च हो गए। यूरोप की यात्रा में जब हम जिम की बड़ी बहन के घर पेरिस गए तो वहाँ भी चर्चा उठी थी-\"तुम राजस्थानियों में विधवा औरतें ज़िंदा जलाई जाती हैं?\"
मैंने कहना चाहा, औरत कहाँ नहीं जलाई जाती-पूरे विश्व में औरत की स्थिति एक जैसी ही है-कहीं वह उम्रभर जलती है, कहीं झटके से एक बार में ही।
\"यह एक कुप्रथा है जिसे राजस्थानी समाज धर्म की आड़ में बढ़ावा दे रहा है जबकि उन लोगों का इतिहास कुछ और ही कहता है। अपनी इच्छा से शरीर त्याग देने वाली सती स्त्रियाँ जब चिता पर बैठती हैं तो चिता अपने आप जल उठती है, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं जलाया जाता।\" जिम ने हक़ीकत पेश की तो मैं उनका चेहरा देखती ही रह गई।
\"इसी प्रथा को आज ज़बरदस्ती विधवा को पति की चिता के साथ जलाकर जीवित रखा गया है। यह समूह के द्वारा की गई हत्या है जिसे धर्म का जामा पहनाया गया है। घोर पाप, मृत्यु दंड भी जिसके लिए छोटा दंड है। मुट्ठी भर लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होना चाहते हैं और इस सनकी ज़िद्द पर उतर आते हैं। क्या हक़ है उन्हें ऐसा करने का?\"
जिम तैश में आ गए थे। ऊपर से उनकी बहन ने आग में घी का काम किया-\"तुम नहीं बचाते इन्हें तो ये जला दी जातीं।\"
उपकार-एहसान-इस सबसे मैं दूर रहना चाहती हूँ। नहीं याद करना चाहती मैं अपना अतीत। धुआँ भरा दमघोंटू अतीत.....जिम! किसी खुली जगह ले चलो मुझे-जहाँ मेरा पीछा एक भी घटना न करे। अब तो मैं अपनी परछाईं से भी डर जाती हूँ।
छठा पन्ना
शिमला आकर मैंने शिमला की वादियों में नए जन्मे पंछी की तरह अपने पंख पसार लिये। जिम के लकड़ी से बने कॉटेज में, जो यूरोपीय स्थापत्य का आभास देता लाल टीन की ढलवाँ छत वाला बेहद खूबसूरत और तमाम सुख-सुविधाओं से पूर्ण था, मैं महारानी की तरह निवास करने लगी। पहाड़ी नौकर तो मानो मेरी और जिम की सेवा करने के लिए ही धरती पर आया था। वह मेरे पाँवों में से सैंडिल उतारता भी था और पहनाता भी था। सप्ताह में एक दिन जिम मुझे डांसिंग क्लब ले जाते हैं जहाँ मैं मात्र दर्शक बनी फ़्लोर पर थिरकते अंग्रेज़ दंपत्तियों को देखती रहती। यह डांसिंग क्लब सिर्फ़ अंग्रेजों के लिए ही बनाया गया था। लोअर जाखू रोड पर उतरते ही बोर्ड लगा है-\'प्राइवेट रोड\'। इस रोड को केवल अंग्रेज़ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात जो मैंने इन लोगों में ख़ास देखी, वह है जीने की भरपूर कला। ज़िंदगी के हर पल का ये जिंदादिली से उपयोग करते हैं और कभी निराश नहीं होते। भले ही थोड़े समय के लिए ये कहीं निवास करें पर वहाँ भी अपनी सुख-सुविधाओं की सामग्री जुटा लेते हैं।
सातवाँ पन्ना
आज मारिया के पत्र ने चौंका देने वाली लेकिन सुखद ख़बर दी कि संध्या की शादी अजय से हो रही है। मुझे इसी का डर था कि कहीं मेरे द्वारा आरंभ किए इस महायज्ञ की पूर्णाहुति यज्ञ अग्नि को बुझा ही न डाले। लेकिन पायल ने गवाही देकर मेरा सिर गर्वोन्नत कर दिया। भविष्य में संभावनाएँ हैं पायल से। प्रताप भवन में बरसों बाद कोई नगीना पैदा हुआ-यही तो कहा था न पायल के बाबा ने। वे महापुरुष थे, तमाम गुणों से पूर्ण। लेकिन ये आज मुझे क्या हो गया? मालविका तो मर चुकी है.....अब प्रताप भवन या पायल के बाबा का ज़िक्र भी मेरे लिए असह्य है। नहीं, मूँदनी ही होंगी आँखें उस ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से।
मारिया ने बताया कि संध्या की शादी बिल्कुल अव्यवस्थित थी। न शान-शौकत, न ज़मीदाराना आभास, कोई बात नहीं। मौका ही ऐसा था। वो तो उनकी शादी हो गई यही महत्त्वपूर्ण बात है। जिम कहते हैं-\"उदास न हो, हम कलकत्ते चलकर शादी सैलिब्रेट करेंगे। जैसा तुम चाहोगी, सारी मन की क़सर निकाल लेंगे।\"
जिम अक़्सर मेरा मन पढ़ लेते हैं और प्रयास करते हैं कि मैं किसी भी तरह दुखी न रहूँ। मेरी छोटी-छोटी बातों का इस क़दर ध्यान रखते हैं कि पापी मन सोचने लगता है कि मालविका बनकर उतने साल प्रताप भवन में क्यों गँवा डाले। क्यों न जिम की होकर पैदा हुई ताउम्र के लिए। कभी-कभी मेरी ऐसी सोच मुझे अपने ही कठघरे में खड़ा कर देती है और मैं जिरह करने लगती हूँ अपने आप से। जैसे पायल करती है हर बात में जिरह। उसे न कोई रीति-रिवाज़ बिना पूर्ण संतुष्ट हुए स्वीकार है और न किसी की सीख। हज़ारों सवाल उसे घेरे रहते हैं। अब तो शांति निकेतन में पढ़ने लगती है। खुले आकाश तले विद्या अध्ययन व्यक्तित्व में और निखार लाएगा। उसे ज़िंदगी की चुनौती स्वीकार है और मेरी आँखों में बस यही ख़्वाब आ बसा है कि मैं पायल को सफलतम इंसान के रूप में देखूँ। इधर मैंने भी वकील साहब से अंग्रेज़ी सीखना आरंभ कर दिया है।
आठवाँ पन्ना
आज जिम मुझे अपना फ़ैमिली फोटो एल्बम दिखा रहे थे। माँ, बाप और तीन बहनें-बीच में सबसे छोटे जिम। उनके पिता बरसों पहले हिंदुस्तान केवल नौकरी करने आए थे लेकिन यहाँ की खूबसूरत प्रकृति, साल भर बदलते रहने वाले मोहक मौसम और बेहद भोले भारतीयों के बीच वे ऐसे रम गए कि यहीं बस गए। यहीं उनके चारों बच्चे हुए, यहीं पले-बढ़े। लेकिन तीनों बेटियों की शादी लंदन में हुईं। जिम ने शादी नहीं की। अपने इस फैसले के लिए उन्हें माँ-बाप का कड़ा विरोध भी सहना पड़ा। अपनी बहू की आस लिये दोनों दुनिया से कूच कर गए। जिम ने तब अपने आपको बहुत कोसा, वे स्वयं को माँ-बाप का दोषी समझने लगे।
\"क़ाश, तुम पहले मिल जातीं मालविका तो मेरा मन अपराध बोध से पीड़ित नहीं होता। बेटा होकर मैंने पिता के प्रति कोई कर्त्तव्य पालन नहीं किया।\"
जिम भावुक हो उठे थे। मैंने सांत्वना दी कि उन दोनों के बाद ही सही आपने शादी करके उनकी आत्मा को शांति पहुँचाई है, यह क्या कम है।
नौवाँ पन्ना
कलकत्ते में संध्या, अजय और पायल से मिलकर बड़ी राहत मिली। संध्या और अजय को शादी के बंधन में बँधा देखा, बेहद अच्छा लगा। मैं यही चाहती थी क्योंकि मैंने दोनों के प्रेम की गहराई देख ली थी। वरना क्या मैं उनके गंधर्व विवाह का जोखिम उठाती? न जाने क्यों संध्या से बेहद लगाव है और पायल तो मेरा ही अंश है, मेरे शरीर का टुकड़ा जो मुझसे जुदा होकर अपने हिसाब से अपने लिए शरीर गढ़ लेगा। जिम कहते हैं कि मैं पायल को अपने पास शिमला बुला लूँ। लेकिन मैं प्रताप भवन के किसी भी सूत्र को पकड़कर कमज़ोर होना नहीं चाहती और यह जिम के प्रति अन्याय होगा। मुझे केवल जिम की होकर रहना चाहिए। उन्होंने मुझे मृत्यु के द्वार से घसीटा है इसीलिए मुझ पर हक़ है उनका।
इसके आगे अंग्रेज़ी की कुछ पंक्तियाँ लिखी थीं दादी ने। फिर कुछ अंग्रेज़ी और हिंदी की कविताएँ। एक-दो पन्नों में मात्र चंद शब्द ही-दादी के बेहद निजी शब्द जो जिम ने उनसे कहे होंगे। इसके बाद था अगला पृष्ठ।
दसवाँ पन्ना
मैंने पेरिस में रहकर केक बनाना सीख लिया है। जैम, जैली, सॉस भी.....क्रिसमस के त्यौहार पर इस बार मैंने बहुत बड़ा केक बनाकर उसे अपने हाथों से सजाया भी था। ताज्जुब है अब जब भी किचन जाती हूँ, सूप, पुडिंग, केक, पैन केक यही बन पाटा है मुझसे। यही अच्छा भी लगने लगा है। लेकिन जिम कुछ और ही उम्मीद करते हैं मुझसे-\"वैसा लंच-डिनर तैयार करो न जैसा प्रताप भवन में बनवाती थीं तुम! चटपटा लज्ज़तदार। जिसे खाकर मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था।\"
मुझे हँसी आ गई-\"आप मेरा नाम मर्लिन क्यों नहीं रख देते?\"
\"क्यों? मैं ही अपना नाम क्यों न बदल लूँ? जयंत या फिर जयशंकर।\"
जयशंकर!.....और हम देर तक हँसते रहे, मैं कहना चाहती थी कि मुझे मालविका को भूलना है या तुम्हें जिम को? जिम ठीक कहते हैं अगर तुम मालविका को भूलना चाहती हो तो जिम को भी भूलना होगा क्योंकि चिता से ज़िंदगी तक की यात्रा जिम ने ही तय की है। वो कड़वा सच तो जिम के साथ भी जुड़ा है। सच बार-बार भूलने या पीछा छुड़ाने की बात करके हम दोनों और अधिक उससे जुड़ते चले जा रहे हैं। कगार पर खड़े होकर लहरों को भूला भी तो नहीं जा सकता और कगार से हटने का उपाय? हाँ, एक चाह है मन में या शायद प्रतिशोध कि मेरी कब्र मालवगढ़ में हो। मैं वहीँ दफ़नाई जाऊँ। यह प्रतिशोध किससे? प्रताप भवन से? नाते-रिश्तेदारों से या उस मिट्टी से जिसमें गिर-गिरकर मैंने चलना सीखा था। बहुत कलपाया है उस मिट्टी ने मुझे। उसी मिट्टी में समाकर मैं जता देना चाहती हूँ कि मैं कोई एहसान फरामोश नहीं। मिट्टी का क़र्ज़ उतारने मेरी निर्जीव देह मिट्टी को समर्पित। मालवगढ़ में जिम के बंगले से वह जगह दिखती है जिसे जिम अपनी पारिवारिक सिमिट्री बनाना चाहते थे। दूर-दूर तक फैला सन्नाटा और पंख पसारे मोर जो ज़मीन पर छिछली टुकड़ा भर हरियाली में बड़े मज़े से टहलते हैं। सच है सुख हमारी अपनी ज़मीन पर है जहाँ हम खड़े हैं। लेकिन हम उसे भूलकर यहाँ-वहाँ तलाशते घूमते हैं।
इसके बाद के बहुत सारे पन्ने मुख़्तसर से थे। कहीं कविताएँ-अंग्रेज़ी में, हिंदी में-कहीं संस्कृत के श्लोक-कहीं एक-दो पंक्तियाँ अस्पष्ट-सी। एक पन्ने पर मर्दाने स्वेटर का नाप लिखा था और दूसरे पन्ने पर खुबानियों के जैम की विधि-फिर लाल पेन से बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था-हम आज़ाद हो गए-यह पंक्ति रेखांकित थी और रेखांकन के दोनों तरफ़ दादी और जिम के हस्ताक्षर.....
ग्यारहवाँ पन्ना
जिम ने मुझे बाँहों में भर लिया और कानों में फुसफुसाए-
\"मुबारक हो मालविका.....इंडिया आज़ाद हो गया।\"
मेरी आँखों से खुशी के आँसू चू पड़े। एकाएक पायल के बाबा याद आ गए। आज़ाद भारत का सपना लिये जो दुनिया छोड़ चुके थे-क़ाश, वे होते और अपनी आँखों से इस आधी रात में भारत के खुलते बंधन देखते।
\"यह आज़ादी उन हज़ारों-लाखों क्रांतिकारियों और शहीदों की बदौलत मिली है जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया, ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचे, घर जलाए, जेल गए, यातनाएँ सहीं और फाँसी चढ़े। ये आज़ादी केवल अहिंसा से नहीं मिली है मालविका बल्कि गुलामी के अंधकार भरे आसमान पर बिजलियाँ इन्हीं ने चमकाई हैं। अपने शरीर की मशाल जलाकर आज़ाद भारत के प्रकाश को रचा है.....आओ, इन शहीदों के लिए हम दो मिनिट ख़ामोश खड़े रहें।\"
दो मिनिट के लिए कॉटेज भी मानो मौन श्रद्धांजलि अर्पित करता-सा लगा। मैं दौड़ी हुई पूजा के कमरे में गई और दीपदान की सारी बत्तियाँ जलाकर कृष्णजी के आगे सिर नवा दिया। फिर आटे के दीये बनाकर कॉटेज को दीवाली जैसी रोशनी से जगमगा दिया। बारिश के आसार थे, रह-रहकर बिजली चमक रही थी।
\"आओ मालविका, कलकत्ता फोन लगाते हैं।\" जिम ने नंबर लगाया और तहेदिल से बधाई दी। पायल को यह चिंता सताए जा रही थी कि अब हम लंदन चले जाएँगे। जिम छोड़ेंगे भारत? उनकी तो जन्मभूमि है ये। कहने को वे अंग्रेज़ हैं पर पूरी तरह हिंदुस्तानी संस्कृति में रचे-बसे और मेरे साथ रहकर तो खानपान में भी अंग्रेज़ियत छोड़ चुके हैं। मैं समझ नहीं पाती कि मेरी ज़िंदगी में जिम इतनी गहराई से कैसे शामिल हो गए। यह मेरे प्रति प्रेम है या भारत के प्रति लगाव है। हाँ, भारत के प्रति लगाव ही। वे भारत को बहुत जल्द आज़ाद देखना चाहते थे। क्रांतिकारियों के हर कार्य, हर प्रयास का वे हमेशा वर्णन करते। जिस क्रांतिकारी ने हमारे घर शरण ली थी, वह पकड़ा गया था और उसे ब्रिटिश हुकूमत ने फाँसी पर चढ़ा दिया था। जिम गए थे जेल में, फाँसी वाले दिन उससे मिलने। लौटकर पूरी घटना ब्योरेवार बताई थी उन्होंने-\"जब उसे फाँसी की सज़ा का पता चला तो उसकी खुशी का पारावार नहीं था। उसका पूरा परिवार भी वहीँ खड़ा था। वह सबसे हँस-हँसकर मिल रहा था। उसके चेहरे पर जो मोहिनी हँसी मैंने देखी.....वह मैं कभी नहीं भूल सकता मालविका। उस हँसी में भारतीय होने का गर्व था और ब्रिटिश सरकार के प्रति हिक़ारत। वह हँसते-हँसते फाँसी के लिए चला गया। उसके परिवार में सभी की आँखें सूनी और उदास थीं। उस वक़्त तो कोई नहीं रोया लेकिन जब कंबल ढँकी उसकी लाश लाई गई तो एक-एक कर सभी की आँखें बरस पड़ीं। मेरी आँखें भी आँसुओं से भर गईं। मैंने उसके पिता के कंधे पर सांत्वना भरे हाथ रखे-इस शहीद की मृत्यु पर आँसू बहाना इसकी शानदार मौत का अपमान करना है। मरना तो सभी को है पर ऐसी मौत किसे मिलती है।\"
मालविका, उसकी वीरता ने मेरे दिल पर गहरा असर कर दिया।
बारहवाँ पन्ना
मारिया के पत्र ने मेरा मन आलोड़ित कर दिया। पत्र जिम ने भी पढ़ा और उनकी आँखों में खुशी के आँसू झिलमिलाने लगे-\"ओह.....ग्रेट। पायल रोम यूनिवर्सिटी से पी-एच.डी. करेगी यह उतनी ग्रेट बात नहीं जितनी अपनी रूढ़ियों को तोड़ने की उसकी कोशिश, औरत का स्वतंत्र होना भी अपने आप में एक क्रांति है।\"
मैंने जिम को गहराई से देखा। वहाँ पायल के प्रयास के लिए गर्व था। पत्र देर से मिला, पायल अब तक इटली के लिए रवाना हो गई होगी वरना उसे बधाई देती फोन पर। उस रात मैं देर तक पूजा घर में बैठी पायल की कामयाबी के लिए प्रार्थना करती रही। जानती थी इस ख़बर का नाते-रिश्तेदारों में जमकर विरोध होगा। जो आज तक नहीं हुआ, पायल उसे करने जा रही है। वैसे भी विभाजन को लेकर देश में दंगे भड़क उठे हैं। और जब बाहर आग लगी हो तो घर की आग बहुत छोटी नज़र आती है। कुछ दिनों में ठंडी पड़ जाएगी। पायल के क़दम अब लौटेंगे नहीं, मैं जानती हूँ।
दादी की डायरी ने मेरे मन के सन्नाटे चीर डाले और हलचल मचा दी। अगला पृष्ठ मेरे नाम सारी संपत्ति करने का खुला दस्तावेज था जिसे अभी पढ़ने की मुझमें ताक़त नहीं थी। जिम के बारे में सोच-सोचकर मैं लगभग शून्य हो चली थी। जितना उन्हें जाना उससे बढ़कर उन्हें पाया। वे फरिश्ता थे जो प्रेम और मानवता का सम्मान करता है। पहले मैं सोचती थी कि जिम दादी को पाकर धन्य हो गए लेकिन अब सोचती हूँ कि दादी जिम जैसे व्यक्ति को पाकर धन्य हो गईं। ये उनके सत्कर्म थे जिसने उन्हें वरदान के रूप में जिम दिया। मैंने हाथ बढ़ाकर नाइटलैंप ऑफ़ किया और बिस्तर में लेटते हुए मन के सारे किनारे तोड़कर मैं बुदबुदा उठी-\"बाबा, जिम बाबा।\"
रोम से एक निमंत्रण पत्र कब से मेज पर रखा हुआ मेरी बाट जोह रहा था। खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। दादी की डायरी ने एक नया अध्याय मेरी ज़िंदगी से जोड़ दिया था। मैं उसी में सोती-जागती मानो नशे में डूबी रहती। संध्या बुआ फोन करके हालचाल जानना चाहतीं-\"आ क्यों नहीं रही हो शाम को, हम तुम्हारे इंतज़ार में बैठे रहते हैं।\"
क्यों बुआ? क्यों मेरा इंतज़ार? मुझे मेरी शामों की तनहाइयों के एहसास में जीने क्यों नहीं देतीं? मैं अनुभव करना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ कि तनहाई क्या होती है? अगर मैं किसी की तनहाई बाँट सकती तो यह ज़िंदगी तो नहीं ही होती न बुआ? मैं तुम्हारी बेटी बनूँ.....क्यों बुआ.....क्यों? लेकिन फोन पर बस इतना ही कहा-आऊँगी बुआ.....कुछ ज़रूरी पर्चे तैयार करने थे जिन्हें सेमिनार में पढ़ना है। अगले महीने बंबई में सेमिनार है न बुआ।
बुआ ने मीठी झिड़की दी-\"अब तू मुझे पुरानी ख़बरों का हवाला न दे। अजय भी तो तेरे ही साथ जॉब करते हैं। तुमसे पहले मुझे सब पता चल जाता है। अच्छा बता, मिहिर की शादी का कार्ड आया?\"
\"नहीं तो......या आया हो तो मैंने तीन-चार दिनों से डाक देखी नहीं, अभी देख लेती हूँ।\"
संध्या बुआ मेरी लापरवाही पर दिल खोलकर हँसीं। फिर बोलीं-\"अच्छा, तुम चिट्ठियाँ पढ़ो। मेरे वफ़ादारों (उनके कुत्ते) के नाश्ते-पानी का वक़्त है। झबरू को इंजेक्शन भी लगवाना है-ओ.के.।\"
रिसीवर रखकर मैंने डाक देखी-सबसे पहले निमंत्रण पत्र। हाँ, मिहिर का ही था। तो मिहिर अपनी रोमन प्रेमिका से आख़िर ब्याह रचाने ही वाला है। उसी की ख़ातिर तो वह रोम में सैटिल हुआ था। उसकी प्रेमिका है भी बेहद अच्छी लड़की। लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी कि मिहिर रोमन तरीक़े से शादी कर रहा है। चर्च में जाकर.....आख़िर विवाह में माँ-बाप भी शामिल होंगे। हिंदू तरीके से ब्याह होना चाहिए उसका या फिर दोनों तरीकों से। आख़िर इतना इंतज़ार किया है मिहिर ने जबकि शादी वो उसी साल करने वाला था जिस साल मैंने रोम से विदा ली थी। कुछ महीनों तक मिहिर के पत्र आते रहे। उसकी माँ को दिल की बीमारी थी.....उनके लिए कोई भी शॉकिंग न्यूज़ जानलेवा हो सकती है इसलिए वह कैसे बताए कि वह रोमन लड़की से शादी करना चाहता है जबकि उसकी माँ कलकत्ते में एक बंगाली लड़की से उसकी शादी तय कर चुकी हैं। बस इसी कशमकश में लंबा अरसा गुज़र गया। अब शायद वह माँ को मना पाया होगा। निमंत्रण पत्र के साथ दो लाइन का ख़त था-\"पायल, तुम्हें रोम आना है और हमारी दोस्ती की डोरी को और मज़बूत करना है।\"
मिहिर का इसरार पूरा नहीं कर पाई। हालाँकि विदेश कई बार गई। सैमिनार अटैंड करने जर्मनी, लंदन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। साल दर साल गुज़रते गये। जिस साल ऑस्ट्रेलिया गई उसी साल मैं बंबई स्थानांतरित हो गई। और ऊँचा ओहदा और ऊँचा सम्मान। शोध के विद्यार्थियों की मेरे नाम से लगती भीड़। शोध ग्रंथों की सजिल्द मोटी किताबें मेरे कमरे की अलमारी में सजती रहीं। मेरे एक विद्यार्थी ने उस अलमारी के बाजू में एक सुंदर-सी तख़्ती टाँग दी जिस पर लिखा था-\'पायल सिंह की लिखी किताबें।\' मानो वह एक प्रमाण पत्र था जो मेरे शिष्यों ने मुझे दिया था। इन शिष्यों के बीच मैं अपने को पूर्णतया भूल चुकी थी। कभी शरीर की नैसर्गिक भूख दस्तक भी देती तो मैं अनसुनी कर अपने को और अधिक व्यस्त कर लेती। जानती थी यह काम वासना एक फूल की उम्र के बराबर है जो खिलता है और अपनी सुगंध, सौंदर्य और रस दूसरों पर लुटाकर मुरझा जाता है बिखरकर स्वाहा हो जाता है, लेकिन जीवन चक्र चलते रहने के क्रम में उस फूल का धरती पर गिरा बीज पुनः जी उठता है। यह मुझे नहीं करना है। पायल एक ही रहेगी.....एक ही अनूठी, निराली, बिरली नारी बनकर.....कोई और पायल हो ही नहीं सकती। यह भी जानती हूँ यह दंभ है मेरा। ईश्वर के जन्म-मृत्यु के चक्र में अनधिकार प्रवेश की चेष्टा है.....पर यह तो उस ईश्वर से लिया बदला है मेरा जिसने सर्वगुणसंपन्न नारी तो बनाई पर उन गुणों को परखने का तराजू पुरुष के हाथ में पकड़ा दिया जिसकी आँखों पर पट्टी बँधी है और जिसके पास इतने वज़नी माप हैं कि नारी के गुणों का पासंग हलका ही नज़र आता है उसे।
मेरे बंबई आने पर वीरेंद्र और बाबूजी आए थे। कुछ सामान अम्मा ने भेजा था। लगे उलाहना देने-\"इस डिब्बी जैसे मकान में ज़मींदार प्रताप सिंह की पड़पोती रहेगी? वो भी अकेली? उधर तो संध्या थी तो हम लोग निश्चिंत थे।\"
\"बाबूजी, आप तो मुझे निरी बच्ची समझते हैं अब तक।\"
\"सो तो तुम हो ही, उसमें समझना क्या? कभी-कभी तो घबरा जाता हूँ कि तुम्हारे बचपन को मेरे बाद सम्हालेगा कौन? अम्मा तुम्हारी इतनी बीमार न होतीं तो खुद आतीं।\" बाबूजी ने हताशा भरे स्वर में कहा।
एक ही बेटी है उनकी, वह भी इतनी विद्रोहिणी! उसके घर, गृहस्थी, दामाद का सपना तो उनकी आँखों में भी अंगड़ाइयाँ लेता होगा। और मैं ऐसी निखिद्ध कि किसी के सपने में खरी नहीं उतरी।
महीने भर रहकर वे अपनी लाड़ली, ज़िद्दी बिटिया के लिए जुहू में बंगला ख़रीदकर, नौकर-चाकर देखभाल कर नियुक्त करके वे उसकी गृहस्थी अपनी ज़मींदाराना रूचि से सजा गए। जबकि मैं ये सब चाहती नहीं थी। मेरे नाम की गई जिम की सारी संपत्ति वीरेंद्र ही सम्हाल रहा था। उसके कंधों पर कितना सारा बोझा था लेकिन उर्मिला भी खूब साथ दे रही थी उसका। पूरा ऑफ़िस का काम वही देखती-भालती थी।
अम्मा काफी बीमार थीं। दो बार मैं भी देख आई थी उन्हें पर मेरी नौकरी ऐसी कि लगन से उनकी सेवा नहीं कर पा रही थी। यह मलाल मुझे खाए जा रहा था। अपना होना तुच्छ-सा लग रहा था कि एक दिन जी कड़ा करके महीने भर की छुट्टी लेकर मैं बनारस चली गई। मेरे पी-एच.डी. के विद्यार्थियों के लिए इतनी लंबी मेरी अनुपस्थिति जायज़ नहीं थी लेकिन मेरे लिए इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था।
अम्मा सूखकर काँटा हो गई थीं। मैं उनके मुट्ठी भर बचे बालों में तेल ठोकती जाती थी और रोती जाती थी। वे अपने कमज़ोर दुर्बल हाथों से मेरी पीठ सहलातीं-\"पायल, तुम्हें इतना कमज़ोर मैंने कभी नहीं पाया।\"
मैंने उनके सीने में मुँह गड़ा दिया-\"अम्मा, न जाने क्यों बड़ा जी घबरा रहा है। ज़िंदगी में जो कुछ चाहा उसे हासिल किया लेकिन ज़िंदगी छले क्यों जा रही है मुझे?\" अम्मा फीकी हँसी हँस दी-\"पगली! क्या कोई अमर होकर आया है? यह ज़िंदगी का छल नहीं बल्कि कठोर सत्य है। पायल, अभी तुम्हारा लक्ष्य पूरा कहाँ हुआ है? जब तक एक भी विद्यार्थी तुम्हारे गाइडेंस का इच्छुक रहेगा तब तक लक्ष्य अधूरा समझो।\"
कितनी बड़ी बात कह दी अम्मा ने। उन्होंने जैसे मुझे ज़िंदगी जीने का अंतहीन सिरा पकड़ा दिया। मैं जो समझे बैठी थी कि मेरी ज़िंदगी की नदी ठहर-सी गई है उसके बहाव को दिशा मिल गई।
मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने को थीं। अम्मा की हालत में भी सुधार हो रहा था। इसी बीच संध्या बुआ भी अम्मा को देखने आ गई थीं। अम्मा मुझे, बुआ को और उर्मिला को सामने बैठाकर प्रताप भवन की यादों में रमी रहतीं। उर्मिला अधिक नहीं बैठ पाती उसे ऑफ़िस भी देखना होता। अम्मा की तबीयत में सुधार से बाबूजी बहुत खुश थे। एक दिन बोले-\"पायल, भृगु संहिता देखोगी? तमाम जन्मों का हवाला है उसमें। यहाँ है भृगु संहिता-तुम चाहो तो चलें।\"
संध्या बुआ ने भी ज़ोर दिया-\"हाँ पायल, देख आओ.....मैंने और अजय ने तो वर्षों पहले देख ली थी।\"
अम्मा जी खुलकर हँसी-\"ले जाओ इसे.....दिखा लाओ, कहीं पिछले जन्म की ये मेरी दादी, पड़दादी न निकले.....नहीं तो मुसीबत।\"
मैंने भी अम्मा का मन हल्का करने के उद्देश्य से चुटकी ली-\"कोई फ़ायदा नहीं बाबूजी। भृगु संहिता में मेरे बारे में कुछ भी वर्णन नहीं मिलेगा। मैं तो अर्धनारीश्वर हूँ। आपकी बेटी भी, बेटा भी।\"
सभी हँसने लगे लेकिन अम्मा का वह स्वस्थ दिखता-सा चेहरा बुझते दीपक की तेज़ लौ थी.....जब तेल चुक जाता है और बत्ती तेज़ी से जल उठती है।
उस रात मेरी ज़िंदगी और प्रताप भवन के सबसे अधिक भयंकर दो हादसे हुए जिन्होंने मुझे हिलाकर रख दिया। रात नौ बजे ख़बर आई कि हरिश्चंद्र घाट की सीढ़ियों पर से बड़े बाबा का पैर फिसल गया है और वे पत्थरों की चोट खाते हुए गंगा में जा गिरे हैं। बड़े-बड़े तैराक गंगा में कूद पड़े थे पर बड़े बाबा किसी को नहीं मिले। हताश वीरेंद्र लौट आया था यह सवाल लिये कि बड़े बाबा गए कहाँ? बेहद पीड़ित कर देने वाली घटना थी वह। संध्या बुआ रोए जा रही थीं और बाबूजी अजय फूफासा को फोन लगा रहे थे। सभी रंज में डूबे हुए अपने-अपने बिस्तरों पर करवटें बदल रहे थे कि क़रीब ग्यारह बजे अम्मा ने आख़िर साँस ली। न तड़पीं, न किसी से कुछ बोलीं, न प्यास, न पानी। अचानक उर्मिला उनके बाजू में सोए गुड्डू और गप्पू को यह कहती उठाने गई कि दोनों भाई चलकर अपने बिस्तरों पर सोएँ यहाँ दादी को तक़लीफ होगी तो गुड्डू ने उनकी ओर इशारा किया-\"दादी हिलती भी नहीं, कुछ बोलती भी नहीं।\"
उर्मिला चीख़ पड़ी। सभी दौड़े। लेकिन खेल ख़त्म था। मैं फटी हुई आँखों से अम्मा के निर्जीव चेहरे को निहार रही थी। होंठ थोड़े खुले हुए से। मानो कह रहे हों-\"न पायल न.....रोना बिल्कुल नहीं.....रोना तो आत्मबल न होने का सबूत है.....बुज़दिली का सबूत है। मूढ़ता का सबूत है कि तुम इतना भी नहीं जानती कि जिसने जन्म लिया है वह मरेगा भी।\"
और मैंने अपने पर काबू पा लिया। आश्चर्य! कैसे? कैसे मैंने अम्मा का जाना स्वीकार कर लिया बल्कि तमाम परंपराओं को ताक पर रखकर मैं तो श्मशान भी गई और दिल की जगह पत्थर रखकर का टुकड़ा स्थापित कर मैंने अम्मा की चिता का जलना भी देखा। बस, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा.....सब कुछ धुएँ में समा गया।
धुआँ अरसे तक मुझे घेरे रहा, बंबई लौटकर भी.....दिन, रात, हफ़्तों, महीनों और जैसी कि धुएँ की आदत होती है दम घोंटने की.....तो सहसा ही यह दमघोंटू विचार तेज़ी से मुझे चीरता चला गया कि बड़े बाबा की लाश क्यों नहीं मिली गंगा में? शायद इसीलिए कि वे संन्यासी हो गए थे और हमें दाह संस्कार के कर्ज़ से भी उबार गए थे। उनकी विरक्ति नाते-रिश्ते और उनके अपने खून तक की विरक्ति बन गई थी। मेरी तीनों बुआएँ उनके खून का अंश आईं ज़रूर लेकिन किसी ने भी ये जिज्ञासा नहीं जताई कि आख़िर गंगा में गिरा उनका मृत शरीर गया कहाँ? क्या काशी करवट बन गया उनका शरीर जिसमें ढोंगी पंडितों ने सशरीर स्वर्ग भेजने का ढोंग रचा था। आदमी अपनी ज़मीन, जायदाद, गहने मंदिर की ट्रस्ट के नाम इसी लालच में कर देता था कि वह सशरीर स्वर्ग चला जाएगा। बस एक करवट लेगा और स्वर्ग के द्वार पर जा खड़ा होगा। भंडा तब फूटा जब एक आदमी काशी करवट की यातना से बचकर आया और उसने अंग्रेज़ कलेक्टर के आगे सारी घटना बयान की। सारी संपत्ति मंदिर ट्रस्ट को दान कराके उसे मंदिर के ही नीचे बने तलघर में ले जाया गया जहाँ एक बड़े-से पलंग पर उसे आँख मूँदकर लेटने के लिए कहा गया-\"बस, आँख मूँदते ही तुम स्वर्ग पहुँच जाओगे।\"
उसने श्रद्धापूर्वक आँखें मूँदी लेकिन घबराकर तुरंत खोल दीं और आँखें खुलते ही उसे छत पर लटकी बड़ी-सी तलवार दिखाई दी जिसकी रस्सी ढीली हो रही थी और वह किसी भी क्षण उसके शरीर के आर-पार हो सकती थी। वह फुर्ती से पलंग से हट गया। तलवार गिरी और बिस्तर में धँस गई। वहाँ कोई न था उस वक़्त। रस्सी काबू में रखने का काम भी छुपे तरीके से पंडित ही करते थे। तलघर की दीवार में एक बहुत बड़ी खिड़की थी जो सीधे गंगा की ओर खुलती थी। इसी खिड़की से रातोंरात मृत शरीर को गंगा में बहा दिया जाता था। वह व्यक्ति भी इसी खिड़की के रास्ते गंगा में कूदकर अपनी जान बचा पाया था। अंग्रेज़ कलेक्टर ने तुरंत छापा मारकर पंडितों को गिरफ़्तार करके मंदिर सील कर दिया था। यह घटना बाबूजी कई बार सुना चुके थे और हर बार इसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पंडितों के प्रति वितृष्णा से मेरे दिमाग़ की नसें तिड़कने लगती थीं।
मैंने यह घटना समित को भी सुनाई थी। समित इलाहाबाद से लैक्चरर की पोस्ट पर यहाँ आया था। उम्र में मुझसे दस-बारह साल छोटा लेकिन ज्ञान और तजुर्बे में मुझसे कहीं बड़ा। वह कवि भी था और उसकी बेहतरीन कविताओं की मैं कायल थी। न जाने कैसे लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता.....समय के व्यतीत होते-होते वह मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हर घटना को जान गया था। ख़ासकर दादी ने उसे बहुत प्रभावित किया था।
\"हाँ समित, मेरी दादी एक असाधारण व्यक्तित्व थीं।\"
\"मुझे बहुत अधिक ताज्जुब होता है पायल, ख़ासकर संध्या बुआ की शादी को लेकर उनकी ओर से की गई पहल का।\"
हम जुहू बीच पर बैठे थे और वह बीच की रेत पर अपनी उंगली की पोर से कविता की एक पंक्ति लिख रहा था-मैं उजड़ चुके अतीत के बियाबाँ में भटकने लगी-
\"समित, केवल संध्या बुआ ही नहीं-मारिया, मैं, बाबा सभी के प्रति उनकी विशालता मुझे विचलित कर जाती है। कहाँ मैं अदना-सी।\"
\"नहीं पायल, ऐसा सोचना भी दादी के प्रति गुनाह होगा। तुम अदना नहीं बल्कि वो मोती हो जो उनकी आँच में पकता रहा है।\"
मैंने कहना चाहा-मोती नहीं वो सहमा हुआ सच हूँ जिसने बहुत छोटी उम्र से दादी के एक-एक पल को बहुत नज़दीक से देखा, परखा और अपने ज़ेहन में उतार लिया और अपनी ज़िंदगी के ठोस फैसले कर डाले। इन फैसलों को लेकर मुझे लानत मलामत भी बहुत मिली लेकिन मैं जानती थी कि ऊपर से मीठी लगती उनकी सीख गन्ने के मीलों फैले वो खेत हैं जिनकी धारदार पत्तियों के बीच से गुज़रते हुए, लहूलुहान होते हुए भी मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती हूँ। मेरे अंदर अम्मा का जज़्बा था और दादी की ताक़त-इन दोनों के अभाव में मैंने उषा बुआ और रजनी बुआ को गृहस्थी में होम होते देखा था। संध्या बुआ अजय फूफासा के कारण होम होने से बच गईं। अजय फूफासा के कायस्थी कुल गोत्र ने संध्या बुआ को संरक्षण दिया।
\"क्या सोचने लगीं?\" समित ने काफी देर की ख़ामोशी के बाद पूछा।
\"नहीं, यूँ ही.....समित, मुझे पूर्ण संतुष्टि है अपने को लेकर। मैं तो दूसरों का सोच-सोचकर व्याकुल होती रहती हूँ।\"
वह ठठाकर हँस पड़ा। लहरें सहमकर वापस समुद्र की ओर लौट गईं। एक घोड़े वाला नज़दीक आकर ज़िद्द करने लगा-\"एक चक्कर लगा लीजिए न साहिब।\"
\"अरे, क्यों भाई? अच्छी ज़बरदस्ती है।\"
\"साहिब, सुबह से कुछ खाया नहीं, एक चक्कर लगा लेते तो.....\"
\"तो ऐसा कहो न?\" समित ने उसे जेब से निकालकर कुछ रुपए दिए-\"लो भई-समझ लो हमने चक्कर लगा लिया।\"
वह अवाक्.....ताज्जुब से भरा कभी हाथ में पकड़ा नोट और कभी हमें देखने लगा। समित ने उसका कंधा थपथपाया-
\"आज हमारी तरफ़ से खाना खा लो।\"
उसके चेहरे पर अविश्वास भरी मुस्कराहट खेल गई-\"हाँ भाई, जाओ अब। अपने घोड़े को भी घास खिला देना।\"
उसने कई बार हमें सलाम ठोंका और तेज़ी से चला गया। एक बड़ी विशाल लहर ने हमारे पाँव भिगो दिए थे।
जुहू बीच पर शाम ढल रही थी। आसमान लुभावना हो उठा था। आमदरफ़्त भी बढ़ती जा रही थी।
\"समित, अब चलें.....घर चलकर कॉफ़ी पिएँगे। मैं कुछ ग़ज़लों के कैसेट्स लाई हूँ अगर सुनना चाहोगे तो.....\"
\"अब लाई हो तो सुनना ही पड़ेगा।\" वह खड़े होकर पैंट पर से रेत झाड़ने लगा। समुद्र गरज रहा था और हवाएँ भी तेज़ हो रही थीं। अचानक पश्चिमी आकाश आँधी के संकेत देने लगा। हम तेज़ी से कार की तरफ़ आए। स्टीयरिंग समित ने ही सम्हाला और मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। घर लौटे तो बंगले के आगे लगे फूलों की क्यारियों में माली पानी सींच रहा था। पाइप क्यारी में डाल वह दौड़ा आया और सलाम ठोंककर फाटक खोला। कार पोर्टिको में खड़ी कर हम अंदर आए। लछमन सेवा में तैनात था। पता नहीं क्यों माली को, लछमन को और खाना पकाने वाली तुलसी को देखकर मैं अपनी सारी उदासी भूल आती हूँ। जैसे मैं एक बड़े परिवार की मालिक हूँ। जब ये बात मैंने समित से कही तो उसके पास इसका काट मौजूद था-\"पायल, ये कैसी इच्छा है तुम्हारी? अगर परिवार ही बसाना था तो फिर शादी क्यों नहीं की?\"
\"शादी भी तो एक सौदा है। खाना, कपड़ा, मकान और औलाद पैदा करने के एवज ज़िंदगी साथ ढोने का सौदा। उस सौदे से ये सौदा अच्छा। ये अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं बिना किसी अपेक्षा के।\"
समित से कुछ कहा नहीं गया था फिर।
तुलसी कॉफ़ी बना
\"इसीलिए तो पायल, तुम्हें संपत्ति सौंपी गई क्योंकि तुम्हें लालच नहीं था, ज़रुरत नहीं थी।\"
मैं समित के तर्क पर चकित थी।
\"अगर यह संपत्ति लालची हाथों में पड़ती तो नामोनिशान मिट जाता अब तक और कोई नहीं चाहता कि दुनिया से जाने के बाद उसका नामोनिशान मिटे।\"
कॉफ़ी का आख़िरी घूँट लेकर समित उठ खड़ा हुआ-\"चलते हैं अब, कल यूनिवर्सिटी में मुलाक़ात होगी।\"
उसके जाने के बाद असीम शांति से भरकर मैंने आरामकुर्सी पर अपना सिर टिका लिया। अब मेरे मन में कोई द्वंद्व न था। संशय के सारे जाले मैंने उतार फेंके थे और एक साफ़ सुथरा एहसास हो रहा था बल्कि अब तो जिम की विरासत को सहेजकर रखने की चाह-सी उठने लगी थी मन में। हाँ, जिम के और दादी के विश्वास को कायम रखना ही होगा। अभी तक इस नज़रिए से तो मैंने सोचा ही नहीं था।
पश्चिमी आकाश में उठने वाली आँधी शांत हो चुकी थी और समुद्री हवाओं में बंगले के फाटक पर लगा अशोक वृक्ष झूम रहा था। रात मैंने वीरेंद्र को फोन लगाया। हालचाल पूछने-बताने के बाद मैंने शिमला से सेब के बगीचे, कॉटेज, मालवगढ़ का बंगला, फार्म हाउस आदि की व्यवस्था के बारे में जानना चाहा तो वीरेंद्र ताज्जुब से भर उठा-\"जीजी! क्या बात है? मन तो ठीक है न आपका?\"
मैं हँस पड़ी-\"मन ने चेताया तभी तो होश आया कि ये तुम्हारी कामचोर जीजी सारा भार तुम्हारे कंधों पर डालकर निश्चिंत बैठी है और तुम खटे जा रहे हो।\"
\"नहीं जीजी, आपके ऊपर भी तो यूनिवर्सिटी के काम की ज़िम्मेवारी है। यहाँ उर्मिला सम्हालती है सब। अगर आप चाहें तो उर्मिला के साथ शिमला और मालवगढ़ जाकर देख आएँ सब। बच्चों की छुट्टियाँ भी रहेंगी, उर्मिला निश्चिंत होकर जा सकेगी।\"
\"हाँ वीरू, जाना पड़ेगा लेकिन शिमला बाद में, पहले मैं मालवगढ़ जाऊँगी। मेरे ऊपर एक बोझ-सा है।\" वीरेंद्र ने उस बोझ को छेड़ना उचित नहीं समझा। फोन बाबूजी को दिया-\"इस बार तुम छुट्टियों में नहीं आ रही हो?\" बाबूजी की काँपती बूढ़ी आवाज़ ने मुझे विचलित-सा कर दिया। एकदम मना नहीं कर पाई। अम्मा के बाद वे अकेलापन बहुत महसूस करने लगे थे।
\"आऊँगी बाबूजी.....मालवगढ़ में रहने के बाद भी अगर छुट्टियाँ बचती हैं तो आऊँगी।\"
बाबूजी ने बुझी हुई आवाज़ में-\'ठीक है बेटा\' कहा और रिसीवर रख दिया। उनकी आवाज़ देर तक मुझे झँझोड़ती रही।
सुबह उठते ही मैंने चाय पीते हुए लछमन को समझा दिया था कि \' इंक्वायरी से पूछ लेना कि मालवगढ़ के नज़दीक तक कौन-सी ट्रेन जाती है, जहाँ से मालवगढ़ के लिए, जीप आसानी से मिल सके। पच्चीस दिसंबर से छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं.....उसी तारीख़ का टिकट ले आना।\'
फिर समित को फोन लगाया-
\"समित, तुम्हें बताना भूल गई थी। आज जहाँगीर आर्ट गैलरी में प्रभा रॉय की एकल प्रदर्शनी है, तुम आओगे न। मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगी आज।\"
\"ओह! लेकिन मेरे पीरियड्स हैं, कोशिश करूँगा।\"
\"हाँ प्लीज़। और सुनो, इस बार क्रिसमस वेकेशन में मैं मालवगढ़ जा रही हूँ।\"
\"क्याऽ.....मालवगढ़? अरे क्यों भई,अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया पायल?\"
\"तुम्हीं ने तो चेताया था वरना इतने बरसों तक मुझे सुध ही नहीं थी।\"
फोन रखकर मैंने इत्मीनान की साँस ली।
\"के सोचो हो बेटी सा! सब उजाड़ हो गयो। इ खाली कोठी मं थारो मन लागणो मुश्किल हे! म्हें थारे वास्ते के करां?\"
अतीत को वर्तमान ने निगल लिया और उस भयानक सत्य से मैं सहम गई। देखा-उदासी और सन्नाटे में डूबे प्रताप भवन का ज़र्रा-ज़र्रा मेरे वर्षों बाद आने की एवज में खुशियाँ जताने की कोशिश कर रहा है। मैं भी सहज होना चाहती हूँ, रामू काका को भी सहज देखना चाहती हूँ जो अपने पिता कोदू के मरने का बाद बड़ी मुस्तैदी और वफ़ादारी से प्रताप भवन को जिलाए हैं।
\"काका! खाना-वाना कौन बनाएगा?\"
\"सब बंदोबस्त हो जावेगा बेटी सा! थारे वास्ते के चीज की कमी ह? एक महाराजिन तो मं बुला ल्यायो हूँ। आप जितना दिन अठे रहोगो, वा अठे ही रहकर थारी सेवा करसी।\"
मैं मुस्कुरा दी। थकान और अतीत की स्मृतियों ने मुझे और भी थका डाला था। नहाकर मैं सोना चाहती थी। सुबह फिर रामू काका को समझाना भी है अपने प्रोग्राम के बारे में। अचानक काम आ जाने की वजह से उर्मिला मालवगढ़ नहीं आएगी, मेरे शिमला पहुँचने पर वहीँ आएगी।
मेरा कमरा! मैंने इस कमरे में बरसों बरस कितनी ज़िंदगियों के उतार-चढ़ाव महसूसे हैं। संध्या बुआ और अजय फूफासा का पावन प्रेम, मारिया और थॉमस का समर्पित प्रेम, उषा बुआ का अनचाहा वैवाहिक जीवन, दादी की त्रासदी, बड़ी दादी का अपने बिस्तर पर बरसों बरस स्लो पॉयज़न लेने के बाद की स्थिति-सा धीमे-धीमे घुलना, छीजना। मेरे अपने जीने के तमाम ऐसे कोने जिन्हें समेटकर मैंने अपनी चादर बुन ली है.....झीनी-झीनी रे बिन लीन्हीं चदरिया.....
आज हम चादर को ओढ़ते-बिछाते-समेटते वर्षों बाद मैं उस टुकड़ा भर धरती पर लौटी हूँ जहाँ से इस चादर का निर्माण शुरू हुआ था। रेशा-रेशा जोश, उद्देश्य, लक्ष्य और एक ठानी हुई मनोभावना से रचा बसा.....
तारों भरी रात थी.....हवाओं में गुलाब की मोहक सुगंध बसी हुई। कहीं से एक टिटहरी \'टीटीहु-टीटीहु\' की पुकार लगाती उड़ी तो घड़ी पर नज़र गई। झाड़फानूस की मद्धम रोशनी में उसके रेडियम से लिखे अंक चमके-एक बजकर बीस मिनट। मैंने ज़बरदस्ती आँखें मूँद लीं।
सुबह-सुबह महाराजिन चाय लेकर कमरे में आई। मैं जाग चुकी थी और तरोताज़ा कमरे से निकलने ही वाली थी-\"बाई सा! नास्ता मं के बणेगा, बता द्यो। थारे न्याणे वास्ते बाथरूम भी तैयार कर दियो ह।\"
\"अरे, इतनी सुबह? अभी तो पूरी तरह कोहरा भी नहीं छँटा है।\"
महाराजिन खिड़की खोलकर परदे वग़ैरह ठीक करने लगी। बाहर घना कोहरा था जिसमें सूरज की किरणें घुसने की चेष्टा कर रही थीं। जैसे स्नान के लिए जल में प्रवेश करती कोई तन्वांगी।
\"घंटा डेढ़ घंटा कोहरो और रहेसी, रात न ठंड भी भोत ही थी.....आओ बाई सा, थारी मालिश कर द्यूँ।\"
महाराजिन मेरे मना करने पर भी कटोरी भर तेल ले आई और मेरी मालिश करने लगी। सचमुच अच्छा लगा। बदन का पोर-पोर खुलने-सा लगा। मालिश के बाद उसने परंपरागत तरीके से मुझे बादाम का उबटन लगाया और फिर बाथरूम की ओर ले आई-\"टब मं हल्को गुनगुनो पानी ह बाई सा! केवड़ा को जल तो डाल दिया है, गुलाब जल तो हो ही नहीं।\"
\"अरे, मुझे इन सबकी आदत नहीं है महाराजिन। महानगर में दो-दो घंटे नहाने में लगाऊँगी तो हो चुका काम।\"
उसकी आँखों में आश्चर्य था। न चाहकर भी सब कुछ अच्छा लग रहा था। पुराने दिनों के लौट आने जैसी आहट कानों में सुनाई दे रही थी.....लेकिन नहीं, मैं कुछ भी याद करना नहीं चाहती। यह पलायन नहीं है बल्कि प्रताप भवन के नियमों, कायदों के विरुद्ध खुला जेहाद है जो मैं बचपन से करती आई हूँ।
नाश्ते की टेबिल पर मैं अकेली थी। महाराजिन परोस रही थी और रामू काका सफ़ेद कुरते धोती पर काली फ़तोई पहने, पीला साफ़ा बाँधे मेरे नज़दीक ही खड़े थे।
\"रामू काका, आप भी जीम लो। आज उधर चलना है बंगले की तरफ़।\"
अधिक विस्तार से कहना नहीं पड़ा। रामू काका समझ गए मैं जिम के बंगले की बात कर रही हूँ। वीरेंद्र आता रहता है, रामू काका ही ले जाते होंगे उसे। पता नहीं वहाँ की देखभाल कौन करता है।
खा-पीकर हम बाहर निकले तो रामू काका ने गैरेज से जीप बाहर निकाली। जाने कब धो पोंछकर चमका ली थी जीप उन्होंने। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठी, रामू काका को अपनी बगल की सीट पर बैठने का संकेत किया। वे संकोच और लिहाजवश सिकुड़े हुए बैठे थे-\"देखिए रामू काका, आप फ्री होकर नहीं बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जीप चलाना। प्लीज़ काका, आप अपने को प्रताप भवन का सदस्य क्यों नहीं समझते?\"
रामू काका की आँखें भर आईं। मैंने जीप कोठी के गेट से नीचे उतार ली। लंबी-सीधी सड़क पर जीप तेज़ी से दौड़ने लगी।
बंगले का गेट खुलते ही बंगले के केयर टेकर भानुप्रताप बाहर निकले, अदब से झुककर सलाम किया और मुझे हॉल के सोफ़े पर बैठाया। मैं बैठी नहीं। सारे कमरों को बारी-बारी से देखकर मैंने भानुप्रताप द्वारा सौंपी फाइल का निरीक्षण किया। सब कुछ बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। वीरेंद्र और उर्मिला के इंतज़ाम की दाद देनी पड़ेगी जिसमें कोई दोष न था। लगभग दो घंटे बंगले में बिताते हुए मुझे एहसास हुआ कि शिमला के कॉटेज में दादी की मौजूदगी जैसी रची-बसी देखी वैसी यहाँ नहीं। यहाँ शायद दादी बेचैनी से दिन गुज़ार रही हों क्योंकि बंगले के टैरेस के पूर्वी भाग से प्रताप भवन की बुर्जियाँ दिखाई देती हैं। दादी को शायद रिस-रिसकर याद आता होगा कोठी का कोना-कोना-नाते-रिश्ते-दास-दासियाँ, क्रिया-कलाप, तीज़-त्यौहार-उनके लिए जी पाना बहुत मुश्किल रहा होगा। मेरी अपनी बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
\"फार्म हाउस चलें?\" रामू काका ने मुझे गुमसुम बैठे देख पूछा।
\"हाँ, चलिए।\"
फार्म हाउस में तमाम फलों के झाड़, पौधों की और सब्ज़ियों की क्यारियाँ तरतीबवार बनी थीं। बीचोंबीच एक कमरा लाल सफ़ेद रंग से पुता, उभरे हुए पत्थरों की कलात्मक दीवार वाला। कमरे के पीछे की तरफ़ कुआँ.....जाली से ढँका, पक्की जगत वाला.....कमरा जिम की सुरुचि का परिचायक था। वीरेंद्र कहता है इतना लंबा अरसा गुज़र गया लेकिन हमने जिम के बंगले और कॉटेज में कोई परिवर्तन नहीं किया, सब कुछ वैसा ही है जैसा वे छोड़ गए थे। लेकिन न जाने क्यों मुझे ये बातें सुकून नहीं देतीं। शिमला में सेब के बगीचे और यहाँ का फार्म हाउस तो ठीक है। उपज होती है और मंडी में जाकर बिक जाती है। ल्रेकिन दोनों जगह के बंगले, कॉटेज क्यों फिजूल में बंद रखे जाएँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास रहने को घर नहीं है और हम भावुकता में इतने बड़े-बड़े घरों को ताला लगाए बैठे हैं। इन जगहों को लाइब्रेरी या म्यूज़ियम में तब्दील किया जा सकता है। प्रताप भवन में भी अच्छा-ख़ासा स्कूल खोला जा सकता है। किसी की स्मृतियाँ बंद घरों में नहीं होतीं बल्कि दिल में होती हैं। आदमी तभी मरता है जब दिल से उसकी स्मृतियाँ पुँछ जाएँ।
लौटते हुए मैं मारिया से मिलने गई थी। एकदम बदल गई है मारिया। सिर के बाल खिचड़ी हो गए हैं। आँखों पर चश्मा चढ़ गया है लेकिन मुझे फौरन पहचान लिया और लिपटकर रो पड़ी-\"पायल बाई.....कहाँ थीं अब तक?\"
थॉमस भी हमारी आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया और एकदम भावुक हो उसने मेरे हाथ थाम लिये। ठंड के कारण हम अस्पताल के पिछवाड़े बने बगीचे के बैंचों पर बैठ गए। वहाँ गुलाबी धूप छिटकी थी।
\'मालविका स्मृति केंद्र\' का बाईं तरफ़ और विस्तार हो गया था। कई कमरे बनवा लिये थे मारिया ने, कई डॉक्टर भी अपॉइंट किए थे। यूनानी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक तीनों पद्दतियों से इलाज करने के विभाग बन गए थे।
\"अब तो काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मालविका स्मृति ट्रस्ट बनानी पड़ी।\"
मैंने मारिया को लाड़ से देखा-\"तुम सचमुच सच्चा प्रेम करने वाली हो मारिया जो तुमने दादी का नाम जीवित रखा। हम सब तो बड़े स्वार्थी निकले।\"
मारिया ने बताया-\"ट्रस्ट का अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। इन कमरों और विभागों को बनवाने में सरकार ने भी मदद की है। अब तो यहाँ सभी तरह का इलाज होता है। ब्लड बैंक भी है और आधा दर्जन एंबुलैंस भी, जो डोनेशन में मिली हैं।\"
\"चलो, हमें दिखाओ सब।\" मैं आतुर थी कि तभी रामू काका थर्मस में चाय और काँच के गिलास लिये चले आए।
\"पहले हम अस्पताल देखेंगे रामू काका।\"
और मैं तेज़ी से मारिया और थॉमस के साथ अस्पताल देखने लगी। ऑपरेशन थियेटर, एक्सरे विभाग, कोल्ड स्टोरेज, जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, चिकित्सा विभाग, ब्लड बैंक और दवाइयों का स्टोर।
\"वाह मारिया, तुमने तो कमाल कर दिया।\"
मारिया मुस्कुराते हुए मुझे मेनगेट से लगे हॉल में ले गई जहाँ बीचोंबीच कृष्ण की दस फीट ऊँची संगमरमर की मूर्ति थी। हॉल का फर्श चमचमा रहा था। जूते-चप्पल बाहर ही उतारे जाते थे। मैंने ताज्जुब से भरकर मारिया की ओर देखा।
उसने चमकती नज़रों से मुझे देखा और बहुत अधिक श्रद्धा से बोली-\"पायल बाई! छोटी आंटी वैष्णव थीं न, इसीलिए।\"
लगा मेरा सिर चकरा गया है। जहाँ प्रभु यीशु होने चाहिए थे वहाँ कृष्ण। किसी के प्रति प्रेम का यह उदात्त और असीमित स्वरुप तो मैंने पहली बार देखा। यह दादी के साथ जिंदगी ने कैसे रंग दिखाए.....वैष्णव थीं तो ज़िंदगी के उत्तरार्ध में कैथोलिक बन गईं और उन्हें प्रेम करने वाली मारिया कैथोलिक है तो उनके वैष्णव धर्म की रक्षा किए हुए हैं और वह भी स्मृतियों में-स्मारक के रूप में-यह कैसा खेल खेला दादी के साथ उनके भाग्य ने-उनकी परिस्थितियों ने। मैंने मारिया के दोनों हाथ अपनी आँखों से छुआए। मेरे अंतर से उठी कृतज्ञता की बूँदें देर तक उसे भिगोती रहीं। मेरी ज़बान निःशब्द थी। पैर, बड़ी देर तक मूर्ति के सामने थमे रहे और जब वहाँ से चलने को हिले तो अपूर्व शांति से मन भरा हुआ था।
आज सुबह से ठंड ज़रा कम है। मेरी छुट्टी के भी चार दिन ही बाकी रह गए हैं। दो दिन लौटने में लग जाएँगे। न शिमला जा पाऊँगी न बनारस। प्रताप भवन से निकलने के पहले मैंने बनारस फोन लगाया और वीरेंद्र को सारा प्रोग्राम बता दिया कि वह उर्मिला को शिमला न भेजे और बाबूजी को भी समझा दे कि अभी मेरा वहाँ आना नहीं हो पाएगा। वीरेंद्र की आवाज़ उदास हो चली थी। मैं ज्यादा बात नहीं कर पाई, आकर जीप में बैठ गई। गुनगुनी धूप में अपने अंदर की भावुकता भरी ठंड को बाहर ढकेल मैं रामू काका से बोली-\"काका, पहले हमें वहाँ ले चलिए जहाँ बाबा की समाधि है।\"
रामू काका हुलसकर जीप में आ बैठे। मैंने जीप स्टार्ट की तो महाराजिन दौड़ी आई। उसके हाथ में पानी से भरी बोतलें थीं। रामू काका ने लपककर बोतलें ले लीं। मेन सड़क पर आते ही छायादार वृक्षों की कतार शुरू हो गई। लगभग आधा घंटे बाद श्मशान भूमि आई। काँटेदार तारों से घिरी, बीचोंबीच फाटक और फाटक पर लाल रंग के हाथों के निशान बने थे।
\"ये निशान कैसे हैं काका?\"
\"बेटी राणी, जो सती होई है, उन्हां का हाथां का निशाण ह ये। चिता पर चढ़ने से पेल्ले हथेल्यां पर महावर चुपड़कर हाथां की छाप बणाकर जावे ह सती माता।\"
मैं वहाँ दादी की हथेलियों की छाप खोजने लगी लेकिन समझ में कुछ आया नहीं। कुछ हथेलियों की छाप तो इतनी छोटी थी.....नन्ही बालिका की हथेली जैसी.....छोटी-छोटी कोमल मासूम हथेलियाँ। जिन्होंने जिंदगी का स्पर्श तक नहीं किया.....वे खिलती कली-सी हथेलियाँ विधवा होने के जुर्म में जला दी गईं जबकि वे शादी का अर्थ तक नहीं जानती थीं। उफ़! ये हथेलियाँ मेरे वजूद पर कठोरता से उठीं और मुझे घायल करने लगीं। इन्हीं में कहीं गुलाबकुँवर की हथेलियाँ भी होंगी। मैं कराह उठी, हिम्मत जवाब दे गई। इसी फाटक पर हथेलियों की छाप बनाकर दादी वहाँ तक गई थीं.....बाबा की जहाँ समाधि बनी है.....तमाम लकड़ियों का ढेर और उस पर बैठी दादी और एक वहशी शोर.....अपने पर काबू कर मैं बाबा की समाधि का स्पर्श कर दो मिनिट मौन खड़ी रही। मन हाहाकार कर रहा था। न ढंग से प्रार्थना की जा रही थी न श्रद्धांजलि देते बन रहा था। रामू काका ने मेरी अंजलि गुलाब की पंखुड़ियों से भर दी। खुद भी अंजलि भर फूल चढ़ाए। मैंने मन-ही-मन बाबा से अपने अस्तव्यस्त मन के लिए माफ़ी माँगी और रामू काका से कहा-\"चलिए काका, सिमिट्री ले चलिए हमें।\"
\"अब बठे के धर्यो ह? से क्यूं तो खतम हो गयो।\"
मैंने काका के चेहरे पर संशय की परछाईं देखी। क्या वहाँ सचमुच सब कुछ खतम हो जाने की पीड़ा थी या.....
\"ख़तम हो गया इसीलिए तो वहाँ जाना है। चलिए जल्दी।\"
बाबा की समाधि से सिमिट्री तक की सड़क छायादार वृक्षों का लंबा सिलसिला थी। क़रीब पैंतालिस मिनट का मौन सफ़र.....रामू काका जड़ बन बैठे थे। जाने कौन-सा अपराध भाव उन्हें लीले जा रहा था। जानती थी अनिच्छा से चल रहे हैं वे और अनिच्छा का सबब है दादी का जिम से विवाह। रामू काका ही नहीं प्रताप भवन का हर इंसान इस मनःस्थिति का शिकार है।
काँटेदार बाड़ से घिरी सिमिट्री के गेट पर रामू काका ने जीप रुकवाई। दूर-दूर तक सन्नाटे का गहरा साम्राज्य था। हवा में पत्तों का मर-मर स्वर सिर धुनता-सा लगा। मैं बोझिल क़दमों से सिमिट्री की ओर बढ़ी। तमाम कब्रों के चबूतरों पर सूखे भूरे, बादामी पत्ते झरे थे। एक मरियल-सा कुत्ता एक कब्र के चबूतरे से टिका अपने ज़ख्मों को चाट रहा था-\"या ही ह मालकिन की समाधि।\"
रामू काका ने कहा और तुरंत पलटकर जीप की ओर बढ़ गए। चबूतरे पर काले सुनहरे अक्षरों में \'मिसेज़ मालविका जिम वेल\' लिखा था। उसी से लगी एक कब्र थी जिस पर मिस्टर जिम वेल लिखा था। मेरी संवेदना निःशब्द झर रही थी। मेरा मन हाहाकार कर उठा। दादी ने हमेशा जिन अंग्रेज़ों से नफ़रत की, जिनका कोठी के मेन हॉल के अतिरिक्त प्रवेश निषेध था, जिनके खाने-पीने के बर्तनों को वे चौके में नहीं घुसने देती थीं अंत में उसी क़ौम के व्यक्ति को उन्हें अपना पति स्वीकारना पड़ा। जो कभी बाबा को खिलाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थीं, बाबा की मृत्यु के बाद उनकी चौखट में प्रवेश न करने की वर्जना भी उन्हें झेलनी पड़ी। और झेलना पड़ा उन तमाम लोगों का तिरस्कार जिनकी सुख-शांति के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण के आगे हज़ारों बार माथा नवाया था। इन्हीं सबने मिलकर मेरी फूल-सी दादी को ज़िंदा जलाने का षड़यंत्र रचा था। इन्हीं सबने मिलकर थोथे आडंबर से पूर्ण धार्मिक कुरीति के निर्वाह का प्रयास किया था। इन्हीं सबके लिए दादी दीपशिखा-सी जलीं और अपना उजाला उन्हें सौंपती रहीं। क्यों भूल गए मालवगढ़ के लोग उनकी सेवा, दान, तप, यज्ञ को.....और क्यों याद रखी मात्र यही एक घटना कि उन्होंने एक अंग्रेज़ से शादी करके अपना धर्म भ्रष्ट किया। इस मुक़ाम तक किसने पहुँचाया उन्हें? कौन है कसूरवार? दादी या प्रताप भवन?
मैं अपने ही आँसुओं में नहा रही हूँ। पूरी सिमिट्री अंधे कुएँ-सी मुझे लीलने को आतुर है। मैं अंधाधुंध दौड़ रही हूँ.....दादी.....दादी.....तुम्हें तो ताबूत में लेटाकर मुर्दे को दफ़न करने की रीति से भय लगता था न? तुम कहती थीं न कि महामूर्छा में नाड़ी गुम हो जाती है..... दादी, कहीं तुम महामूर्छा में तो न थीं?
\"रामू काका.....दादी को कब्र से निकालिए.....हम उनका दाह संस्कार करेंगे। दादी की आत्मा ताबूत में बेचैन है। रामू काकाऽऽऽ\"
और रामू काका ने दौड़कर मुझे बाँहों में सम्हाल लिया।
\"अरे बेटी सा, क्यूं पगलावे है। अरे, मुर्दो भी कठ बेचैन होयो है? स कुछ तो खतम हो ग्यो।\"
तभी तेज़ हवा चली और काका के बोल झरे पीले पत्तों के शोर में दब गए।

